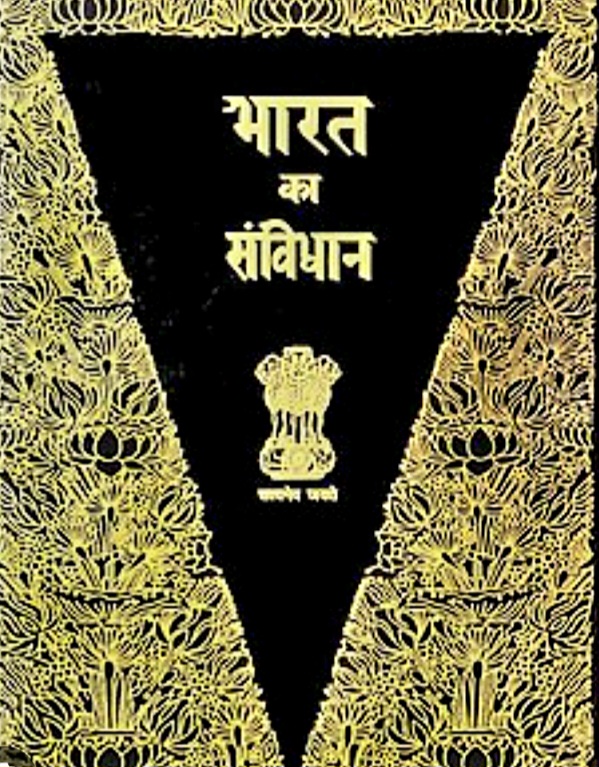प्रश्न 1. विधि के समक्ष समता का अर्थ बतलाइए।
What is meant by equality before Law.
उत्तर– विधि के समक्ष समता (Equality before Law)– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को, विधि के समक्ष समता के अधिकार की प्रत्याभूति (guarantee) देता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह आदेश देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण (Equality before Law and Equal protection of Law) से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार यह अनुच्छेद राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, समान प्रतिष्ठा तथा समान अवसर की प्रतिभूति (guarantee) देता है। यह अनुच्छेद उद्देशिका में अभिव्यक्त समता के आदर्श को अन्तर्विष्ट करता है। विधि के समक्ष समता (equality before Law) इंग्लैण्ड में प्रचलित डायसी के सिद्धान्त के विधि के शासन (Rule of Law) के समतुल्य है। परन्तु भारत में इस नियम से विदेशी राजनयिकों, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोक अधिकारी तथा न्यायाधीशों को छूट की गई है।
प्रश्न 2. न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है?
What is Judicial Review.
उत्तर- न्यायिक पुनर्विलोकन– न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) शब्द का प्राथमिक तथा विधिक अर्थ किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को | दोषसिद्धि अथवा आज्ञप्ति (Decree) के अभिनिश्चय का पुनर्विचारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के सन्दर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करना है। कारविन ने न्यायिक पुनर्विलोकन को न्यायालयों के उस अधिकार के रूप में परिभाषित किया है जिसके अन्तर्गत न्यायालय विधान मण्डलों द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की परख कर सकते हैं तथा किसी भी असंवैधानिक विधि को रोक देने का अधिकार रखते हैं।
प्रश्न 3. युक्तियुक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Reasonable Classification?
उत्तर – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण की प्रतिभूति देता है। परन्तु किसी भी समाज में या राष्ट्र में असमान व्यक्तियों के मध्य समानता सम्भव नहीं है। एक सर्व सुविधा सम्पन्न व्यक्ति तथा एक अकिंचन व्यक्ति को एक तराजू में तौलना सम्भव नहीं है। इन दो वर्गों के मध्य पूर्ण समानता का व्यवहार असम्भव हो जाता है। इन दोनो वर्गों के व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण प्रदान होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है परन्तु समाज के उपरोक्त वर्गों को एक समान करना सम्भव नहीं है अतः यह श्रेयस्कर होना चाहिए कि उन वर्गों के व्यक्तियों के मध्य असमानता न हो. परन्तु उन दोनों वर्गों के मध्य समान व्यवहार करने के सिद्धान्त में अपवाद जा सकता है। जैसे सुविधा सम्पन्न समाज के व्यक्तियों के मध्य समानता का व्यवहार किया जाना आवश्यक है परन्तु सुविधा सम्पन्न तथा अकिंचन इन दोनों वर्गों के मध्य असमानता करना समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं है। सामाजिक स्थिति या जाति के आधार पर किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है।
चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1951 एस० सी० 41 नामक वाद उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि विधायिका को विधिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण करने की शक्ति प्राप्त है। वह कुछ व्यक्तियों का एक वर्ग बना सकती है जो एक समान चरित्र धारण करते हो तथा यदि उस वर्ग में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो उस पर अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत आपत्ति नहीं की जा सकती परन्तु वर्गीकरण का यह कार्य युक्तियुक्त (Reasonable) होना चाहिए। वर्गीकरण के लिए अपनाए ग सिद्धान्त तर्कसंगत तथा यथोचित होने चाहिए, अर्थात् दो वर्गों के मध्य असमानता का व्यवहार अनुचित नहीं है परन्तु एक वर्ग के व्यक्तियों के मध्य असमानता करना अनुच्छेद 14 का उल्लघंन होगा। एक व्यक्ति एक वर्ग हो सकता है।
प्रश्न 4. आधारभूत ढाँचा से आप क्या सते हैं?
What do you understand by Basic structure?
उत्तर- आधारभूत ढाँचा (Basic Structure)- आधारभूत ढाँचे के सम्बन्ध में करने वाला संशोधन नहीं कर सकती है पर “आधारभूत ढाँचा क्या है इसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी महोदय द्वारा संविधान के मूलभूत ढाँचे में निम्नलिखित दृष्टान्त दिये गये हैं –
(a) संविधान की सर्वोपरिता
(b) संविधान का गणतन्त्रतात्मक एवं लोकतान्त्रिक स्वरूप
(c) संविधान का धर्म निरपेक्ष स्वरूप
(d) विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
(e) संविधान की संघात्मक प्रकृति
उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे’ की कड़ी में निम्न दृष्टान्त और जोड़ दिये हैं –
(i) विधि शासन
(ii) न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति
(iii) स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतन्त्र और जोड़ दिये हैं
प्रश्न 5. अभित्यजन के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Doctrine of Waiver?
उत्तर- अभित्यजन का सिद्धान्त (Doctrine of Waiver)- मूलभूत या भौतिक अधिकारों (Fundamental Rights) के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या को नागरिक इन अधिकारों का अभिव्यजन (Waiver) कर सकता है? कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों का अभित्यजन नहीं कर सकता।
विवेश्वर नाथ बनाम कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स, ए० आई० आर० 1955 सु० को 123 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने कहा कि किसी भी स्थिति में भारत में ऐसा नियम लागू नहीं किया जा सकता जो भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को नष्ट कर दे। न्यायमूर्ति के० सुव्याराव ने भी अभित्यजन के सिद्धान्त के विपरीत यह अभिमत व्यक्त किया कि संविधान के भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों के अभित्यजन (Waiver) को किसी भी नागरिक को छूट नहीं है। परन्तु इसके विपरीत न्यायमूर्ति एस० के० दास का मत था कि यदि संविधान किसी व्यक्ति को अधिकार या सुविधा उसी के लाभ के लिए देता है तो वह व्यक्ति अपने उस अधिकार या सुविधा का अभित्याग कर सकता है। परन्तु अभित्याग तभी स्वीकार होगा जब ऐसे अभित्याग से किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार प्रभावित न हो तथा उसका अभित्याग न तो किसी विधि द्वारा वर्जित हो न हो लोकनीति व लोक नैतिकता के विपरीत हो।
संक्षेप में कहें तो यह नियम स्वीकारना श्रेयस्कर होगा कि अमेरिका की भाँति भारत में भी किलो नागरिक को अपने मूल अधिकारों के अभित्याग की छूट नहीं होगी।
प्रश्न 6. भारतीय संविधान के तहत ‘राज्य’ से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लेख भारत कीजिए।
उत्तर – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार-“राज्य” के अन्तर्गत भारत को सरकार एवं संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधान मण्डल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधीन नियन्त्रण में सभी स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारी हैं। इस प्रकार राज्य के अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया गया है
(1) भारत सरकार तथा भारत की संसद (Government of India and Indian Parliament);
(2) राज्य सरकार तथा राज्य की विधान सभाएँ (State Government and Legislature of State);
(3) स्थानीय प्राधिकारी (Local Authorities); तथा
(4) अन्य प्राधिकारी (Other Authorities)।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा में भारत सरकार को सम्मिलित किया गया है अर्थात् मूल अधिकार भारत की सरकार के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को राज्य सरकार तथा राज्य विधान मण्डल के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रत्याभूत किये गये हैं। ‘राज्य’ के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी आते हैं। इसके अन्तर्गत नगरपालिकाएँ, जिला परिषद्, ग्राम पंचायत आदि जबकि अन्य प्राधिकारी के अन्तर्गत विद्युत परिषद् राजस्थान, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एसोसिएशन आते हैं।
प्रश्न 7. क्या निम्नलिखित ‘राज्य’ शब्द के अन्तर्गत सम्मिलित हैं ?
(1) उच्च न्यायालय (High Court)
(2) नगर पालिका (Municipal)
(3) भारतीय खाद्य निगम (IFC)
(4) विश्वविद्यालय (University)
(5) जीतेन्द्र उपाध्याय (Jeetendra Upadhyay)
(6) जीवन बीमा निगम (LIC)
उत्तर – ( 1 ) उच्च न्यायालय- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय ‘राज्य’ की परिभाषा में आता है।
परमात्मा बनाम मुख्य न्यायाधीश, ए० आई० आर० 1961 सु० को० 13 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को राज्य माना, जब वह न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
( 2 ) नगरपालिका– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत नगरपालिका ‘राज्य’ की परिभाषा में आता है। नगरपालिका स्थानीय प्राधिकारी के अन्तर्गत आता है।
मुहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी, ए० आई० आर० 1952 सु० को० 115 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नगरपालिका अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य माना जायेगा।
( 3 ) भारतीय खाद्य निगम – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 जिसके अन्तर्गत ‘राज्य’ की परिभाषा में अन्य प्राधिकारी भी आते हैं और भारतीय खाद्य निगम एक अन्य प्राधिकारी है अतः भारतीय खाद्य निगम अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत ‘राज्य’ माना जायेगा। यही बात सुखदेव सिंह बनाम भगत सिंह, ए० आई० आर० 1975 सु० को० 1331 नामक वाद में भी कही गयी कि भारतीय खाद्य निगम अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारी है अतः वे राज्य हैं। इनको अपने कर्मचारियों की सेवाएँ विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
( 4 ) विश्वविद्यालय – विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत “राज्य’ की परिभाषा में आता है क्योंकि विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी के तहत आता है, अन्य प्राधिकारों में उन सभी को सम्मिलित माना गया जो संविधान या किसी संविधि द्वारा स्थापित होते हैं एवं जिन्हें विधि, उप-विधि आदि बनाने की शक्ति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये शासकीय या प्रभुतासम्पन्न शक्ति का प्रयोग करें। उमेश बनाम वी० एन० सिंह, ए० आई० आर० 1968, पटना 3 नामक वाद में पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विश्वविद्यालय राज्य की परिभाषा में आता है।
(5) जीतेन्द्र उपाध्याय – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अतंर्गत ‘राज्य’ की परिभाषा में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं किन्तु कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगे जब तक उन्हें किसी विधि द्वारा कुछ विधिक अधिकार प्रदान न किया गया हो। इसलिए जीतेन्द्र उपाध्याय नामक व्यक्ति राज्य की परिभाषा में नहीं आयेगा।
( 6 ) जीवन बीमा निगम– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत ‘राज्य’ की परिभाषा में जीवन बीमा निगम भी आता है। सुखदेव सिंह बनाम भगतराम, ए० आई० आर० 1975 स० को० 1331 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जीवन बीमा निगम, तेल, प्राकृतिक गैस आयोग तथा कारखाना वित्त निगम अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारी हैं अतः वे राज्य हैं।
प्रश्न 8 संविधानोत्तर विधियाँ क्या हैं?
What are Constitutional Laws?
उत्तर- संविधानोत्तर विधियाँ – संविधानोत्तर विधियों के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (2) में उपबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 13 (2) के अनुसार, संविधान के लागू होने के पश्चात् राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो :
(1) मूल अधिकारों को छीनती हो, या
(2) मूल अधिकारों को कम करती हो या
(3) मूल अधिकारों से असंगत हो।
ऐसी विधियाँ आरम्भ से ही शून्य होती हैं अर्थात् वे मृत रूप में ही बनती हैं और उनके जीवित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
‘सगीर अहमद’ के मामले में आच्छादन के सिद्धान्त का संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होने का मुख्य कारण यह बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ आरम्भ से ही शून्य होती हैं, उन्हें बाद के संविधान संशोधनों द्वारा विधिमान्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसी विधियों को नये सिरे से पारित किया जाना आवश्यक है।
रेणु बनाम डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स जज तीस हजारी, ए० आई० आर० (2014) एस० सी० 2175 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 13 (2) का मुख्य उद्देश्य संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की सुरक्षा की सर्वोपरिता को बनाये रखना है।
प्रश्न 9. विधि का शासन की व्याख्या कीजिए।
Explain Rule of Law.
उत्तर-विधि का शासन (Rule of Law)- डायसी ने ‘विधि के शासन की संकल्पना इंग्लैण्ड को ध्यान में रख कर की थी। डायसी ने कहा था कि इंग्लैण्ड में विधि का शासन है न कि व्यक्ति का अर्थात् विधि के शासन में भेदभाव तथा असमानता का सदैव अभाव होना चाहिए। भेदभाव या मनमानापन तथा पक्षपात व्यक्ति के शासन का गुण है। विधि का शासन इन बुराइयों से मुक्त है। विधि के शासन का वास्तविक अर्थ है विवेक (discretion) की अनुपस्थिति विधि का शासन मनमानेपन या विवेकाधीन शक्ति का विलोम है। इस परिकल्पना का दूसरा अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त (सामान्य) प्रक्रिया द्वारा स्थापित विधि के अन्तर्गत ही विधि के अतिक्रमण के लिए सिर्फ न्यायालय द्वारा ही शारीरिक या साम्पत्तिक रूप से दण्डित किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
यद्यपि विधि के शासन की परिकल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड कोक द्वारा प्रस्थापित की गई। परन्तु प्रो० ए० वी० डायसी ने अपनी पुस्तक The Law of Constitution’ में विधि के प्रशासन ‘Rule of Law’ की परिकल्पना की विस्तृत मीमांसा प्रस्तुत की जो विधि विद्वानों में काफी चर्चित रही।
डायसी के विधि के शासन (Rule of Law) की परिकल्पना (Concept) के तीन अर्थ हैं –
(1) विधि की सर्वोच्चता (Supremacy of law)
(2) विधि के समक्ष समानता (Equality before law)
(3) न्यायालयों की संप्रभुता (Predominance of Courts)
भारत में संविधान सर्वोच्च है अतः संविधान के प्रावधान स्वयं में विधि के शासन की भाँति प्रशासी कृत्यों पर एक अंकुश हैं। यदि कार्यपालिका का कोई भी कार्य संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह अवैध तथा अधिकारातीत (ultra virers) होने के कारण निरस्त कर दिया जायेगा।
विधि के समक्ष समानता – भारतीय संविधान के अन्तर्गत समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत सुनिश्चित किया गया है। इस अनुच्छेद का आशय यह है कि समान परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, पद तथा निवास स्थान के आधार पर विभेद (discrimination) की अनुमति नहीं होगी।
न्यायालय की सर्वोच्चता (Supremacy of law)- भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त अधिकार न्यायालय के माध्यम से लागू करवाये जाते हैं। हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता (judicial activism) ने इस तथ्य को साबित कर दिया है। न्यायालय की सर्वोच्चता भारत में मन्त्री, विधायिका तथा सभी वर्गों ने स्वीकार की हैं।
इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में विधि के शासन के तीनों सिद्धान्त अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान, विधि के समक्ष समानता, मनमानेपन का अपवर्जन तथा न्यायिक अधिकारिता को सर्वोच्चता से ही स्वीकार करता है।
प्रश्न 10. मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अन्तर कीजिए।
Distinguish between Fundamental Rights and Human Rights.
उत्तर – मानव अधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलने चाहिए क्योंकि वह मनुष्य है। इन्हें बहुधा मूल अथवा मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा सामान्यतया इस प्रकार दी जा सकती है कि यह वह अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अन्तर्निहित है तथा जिसके बिना हम मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतायें हमें अपने मानवीय गुणों का विकास तथा आध्यात्मिक एवं अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक होती हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत मानव अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र बार्टर की प्रस्तावना (Preamble) के प्रथम सारवान पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि “संयुक्त राष्ट्र (संघ) के लोग मौलिक मानवाधिकार मानव की योग्यता तथा सम्मान में, पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकारों में, बड़े या छोटे राज्यों (राष्ट्रों) के समान अधिकारों में अपना विश्वास पुनः पुष्ट करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद एक के पैरा 3 में मानवाधिकार के सम्बन्ध में उनके विकास तथा संवर्धन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना तथा जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) को सुनिश्चित किये जाने की भी पुष्टि की गयी है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 55 यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र (संघ) जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के विभेद के बिना सभी के लिए मानवाधिकार तथा मौलिक अधिकार के पालन तथा उसके सार्वभौमिक सम्मान (universal respect) का संवर्धन करेगा। भारतीय संविधान के निर्माता स्पष्टतया मानव अधिकारों की धारणा से प्रभावित थे तथा सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया तथा सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों को उन्होंने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में रखा एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संविधान के भाग 4 में निदेशक सिद्धान्तों के रूप में सम्मिलित किया। गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० (1967) एस० सी० 1643 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि “परम्परागत जिसे ‘वैसर्गिक अधिकार’ कहते थे उसका आधुनिक नाम मौलिक अधिकार है।”
प्रश्न 11. न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए।
Define Judicial Activism.
उत्तर- न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)–न्यायिक सक्रियता का क्षेत्र सन् 1995-96 से उभर कर सामने आये हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से दो कदम आगे बढ़कर विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर समाज, शासन एवं राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफास किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेंट किट्स, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत काण्ड, चंन्द्रास्वामी काण्ड, चारा घोटाला प्रकरण, सतीश शर्मा प्रकरण, हवाला काण्ड आदि मामलों में उच्च पदों पर आसीन मन्त्रियों एवं अधिकारियों को एक बार यह आभास करा दिया है कि भारत में विधि का शासन (Rule of Law) अभी भी विद्यमान है। कुछ राजनेताओं द्वारा न्यायिक सक्रियता पर भले ही कटाक्ष किया गया हो, लेकिन जन साधारण इससे काफी प्रसन्न नजर आ रहा है।
न्यायिक सक्रियता का मुख्य उद्देश्य शासन-प्रशासन एवं सरकार को पारदर्शी बनाना तथा शासन एवं प्रशासन को अपने कर्त्तव्यों का बोध कराना है। परन्तु ऑल इण्डिया कौंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन बनाम ओमवीर कौशिक, ए० आई० आर० 2006 एन० ओ० सी० 496 दिल्ली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक सक्रियता का प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये तथा वहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ परिस्थितियाँ ऐसा करने के लिए बाध्य करती हों। साथ ही न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करते समय राष्ट्रहित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।
प्रश्न 12 शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Separation of Power?
उत्तर- शक्ति पृथक्करण (Separation of Power) – सुप्रसिद्ध संवैधानिक विधि विद्वान प्रोफेसर ए० वी० डायसी ने कहा था, शक्तियाँ व्यक्तियों को भ्रष्ट बनाती हैं (powers corrupts the man and absolute power corrupts absolutely)। इसलिए यह वांछनीय है कि शक्तियों का एक राज्य के एक ही अंग में केन्द्रीयकरण (सान्द्रीकरण : Concentration) न हो अर्थात् राज्य की शक्तियों का राज्य के विभिन्न अंगों में पृथक्करण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य की कार्यपालिका में विधायी शक्ति तथा न्यायिक शक्ति विहित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार विधायिनी में कार्यपालिका शक्ति तथा न्यायिक शक्ति विहित नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका (executive) तथा विधायी शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त कहते हैं।
प्रश्न 13. अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Untouchability?
उत्तर – अस्पृश्यता (Untouchability)- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अन्त करता है। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है तथा अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा तथा विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। इसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त कर संसद ने अस्पृश्यता (Untouchability) अधिनियम, 1955 को पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो समाज के उच्च वर्ग का है किसी छोटे वर्ग के व्यक्ति का अपमान करता है, अपनी सेवा उन्हें अर्पित करने से इन्कार करता है अथवा इन्हें किसी मन्दिर में प्रवेश करने से रोकता है तो उसका यह कार्य दण्डनीय होगा।
प्रश्न 14. उपाधियों के अन्त पर टिप्पणी लिखें।
Write short notes on abolition of titles.
उत्तर- उपाधियों का अन्त – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अन्त कर दिया गया है। इस अनुच्छेद के चार खण्डों में से खण्ड (1) में उपबन्ध किया गया है कि “राज्य सेना या विद्या सम्बन्धी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।”
इस उपबन्ध का सहारा लेकर याचिका कर्ताओं ने भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले सम्मान यथा भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म श्री को चुनौती दी एवं न्यायालय से निवेदन किया कि इनका अन्त कर दिया जाय। लेकिन न्यायालय ने इस सम्मानों को इस अनुच्छेद की परिधि से बाहर माना क्योंकि इन सम्मानों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन्हें अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता है।
प्रश्न 15 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ।
Freedom of speech and expression.
उत्तर – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता– वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (क) द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। वाक् और अभिव्यक्ति से अभिप्राय है-शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिह्नों आदि के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। इसके अलावा और भी ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है और ऐसे सब माध्यमों को ‘वाक् और अभिव्यक्ति’ के अन्तर्गत माना जाता है। अंक, चिह्न, संकेत आदि क्रियायें भी अभिव्यक्ति में सम्मिलित हैं।
शब्द ‘अभिव्यक्ति’ का क्षेत्र तो इतना व्यापक है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में ‘प्रेस की स्वतन्त्रता’ भी सम्मिलित हो जाती है। कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों में लेख, कार्टून, विज्ञापन आदि के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। यही प्रेस की स्वतन्त्रता है। (इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर प्रा० लि० और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य, ए० आई० आर० (1986) एस० सी० 515) वाक् और अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता के पीछे ‘जानने का अधिकार’ भी निहित होता है। लोकतान्त्रिक सरकार चूँकि खुली सरकार होती है; अत: उसके विषय में जनता को जानने का पूर्ण अधिकार होता है।
फिर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अभिप्राय केवल अपने विचारों के प्रचार प्रसार तक हो सीमित नहीं है। इसमें दूसरों के विचारों के प्रचार-प्रसार की स्वतन्त्रता भी निहित है जो मात्र प्रेस की स्वतन्त्रता द्वारा ही सम्भव है।
उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का मुख्य उद्देश्य है-(i) व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होना; (ii) सत्य की खोज में सहायक होना; (iii) व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना; (iv) स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होना। इससे आत्मविश्वास भी प्रबल होता है।
प्रश्न 16. भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार एवं उन पर प्रतिबन्धों की विवेचना करें।
Discuss the right to freedom of speech and the restriction on them.
उत्तर – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार भी आता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र होकर प्रयोग कर सकता है। स्वतन्त्र एवं निडर होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। परन्तु अनुच्छेद 19 (2) के अन्तर्गत वर्णित आधारों पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं जो निम्न हैं—(क) भारत की प्रभुता और अखण्डता; (ख) राज्य की सुरक्षा; (ग) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध; (घ) लोक व्यवस्था; (ङ) शिष्टाचार; (च) सदाचार; (छ) न्यायालय- अवमान; (ज) मानहानि (झ) अपराध-उद्दीपन; (ञ) साधारण जनता का हित (ट) अनुसूचित जनजातियों के हित का संरक्षण; आदि के लिए निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं।
प्रश्न 17. मौलिक अधिकारों की उपलब्धता राज्य के विरुद्ध है या सामान्य व्यक्तित्व के विरुद्ध है।
Availability of fundamental rights are against State or Private Individual.
उत्तर – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत ‘राज्य’ की परिभाषा में भारत सरकार तथा भारत की संसद, राज्य सरकार तथा राज्य की विधान सभाएँ, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आयेंगे जब तक उन्हें किसी विधि द्वारा कुछ विधिक अधिकार प्रदान न किया गया हो।
प्रश्न 18 क्या मूल अधिकार पूर्ण हैं।
Are the Fundamental Rights absolute?
उत्तर– कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग-3 के अन्तर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं। इन पर निम्न आधारों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है :
(1) राज्य की सुरक्षा (Security of states)
(2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
(Friendly relation with Foreign Country)
(3) लोक व्यवस्था (Republic Order)
(4) शिष्टाचार या सदाचार (Deceny and Morality)
(5) न्यायालय अवमानना (Contempt of court)
(6) भारत की प्रभुता और अखण्डता (Sovereignty and Integrity of India)
प्रश्न 19. दोहरे दण्ड के विरुद्ध संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by protection against Double Jeopardy.
उत्तर- दोहरे दण्ड के विरुद्ध संरक्षण- संविधान का अनुच्छेद 20 (2) दुहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण (Protection Against Double Jeopardy) का अधिकार प्रत्याभूत करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध (एक समान अपराध नहीं) के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा। इस सिद्धान्त को दुहरे परिसंकट या दुहरे संकट का सिद्धान्त कहा जायेगा अर्थात् यदि कोई व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से किसी दोष के लिए सिद्ध किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए पुनः उसके विरुद्ध दोषसिद्धि की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। [NEMO DE BET PRO EDEM CAUSA BIS VEXARE]
जैसे-‘क’, ‘ख’ के घर दिनांक 15-10-2014 को चोरी करता है तथा उसी दिन वह ‘ग’ के घर भी चोरी करता है। यह एक समान अपराध हुआ था कि ‘क’, ‘ख’ के घर चोरी करने के लिए दोषसिद्ध (Convict) या दोषमुक्त (Acquit) हो जाता है तो उसे ‘ग’ के घर चोरी करने के अभियोग में अभियोजित किया जा सकेगा। परन्तु यदि ‘क’, ‘ख’ के घर (05-04-2015 को चोरी करता है तथा उसे इस अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उसे ‘ब’ के घर 05-04-2015 को चोरी करने के अपराध के लिए दुबारा अभियोजित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त उदाहरण एक समान अपराध का है तथा दूसरा उदाहरण एक ही अपराध का है। सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त या दोषसिद्ध का अर्थ अन्तिम सक्षम न्यायालय द्वारा है अर्थात् यदि अपील के अनुसार प्राप्त था तो अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त या दोषसिद्ध या अपील समय सीमा के अन्तर्गत नहीं की गई हो।
प्रश्न 20. आत्म-अभिशंसन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। Explain “self-incrimination”.
उत्तर- आत्म अभिसंशन या स्वयं को अपराध में फँसाने का सिद्धान्त – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 (3) अपराधों में स्वयं को फँसाने के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण अंग्रेजी सूत्र VEMO TENTUR SE INSUM ACCUSARE (no man is bound to incriminate himself) पर आधारित है जिसका तात्पर्य है, कोई व्यक्ति अपने को किसी अपराध में फँसाने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है एक अभियुक्त एक सक्षम साक्षी है। उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है परन्तु उसे ऐसा साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे वह किसी अपराध में फँसता हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संविधान का पाँचवाँ संशोधन यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में स्वयं अपने प्रतिकूल साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself) यह उन्मुक्ति अभियुक्त के साथ-साथ अन्य साक्षियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 (3) के अन्तर्गत अपराध के अभियुक्त को मौन रहने का अधिकार भी समाविष्ट है। अनुच्छेद 20 (3) का संरक्षण व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों –
(1) व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो,
(2) उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो,
(3) उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाये।
प्रश्न 21. प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण।
Protection of life and personal liberty.
उत्तर- प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (Protection of life and personal liberty)— संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हो वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं अर्थात् किसी व्यक्ति को विधि की प्रक्रिया के अन्तर्गत नियम या अधिनियम बनाकर उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उसे उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा।
मृत्यु दण्ड का आदेश गिरफ्तार व्यक्ति को प्राण की स्वतंत्रता से वंचित करता है। जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 947 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में दिये जाने वाले मृत्युदण्ड को संवैधानिक माना है क्योंकि मृत्युदण्ड का आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है।
प्रश्न 22. शिक्षा का अधिकार। Right to Education.
उत्तर- शिक्षा का अधिकार (Right to Education)–संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है। कि “राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।”
शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को भी विकास की ओर बढ़ने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है इसलिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्त्तव्य संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में भाग 4 में रखा था। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्त्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निदेश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगी। नीति निदेशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है।
भारतीय सेवा समाज ट्रस्ट बनाम योगेशभाई अम्बालाल पटेल, ए० आई० आर० (2012) एस० सी० 3285 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। प्रारम्भिक एवं बेसिक शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
प्रश्न 23. एक गिरफ्तार व्यक्ति के कौन से अधिकार हैं?
What are rights of an arrested Person?
उत्तर- गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार – भारतीय संविधान का अनु० 22 खण्ड (1) और (2) एक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदत करते हैं –
(1) गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रातिशीघ्र बताये जाने का अधिकार
(2) अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार
(3) गिरफ्तारी के बाद 24 घण्टों के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार।
(4) 24 घण्टे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतन्त्रता।
प्रश्न 24. सम्यक् विधि प्रक्रिया क्या है?
What is Due Process of Law?
उत्तर– सम्यक् विधि प्रक्रिया – सम्यक् विधि प्रक्रिया से तात्पर्य विधि की ऐसी प्रक्रिया से है जो समय के अनुसार उचित हो सम्यक् विधि प्रक्रिया का उपबंध अमेरिकन संविधान में किया गया है। अमेरिकन संविधान का 5वाँ संशोधन यह उपबंधित करता है कि “कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।” बल्कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबन्धित करता है कि “किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हो वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।”
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सम्यक् विधि प्रक्रिया शब्दावली से संकीर्ण पदावली है। अमेरिकन न्यायालयों ने सम्यक् विधि प्रक्रिया का बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया है और इसकी तुलना नैसर्गिक न्याय से की है।
प्रश्न 25. प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के कुछ आयामों का उल्लेख करें।
Explain some features of life and personal liberty.
उत्तर– उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्राण तथा दैहिक स्वतन्त्रता के निम्न आयाम बनाये हैं अर्थात् निम्न को प्राण तथा दैहिक स्वतन्त्रता माना है –
(1) विदेश जाने का अधिकार, पासपोर्ट प्रदान करने का अधिकार।
(2) किसी को बिना विधिक अधिकार के गिरफ्तार न किये जाने का अधिकार।
(3) विचाराधीन कैदी को बिना विधिक अधिकार के उसकी स्वतन्त्रता से वंचित न किए जाने का अधिकार
(4) दोषयुक्त कैदी के साथ नियमानुसार व्यवहार किये जाने का अधिकार।
(5) विचाराधीन कैदी को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
(6) गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध के पूर्व व निरोध (detention) के पश्चात् चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करने का अधिकार।
(7) निर्धन अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार ।
(8) रोगग्रस्त व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
(9) शिक्षा का अधिकार।
(10) महिलाओं को क्रूरता या छेड़छाड़ के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
प्रश्न 26. मरने का अधिकार। Right to die.
उत्तर– मरने के अधिकार को जीने के अधिकार में शामिल किया जाये या न किया जाये इस विषय पर न्यायालय में विभिन्न मत रहे हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल, (1987) Cr. L.J. 743 के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन ‘जीने का अधिकार’ (Right to live) में मरने का अधिकार भी शामिल है।
इसके विपरीत चेन्ना जगादेश्वर बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1988 Cr. L.J. 549 के वाद में आन्ध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा-309 जो कि आत्महत्या के प्रयास को दण्डनीय बनाती है, संवैधानिक है तथा वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। पी० रतीनाम बनाम भारत संघ, (1994) 3 एस० सी० सी० 394 के बाद में उच्चतम यालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत ‘जीवन के अधिकार’ में ‘मरने का अधिकार’ भी शामिल है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा-309, अनुच्छेद 21 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-309 क्रूर तथा न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने का प्रावधान करती है, जो पहले से ही पीड़ित है और जिसे मानसिक रोग से जूझने की सलाह की आवश्कयता है और दूसरों को कोई हानि नहीं पहुँचाता है।
परन्तु ज्ञान (ग्यान) कौर बनाम पंजाब राज्य, (1996) 2 एस० सी० सी० 649 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलट दिया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत ‘जीवन के अधिकार’ में ‘मरने का अधिकार’ शामिल नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अन्तिम क्षण तक गरिमा से मरने के अधिकार की तुलना जीवन की सामान्य अवधि को कम करके अप्राकृतिक रूप से मरने का अधिकार नहीं कही जा सकती है।
प्रश्न 27. फर्जी मुठभेड़ तथा अनुच्छेद 21.
False encounters and Art. 21.
उत्तर– फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा व्यक्तियों को जान से मार डालना अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है। पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1997) एस० सी० 1203 के मामले में पिटीशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद फाइल करके न्यायालय से प्रार्थना की कि इम्फाल पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ जिसमें दो व्यक्ति मारे गए थे, की जाँच का आदेश दे, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का निर्देश दे तथा मृतक के परिवारजनों को प्रतिकर प्रदान करे। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुलिस मुठभेड़ में दो व्यक्तियों को जान से मार डालना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है और इस मामले में संप्रभु की विमुक्ति का प्रतिवाद लागू नहीं होता है और सरकार इसके लिए दायी है। न्यायालय ने प्रत्येक मृतक के लिए एक-एक लाख रुपये नुकसानी प्रदान किया।
प्रश्न 28 बलात् श्रम क्या है?
What is forced labours?
उत्तर- बलात् श्रम (Forced labours)- यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध या दबाव से कार्य करना पड़ता है तो भले ही उसे पारिश्रमिक मिला हो, वह अनुच्छेद 23 के अधीन ‘बलात् श्रम’ माना जायेगा। ‘बलात् श्रम’ कई तरीके से लिया जा सकता है। इसमें शारीरिक दबाव, विधिक दबाव (जहाँ किसी विधि के अधीन न कार्य करने पर दण्ड का उपबन्ध होता है) तक ही सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न दबाव भी शामिल है, जहाँ उसे कम पारिश्रमिक में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
दीना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का मामला, ए० आई० आर० (1983) एस० सो० 1155- इसमें ‘बलात् श्रम’ की व्याख्या की गयी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कारागृह में कैदियों से उचित पारिश्रमिक दिये बिना काम लेना बलात् श्रम है। कैदियों को अपने काम के एवज में मजदूरी पाने का हक है। न्यायालय का भी यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कैदियों के दावे को प्रवर्तित करे। यदि कैदियों को उनके काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।
प्रश्न 29 शोषण के विरुद्ध अधिकार।
Right against exploitation.
उत्तर- शोषण के विरुद्ध अधिकार – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में उपबन्ध किया गया है। वैसे तो मनुष्य ही मनुष्य का शोषण कर रहा, उससे बेंगार ले रहा है, बन्धुआ मजदूर के रूप में उसे दासता की बेड़ियों में जकड़ रहा है। उसे भीख माँगने, वेश्यावृत्ति करने, आदि के लिए विवश कर रहा है और भी न जाने क्या-क्या करना चाहता है वह हमारे संविधान में इन्हें स्थान देकर यह साबित कर दिया गया है कि सन्तों महन्तों और ऋषि मुनियों के देश में शोषण और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुच्छेद 23 एवं 24 के प्रावधान इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।
मानव-दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध– अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। इतना ही नहीं यह इन सभी को दण्डनीय अपराध भी घोषित करता है। संविधान में अस्पृश्यता के बाद दण्डनीय माना जाने वाला यह दूसरा अपराध है। यह सब दासता के प्रतीक कृत्य हैं। अतः स्वतन्त्रता के पश्चात् यदि इनका प्रतिषेध किया जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निम्नांकित नियोजनों को प्रतिषेधित किया गया है –
(1) कारखाने में नियोजन,
(ii) खानों में नियोजन, अथवा
(iii) ऐसे ही अन्य परिसंकटमय नियोजन यही कारण है कि इन नियोजनों से बालकों को दूर रखने के लिये यह व्यवस्था की गयी है।
प्रश्न 30. धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। Discuss the right to religious freedom.
उत्तर- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतन्त्रता के बारे में हैं। भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। यह प्रत्येक धर्म को समान आदर प्रदान करता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि धर्म क्या है? संविधान में धर्म की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। न्यायिक निर्णयों के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म में केवल विश्वास ही नहीं आता, बल्कि धार्मिक आचरण भी सम्मिलित होता है –
अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को दो प्रकार की स्वतन्त्रवायें प्रदान करता है
(1) अन्तःकरण अर्थात् धार्मिक आस्था की स्वतन्त्रता
(2) धार्मिक आचरण या प्रचार की स्वतन्त्रता
धर्म प्रचार में किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतन्त्रता पर निम्नलिखित निर्बन्धन हैं
(1) ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो
(ii) धर्म के नाम पर किये गये वे ही कार्य संरक्षित हैं जिनमें धर्म का तत्व प्रधान है। मोहम्मद हनीफ कुरेशी बनाम बिहार राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि बकरीद पर गाय काटना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। रमेश बनाम भारत संघ, (1998) 1 ए० सी० सी० 688 के बाद में यह कहा गया कि धार्मिक सहिष्णुता कायम रखने के लिए न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशुतोष लाहिरी, ए० आई० आर० 1955 सु० को० के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गो-वध मुस्लिम धार्मिक क्रिया का अंग नहीं है।
(iii) यदि धार्मिक स्वतन्त्रता समाज कल्याण एवं सुधार में बाधा उत्पन्न करती है तो ऐसी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
प्रश्न 31. चकमा माइग्रेन्ट क्या है?
What is Chakmas Migrant Case?
उत्तर- चकमा माइग्रेन्ट का मामला – उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणांचल प्रदेश राज्य, (1996) 1 एस० सी० सी० 742 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि राज्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक मनुष्य के “प्राण और दैहिक स्वाधीनता” की रक्षा करे चाहे वह नागरिक हो या अनागरिक। प्रस्तुत मामले में तथ्य यह था कि 1964 में भारी संख्या में चकमा शरणार्थी बंगलादेश से भारत आये और अरुणांचल प्रदेश में बसने लगे तो वहाँ के विद्यार्थी संगठनों ने उन्हें राज्य से बाहर चले जाने की धमकियाँ दी। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी और माँग की कि संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का संरक्षण सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिये चाहे वे नागरिक हों या अन्य कोई व्यक्ति न्यायालय ने इसे स्वीकारते हुए राज्य सरकार को चकमा शरणार्थियों के प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा करने का निदेश प्रदान किया।
प्रश्न 32. धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? What do you understand by secularism?
उत्तर- धर्म निरपेक्षता (Secularism ) – धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाना। सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना। जनता को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता का ही प्रतीक है। राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप 1 नहीं करना चाहिये। राज्य राजकीय कार्यों में संप्रभु होता है, धार्मिक क्षेत्र में इसका क्षेत्राधिकार नहीं होता है। कई बार धर्मनिरपेक्षता को धर्म के विरुद्ध माना जाता है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक स्वतन्त्रता दोनों का साथ में अस्तित्व हो सकता है। धर्म अन्तःकरण का विषय है। इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसका सीधा सम्बन्ध मन अर्थात् आत्मा से है। भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। यह प्रत्येक धर्म को समान आदर प्रदान करता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
प्रश्न 33. अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है? What do you mean by minorities?
उत्तर—अल्पसंख्यक (Minorities) – अल्पसंख्यक से तात्पर्य एक ऐसे समुदाय से है जिसके सदस्यों की संख्या सम्पूर्ण राज्य की जनसंख्या को आधी से कम हो अर्थात् 50% से कम हो। इसका विनिश्चय सम्पूर्ण राज्य में फैले लोगों की गणना के आधार पर किया जायेगा न कि किसी क्षेत्र विशेष में बसे लोगों के आधार पर किसी एक क्षेत्र में किसी समुदाय के लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यदि सम्पूर्ण राज्य में उनकी संख्या अधिक है तो उसे “अल्पसंख्यक वर्ग’ की कोटि में नहीं माना जायेगा।
प्रश्न 34. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत याचिकाएँ अथवा उपचारात्मक याचिका । Writs under Article 32 of Indian Constitution or curative petition.
उत्तर– -भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा संविधान के भाग-3 के अन्तर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की प्रतिभूति (guarantee) दी गई है तथा कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय से आदेश, निर्देश या याचिका (Writ) जारी करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
किसी भी व्यक्ति, जिसके मूल अधिकारों पर चाहे विधायिका द्वारा चाहे कार्यपालिका द्वारा, अतिक्रमण किया गया है, उच्चतम न्यायालय में-
(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
(2) परमादेश (Mandamus)
(3) प्रतिषेध (Prohibition)
(4) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
(5) उत्प्रेषण (Certiorary)
नामक रिट जारी करने हेतु आवेदन कर सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान के समस्त अनुच्छेदों का सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसके माध्यम से मूल अधिकारों (Fundamental Rights) का प्रवर्तन किया गया है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा तथा संविधान का हृदय कहा है। यह अनुच्छेद संविधान का संरक्षक है।
प्रश्न 35 बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख । Writ of Habeas Corpus.
उत्तर- बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of ‘Habeas Corpus’ )—यह सर्वाधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण रिट है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करना है। इसका शाब्दिक अर्थ है-‘निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से परिरोधित अथवा निरुद्ध रखा जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को इसी रिट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। न्यायालय इस रिट के द्वारा-
(i) निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किये जाने के कारण पूछता है,
(ii) निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है, एवं
(iii) अवैध रूप से निरुद्ध किये जाने पर उसे मुक्त अर्थात् स्वतन्त्र करने का निर्देश देता है।
इस प्रकार यह रिट व्यक्ति की शारीरिक स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखती है।
सुनील बत्रा का मामला– सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1579 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि बन्दी- प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य बन्दी को मुक्त कराना मात्र ही नहीं है अपितु उसकी अमानवीय एवं निर्दयतापूर्ण व्यवहार से सुरक्षा करना भी है।
प्रश्न 36. परमादेश लेख । Writ of Mandamus.
उत्तर- परमादेश लेख (Writ of Mandamus) – परमादेश लेख (Writ of Mandamus) एक प्रकार की आज्ञा (आदेश) (Command) है जो निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण (Tribunal), परिषद् (Boards), निगम या प्रशासी अधिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके अन्तर्गत एक ऐसे विशिष्ट कर्त्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है जो या तो विधि द्वारा उन पर निश्चित किया गया होता है या कर्त्तव्य उस व्यक्ति द्वारा धारण किये जा रहे पद से जुड़ा होता है।
प्रो० एस० टी० मारकोस के अनुसार परमादेश लेख न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा कर्तव्य करने के लिए बाध्य करने वाली आज्ञा या आदेश है जो करना उसका विधिक कर्त्तव्य है। भारत में यह लेख (Writ) एक न्यायिक उपचार है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के रूप में किसी सांविधानिक, कानूनी या अकानूनी (Non-legal) अभिकरण को कोई विनिर्दिष्ट कार्य करने या करने से विरत रहने के लिए जिसके हेतु वह विधि के अधीन बाध्य है, जारी किया जाता है, जो लोक कर्त्तव्य कानूनी कर्त्तव्य की प्रकृति का है।
संक्षेप में परमादेश लेख उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत किसी याचिका (Petition) पर निर्गत किया जाने वाला ऐसा आदेश है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति या निकाय को ऐसा करने के लिए या ऐसा कुछ करने से विरत रहने के लिए किया जाता है जिसे करने या करने से विरत रहने क कर्तव्य विधि द्वारा उस व्यक्ति या निकाय पर अधिरोपित किया गया होता है।
प्रश्न 37. प्रतिषेध लेख क्या है? What is Writ of Prohibition?
उत्तर- प्रतिषेध का लेख (Writ of Prohibition ) – प्रतिषेध का लेख अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायाधिकरण (Inferior Tribunal) को निर्गत किया जाने वाला एक आदेश है जो प्रवर न्यायालय (Superior Court) अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसा कुछ करने से रोकने के लिए होता है जो अधीनस्थ न्यायालय करने जा रहा है। यह लेख किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, जो उसे प्राप्त नहीं है। जिस प्राधिकरण (authority) को प्रतिषेध का लेख जारी किया जाता है वह न्यायिक या कल्प (अर्द्ध) न्यायिक कृत्य कर रहा होना चाहिए। प्रतिषेध लेख तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही जारी होती है तथा यह कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बाहर या अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग में य नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अतिक्रमण में की जा रही होती है या देश की किसी विधि के विरुद्ध होती है अर्थात् प्रतिषेध लेख प्रवर न्यायालय (उच्चतम या उच्च न्यायालय) अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध उस प्रक्रम (stage) पर जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण (Tribunal) ने निर्णय नहीं किया होता है। परन्तु जहाँ न्यायालय या न्यायाधिकरण ने मामले में निर्णय पूरा कर लिया है उस अवस्था में उत्प्रेषण का लेख (writ of certiorari) जारी किया जाता है।
प्रतिषेध के लेख का उद्देश्य अन्य न्यायाधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकाराधीन से बचाना है। इसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायाधिकरण की कार्यवाही को रोकना है। प्रतिषेध के लेख की प्रकृति अपील तथा उत्प्रेषण के लेख से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय कई प्रकार की गम्भीर त्रुटि कर सकता है। परन्तु प्रतिषेध का लेख उस त्रुटि के लिए जारी किया जाता है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया होता है।
प्रश्न 38 उत्प्रेषण लेख क्या हैं? What is Writ of Certiorari?
उत्तर- उत्प्रेषण लेख (Writ of Certiorari)—उत्प्रेषण का लेख एक उच्चतर न्यायालय (Superior Court) का आदेश (Command) है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने समक्ष लम्बित किसी वाद के अभिलेख उच्चतर न्यायालय को अन्तरित कर दे जिससे कि मामला उच्चतर न्यायालय द्वारा देखा जाए तथा यदि उच्चतर न्यायालय (Superior Court) यह पाता है कि मामला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बिना सुना गया था या यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त या अपास्त कर दिया जाय ।
यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आवेदन पर इस बात से सन्तुष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के किसी निर्णय को सुधारने की आवश्यकता है या किसी लोक प्राधिकारी का निर्णय शक्ति बाह्य तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की उपेक्षा के कारण त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों (Tribunals) को आदेश देकर उनसे सम्बन्धित बाद के सभी अभिलेख मँगवा ले तथा उसकी वैधता का परीक्षण करे तथा यदि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी कारण अवैध है तो उसे निरस्त या अपास्त कर दे। इस प्रकार उच्चतम या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विचारोपरान्त प्रमाणित कर सके, यही उत्प्रेषण के लेख का मुख्य प्रयोजन है।
प्रश्न 39. अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 में प्रमुख अन्तर क्या हैं? Distinction between Article 32 and Article 2262
उत्तर – संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 में प्रमुख अन्तर निम्न हैं-
(1) अनुच्छेद 32 मूल अधिकार है परन्तु अनुच्छेद 226 मूल अधिकार (Fundamental Rights) नहीं है।
(2) अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत रिट (Wirt) जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है जबकि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट (Writ) जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय (High Court) को है।
मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में जाने से पूर्व अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है।
प्रश्न 40. लोकहित वाद क्या है? What is P.I.L.?
उत्तर- लोकहित वाद (P.I.L.) – वाद लाने के अधिकार के सम्बन्ध में प्रारम्भिक धारणा यह थी कि व्यक्ति जो स्वयं अपने अधिकार के अतिक्रमण से पीड़ित नहीं है अथवा जो स्वयं विक्षुब्ध पक्षकार नहीं है, न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के निमित्त सुने जाने का अधिकार नहीं रखता। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इसी स्थिति में परिवर्तन कर इस अवधारणा को जन्म दिया कि जहाँ किसी संवैधानिक अथवा विधिक अधिकार के अतिक्रमण के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्ति के निश्चित वर्ग को कोई विधिक अपकार अथवा विधिक क्षति कारित हुई है अथवा किसी संवैधानिक या विधिक उपबन्ध के अतिलंघन में अथवा विधिक अधिकार के बिना ऐसे व्यक्ति या वर्ग पर कोई भार डाला गया है या ऐसे विधिक अधिकार या विधिक क्षति अथवा अवैध भार की धमकी दी गई है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्यिों का वर्ग निर्धनता, विवशता, असहायता, निर्योग्यता अथवा सामाजिक या आर्थिक असुविधा के कारण उपचार निमित्त न्यायालय में जाने में असमर्थ है, वहाँ जनता का कोई भी सदस्य, अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत समुचित निर्देश या आदेश के निमित्त रिट कर सकता है। तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के मूल अधिकार के अतिलंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय से निर्देश या आदेश प्राप्त करने हेतु रिट दाखिल कर सकता है। ऐसा किसी न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर भी किया जा सकता है। न्यायालय ऐसे पत्र को या तार को रिट पेटिशन मान कर यथोचित व्यवहार करेगा। लोकहित याचिका करने का अधिकार किसी पंजीकृत सोसाइटी को या स्वयं किसी संगठन को भी है।
प्रश्न 41. राज्य के उन नीति निदेशक तत्वों को वर्णित कीजिए जिन्हें मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है?