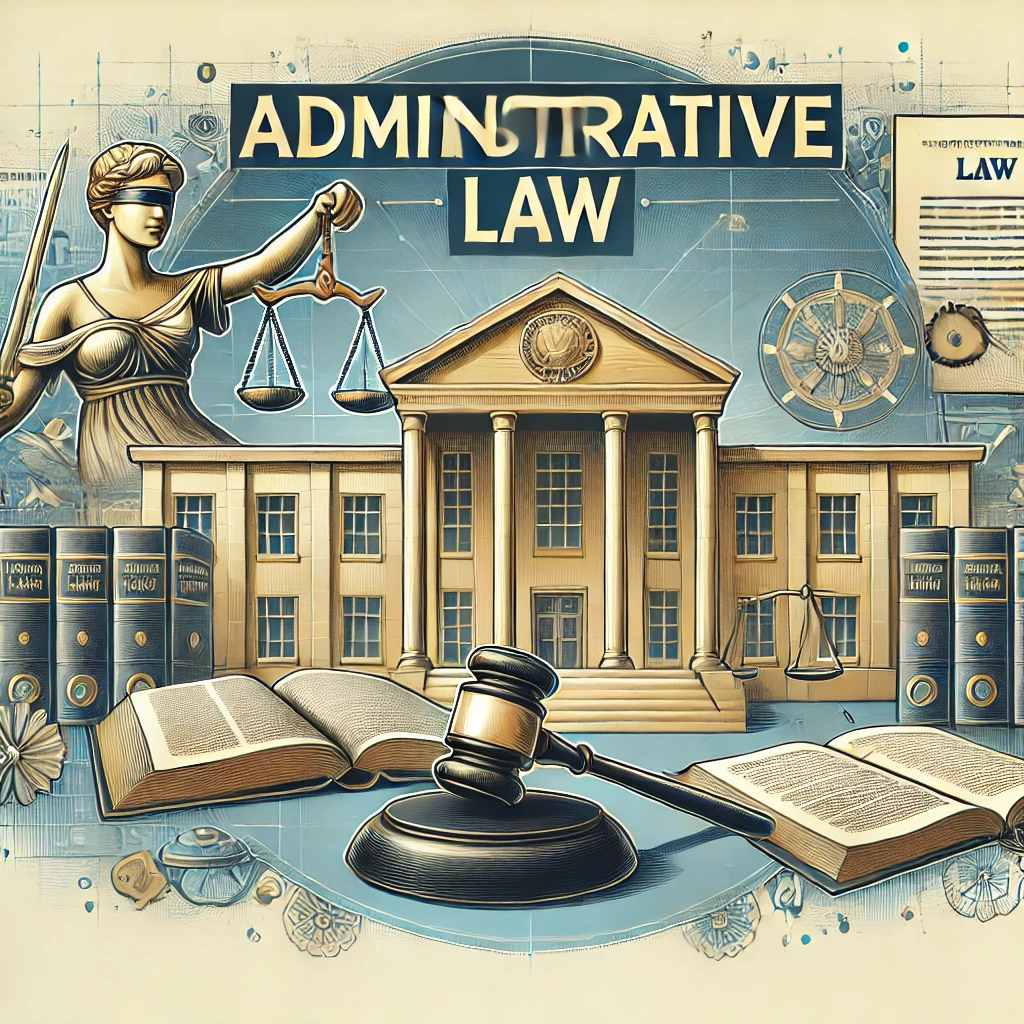प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Doctrine of Natural Justice)
प्रस्तावना
न्याय (Justice) मानव समाज का मूलाधार है। किसी भी सभ्य राज्य का अस्तित्व और उसकी विधि-व्यवस्था तभी स्थिर रह सकती है, जब उसमें न्याय की गारंटी दी जाए। न्याय की अवधारणा केवल विधिक (Legal) ही नहीं बल्कि नैतिक (Moral) और सामाजिक (Social) भी होती है। कानून के शासन (Rule of Law) का वास्तविक आधार केवल विधि के अक्षरशः पालन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें निष्पक्षता, तर्कसंगतता और उचित प्रक्रिया भी शामिल होती है। इसी सन्दर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Doctrine of Natural Justice) विकसित हुआ है।
प्राकृतिक न्याय किसी भी विधिक प्रणाली का अभिन्न अंग है। यह न्याय का ऐसा स्वरूप है, जो केवल लिखित कानूनों (Statutory Law) तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नैतिकता और निष्पक्षता (Fairness) की भावना पर आधारित होता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय निष्पक्ष, न्यायोचित और उचित अवसर प्रदान करने के बाद ही लिया जाए।
प्राकृतिक न्याय का अर्थ (Meaning of Natural Justice)
‘Natural Justice’ शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ी विधि में हुआ। ‘Natural’ का तात्पर्य है – प्रकृति या स्वाभाविक, और ‘Justice’ का अर्थ है – न्याय। अर्थात्, प्राकृतिक न्याय वह न्याय है, जो व्यक्ति की सहज बुद्धि, नैतिकता और विवेक के अनुरूप है।
कई विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है –
- Russell के अनुसार – “Natural Justice is the justice of common sense and honesty.”
(प्राकृतिक न्याय सामान्य बुद्धि और ईमानदारी पर आधारित न्याय है।) - Lord Esher के अनुसार – “The principles of natural justice are the principles which every civilized man understands.”
(प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत वे हैं, जिन्हें हर सभ्य व्यक्ति सहज ही समझता है।)
भारत में भी न्यायपालिका ने इसे न्याय, निष्पक्षता और उचित अवसर का पर्याय माना है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice)
प्राकृतिक न्याय के मुख्यतः दो (और आधुनिक समय में तीन) मूलभूत सिद्धांत माने गए हैं –
- Nemo judex in causa sua – No one should be a judge in his own cause
(कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। अर्थात्, न्यायाधीश निष्पक्ष होना चाहिए।) - Audi alteram partem – Hear the other side
(किसी पक्ष को दंडित करने या उसके अधिकार प्रभावित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।) - Speaking Orders / Reasoned Decisions (आधुनिक विकास)
(प्रशासनिक अथवा न्यायिक आदेश में कारणों का उल्लेख होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय न्यायसंगत है।)
अब इन सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करते हैं –
1. Nemo judex in causa sua (निष्पक्षता का सिद्धांत)
इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यदि न्याय करने वाला व्यक्ति मामले में किसी प्रकार का हित रखता है, तो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।
- उदाहरण: यदि किसी विश्वविद्यालय का कुलपति अनुशासनात्मक मामले में स्वयं शिकायतकर्ता भी है, तो वह उस मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता।
- केस कानून:
- Dimes v. Grand Junction Canal (1852) में निर्णय दिया गया कि यदि न्यायाधीश का किसी मामले में आर्थिक हित हो, तो उसका निर्णय शून्य (Void) माना जाएगा।
- भारत में A.K. Kraipak v. Union of India (1969) मामले में कहा गया कि निष्पक्षता केवल न्याय करने में ही नहीं बल्कि न्याय करते हुए दिखने में भी होनी चाहिए।
2. Audi alteram partem (सुनवाई का अवसर देने का सिद्धांत)
यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का हृदय है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या उसके अधिकारों को प्रभावित करने से पूर्व उसे अपने पक्ष में सफाई देने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं –
- सूचना (Notice) का अधिकार
- सुनवाई (Hearing) का अधिकार
- गवाहों से जिरह (Cross-examination) का अधिकार
- अभिलेखों तक पहुँच (Access to relevant records) का अधिकार
- केस कानून:
- Ridge v. Baldwin (1964) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त करना अवैध है।
- भारत में Maneka Gandhi v. Union of India (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ से संबंधित किसी भी कार्रवाई में ‘Fair Procedure’ (निष्पक्ष प्रक्रिया) आवश्यक है।
3. Speaking Orders / Reasoned Decisions (कारणयुक्त आदेश का सिद्धांत)
आधुनिक समय में न्यायालयों ने यह सिद्धांत विकसित किया कि किसी भी प्रशासनिक अथवा न्यायिक निर्णय में कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
कारणयुक्त आदेश (Reasoned Order) से –
- निर्णय की पारदर्शिता बनी रहती है।
- अपील या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालयों को समीक्षा करने में आसानी होती है।
- पक्षकारों का विश्वास न्यायपालिका में मजबूत होता है।
- केस कानून:
- Siemens Engineering v. Union of India (1976) – सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “Record of reasons is an essential part of natural justice.”
भारत में प्राकृतिक न्याय का विकास (Development in India)
भारतीय न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय को संविधान की आत्मा माना है। यद्यपि संविधान में “Natural Justice” शब्द का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), तथा अनुच्छेद 311 (सरकारी सेवकों की सुरक्षा) से व्याख्यायित किया है।
- State of Orissa v. Dr. Binapani Dei (1967) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उसे सुनवाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।
- Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner (1978) – कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है, क्योंकि यह न्यायिक तथा प्रशासनिक निर्णयों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
प्राकृतिक न्याय की अपवाद स्थितियाँ (Exceptions to Natural Justice)
हालाँकि प्राकृतिक न्याय का पालन सामान्यतः आवश्यक है, परन्तु कुछ परिस्थितियों में इसे लागू नहीं किया जा सकता, जैसे –
- आपातकाल (Emergency) – जब तत्काल निर्णय आवश्यक हो।
- निरर्थक औपचारिकता (Useless Formality) – जब सुनवाई देने के बाद भी परिणाम में कोई परिवर्तन संभव न हो।
- गोपनीयता का प्रश्न (Confidential matters) – जैसे – राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले।
- वैधानिक प्रावधान (Statutory Exclusion) – जब किसी अधिनियम में स्पष्ट रूप से सुनवाई का प्रावधान न हो।
महत्व और आवश्यकता (Importance and Need of Natural Justice)
- यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है।
- यह प्रशासनिक मनमानी और पक्षपात को रोकता है।
- यह न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखता है।
- यह विधिक शासन (Rule of Law) को मजबूत करता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत विधि की आत्मा और न्याय की आधारशिला है। इसका मूल उद्देश्य केवल कानून के अक्षर का पालन करना नहीं है, बल्कि न्याय का वास्तविक और निष्पक्ष रूप प्रदान करना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा सर्वोपरि है।
भारत में न्यायपालिका ने समय-समय पर इसे संविधान का अभिन्न हिस्सा मानते हुए विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित किया है। अतः कहा जा सकता है कि –
“प्राकृतिक न्याय ही वह सूत्र है, जो कानून को जीवंत, न्यायपूर्ण और मानवोचित बनाता है।”