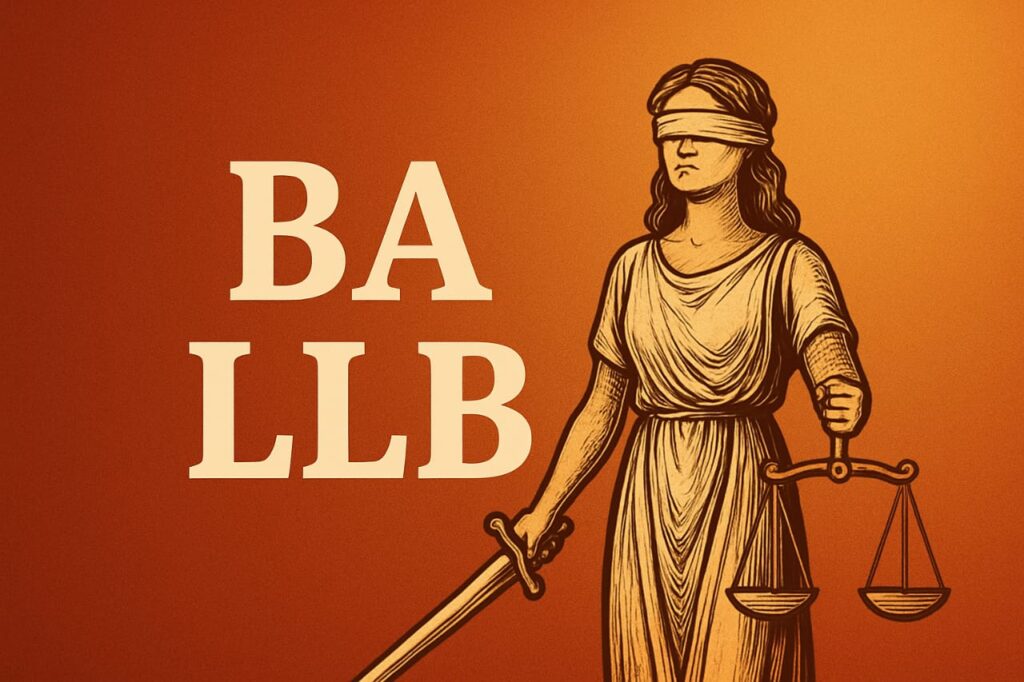“मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे और अशोक की धम्म नीति का मूल्यांकन तथा भारतीय शासन व्यवस्था और न्यायिक परंपरा पर प्रभाव”
प्रस्तावना
भारत के राजनीतिक इतिहास में मौर्य साम्राज्य (321 ई.पू.–185 ई.पू.) को पहली बार एक सशक्त और केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित और चाणक्य (कौटिल्य) के ‘अर्थशास्त्र’ से प्रेरित प्रशासनिक ढांचा तत्कालीन भारतीय शासन प्रणाली का उच्चतम रूप था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष अशोक महान (273–232 ई.पू.) के समय हुआ।
अशोक का महत्व केवल साम्राज्य विस्तार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी धम्म नीति ने भारतीय समाज, राजनीति और न्यायिक परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। अशोक ने युद्ध की नीति त्यागकर नैतिक शासन, प्रजा-कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को शासन का मूल आधार बनाया।
इस प्रश्न में हम पहले मौर्य प्रशासन की संरचना का मूल्यांकन करेंगे, फिर अशोक की धम्म नीति का विवेचन करेंगे और अंत में भारतीय शासन व्यवस्था व न्यायिक परंपरा पर इनके प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।
1. मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा
मौर्य प्रशासन का मुख्य आधार केंद्रीकृत व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त ने जिस व्यवस्था की नींव डाली, उसे अशोक ने और परिपक्व बनाया। इसे विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है –
(क) केंद्रीय प्रशासन
- सम्राट (Emperor)
- सम्राट सर्वोच्च शासक और शक्ति का केंद्र था।
- उसका आदेश ही सर्वोच्च कानून था।
- वह न्याय, प्रशासन और सैन्य शक्ति का अंतिम निर्णायक था।
- मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों की महत्ता बताई गई है।
- मंत्रीगण परामर्श देते थे, परंतु अंतिम निर्णय सम्राट का होता था।
- अमात्य वर्ग
- प्रशासनिक अधिकारी, जो राजस्व, न्याय, सेना और विदेश नीति देखते थे।
- कौटिल्य के अनुसार अमात्य “राज्य के स्तंभ” थे।
(ख) प्रांतीय प्रशासन
- साम्राज्य को कई प्रांतों (जैसे तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरि) में बाँटा गया।
- प्रत्येक प्रांत में कुम्मार / आर्यपतिस या युवराज को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था।
- प्रांतों के अधीन जिलों और ग्रामों का प्रशासन था।
(ग) नगर प्रशासन
- विशेषकर पाटलिपुत्र का प्रशासन एक नगर परिषद (Paura-Janapada) द्वारा किया जाता था।
- यूनानी यात्री मेगास्थनीज़ ने ‘इंडिका’ में नगर प्रशासन का वर्णन किया है –
- नगर को छह समितियों में बाँटा गया था: उद्योग, विदेशियों, जनगणना, व्यापार, कर व जनकल्याण।
(घ) राजस्व और आर्थिक प्रशासन
- भूमि कर (भूमिकर) राज्य की आय का मुख्य स्रोत था।
- व्यापार, खनन, वनों और लवण (नमक) पर कर लगाए जाते थे।
- राज्य कृषि और उद्योग को प्रोत्साहित करता था।
(ङ) न्याय व्यवस्था
- सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था।
- “धर्मस्थ” और “प्रादेश” नामक न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे।
- दीवानी और फौजदारी न्याय का प्रावधान था।
- दंडनीति कठोर थी; कौटिल्य का मत था – “दंड ही शासन का आधार है।”
(च) सैन्य संगठन
- विशाल स्थायी सेना – पैदल, अश्वारोही, रथ और हाथी।
- मेगास्थनीज़ के अनुसार सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे।
- एक विशेष युद्ध परिषद सैन्य संचालन करती थी।
➡️ मूल्यांकन: मौर्य प्रशासन का ढांचा अत्यंत केंद्रीकृत, संगठित और अनुशासित था। यह उस युग के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जा सकता है।
2. अशोक की धम्म नीति (Ashoka’s Dhamma Policy)
(क) पृष्ठभूमि
कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) के बाद अशोक ने हिंसा और युद्ध त्याग दिया। युद्ध की भीषण त्रासदी से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म और धम्म को राज्य-नीति का आधार बनाया।
(ख) धम्म नीति की विशेषताएँ
- अहिंसा और करुणा – प्राणियों की हत्या न करना, सभी प्राणियों के प्रति दया।
- धार्मिक सहिष्णुता – सभी पंथों के प्रति सम्मान और सह-अस्तित्व।
- नैतिक आचरण – माता-पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आदर, सत्यवादिता और संयम।
- प्रजा-कल्याण – चिकित्सा व्यवस्था, वृक्षारोपण, कुओं की खुदाई, सड़कों के किनारे धर्मशालाएँ।
- धम्म महामात्र – विशेष अधिकारियों की नियुक्ति जो प्रजा के बीच जाकर धम्म का प्रचार और विवाद निवारण करते थे।
- शिलालेख और स्तंभ लेख – अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया।
(ग) मूल्यांकन
- अशोक ने युद्ध नीति को त्यागकर नैतिक शासन की अवधारणा दी।
- उसकी धम्म नीति धार्मिक सहिष्णुता और बहुलतावाद की नींव थी।
- परंतु, कुछ इतिहासकार (जैसे आर.सी. मजूमदार) मानते हैं कि धम्म नीति ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य शीघ्र पतन की ओर बढ़ा।
3. भारतीय शासन व्यवस्था और न्यायिक परंपरा पर प्रभाव
(क) शासन व्यवस्था पर प्रभाव
- केंद्रीकरण की परंपरा – मौर्य प्रशासन ने केंद्रीकृत शासन की परंपरा स्थापित की, जो आगे गुप्त, मुगल और आधुनिक भारतीय राज्य व्यवस्था में भी दिखाई देती है।
- नौकरशाही का विकास – अमात्य और महामात्र वर्ग ने आधुनिक सिविल सेवा की जड़ों को मजबूत किया।
- प्रांतीय प्रशासन – आज के राज्यों और केंद्र-राज्य संबंधों का प्रारंभिक रूप।
- कल्याणकारी राज्य की अवधारणा – अशोक की धम्म नीति से प्रेरित होकर भारतीय शासन में प्रजा-कल्याण की परंपरा जुड़ी।
(ख) न्यायिक परंपरा पर प्रभाव
- कानून और दंड व्यवस्था – कौटिल्य की दंडनीति ने न्याय को शासन का मूल आधार माना।
- न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति – धर्मस्थ और प्रादेश जैसी पदवियों ने बाद की न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित किया।
- न्याय में नैतिकता का समावेश – अशोक की धम्म नीति ने न्याय में करुणा और नैतिकता को जोड़ा।
- धार्मिक सहिष्णुता – बहुलतावादी समाज में न्याय की नींव रखी, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर देखा जा सकता है।
4. आलोचनात्मक विवेचन
- मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका केंद्रीकृत और संगठित स्वरूप था, परंतु अत्यधिक केंद्रीकरण ने स्थानीय स्वशासन की संभावना को दबा दिया।
- अशोक की धम्म नीति ने नैतिक और मानवीय मूल्यों को शासन का आधार बनाया, परंतु उसकी युद्ध-विरति ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर किया।
- दोनों की सम्मिलित देन भारतीय शासन और न्यायिक परंपरा में यह रही कि सत्ता केवल बल पर नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और लोककल्याण पर आधारित होनी चाहिए।
निष्कर्ष
मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा भारतीय इतिहास का पहला संगठित केंद्रीकृत शासन था, जिसने शासन की स्थिरता, अनुशासन और दक्षता दिखाई। वहीं, अशोक की धम्म नीति ने भारतीय राजनीति को नैतिकता और प्रजा-कल्याण की दिशा दी।
इन दोनों की सम्मिलित विरासत भारतीय शासन व्यवस्था और न्यायिक परंपरा में आज भी दृष्टिगोचर होती है –
- केंद्रीकरण और नौकरशाही का ढांचा,
- प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप,
- न्याय में नैतिकता और सहिष्णुता,
- तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा।
इस प्रकार, मौर्य प्रशासन और अशोक की धम्म नीति भारतीय इतिहास ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की अमिट नींव है।