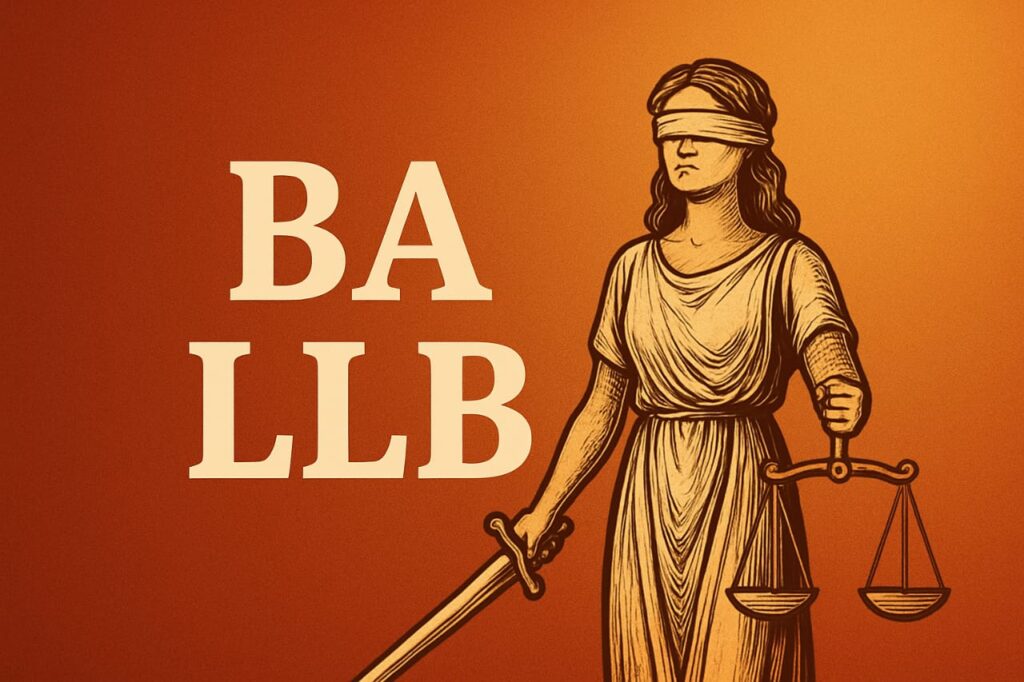भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक संवैधानिक विकास का आलोचनात्मक विवेचन
प्रस्तावना
भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दोनों का मिश्रित परिणाम है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक लगभग 174 वर्षों का यह कालखंड भारतीय संवैधानिक यात्रा का साक्षी है। ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए प्रारंभिक अधिनियम केवल औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हेतु बनाए गए थे, जिनमें भारतीय जनता की भागीदारी नगण्य थी। धीरे-धीरे भारतीय राष्ट्रवाद, सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों और विश्व-परिस्थितियों के दबाव ने ब्रिटिशों को संवैधानिक सुधारों की ओर बाध्य किया। अंततः यह प्रक्रिया 1947 में भारत की स्वतंत्रता पर जाकर समाप्त हुई। इस समूचे विकास की आलोचनात्मक विवेचना आवश्यक है क्योंकि यह समझना ज़रूरी है कि भारत की स्वतंत्रता एक संघर्षमय संवैधानिक यात्रा का परिणाम थी, न कि ब्रिटिशों का कोई परोपकार।
1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
विशेषताएँ
- ब्रिटिश संसद का भारत के मामलों में पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
- बंगाल के गवर्नर को “गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल” की उपाधि दी गई।
- गवर्नर-जनरल (वारेन हेस्टिंग्स) और चार सदस्यीय परिषद गठित।
- कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना।
आलोचना
- परिषद और गवर्नर-जनरल के बीच निरंतर संघर्ष हुआ।
- सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक निकायों के बीच अधिकारों की अस्पष्टता ने अराजकता फैलाई।
- यह अधिनियम कंपनी के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हुआ।
➡️ आलोचनात्मक दृष्टि से, यह अधिनियम भारतीयों के लिए लाभकारी न होकर केवल ब्रिटिश संसद और कंपनी के बीच शक्ति-संतुलन का प्रयास था।
2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
विशेषताएँ
- कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्ति-संतुलन हेतु “बोर्ड ऑफ कंट्रोल” का गठन।
- राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों में स्पष्ट विभाजन।
आलोचना
- भारतीय जनसाधारण के हितों की कोई चिंता नहीं।
- कंपनी का आर्थिक शोषण यथावत रहा।
➡️ यह अधिनियम भी औपनिवेशिक नियंत्रण की सुदृढ़ता का प्रतीक था।
3. चार्टर एक्ट्स (1813, 1833, 1853)
चार्टर एक्ट, 1813
- कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, पर चीन और चाय व्यापार पर एकाधिकार बरकरार।
- मिशनरियों को प्रचार की अनुमति।
चार्टर एक्ट, 1833
- गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल को “गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया” घोषित (विलियम बेंटिंक)।
- लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग।
- कंपनी को पूर्ण प्रशासनिक संस्था बना दिया गया।
चार्टर एक्ट, 1853
- परिषद में विधायी और कार्यपालिका कार्यों का पृथक्करण।
- सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की व्यवस्था।
आलोचना
- भारतीयों को प्रशासन से बाहर रखा गया।
- अंग्रेजी शिक्षा और विधि सुधार का प्रारंभ हुआ, जिसने राष्ट्रवाद की चेतना को जन्म दिया।
➡️ इन अधिनियमों ने भारतीय समाज में नई राजनीतिक चेतना और विधिक ढाँचे की नींव डाली।
4. भारत सरकार अधिनियम, 1858
विशेषताएँ
- 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त।
- भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन।
- भारत सचिव और उसकी परिषद नियुक्त।
- गवर्नर-जनरल को वायसराय की उपाधि।
आलोचना
- भारतीयों की आकांक्षाओं की उपेक्षा।
- केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादी नियंत्रण को सुदृढ़ करने का साधन।
➡️ यह अधिनियम औपनिवेशिक शोषण को और भी संगठित रूप देता है।
5. भारतीय परिषद अधिनियम (1861, 1892, 1909)
1861 अधिनियम
- विधायी परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों की नामित नियुक्ति।
- प्रांतीय परिषदों का गठन।
1892 अधिनियम
- परिषदों का आकार बढ़ा।
- बजट पर सीमित चर्चा का अधिकार।
1909 अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार)
- कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया।
- मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था।
आलोचना
- 1909 का अधिनियम सांप्रदायिकता का बीज बोने वाला सिद्ध हुआ।
- परिषदों के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं।
➡️ इन अधिनियमों ने भारतीय राजनीति में भागीदारी की आभासी व्यवस्था बनाई, परंतु साम्प्रदायिक विभाजन की नींव भी रखी।
6. भारत सरकार अधिनियम, 1919
विशेषताएँ
- द्वैध शासन (Dyarchy) – प्रांतीय विषयों का विभाजन (आरक्षित व अंतर्विश्वासित)।
- केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल।
- भारत को क्रमशः स्वशासन की ओर ले जाने का वादा।
आलोचना
- द्वैध शासन असफल; वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास।
- भारतीय असंतोष ने असहयोग आंदोलन (1920) को जन्म दिया।
➡️ यह अधिनियम भारतीयों को आंशिक अधिकार देकर असंतोष को और बढ़ाता है।
7. साइमन कमीशन (1927) और नेहरू रिपोर्ट (1928)
- साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था – “Simon Go Back” का नारा।
- नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस, मौलिक अधिकार और संघीय ढाँचे का प्रस्ताव।
- मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सूत्र पेश किए, जिसने सांप्रदायिक खाई को गहरा किया।
➡️ इस दौर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब पूर्ण स्वराज से कम पर संतुष्ट नहीं होंगे।
8. भारत सरकार अधिनियम, 1935
विशेषताएँ
- अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत अधिनियम।
- प्रांतों को “संपूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता”।
- संघीय ढाँचे और द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान।
- संघीय न्यायालय की स्थापना (1937)।
- 1937 में कांग्रेस सरकारों का गठन।
आलोचना
- संघीय ढाँचा लागू न हो सका।
- गवर्नर व वायसराय की विशेष शक्तियाँ बनी रहीं।
- यह अधिनियम ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का साधन था।
➡️ हालांकि, इसने भारतीयों को शासन का वास्तविक अनुभव दिया और स्वतंत्रता की चेतना को बल मिला।
9. द्वितीय विश्वयुद्ध काल – क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन
- क्रिप्स मिशन (1942) – युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव; अस्वीकृत।
- कैबिनेट मिशन (1946) – संविधान सभा गठित करने की योजना, जिसने भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
10. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
विशेषताएँ
- भारत और पाकिस्तान, दो प्रभुत्वशाली राष्ट्र बने।
- गवर्नर-जनरल अपने-अपने देशों में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि।
- संविधान सभा को संविधान बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता।
आलोचना
- भारत का विभाजन – सांप्रदायिक दंगे, लाखों लोगों का विस्थापन और नरसंहार।
- ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता तो दी, पर साथ ही एक गहरी त्रासदी भी छोड़ गए।
➡️ यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता की ऐतिहासिक उपलब्धि था, लेकिन विभाजन इसकी सबसे बड़ी कीमत।
निष्कर्ष
1773 से 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास एक लंबी, जटिल और संघर्षमय प्रक्रिया थी।
- 1773 से 1858 तक के अधिनियम केवल औपनिवेशिक हितों के लिए बने।
- 1858 से 1919 तक भारतीयों को राजनीति में सीमित स्थान मिला।
- 1919 से 1935 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को झुकने पर विवश किया।
- अंततः द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय संघर्षों के दबाव में 1947 का अधिनियम स्वतंत्रता का मार्ग बना।
आलोचनात्मक रूप से कहा जाए तो, ब्रिटिश संवैधानिक सुधार कभी भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखकर नहीं लाए गए, बल्कि हर सुधार ब्रिटिश शासन की मजबूरी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने इन सुधारों को लोकतांत्रिक दिशा दी।
भारत की स्वतंत्रता कोई “उपहार” नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष, बलिदान और संवैधानिक चेतना का परिणाम थी।