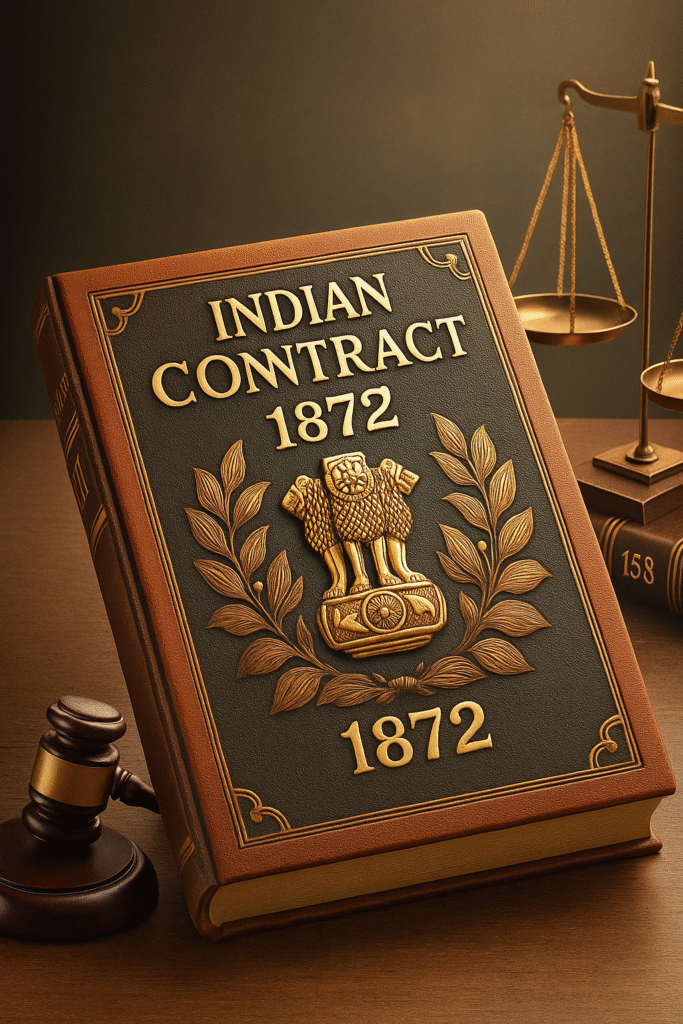वैध अनुबंध (Valid Contract) के आवश्यक तत्व
प्रस्तावना
मानव जीवन में अनुबंधों (Contracts) का अत्यधिक महत्व है। दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाओं से लेकर व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों तक हर जगह अनुबंध की भूमिका दिखाई देती है। वस्तुतः, समाज का आर्थिक ढांचा अनुबंधों की नींव पर टिका हुआ है। अनुबंध का सामान्य अर्थ है – दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी कार्य को करने या न करने की कानूनी रूप से प्रवर्तनीय सहमति।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(ह) में अनुबंध को परिभाषित किया गया है –
“अनुबंध वह समझौता है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो।”
अर्थात, हर समझौता (Agreement) अनुबंध नहीं होता। केवल वही समझौता अनुबंध है जिसे कानून लागू कर सके। अतः, किसी अनुबंध को वैध (Valid) बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है।
अनुबंध और समझौते में भेद
- Agreement (समझौता): दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति।
- Contract (अनुबंध): वह समझौता जो विधि द्वारा लागू करने योग्य है।
इस प्रकार हर अनुबंध समझौता है, परंतु हर समझौता अनुबंध नहीं है।
वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और न्यायालयों की व्याख्या के अनुसार वैध अनुबंध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व (Essentials of a Valid Contract) माने गए हैं –
1. प्रस्ताव और स्वीकृति (Offer and Acceptance)
किसी भी अनुबंध की नींव प्रस्ताव (Offer/Proposal) और उसकी स्वीकृति (Acceptance) पर आधारित होती है।
- प्रस्ताव स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए।
- स्वीकृति बिना शर्त और प्रस्ताव के अनुसार होनी चाहिए।
- स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक तक उचित माध्यम से पहुँचनी चाहिए।
- प्रस्ताव और स्वीकृति का मेल ही ‘Agreement’ कहलाता है।
न्यायिक निर्णय: Lalman Shukla v. Gauri Dutt (1913) में न्यायालय ने कहा कि केवल वही स्वीकृति वैध है जो प्रस्तावक की जानकारी में लाई जाए।
2. वैधानिक प्रतिफल (Lawful Consideration)
“Consideration” अनुबंध की आत्मा है। इसका अर्थ है कि अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष को कुछ न कुछ लाभ या हानि मिलनी चाहिए।
- प्रतिफल वास्तविक और वैधानिक होना चाहिए।
- प्रतिफल अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।
- प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है।
न्यायिक निर्णय: Chinnaya v. Ramaya (1882) – न्यायालय ने माना कि Consideration तीसरे पक्ष द्वारा भी दिया जा सकता है, बशर्ते यह विधिक हो।
3. संविदा की पात्रता (Capacity to Contract)
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अनुबंध करने के लिए व्यक्ति का सक्षम होना आवश्यक है। अनुबंध के लिए सक्षम व्यक्ति वह है –
- जो बालक (Minor) न हो (यानी 18 वर्ष से अधिक आयु)।
- जो सुदृढ़ मानसिक दशा (Sound Mind) का हो।
- जिसे विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो (जैसे दिवालिया, विदेशी शत्रु आदि)।
न्यायिक निर्णय: Mohiri Bibi v. Dharmodas Ghose (1903) – अल्पवयस्क के अनुबंध को पूर्णतया शून्य (Void) घोषित किया गया।
4. स्वतंत्र सहमति (Free Consent)
अनुबंध के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र (Free) होनी चाहिए। यदि सहमति निम्न परिस्थितियों से प्राप्त की गई हो तो अनुबंध अवैध होगा –
- बल प्रयोग (Coercion) – धमकी या दबाव डालकर।
- अवैध प्रभाव (Undue Influence) – विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग।
- कपट (Fraud) – धोखे से तथ्य छिपाना या झूठा कथन।
- कपटाचरण (Misrepresentation) – बिना धोखा देने की नीयत से गलत तथ्य बताना।
- भ्रम (Mistake) – तथ्य या विधि में त्रुटि।
न्यायिक निर्णय: Ranganayakamma v. Alwar Setti (1889) – जबरदस्ती विवाह हेतु सहमति ली गई, इसे अमान्य माना गया।
5. वैध उद्देश्य (Lawful Object)
अनुबंध का उद्देश्य विधिक और सार्वजनिक नीति के अनुकूल होना चाहिए।
- चोरी, हत्या, नशीली वस्तुओं की बिक्री जैसे अनुबंध अवैध हैं।
- ऐसे अनुबंध जो नैतिकता या समाज के विरुद्ध हों, वे भी शून्य हैं।
न्यायिक निर्णय: Gherulal Parakh v. Mahadeodas Maiya (1959) – सट्टेबाजी संबंधी अनुबंध अवैध और प्रवर्तनीय नहीं माने गए।
6. विधिक संबंध स्थापित करने की मंशा (Intention to Create Legal Relationship)
सिर्फ सामाजिक या घरेलू समझौते अनुबंध नहीं होते। अनुबंध तभी वैध होगा जब उसमें कानूनी दायित्व स्थापित करने की मंशा हो।
- जैसे – मित्रों के बीच चाय पर मिलने का वादा अनुबंध नहीं है।
- किंतु व्यापारिक समझौते सदैव कानूनी रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं।
न्यायिक निर्णय: Balfour v. Balfour (1919) – पति-पत्नी के बीच घरेलू खर्च का समझौता अनुबंध नहीं माना गया।
7. निश्चितता और स्पष्टता (Certainty and Possibility of Performance)
अनुबंध की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। कोई भी अस्पष्ट या असंभव अनुबंध वैध नहीं है।
- वस्तु, मूल्य, समय आदि निश्चित होने चाहिए।
- असंभव कार्य हेतु किया गया अनुबंध शून्य है।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति कहे कि “मैं तुम्हें चाँद खरीदकर दूँगा”, तो यह असंभव अनुबंध है।
8. विधि द्वारा घोषित शून्य न होना (Not Declared Void)
भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार कुछ अनुबंध स्वतः ही शून्य (Void) घोषित हैं, जैसे –
- अल्पवयस्क का अनुबंध
- विवाह-निरोधक अनुबंध
- व्यापार या पेशे पर प्रतिबंध लगाने वाले अनुबंध
- अनिश्चित या असंभव कार्य हेतु अनुबंध
9. विधिक औपचारिकताएँ (Legal Formalities)
कुछ अनुबंध मौखिक भी मान्य होते हैं, परंतु कुछ विशेष अनुबंध लिखित, पंजीकृत और स्टाम्प शुल्क युक्त होने आवश्यक हैं, जैसे –
- बिक्री विलेख (Sale Deed)
- बंधक अनुबंध (Mortgage)
- साझेदारी पंजीकरण (Partnership Registration)
10. द्विपक्षीय दायित्व (Mutual Obligation)
अनुबंध में दोनों पक्षों पर कुछ न कुछ कर्तव्य और अधिकार अवश्य होने चाहिए। यदि केवल एक पक्ष पर दायित्व हो और दूसरे पर कुछ न हो, तो वह अनुबंध नहीं कहलाएगा।
न्यायिक दृष्टांत (Case Laws Summary)
- Mohiri Bibi v. Dharmodas Ghose (1903): अल्पवयस्क का अनुबंध शून्य।
- Balfour v. Balfour (1919): घरेलू समझौते अनुबंध नहीं।
- Chinnaya v. Ramaya (1882): प्रतिफल तीसरे पक्ष द्वारा दिया जा सकता है।
- Gherulal Parakh v. Mahadeodas Maiya (1959): अवैध उद्देश्य के अनुबंध अमान्य।
- Lalman Shukla v. Gauri Dutt (1913): प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति अमान्य।
निष्कर्ष
इस प्रकार, वैध अनुबंध बनने के लिए केवल सहमति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वैधानिक होना आवश्यक है। अनुबंध तभी वैध और प्रवर्तनीय होगा जब उसमें – प्रस्ताव और स्वीकृति, वैधानिक प्रतिफल, संविदा की पात्रता, स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य, कानूनी संबंध बनाने की मंशा, निश्चितता, औपचारिकताएँ तथा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त शर्तें शामिल हों।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ने इन तत्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर न्यायालयों को अनुबंध संबंधी विवादों के समाधान का ठोस आधार प्रदान किया है। एक मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंधों को वैधता की कसौटी पर परखा जाए और केवल वही अनुबंध लागू हों जो इन आवश्यक तत्वों पर खरे उतरें।