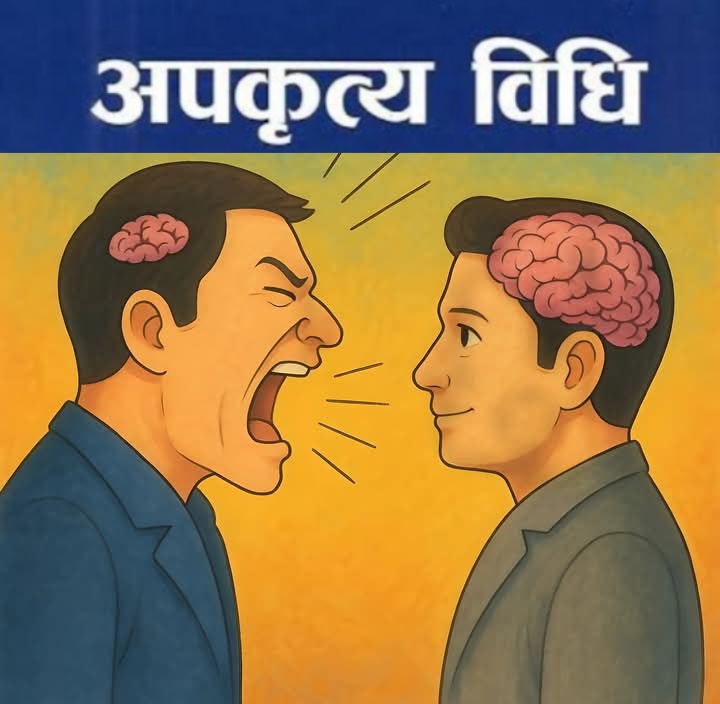प्रश्न 21. विद्वेष (Malice) का अपकृत्यात्मक उत्तरदायित्व में क्या महत्व है? निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट करिये।
What is the importance of Malice in tortious liabilities. Explain with the help of case law.
उत्तर– अपकृत्यात्मक उत्तरदायित्व में विद्वेष दो तरह का होता है। पहला विधि के अन्तर्गत विद्वेष (Malice in Law) दूसरा-तथ्य के अन्तर्गत विद्वेष (Malice in fact)।
विधि के अन्तर्गत विद्वेष (Malice in Law)- विधि के अन्तर्गत विद्वेष का साधारण अर्थ जानबूझ कर किया गया वह कार्य है जो बिना उचित कारण और प्रतिहेतु के किया गया। हो। इसका भावार्थ किसी कार्य को करने के लिए अनुचित हेतु नहीं है।
हाल्डेन महोदय ने विधि के अन्तर्गत विद्वेष को इस प्रकार स्पष्ट किया है-“यदि एक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति पर क्षति की परिणति करता है तो उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने इस कार्य को निर्दोषपूर्ण मनः स्थिति से किया था, यह माना जाता है कि वह विधिक प्रावधानों को जानता था, और उसे विधि के अन्तर्गत ही कार्य करना चाहिए था। अतः वह विधि के अन्तर्गत विद्वेषण का दोषी है, यद्यपि जहाँ तक उसकी मनःस्थिति का प्रश्न है, चाहे उसने अनभिज्ञता में कार्य किया हो, और इस भावबोध के अन्तर्गत उसका कार्य निर्दोषिता से परिपूर्ण हो ।’
(2) तथ्य के अन्तर्गत विद्वेष या बुरा प्रयोजन (Malice in fact or Evil Motive)– यहाँ पर ‘तथ्य के अन्तर्गत विद्वेष’ से तात्पर्य कोई दोषपूर्ण या बुरा प्रयोजन है। प्रतिवादी, जब कोई दोषपूर्ण कार्य घृणा, प्रतिशोध अथवा बुरी इच्छा के प्रभाव में आ कर करता है, तो यह कहा जाता है, कि वह कार्य ‘दुर्भावना’ अथवा ‘विद्वेष’ से किया गया है।
एक सामान्य नियम के रूप में अपकृत्य विधि के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के दायित्व के निर्धारण के लिए हेतु अथवा उद्देश्य पूर्णतः अप्रासंगिक होता है। कोई दो षपूर्ण कार्य मात्र इस कारण विधिपूर्ण नहीं हो जाता क्योंकि उसका प्रयोजन या हेतु अच्छा है। इसी प्रकार कोई विधिपूर्ण कार्य इसलिए दोषपूर्ण नहीं हो जाता है क्योंकि उसके साथ कोई बुरा प्रयोजन अथवा विद्वेष हैं।
साउथ वेल्स माइनर्स फेडरेशन बनाम गलोभोरग्न कोल कम्पनी के मामले में, वादी, जो कोयले की खानों के मालिक थे, प्रतिवादी के विपरीत कार्यवाही लाये। प्रतिवादी खान कर्मियों के संघ के थे। प्रतिवादी ने अपने कर्मियों को कुछ दिनों का अवकाश ले लेने का आदेश देकर उन्हें अपने नियोजन के संविदा भंग के लिए उत्प्रेरित किया था। प्रतिवादी का कार्य किसी भी प्रकार के विद्वेष से उत्प्रेरित नहीं था क्योंकि उसका उद्देश्य कोयले के मूल्य की वृद्धि करना था जिससे उनके वेतन विनियमित होते थे। प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया।
मेयर ऑफ बैडफोर्ड कारपोरेशन बनाम पिकिल्स, (1895) ए० सी० 587 के वाद में प्रतिवादी ने वादी के विपरीत कुभावना से प्रेरित होकर अपनी ही भूमि में कुछ खोदाई का कार्य किया था, क्योंकि वादी ने प्रतिवादी की भूमि को उसकी इच्छा के अनुरूप मूल्य देकर खरोदने से इन्कार कर दिया। इस खोदाई के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को भूमि के नीचे बहकर बगल की बादी की भूमि में जाने वाला जल बदरंग और कम हो गया। वहाँ वादी को क्षति विद्वेष के कारण हुई थी, परन्तु प्रतिवादी चूँकि अपनी स्वयं की भूमि का विधिपूर्ण प्रयोग कर रहा था, इसलिए उसे उत्तरदायी नहीं माना गया।
टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल, (ए० आई० आर० 1975 इला० 132) के मामले में वादी ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किये बिना कुछ निर्माण कार्य किया था। प्रतिवादियों ने यह निर्माण ध्वस्त कर दिया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दाखिल किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा निर्माण ध्वस्त करने का कार्य अवैध था, क्योंकि टाउन एरिया कमेटी के कुछ अधिकारियों ने उस निर्माण को ध्वस्त करने में दुर्भावना का कार्य किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि अवैध रूप से निर्मित किसी निर्माण का ध्वस्त किया जाना पूर्णत: विधि सम्मत है। न्यायालय ने इस प्रश्न पर कोई जाँच-पड़ताल नहीं की क्या ध्वस्त कार्य विद्वेष के कारण किया गया था अथवा नहीं क्योंकि इसे अप्रासंगिक माना गया था। इस वाद का निर्णय देते समय न्यायाधीश हरि स्वरूप ने कहा कि “वादी केवल तभी प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, यदि वह यह साबित कर देता है तक उसे प्रतिवादी के अवैध कार्य से हानि हुई है अन्यथा नहीं, यहाँ दुर्भावना के उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई विधिक कार्य चाहे भले वह दुर्भावना से संप्रेरित हो, उसके कर्ता को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता मात्र यह कारण कि कुछ अधिकारी एक ऐसे नागरिक के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त हैं, जिसने कोई दोषपूर्ण कार्य किया है, प्राधिकारी के कार्य को अवैध नहीं बना देता, यदि वह अन्यथा विधि के अनुसार किया गया है। केवल दुर्भावना किसी व्यक्ति को इस बात के लिए अनधिकृत नहीं बना देती कि वह किसी गलत कार्य को रोकने के लिए विधिपूर्ण कार्य न करें।”
प्रश्न 22. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तक के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करते हुए इसके उद्देश्य एवं प्रकृति का वर्णन करें।
Mention objects and nature of Consumer Protection Act, 1986 by describing its historical development.
उत्तर– यह युग औद्योगिक क्रान्ति का युग है। उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए कारखानों में असंख्य चीजों का उत्पादन किया जा रहा है जिनका पहले कोई नाम भी नहीं जानता था जैसे-रेफ्रीजरेटर, फ्रीजर, टेलीविजन आदि। इन वस्तुओं की उपभोक्ताओं में खपत आज बहुत बढ़ गई है। समाज के हर वर्ग के लोग इन वस्तुओं को खरीद रहे हैं। फलत: इन वस्तुओं के उत्पादनकर्ता इस बात का भरसक प्रयास करते हैं कि उस वस्तु का मूल्य कम हो भले ही गुणवत्ता कम हो जाय। निम्न आय वर्ग के लोगों को बाध्यतः इन घटिया किस्म के उत्पादनों को खरीदना पड़ता है। यही नहीं इन वर्गों के लोगों में उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित विधि की जानकारी भी नहीं होती है। ऐसे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए अन्य देशों का अनुसरण करते हुए 1986 में भारत में भी संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया। पुनः वर्तमान में हमारी संसद ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 की पारित कर 9 अगस्त, 2019 को नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का निर्माण किया।
औद्योगिकरण के विकास के साथ उत्पादों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के फलस्वरूप होने वाली क्षतियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुकता आई है और अपने दावों के चलाने के बारे में स्वैखिक संस्थाओं की सहायता लेने की प्रवृति में वृद्धि होने की आशा है। अगले कुछ वर्षों में और अधिक उपभोक्ता विवाद फोरमों की स्थापना किये जाने की उम्मीद है जिसका कि उपभोक्ता सरलता से लाभ उठा सकेंगे। प्रो० विनफील्ड के अनुसार उपेक्षा अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी बादी को क्षति पहुँचती है।
इस तरह उपेक्षापूर्ण दायित्व के निम्नलिखित आवश्यक तत्य है –
(1) सावधानी बरतने का कर्तव्य
(2) कर्तव्य भंग; तथा
(3) कर्तव्य भंग के परिणामस्वरूप हुई क्षति ।।
अधिनियम का उद्देश्य – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अपने आप में एक अनोखा अधिनियम था। किसी भी देश में उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालयों या अधिकरणों की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन भारत में उपभोक्ताओं के •विवादों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की गई है। भारत में उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अर्द्ध न्यायिक निकायों की स्थापना का उपबन्ध करता है और उन्हें स्थापित न्यायालयों की भांति ही अधिकारिता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शीघ्रतर और कम खर्चीला न्याय प्रदान करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण करना है –
(क) जीवन और सम्पत्ति के लिए परिसंकटमय माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार;
(ख) माल की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार जिससे अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता का संरक्षण किया जा सके:
(ग) जहाँ भी सम्भव हो वहाँ प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल सुलभ कराने का आश्वासन दिये जाने का अधिकार;
(घ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ता के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार;
(ङ) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।
उपर्युक्त उद्देश्यों का संवर्द्धन और संरक्षण करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बनाने का उद्देश्य इन उद्देश्यों को अधिक सुदृढ़ एवं सफल बनाना है।
लखनऊ विकास अधिकारी बनाम एम० के० गुप्ता, ए० आई० आर० (1994) एस० सी० 787 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया अधिनियम है इसलिए इसके उपबन्धों का निर्वाचन उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।
संरक्षण की प्रकृति- अधिनियम की धारा 100 यह कहती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में इसका तात्पर्य यह है कि अधिनियम उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त उपचार प्रदान करता है, किन्तु पहले से विद्यमान मौलिक विधियों को समाप्त नहीं करता है। अतः वे अभी भी लागू रहेंगी और यदि कोई व्यक्ति उनके अधीन उपचार प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है। किन्तु इन विधियों के अन्तर्गत उपचार पाने के लिए उन्हें सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित करना पड़ेगा जहाँ बहुत विलम्ब होता है और कोर्ट फौस भी देनी पड़ती है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अर्द्धन्यायिक निकायों में उपचार पाने को प्रक्रिया बहुत सरल और कम खर्चीली है। इनमें वकील करने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ कोर्ट फीस नहीं लगती है।
प्रश्न 23. (i) जिला उपभोक्ता फोरम की संरचना तथा क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। जिला उपभोक्ता फोरम का सदस्य कौन हो सकता है?
Discuss the composition and powers of District Consumer Forum. Who can be member of District Consumer Forum ?
(ii) परिवाद प्राप्त होने पर जिला उपभोक्ता मंच की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
Discuss the procedure of District Consumer Forum on receipt of complaint.
उत्तर (i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता हितो का श्रेष्ठतर (better) संरक्षण तथा इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता विवादों के निपटारा करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निपटारा अधिकरणों को स्थापना करना है। उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत तीन स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निपटारा अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने हेतु जिला आयोग का राज्य स्तर पर राज्य आयोग का तथा केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है।
जिला उपभोक्ता फोरम की संरचना – प्रत्येक जिला में एक जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत है। प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला आयोग की स्थापना करेगी। परन्तु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित कर सकेगी।
अधिनियम की धारा 28 जिला उपभोक्ता फोरम की संरचना के बारे में है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक जिला आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा- (क) अध्यक्ष (ख) दो से अन्यून और ऐसी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विहित किये जाएं। राज्य सरकार जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की संस्तुति पर करेगी। इस चयन समिति में (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष, (2) राज्य सरकार का सचिव, तथा (3) राज्य के उपभोक्ता विभाग का सचिव सम्मिलित होगा।
जिला उपभोक्ता फोरम (पीठ) का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश है, या किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है।
जिला उपभोक्ता फोरम के अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति किसी ऐसे व्यक्तियों में से को जायेगी जो योग्य, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे तथा जो 35 वर्ष की आयु एवं जिनमें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म (Accountancy) या प्रशासन का कम से कम 10 वर्ष का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव होगा या उससे सम्बन्धित कार्य करने की योग्यता होगी। इन दो सदस्यों में से एक महिला होना आवश्यक है।
जिला उपभोक्ता फोरम का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की समायावधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक या इनमें से जो पहले हो अपने पद पर रहेगा। जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ये सदस्य अपनी पदावधि पूरी होने के पूर्व त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं।
जिला आयोग की क्षेत्राधिकारिता (Jurisdiction) (धारा 34 )
प्रत्येक जिला उपभोक्ता फोरम को अपने जिले की स्थानीय सीमा से सम्बन्धित उन विवादों पर निर्णय का अधिकार होगा जिसमें माल या सेवा का मूल्य तथा दावा प्रतिकर मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इस प्रकार जिला उपभोक्ता फोरम की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता एक करोड़ रुपये तक है।
परिवाद किये जाने की रीति (धारा 35 ) – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अनुसार विक्रय या परिदान के लिए सहमत किसी माल के सम्बन्ध में या उपलब्ध कराई गई सेवा के सम्बन्ध में कोई परिवाद निम्नलिखित द्वारा जिला आयोग में किया जा सकेगा जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी है (क) (i) उपभोक्ता जिसको ऐसा माल विक्रय या परिदत्त किया गया है अथवा विक्रय या परिदान के लिए सहमति दी गई है या ऐसी सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं अथवा सहमति प्रदान की गई है, या
(ii) जो ऐसे मालों या सेवाओं के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार, व्यवहार का अभिकथन करता है।
(ख) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, चाहे वह उपभोक्ता, जिसे ऐसे मालों का विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या जिसे ऐसे मालों का विक्रय करने या परिदान करने की सहमति दी गई है या ऐसी सेवा प्रदान की गई है या प्रदान करने की सहमति दी गई है या जो ऐसे मालों या सेवाओं के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन करता है, ऐसे संगम का सदस्य है या नहीं;
(ग) एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जहाँ अनेक ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका हित समान है, जिला आयोग की अनुज्ञा से सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके फायदे के लिए इस प्रकार हितबद्ध सभी उपभोक्ता या
(घ) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकारण या राज्य सरकार, परन्तु इस उपधारा के अधीन परिवाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाएँ फाइल किया जा सकेगा।
धारा 35 (2) के अनुसार प्रत्येक परिवाद के साथ शुल्क संलग्न होगा और ऐसी रीति में संदेय होगा, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप भी है की ऐसी धनराशि देय होगी जो विहित की जाये। ऐसे किसी परिवाद के प्राप्त होने पर जिला आयोग आगे की कार्यवाही का आदेश देगा या उसे अस्वीकृत कर सकेगा किन्तु किसी परिवाद के अस्वीकृत करने के पहले परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। परन्तु ऐसे परिवाद की ग्राह्यता पर विनिश्चय सामान्य रूप से परिवाद प्राप्त करने की तिथि से 21 दिनों के भीतर कर दिया जाना आवश्यक होगा। जब जिला आयोग परिवाद पर कार्यवाही किये जाने के लिए स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। जब उपधारा 3 के अधीन जिला फोरम परिवाद को ग्रहण कर लेता है तो किसी अन्य विधि के द्वारा स्थापित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अधिकारी के समक्ष परिवाद का अन्तरण नहीं किया जा सकता है।
धारा 35 (2) द्वारा पहली बार उपभोक्ता फोरम के अधीन शुल्क देने का उपबन्ध किया गया है। शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार करेगी।
नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि० बनाम एम० मधुसूदन रेड्डी, ए० आई० आर० (2012) सुप्रीम कोर्ट 1160 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी अभिकरण द्वारा किसानों को घटिया बीज बेचे जाने के विरुद्ध जिला पीठ में परिवाद किया जा सकता है। यद्यपि कि “बीज अधिनियम” उत्तम बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष अधिनियम है किन्तु यह किसानों को खराब बीज बेचे जाने के फलस्वरूप उनको हुई हानि की क्षतिपूर्ति का कोई उपबन्ध नहीं करता। इसके अतिरिक्त बीज अधिनियम का कोई भी उपबन्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रयोज्यता को वर्जित नहीं करता।
जिला आयोग स्थगन आदेश जारी नहीं कर सकता- यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवादों को निपटाते समय जिला आयोग स्थगन आदेश नहीं दे सकता है।
जिलापीठ द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। किन्तु जहाँ किसी प्रश्न पर मतभेद है, वहाँ बहुमत की राय जिलापीठ का आदेश होगा।
पंजाब नेशनल बैंक बनाम कन्प्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ए० आई० आर० (2012) केरल 8 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार जिलापीठ को बैंक को वित्तीय सम्पत्ति सुरक्षा व पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अपने अधिकारों को प्रवर्तित करने के विरुद्ध व्यादेश देने अथवा रोकने की शक्ति नहीं है।
उच्चतम न्यायालय चिकित्सीय उपेक्षा के मामले में किये गये दावों में प्रतिकर की धनराशि का परिणाम निर्धारित किये जाने हेतु गुणक विधि की जटिलतापूर्ण प्रक्रिया का प्रयोग किये जाने को लेकर संशयात्मक रहा है। बलराम प्रसाद बनाम कुनाल साहा, (2014) 1 एस० सी० सी० 384 जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मुआवजे की राशि निर्धारण करने में मृतक की प्रतिष्ठा, पद, प्रास्थिति, भविष्य की सम्भावना व शैक्षणिक योग्यता पर विचार किया जाना आवश्यक है। मृतक की भविष्य की सकल आय अर्जन का उचित योग करके उसमें उसके व्यक्तिगत व्ययों को घटा दिया जाना चाहिए।
इसके साथ ही क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय मुद्रास्फीति को भी स्थान में रखा जाना चाहिए। जहाँ वाद 15 वर्षों से लम्बित था वहाँ मुद्रा के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए दावाकर्ता के दावे को मुद्रा के वर्तमान मूल्य के अनुसार बढ़ाया गया।
जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील (धारा 41) – जिला आयोग द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर आदेश के विरुद्ध ‘राज्य आयोग’ में अपील कर सकेगा। राज्य आयोग उक्त 45 दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था। अपील का प्रारूप और रीति राज्य द्वारा बनाए नियमों के अनुसार होगा।
किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे जिलापीठ के आदेश के अनुसार किसी धनराशि का भुगतान करना आवश्यक है, द्वारा कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक अपीलार्थी ने उस धनराशि का 50% या 2500 रुपये, जो भी कम हो, जमा न कर दिया हो।
परन्तु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यक्ता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी।
(ii) परिवाद प्राप्त होने पर प्रक्रिया (Procedure on receipt of complaint) – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 के अनुसार-(1) जिला आयोग किसी परिवाद को ग्रहण करने पर या मध्यक्ता द्वारा परिनिर्धारण के लिए असफल होने की दशा में मध्यक्ता के लिए निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में ऐसे परिवाद पर आगे कार्रवाई करेगा।
(2) जहाँ परिवाद किन्हीं मालों से सम्बन्धित है तो जिला आयोग –
(क) ग्रहण किए गए परिवाद की एक प्रति उसके ग्रहण करने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिन की अवधि या पन्द्रह से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो मंजूर की जाएँ, मामले के बारे में अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करें:
(ख) विरोधी पक्षकार खण्ड (क) के अधीन उसकी निर्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति पर परिवार में अन्तर्विष्ट अभिकथनों से इन्कार करता है या उनका प्रतिवाद करता है, या जिला आयोग द्वारा दिये गये समय के भीतर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है वहाँ उपभोक्ता विवाद को खण्ड (ग) से खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति में निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा:
(ग) परिवादी ने माल में किसी ऐसी त्रुटि का अभिकथन किया है, जिसका अवधारण माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है वहाँ परिवादी से माल का नमूना अभिप्राप्त करेगा, उसे सीलबन्द करेगा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएँ, अधिप्रमाणित करेगा और इस प्रकार सीलबन्द नमूने को इस निदेश के साथ समुचित प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा कि ऐसी प्रयोगशाला यह पता लगाने की दृष्टि से ऐसे विश्लेषण या परीक्षण, जो भी आवश्यक हो, करे कि ऐसे माल में परिवाद में अभिकथित कोई त्रुटि है या नहीं अथवा माल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट निर्देश की प्राप्ति के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिला आयोग द्वारा मंजूर की गई हो, को भेजेगा;
(घ) खण्ड (ग) के अधीन किसी समुचित प्रयोगशाला को माल के किसी नमूने को निर्दिष्ट किये जाने से पूर्व, परिवादी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रश्नगत मालों के सम्बन्ध में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए समुचित प्रयोगशाला को संदाय के लिए ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाएँ, आयोग के जमा खाते में जमा करें,
(ङ) समुचित प्रयोगशाला को खण्ड (घ) के अधीन अपने जमा खो में जमा की गई रकम को प्रेषित करेगा जिससे कि वह खण्ड (ग) में वर्णित विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके और समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर विरोधी पक्षकार को ऐसी टिप्पणी जो वह समुचित समझे, के साथ रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा;
(च) यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार समुचित प्रयोगशाला के निष्कर्षों की शुद्धता पर विवाद करते हैं या समुचित प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या जाँच की पद्धतियों की शुद्धता पर विवाद करते हैं तो विरोधी पक्षकार या परिवादी से यह अपेक्षा करेगा कि वह समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने आक्षेप लिखित में प्रस्तुत करें।
(छ) समुचित प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा के सम्बन्ध में परिवादी के साथ विरोधी पक्षकार को सुने जाने का और खण्ड (च) के अधीन उसके सम्बन्ध में किये गये आक्षेप तथा धारा 39 के अधीन समुचित आदेश जारी करने के बारे में भी युक्तियुक्त वसर देगा।
(3) यदि धारा 36 के अधीन उसके द्वारा स्वीकार किया गया परिवाद उन मालों के सम्बन्ध में है जिनकी बाबत उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता या परिवाद किन्हीं सेवाओं से सम्बन्धित है, तो जिला आयोग –
(क) विरोधी पक्षकार को ऐसे परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करते हुए निदेश देगा कि वह मामले के अपने पक्ष को तीस दिन की अवधि के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी विस्तारित, जो जिला आयोग द्वारा अनुदत की जाए के भीतर प्रस्तुत करे
(ख) जहाँ विरोधी पक्षकार, खण्ड (क) के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई परिवाद की प्रति के प्राप्त हो जाने पर परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उन पर विवाद करता है या जिला आयोग द्वारा प्रदान किये गये समय के भीतर अपने मामले का व्यपदिष्ट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो उपभोक्ता विवाद का निपटारा –
(1) उसकी सूचना में परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा लाए गए साक्ष्य के आधार पर यदि विरोधी पक्षकार परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों से इन्कार करता है या उन पर विवाद करता है; या
(ii) जहाँ विरोधी पक्षकार आयोग द्वारा प्रदान किये गये समय के भीतर अपना मामला व्यपदिष्ट नहीं करता है या करने में असफल रहता है वहाँ परिवादी द्वारा उसके ध्यान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करेगा।
(ग) परिवाद का गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करेगा यदि परिवादी सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है।
(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए जिला आयोग आदेश द्वारा किसी इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदाता से ऐसी सूचना दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे।
(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाली कार्यवाहियों को इस आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया गया है।
(6) प्रत्येक परिवाद की सुनवाई जिला आयोग द्वारा शपथ-पत्र और अभिलेख पर रखे गये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर की जाएगी :
परन्तु जहाँ सुनवाई के लिए या वैयक्तिक रूप से या वीडियो संगोष्ठी के माध्यम से पक्षकारों की परीक्षा के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो जिला आयोग पर्याप्त हेतुक उपदर्शित करने पर और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् वैसा करने को अनुज्ञात कर सकेगा।
(7) प्रत्येक परिवाद पर यथासम्भव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परिवाद को विनिश्चित करने का वहाँ प्रयास किया जाएगा जहाँ परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा की जाती है :
परन्तु जिला आयोग द्वारा स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक पर्याप्त हेतुक नहीं दर्शाया जाता है और स्थगन की मंजूरी के कारणों को आयोग द्वारा लेखबद्ध न कर दिया गया हो।
परन्तु यह और कि जिला आयोग स्थगन के कारण उपगत होने वाली लागतों के सम्बन्ध में ऐसे आदेश करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद का परिनिर्धारण किये जाने की दशा में जिला आयोग उक्त परिवाद के परिनिर्धारण के समय, उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।
(8) जहाँ जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, आयोग को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसा अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित हो।
(9) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला आयोग को वही शक्तियाँ होंगी जो निनलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात् :
(क) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा करना;
(ख) साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु के प्रकटोकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;
(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) समुचित प्रयोगशाला से या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से सम्बद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और
(च) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित किया जाए।
(10) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिला आयोग दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ दाण्डिक न्यायालय समझा जाएगा।
(11) जहाँ प्रतिवादी धारा 2 के खण्ड (5) के उपखण्ड (vi) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश के नियम 8 के उपन्ध इस 1 उपान्तरण के अध्यधीन लागू होंगे कि किसी वाद या डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह परिवाद या उस पर जिला आयोग के आदेश के प्रति निर्देश है।
(12) किसी परिवादी जो उपभोक्ता है या विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद फाइल किया गया है, कि मृत्यु की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 के उपबन्ध इस उपान्तरण के अध्यधीन लागू होंगे कि वादी और प्रतिवादी के प्रति उसमें किया गया प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, परिवादी या विरोधी पक्षकार के प्रति निर्देश है।
किन्तु यूरेका इस्टेट्स प्राइवेट लि० बनाम ए० पी० एस० डी० आर० कमीशन, ए० आई० आर० (2005) आन्ध्र प्रदेश 118 के मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जिला फोरम या राज्य आयोग के समक्ष की गई कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13(4) में विहित सीमा के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू नहीं होगी अतः जिला फोरम या राज्य आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के अधीन पुनर्विलोकन की अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
यदि धारा 38 के अधीन की गई कार्यवाही के अधीन जिलापीठ को यह समाधान हो जाता है कि मामले में परिवाद में विनिर्दिष्ट कोई त्रुटि है या सेवाओं के बारे में कोई अभिकथन साबित हो जाता है तो वह विरोधी पक्षकार को निम्नलिखित में से कोई बातें करने का निर्देश देने वाला आदेश जारी करेगा –
(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना;
(ख) माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलना;
(ग) परिवादी द्वारा विरोधी पक्षकार को संदत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों (Charges) को परिवादी को वापस लौटाना;
(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए परिवादी को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की गई है।
परन्तु जिलापीठ को दण्डात्मक क्षतिपूर्ति ऐसी परिस्थितियों में मंजूर करने की भी शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे।
प्रश्न 24. (i) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद से आप क्या समझते हैं?
What do you know about the State Consumer Protection Council?
(ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत राज्य आयोग की संरचना तथा क्षेत्राधिकार की चर्चा करें।
Discuss the constitution and jurisdiction of State Commission under Consumer Protection Act, 1986.
उत्तर (i) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (State Consumer Protection Council)– राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से सम्बन्धित प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 तथा धारा 7 में किये गये हैं।
धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके (By notification) एक परिषद् (council) की स्थापना करेगी जिसे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के नाम से जाना जायेगा।
धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में निम्न सदस्य होंगे –
(1) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग का प्रभारी मंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होगा।
(2) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य इतनी संख्या में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जा सकेंगे जितनी संख्या में राज्य सरकार उचित समझे।
(3) अन्य शासकीय या अशासकीय सदस्यों की इतनी संख्या, जो दस से अधिक नहीं होगी, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाए।
धारा 6 उपधारा (3) के अनुसार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार वर्ष में हो सकती है परन्तु प्रत्येक वर्ष में परिषद् की कम से कम दो बैठक होना अनिवार्य है।
धारा 6 उपधारा (4) के अनुसार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक का स्थान तथा समय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा परिषद् का कार्य-कलाप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जायेगा।
अधिनियम की धारा 7 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के उद्देश्यों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। जैसे –
(1) जीवन तथा सम्पत्ति के लिए संकटपूर्ण मूल्य या सेवा के विपणन के विरुद्ध संरक्षण।
(2) माल या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा सके।
(3) जहाँ भी सम्भव हो प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों के माल या सेवा सुलभ कराने के आश्वासन का अधिकार।
(4) सुने जाने का अधिकार तथा उपभोक्ता विवाद निपटारा अधिकरणों के माध्यम से उपचार प्राप्त करने का अधिकार।
(5) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार।
(6) उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार।
उत्तर (ii) उपभोक्ता विवादों के निपटारा करने हेतु गठित अधिकरणों में राज्य, 2019 आयोग एक अपीलीय अधिकरण (appellate authority) है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 42 राज्य सरकार को प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग नामक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देती है।
राज्य आयोग साधारणत: राज्य की राजधानी में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कृत्यों को पालन करेगा जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करे। परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर जो वह ठीक समझे, राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखाएं स्थापित कर सकेगी।
धारा 42 की उपधारा (3) के अनुसार, प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा- (क) एक अध्यक्ष और (ख) चार से अन्यून और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विहित की जाएँ।
केन्द्रीय सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। (धारा 43 )
राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी (धारा 44 ) – (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उसके कृत्यों को निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और वह आयोग को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझे।
(2) राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
(3) राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएँ।
राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of State Commission) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47 राज्य आयोग की अधिकारिता के बारे में है। इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के तीन प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है –
(1) प्रारम्भिक अधिकारिता- (i) ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जहाँ माल या सेवाओं का मूल्य और दावा प्रतिकर एक करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 10 करोड़ से अधिक नहीं है।
परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
(ii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद जहाँ प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
(2) अपीलीय अधिकारिता – उस राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपोल ग्रहण करना।
(3) पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकारिता – जहाँ राज्य आयोग को यह प्रतीत हो कि जिलापीठ ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहता है या अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता किया गया है तो वह ऐसे उपभोक्ता विवाद को जो जिलापीठ में लम्बित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया गया है, के अभिलेखों को मंगा सकता है और समुचित आदेश पारित कर सकता है।
(2) राज्य आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा जैसा अध्यक्ष ठीक समझे:
परन्तु ज्येष्ठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा।
(3) जहाँ न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर राय पर मतभेद है वहाँ मुद्दों पर बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, यदि बहुमत है किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर घंटे हुए हैं, तब वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनमें मतभेद है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या महों को स्वयं सुनेगा या ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए मामलों को अन्य सदस्यों में एक अधिक सदस्य को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा जिन्होंने मामले पर सुनवाई की है जिसमें वे सदस्य भी हैं जिन्होंने इसे पहली बार सुना था:
परन्तु यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर इस निर्दिष्ट मुद्दा या मुद्दों पर राय देगा या देंगे।
(4) परिवाद ऐसे राज्य आयोग में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर –
(क) विरोधी पक्षकार या जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहाँ विरोधी पक्षकारों में उनमें से प्रत्येक पक्षकार परिवाद के संस्थित किये जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, या
(ख) जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहाँ विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किये जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जब ऐसे मामले में राज्य आयोग की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, या
(ग) वाद हेतुक पूर्णत: या भागत: उत्पन्न होता है;
(घ) परिवादी निवास करता है या काम करता है।
अपील– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51 के अनुसार, राज्य आयोग द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा;
परन्तु यह कि राष्ट्रीय आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारण थे :
परन्तु यह भी कि किसी व्यक्ति की, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबन्धनों में किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा है, कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है।
इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित किसी आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील की जाएगी यदि राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित हैं।
किसी ऐसी अपील में जिसमें विधि एक प्रश्न अन्तर्वलित है, अपील के ज्ञापन में अपील में अन्तर्वलित विधि के सारवान प्रश्न का ठीक ठीक कथन होगा।
जहाँ राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है वहाँ वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और उस प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा।
धारा 52 के अनुसार, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथासम्भव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और अपील के उसके ग्रहण किये जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से निपटान करने के लिए प्रयास किया जाएगा।
महेन्द्र ठाकुर बनाम देवेन्द्र कोठारी [1992 (1) सी० पी० आर० 23.] राज्य आयोग लखनऊ के बाद में यह निर्णय दिया गया कि अपील कर्ता को अपील करने में विलम्ब को क्षमा करने के लिए आवेदन देते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अपील प्रस्तुत करने में तत्परता से कार्य किया गया था। यदि कोई कार्य समुचित देख-रेख तथा ध्यान देकर नहीं किया जाता तो यह नहीं माना जा सकता कि कार्य तत्परता से किया गया है।
प्रश्न 25. राष्ट्रीय आयोग के गठन, संरचना तथा क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें।
Discuss the establishment, constitution and jurisdiction of National Commission.
उत्तर– उपभोक्ता विवादों के निपटारा हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले उपभोक्ता विवाद निपटारा अधिकरणों में राष्ट्रीय आयोग सर्वोच्च अधिकरण है। राष्ट्रीय आयोग पूरे देश में एक होगा।
राष्ट्रीय आयोग का गठन धारा 54 में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। धारा 53 (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग का गठन अधिसूचना द्वारा करेगी। राष्ट्रीय आयोग की संरचना से सम्बन्धित प्रावधान अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत किया गया है।
धारा 54 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्यों से मिलकर होगा।
राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएँ (धारा 55) – केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, पद के निबन्धन, वेतन और भत्ते, पद त्याग, हटाया जाना और सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी:
परन्तु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएँ किन्तु ऐसी तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:
परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण नहीं करेगा जो –
(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु:
(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में सहसठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगे।
(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों और न ही उनकी सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन किया जाएगा।
राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी (धारा 57 ) – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 57 के अनुसार (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या का उपबन्ध करेगी, जो वह ठीक समझे।
(2) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के साधारण अधोक्षण में अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
(3) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे जो विहित की जाएँ।
राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्राधिकारिता (Jurisdiction of National Commission)– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित अधिकारिता होगी –
(1) प्रारम्भिक अधिकारिता
(2) अपीलीय अधिकारिता
(3) पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकारिता
(1) प्रारम्भिक अधिकारिता – (i) ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जहाँ सेवाओं का मूल्य अथवा दासा प्रतिकर, दस करोड़ से अधिक है।
परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
(iii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद जहाँ प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है।
(2) अपीलीय अधिकारिता – (1) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करना।
(ii) केन्द्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें
अपील करने की सीमा अवधि 30 दिनों तक की है। आयोग अपील का निपटारा को प्रथम तिथि से लेकर 90 दिनों तक की अवधि के भीतर करेगा आयोग के आदेश की प्रतियाँ ‘दोनों पक्षों को निःशुल्क भेजी जायेंगी।
मारघेश के० पारेख बनाम मयूर एय० मेहता, ए० आई० आर० (2011) सु० को० 249 के मामले में चिकित्सा में असावधानी सिद्ध होने पर राज्य आयोग ने पाँच लाख रुपये प्रतिकर प्रदान करने का आदेश किया था जिसके विरुद्ध चिकित्सकों द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील करने पर आयोग ने अपील को स्वीकृत करते हुए राज्य आयोग के अधिनिर्णय को निरस्त कर दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। न्यायालय ने पाया कि राज्य आयोग के समक्ष सुनवाई में चिकित्सकों द्वारा मामले के महत्वपूर्ण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था व उपचार करने वाले चिकित्सक का शपथपत्र भी नहीं दिया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय आयोग इसके लिये कर्त्तव्यबद्ध है कि वह इस लोप को गम्भीरतापूर्वक देखे कि महत्वपूर्ण अभिलेखों व शपथ-पत्र 6 वर्षों तक के दीर्घ काल तक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया जो कि उपचार प्रक्रिया के प्रकटीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण थे। अतः राष्ट्रीय आयोग का यह गम्भीरतम लोप न्याय की विफलता कारित करता है। उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकृत करते हुए राष्ट्रीय आयोग के निर्णय को निरस्त कर दिया व मामले के पुन: निर्णयन हेतु राष्ट्रीय आयोग की निर्देशित किया।
(3) पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकारिता– यदि राष्ट्रीय आयोग को यह प्रती हो कि राज्य आयोग ने किसी ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें विहित नहीं हैं या जो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहता है या अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है तो वह ऐसे उपभोक्ता विवाद को राज्य आयोग में लम्बित है या उसके द्वारा विनिश्चय किया गया है उसके अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना।
उस दशा में जहाँ कि “दण्डात्मक प्रतिकर” हेतु दावा न तो मूल वादपत्र में, न राज्य अधिकारिण के समक्ष और न ही राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किया गया हो, वहाँ राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन दण्डात्मक प्रतिकर प्रदान किया जाना अनुज्ञेय नहीं है। [जनरल मोटर्स (इण्डिया) प्रा० लि० बनाम अशोक रमणिक लाल, (2015) 1 एस० सी० सी० 429]
सी० सी० आई० चेम्बर्स को० आ० सोसायटी लि० बनाम डी० सी० बैंक लि०, ए० आई० आर० (2004) एस० सी० 184 के मामले में अपीलार्थी जिसका बैंक में खाता था, राष्ट्रीय आयोग में एक परिवाद फाइल किया और बैंक पर सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए अभिकथन किया कि उसने अपीलार्थी के ऐसे चेक, जिन पर उसके कूटरचित / जाली हस्ताक्षर बनाये गये थे व ऐसे चेक जिनके अंक बदल दिये गये थे, स्वीकार कर लिये थे परिणामस्वरूप उसके खाते से 75,70,325 रुपये अनुचित रूप से निकल लिये गये थे। राष्ट्रीय आयोग ने बैंक को बिना नोटिस दिये परिवाद को मात्र इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसमें तथ्य व विधि के जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त थे और परिवादी को सिविल न्यायालय जाने की सलाह दी गयी।
उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परम्परागत न्यायालयों में उनके कार्यों का बोझ कम करना है। अतः मात्र इसलिए कि मामले की निर्णीत किये जाने हेतु अत्यधिक अन्वेषण व साक्ष्य अपेक्षित हैं, कोई भी आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत परिवादी के लिये अपने द्वार को बन्द नहीं कर सकता है। आयोग का निर्णय अविचारित है, प्रत्यर्थी बैंक को नोटिस दिया जाना व उसके अभिकथन को लिया जाना चाहिए था। केवल तब जब दोनों पक्षों के अभिवचन उपलब्ध हो तभी आयोग जाँच की प्रकृति और परिधि के बारे में अपनी राय निश्चित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय आयोग के निर्णय को अपास्त कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए उसे पुनः प्रेषित कर दिया।
राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में अपील (धारा 67) – राष्ट्रीय आयोग के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उसके आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है [ धारा 21 (क) (i) ] । परन्तु उच्चतम न्यायालय 30 दिनों की अवधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील विलम्ब से फाइल करने का पर्याप्त कारण था। किन्तु ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश के तहत किसी धनराशि के भुगतान, करने के दायित्वाधीन भी है उसकी अपील को उच्चतम न्यायालय तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसने उक्त धनराशि का 50% या 50,000 रुपये, जो भी कम हो, विहित रीति से जमा न कर दिया हो।
आदेशों की अन्तिमता (धारा 68) – जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, तो उसका निर्णय अन्तिम होगा।
परिसीमा अवधि [ धारा 69] – जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग किसी भी वाद को ग्रहण नहीं करेंगे यदि वह वाद कारण उत्पन्न होने के दिन से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता अधिनियम के अधीन किसी परिवाद की प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि दो वर्ष है। इसके पश्चात् परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
किन्तु उक्त अवधि के बीतने के पश्चात् भी परिवाद ग्रहण किया जा सकता है, यदि परिवादी उपर्युक्त उपभोक्ता फोरमों को सन्तुष्ट कर देता है कि उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का उसके पास समुचित कारण थे
प्रश्न 26. उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्ता वाद की उपयोगिता एवं विकास की व्याख्या कीजिए।
What is Consumerism? Discuss the utility and progress of Consumerism?
उत्तर – उत्पादक को यह शक्ति या अधिकार है कि वह प्रोडक्ट को डिजायन करें, उसकी रूपरेखा आकार बनायें, विज्ञापन करें, वितरण और मूल्य निर्धारण करें, जबकि उपभोक्ता को केवल यह अधिकार है कि उसे न खरीदें। उत्पादक को अधिक रिस्क उठाना होता है जबकि निषेधाधिकार उपभोक्ता के हाथ होता है। लेकिन उपभोक्ता अक्सर महसूस करता है कि वह इस अधिकार का उपयोग अपने ही हित में करने को कमजोर है इसका कारण स्पर्धा करने वाले उत्पादक की ओर से अपूर्ण या मिथ्या सूचना हो सकती है या पर्याप्त सूचना का अभाव।
उपभोक्तावाद से तात्पर्य है- उपभोक्तावाद उपलब्ध धन में माल की खरीद से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद करेगा, उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भी बिना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माल प्राप्त करने में सहायक होगा, उन्हें अपने अधिकारों की सम्यक् जानकारी देगा, प्रशिक्षित करेगा। उनके हितों की सीमा बताएगा उनसे सजग रहने का उपाय भी सुझायेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार, जीवन व वैचारिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस पदावली को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। जीवन के लिए खाने-पीने, चलने फिरने, अमन चैन से रहने, स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19 (1) भी प्रत्येक व्यक्ति को मनचाहे वृत्तिक व्यापार, कारोबार करने के अधिकार की गारण्टी देता है। लेकिन इसके दुरुपयोग पर भी अवरोध लगाता है जिससे कि सामान्य लोगों के व्यवहार पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके।
उपभोक्तावाद की उपयोगिता- सुसंगत एवं प्रगतिशील समाज से निम्नलिखित परिणाम पाने की आशा की जा सकती है –
(1) उत्पादक एवं विक्रेता प्राय: ग्राहकों पर भरोसा नहीं करते परन्तु जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के संरक्षण में अधिक ताकतवर लगता है तो व्यापारी अनुचित श्रम व्यवहार करने से बचने लगेंगे।
(2) उपभोक्तावाद व्यापार को ‘फीड बैक’ उपलब्ध करायेगा। यह उत्पादकों को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने में समर्थ बनायेगा, यह मारकेटिंग कान्सेप्ट, जो उपभोक्ता की प्रकृति पर निर्भर करेगा, को कारगर ढंग से लागू करने में सहायक होगा।
(3) उत्पादक अपने वितरण की सूचियों को उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार सूचीबद्ध करने में सफल होंगे। प्रायः जमाखोरी तथा चोरबाजारी से क्षीण आपूर्ति की स्थिति अत्यधिक खराब हो जाती है। वास्तविक मूल्य से अत्यधिक मूल्य ले लेते हैं।
(4) उपभोक्तावाद सरकार को उपभोक्ता हितों के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी बनाने में कारगर होगा, उसे सम्बन्धित आवश्यक उपायों को करने के लिए प्रेरित करेगा।
उपभोक्तावाद का विकास- सर्वप्रथम उपभोक्तावाद का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में 1927 में हुआ और इसको 1936 में आगे विकसित किया गया। आज भी उन्नत देशों में उपभोक्ता स्पष्ट रूप से भारत के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिकारों एवं हितों के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं। 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ० कैनेडी और 1965 में राष्ट्रपति विल्सन जानसन ने उपभोक्ता अधिकार पर अधिक जोर दिया तथा उपभोक्तावाद के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायक बना। 15 मार्च, 1962 में उपभोक्ता के “बिल ऑफ राइट्स’ में 4 अधिकारों को चिन्हित किया गया। यही ‘बिल ऑफ राइट्स’ अमेरिका में सही मायने में उपभोक्ता अधिकारों का मैग्नाकार्टा माना गया।
उपभोक्ताओं के महत्वपूर्ण अधिकारों में सम्मिलित है
(1) अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में शोषण के विरुद्ध अधिकार;
(2) ऐसे माल व सेवा जिसे उपभोक्ता खरीदते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण का अधिकार;
(3) उत्पादों के गुण-अवगुण के बारे में सूचना पाने का अधिकार,
(4) शिकायत या सुझाव को सुने जाने का अधिकार;
(5) शिकायतों को दूर कराने का अधिकार;
(6) अनेकानेक माल में सबसे अच्छे माल को लेने चुनने का अधिकार;
(7) जीवन की क्वालिटी को सुरक्षित रखने का अधिकार;
इस प्रकार अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देशों में बड़ी तेजी से उपभोक्ताओं के अधिकारों व हितों के संरक्षण के प्रति जागरूकता आयी। इस प्रकार बहुत देश जहाँ उपभोक्ता हितों के संरक्षण को मान्यता देते हैं वहीं अधिनियम भी बनाते हैं।
भारत में उपभोक्तावाद – सामान्यतः भारतवर्ष में उपभोक्तावाद नाम की कोई चीज नहीं थी। इसका कारण था भारतीय उपभोक्ता बड़े ही सहनशील, क्षमाशील और अपने अधिकारों तथा हितों के प्रति उदास, असावधान हैं। साधारण नागरिक शिकायत करने और लड़ाई लड़ने के स्थान पर वह कार्यालयों की अवांछित फन्क्शनिंग के दबाव को झेलना बेहतर समझता है अपेक्षाकृत उसका डट कर मुकाबले करने की। इस प्रकार भारत में उपभोक्तावाद अपने शैशवास्था में ही रह गया था जैसे-कन्ज्यूमर गाइडेन्स सोसाइटी ऑफ इण्डिया और कन्ज्यूमर एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेण्टर जो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा का विकास 1960 और 1970 में हुआ लेकिन 1980 में यह अपने उत्कर्ष पर पहुँच गया। उपभोक्तावाद पर एक सेमिनार जनवरी 1986 में दिल्ली में हुआ जिसमें राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसी विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया गया। पुनः संसद द्वारा 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पारित किया गया है। जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।
प्रश्न 27. संक्षिप्त टिप्पणी लिखें –
(1) सांविधिक प्राधिकार (Statutory Authority)
(2) अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Unliquidated damages )
(3) आवश्यकता के कार्य (Act of necessity)
(4) उपभोक्ता (Consumer)
(5) प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा (Prohibited Trade Practice)
(6) सेवा पदावली (Term Service)
उत्तर – (1) सांविधिक प्राधिकार (Statutory Authority) – यदि क्षति किसी ऐसे कार्य से उत्पन्न होती है, जिसे विधान मण्डल ने करने के लिए प्राधिकृत किया है तो वह क्षति वाद योग्य नहीं है। जब कोई कार्य किसी अधिनियम के प्राधिकार से किया। जाता है, तो यह एक पूर्ण प्रतिरक्षा के रूप में मान्य है और क्षत-पक्षकार को उस उपचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार नहीं मिल सका, जो स्वयं उस संविधि में प्रदान किया गया है।
उदाहरण– यदि किसी रेल-पथ का निर्माण किया जाता है, तो वह किसी प्राइवेट भूमि के साथ हस्तक्षेप भी हो सकता है। जब रेलगाड़ी चलती है, तब उनके शोर, प्रकम्पन, धुएँ और चिन्गारियों के उड़ने आदि से भी कुछ हानि हो सकती है। ऐसे किसी प्रकार के हस्तक्षेप से चाहे वह भूमि का हस्तक्षेप हो अथवा आनुषंगिक हानि, उसे अपकृत्य मानकर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु यदि उसके लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान की अधिनियम में व्यवस्था की गई है तो केवल उसके लिए बाद लाया जा सकता है। बाघन बनाम टैफ्फ वेल रेल कम्पनी, (1860) 5 एच० एण्ड एन० 679 के बाद में प्रतिवादी रेल कम्पनी के एक इंजन से निकली हुई चिनगारी ने वादी के जंगल में आग लगा दी, जो रेलवे लाइन के बगल में था। इस कम्पनी को रेलगाड़ी चलाने का प्राधिकार प्राप्त था। वह धारित किया गया कि चूँकि प्रतिवादी ने चिन्गारियों का निकलना रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती थी, और उन लोगों ने उस कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य भी नहीं किया था, जिसके लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया था अतः वे उत्तरदायी न थे।
हैम्मरस्मिथ रेल कम्पनी बनाम ब्राण्ड, (1869) एल० आर० एच० एल० 171 के बाद में रेलगाड़ियों के चलने के कारण उससे उत्पन्न शोर, प्रकम्पन और धुएँ से वादी की सम्पत्ति के मूल्य में बहुत अधिक कमी हो गई। रेल पथ जिस पर ये गाड़ियों चलती थीं सांविधिक प्राधिकार से निर्मित किये गये थे। संविधि द्वारा प्राधिकृत गाड़ियों के कारण जो क्षति हुई थी, वह चूँकि आवश्यकत: आनुषंगिक थी, इसलिए यह धारित किया गया कि क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
स्मिथ बनाम लंदन एण्ड साउथ वेस्टर्न रेलवे कम्पनी, (1870) एल० आर० 6 सी० पी० 14 के बाद में रेलवे कम्पनी के कर्मचारियों ने घास और बाड़ों के काट-छाँट के ढेर को उपेक्षा के साथ रेल-पथ के समीप छोड़ दिया। एक इंजन से निकली हुई चिंगारियों के कारण इस ढेर में आग लग गई, वह आग रेल पथ से 200 गज दूर हवा के तेज झोंकों के कारण वादी की झोपड़ी तक पहुँच गई झोपड़ी जलकर राख हो गई। चूँकि यह रेल कम्पनी के कर्मचारियों की उपेक्षा का एक मामला था, अतः रेल कम्पनी उत्तरदायी मानी गई।
उत्तर – (2) अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Unliquidated damages) – किसी भी दीवानी (civil) अपकार का उपचार प्रतिकर है और चूँकि अपकृत्य एक दीवानी अपकार है इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अपकृत्य करता है तो उसे उसके द्वारा किये गये क्षति के लिए क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकर देना पड़ेगा और यहाँ तक कि प्रतिकर कैसा होना चाहिए चूँकि प्रतिकर तो कई प्रकार का होता है जैसे-परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, अवमानात्मक क्षतिपूर्ति प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति आदि। अतः सामण्ड, विनफील्ड व अन्य विधिज्ञों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि प्रतिकर, अपरिनिर्धारित प्रतिकर (unliquidated damages) होना चाहिये।
अब यहाँ पर बात यह उठती है कि अपरिनिर्धारित प्रतिकर क्या होता है। जब प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि पूर्व निश्चित होती है तो उसे परिनिर्धारित नुकसानी कहते है किन्तु जब प्रतिकर के रूप में देय धनराशि पूर्व-निश्चित नहीं होती तथा वह न्यायालय जो उचित समझे उसे निश्चित करे तो उसे ‘अनिर्धारित नुकसानी’ कहते हैं। अपकृत्य के किसी मामले में पक्षकारों द्वारा प्रतिकर की राशि की संविदा जैसे पूर्व निर्धारण सम्भव नहीं है क्योंकि जब तक कोई अपकृत्य हो नहीं जाता तब तक उसके पक्षकार एक दूसरे को जानते ही नहीं, और इसके अतिरिक्त अपकृत्य के मामले में पहले से ही हानि की मात्रा की कल्पना करना अत्यन्त कठिन है। अतः अनिर्धारित नुकसानी की स्थित में प्रतिकर के निर्धारण का कार्य न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।
उत्तर- (3) आवश्यकता के कार्य (Act of necessity) आवश्यकता का बचाव दो सिद्धान्तों पर आधारित है। प्रथम यह कि आवश्यकता कोई विधि नहीं जानती तथा दूसरा यदि बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए कोई छोटा अपकृत्य किया गया है तो उससे होने वाली क्षति के लिए बाद नहीं चलाया जा सकता। अर्थात् बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए यदि आवश्यक है तो कोई छोटी क्षति कारित की जा सकती है। आवश्यकता के कार्य तथा आत्मरक्षा में किए गए कार्य में प्रमुख अन्तर यह है कि आवश्यकता के कार्य में क्षति निर्दोष व्यक्ति को भी हो सकती है परन्तु आत्म प्रतिरक्षा में क्षतिग्रस्त पक्षकार दोषी व्यक्ति होता है। आवश्यकता के कार्य तथा अपरिहार्य दुर्घटना में प्रमुख आधार यह है कि आवश्यकता के कार्य में क्षति आशय के साथ होती है जबकि अपरिहार्य दुर्घटना में प्रतिवादी का आशय क्षति कारित करना नहीं है।
जहाज से जहाज के भार को हल्का करने के लिए सामन बाहर फेंकना, आग को आगे फैलने से रोकने के लिए बीच के घर को गिरा देना, किसी डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध पानी से बाहर निकालना, बेहोश व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से बेहोश व्यक्ति की सहमति के बिना आपरेशन करना आवश्यकता के कार्य हैं।
लेग बनाम ग्लैडस्टोन [ (1909) 26 टी० एल० आर० 139.] नामक बाद में भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति की जान बचाने हेतु उसको जबरदस्ती खाना खिलाना आवश्यकता का कार्य करना गया।
कोप बनाम शार्प [ (1891) 1 के० वी० 496.] नामक वाद में संलग्न भूमि पर आग फैलने से रोकने के लिए वादी की भूमि पर प्रतिवादी ने प्रवेश किया। यह प्रतिवादी को अतिचार का उत्तरदायी नहीं बनाता परन्तु चार्टर बनाम थोमस [ (1891) क्यू० बी० 673.] नामक वाद में अग्निशमन दल के आगमन के पश्चात् प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर प्रवेश किया, वह अतिचार (trespass) का दोषी माना गया।
उत्तर – (4) उपभोक्ता (Consumer)– उपभोक्ता की परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (7) में दीगयी है। इसके अनुसार उपभोक्ता ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो –
(1) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया जाता है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है और इसके अन्तर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका प्रदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है। जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है, और
(2) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपभोग करता है और इसके अन्तर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है और वचन दिया गया है और भागत: संदाय किया गया है या भागत: वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपभोग करता है, ऐसी सेवाओं का कोई हितकारी भी है जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है। किन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन से ऐसी सेवाओं का उपयोग करता है।
इस प्रकार कोई व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता हो सकता है –
(1) माल का उपभोक्ता (Consumer of Goods); तथा
(2) सेवाओं का उपभोक्ता (Consumer of Services)
अर्थात् जब कोई व्यक्ति कोई माल खरीदता है जैसे कि पंखा, फ्रिज, गैस का चूल्हा, टी० वी० अथवा कोई अन्य वस्तु तो वह उसका उपभोक्ता हो सकता है। इसी प्रकार जब कोई सेवा या सेवाएँ भाड़े पर लेता है अथवा उसका सेवन करता है, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि मैं यदि बैंक में खाता खोलकर बैंक की सेवायें प्राप्त करूँ या अपना या अपनी सम्पत्ति आदि का बीमा करवाऊँ या किसी वाहक द्वारा अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजूं या किसी वकील या डॉक्टर की सेवायें प्राप्त करूं तो मैं उन सेवाओं का उपभोक्ता कहलाऊँगा। यदि खरीदे गये माल में कुछ खराबी है जैसे कि फ्रिज ठीक से काम नहीं करता या खरीदो गयो घड़ी ठीक से नहीं चल रही है तो यह एक उपभोक्ता विवाद बन सकता है।
अधिनियम की धारा 2 (7) में दी हुई परिभाषा को तीन भागों में बाँट सकते हैं –
(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिफल के लिए किसी माल का क्रय करता है जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत; वचन दिया गया है।
(2) इस धारा के अन्तर्गत उपभोक्ता के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है जो क्रेता की अनुमति से माल का प्रयोग करता है या सेवाओं को प्राप्त करता है यद्यपि वह स्वयं क्रेता या सेवाओं का हिताधिकारी नहीं है।
(3) ऐसे प्रतिफल के लिए सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है।
अपवाद – (1) धारा 2 (i) के अनुसार ‘उपभोक्ता’ के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
आता है जो माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है।
(2) सेवाओं के सन्दर्भ में इसके अन्तर्गत वैयक्तिक सेवा की संविदा के अन्तर्गत कोई निः शुल्क सेवा भी नहीं आती है।
धारा 2 (7) के उपखण्ड (ii) का स्पष्टीकरण का स्पष्ट करता है कि उपखण्ड (i) के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए स्वरोजगार के साधनों द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए माल को क्रय करता है या उन सेवाओं का उपयोग करता है उपभोक्ता में शामिल नहीं है।
उक्त परिभाषा के अनुसार ‘उपभोक्ता’ वह व्यक्ति है जो कोई माल प्रतिफल के लिए क्रय करता है। इस प्रकार इसके अन्तर्गत प्रतिफल के लिए सभी प्रकार के माल का अन्तरण आता है चाहे वह रुपए देकर या वस्तु के बदले में वस्तु देकर या किसी सेवा के लिए किया गया हो। माल विक्रय अधिनियम के अधीन माल का क्रय केवल रुपए के प्रतिफल तक सीमित है और माल के बदले में माल देने के मामले में लागू नहीं होता है। उपभोक्ता अधिनियम के अधीन यह भी अनिवार्य नहीं है कि प्रतिफल तत्काल दिया जाए, प्रतिफल का संदाय तत्काल किया जा सकता है या संदाय का वचन देकर या भागत: संदाय करके और भागत: वचन देकर या किसी आस्गित संदाय पद्धति के अनुसार भी किया जा सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिनियम में उपभोक्ता शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है। प्रथमतः उक्त परिभाषा को संविदात्मक सम्बन्ध (Privity) के विवाद से पृथक रखा गया है।
कौन उपभोक्ता नहीं है? (Who is not consumer?) कभी-कभी प्रथम दृष्टि में कोई व्यक्ति उपभोक्ता या क्रेता लग सकता हो परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता और यदि कोई व्यक्ति स्वयं को उपभोक्ता कहता है तो उसे ही यह साबित करना होता है कि वह उपभोक्ता है या नहीं। उपभोक्ता की विशेषता उसमें स्वयं ही पायी जाती है।
जैसे- श्री लक्ष्मी नारायण राइस मिल्स बनाम एफ० सी० आई० (1996) 1 C.P.J. 161N.C. के मामले में कम्पोटिटिव टेण्डर के माध्यम से चावल को अधिक मात्रा खरीदने वाले को उपभोक्ता नहीं माना गया। इसी प्रकार जहीद हुसैन बनाम शाह एण्ड लोहिया आटो, (1991) C.P.J. 56N.C. के बाद में राष्ट्रीय आयोग ने अपीलकर्ता को उपभोक्ता नहीं माना जिसने एक लारी खरीदा था कि ताकि वह खानों से पत्थर उस स्थान तक ले जाये जहाँ से उन्हें बेचा जाना था। लारी खरीदने का उद्देश्य वाणिज्यिक प्रयोजन माना गया क्योंकि ट्रक ऑपरेट करने के पीछे भाड़ा कमाने की बात छिपी थी।
क्या बस यात्री उपभोक्ता है? – इस सन्दर्भ में प्रभात नलिनी देवी बनाम रश्मि ट्रैवेल्स, (1995) 2. C.P.J. 54 उड़ीसा के मामले में इस बात को लेकर एक विवाद उठा कि यात्री का सामान नष्ट हो जाने पर बस मालिक या कैरियर किस सीमा तक दायित्वाधीन होंगे। इसमें एक महिला का सूटकेस खो गया। पहले तो उसने अपने VIP बैग को अपनी सीट के पास रखा था लेकिन कण्डक्टर के बार-बार कहने पर उसने उसे बस की छत पर रख दिया था। रास्ते में बैग किसी ने चुरा लिया। महिला का दावा था कि उसके बैग में चीजों के अलावा महँगे आभूषण और साड़ियाँ भी थीं और वह एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रही थी। परन्तु फोरम तथा आयोग ने महिला की गिनाई गयी वस्तु के होने से इन्कार कर दिया और अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सामान्यतया एक महिला यात्री जो चीजें व्यक्तिगत रूप से ले जा सकती है, उतने तक के लिए वाहक जिम्मेदार माना जायेगा। ऐसी दशा में उसे 10,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिये जाने का आदेश हुआ। इसे यह स्पष्ट होता है कि बस यात्री भी उपभोक्ता है। जबकि मालापुरम् डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट बस आपरेटर्स असोसिएशन, मैनेजर और अन्य बनाम एम० पी० मोहन और अन्य, ए० आई० आर० 2000 केरल 192, के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बस यात्री उपभोक्ता नहीं है और वे इस अधिनियम का लाभ नहीं ले सकते।
क्या छात्र-छात्राएं उपभोक्ता हैं? – इस सन्दर्भ में अभी तक उच्चतम न्यायालय का कोई विनिश्चय नहीं आया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि छात्र-छात्राएँ उपभोक्ता नहीं है। परन्तु अधिनियम की धारा 2 (42) में जिन सेवाओं पर अधिनियम के प्रावधानों के लागू किये जाने की बात कही जाती है उसके अन्तर्गत शैक्षणिक, तकनीकी या व्यावसायिक सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। वैसे अलग-अलग तो माल व सेवाओं के सन्दर्भ में हर छात्र छात्रा और संस्था उपभोक्ता है। लेकिन क्या उपभोक्ता की परिभाषा इनके ऊपर लागू होती है? यही विचारणीय प्रश्न है –
सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन बनाम एम० सुरेश (1992) | C.P.R. 214, आन्ध्र प्रदेश राज्य आयोग तथा रुचिका भाटिया बनाम सी० वी० एम० ई०, (1995) 2 C.P.J. 969, दिल्ली तथा रजिस्ट्रार इवैलुएशन, कर्नाटक यूनिवर्सिटी बनाम पूर्णिमा भण्डारी, (1992) 2 C.P.R. 27 N.C. के मामलों में राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट शब्दों में परीक्षार्थी/शिक्षार्थी को अधिनियम की परिधि में माना है तथा प्रतिपक्षियों की दलीलों को अमान्य कर दिया है। इस प्रकार ढेरों उदाहरणों से स्पष्ट है कि छात्र-छात्राएँ न केवल उपभोक्ता हैं बल्कि वे बहैसियत उपभोक्ता के अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।
एबेल पाचेको ग्रैसियस बनाम प्रिंसिपल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, (1992) | C.P.J. 105 महाराष्ट्र के निर्णय से यह स्पष्ट है कि छात्रों की शिकायत को दूर करने के लिए जिला फोरम उचित कार्य कर सकता है। इसमें अपीलकर्ता के पुत्र ने प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रतिपक्षी कालेज की इंजीनियरिंग कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ट्यूशन फीस के रूप में 8,250 रुपये तथा छात्रावास शुल्क के बतौर 8,875 रुपये जमा किये। पुनः संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अन्यत्र नाम लिखवाने के उद्देश्य से जमा की गयी राशि के रिफण्ड करने की प्रार्थना किया जिस पर 2,364 रुपये हो वापस किया गया। पूरी राशि न मिलने पर छात्र ने जिला फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया परन्तु वहाँ के आदेश से व्यथित होकर महाराष्ट्र राज्य आयोग के समक्ष संरक्षक ने अपील दाखिल किया जिसे स्वीकार करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्था में विद्यार्थी आवश्यक रूप से उपभोक्ता होता है। यदि शुल्क लिया जाता है तो शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा न करना सेवा में कमी माना जायेगा। छात्र को पूरी स्वतन्त्रता होती है कि वह उचित कारणों से अपना प्रवेश रद्द करा दे। उसे किसी एक संस्था में अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वापसी का सिद्धान्त दैनिक जीवन में एक सिद्धान्त सा बन गया है। अतः इस मामले में छात्र का शिक्षा शुल्क न लौटाना अनुचित, अवैध एक अतार्किक है। इसी आधार पर आयोग ने आदेश दिया कि ट्यूशन फीस की बकाया राशि 5816 रुपये 30 दिनों के भीतर लौटा दिये जायें नहीं तो उसके वसूल करने की तिथि तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। कालेज द्वारा डी० फार्मेसी में नियम विरुद्ध प्रवेश देना अवैध और सेवा में कमी माना जायेगा।
क्या अध्यापक के विरुद्ध छात्र उपभोक्ता है? – इसका उत्तर कलकत्ता के उपभोक्ता फोरम के एक वाद में मिलता है। फोरम में छात्रा के पिता ने स्वयं एवं छात्रा की ओर से इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि स्कूल की अध्यापिका द्वारा लड़की का ट्यूशन न कराये जाने से वह नाराज है। परीक्षा में छात्रा को फेल कर दिया गया है तथा बोर्ड की परीक्षा में उसे बैठने से रोका जा रहा है। परीक्षा में बैठने की सम्भावना न दिखने पर वह उपभोक्ता फोरम की शरण में गया। इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तथ्यों, सुसंगत परिस्थितियों तथा सम्बन्धित कानून पर बड़ी गहराई से विचार किया और उपभोक्ता तथा छात्र के अर्थ को स्पष्ट किया। छात्र का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो अध्ययन करे या अध्यापन के प्रति समर्पण का भाव रखता हो, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यापक व छात्र के बीच ‘कान्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस’ नहीं होता। अध्यापक द्वारा किया जाने वाला विद्यालय का कार्य अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित ‘सेवा’ शब्दों की परिधि में नहीं आता। छात्र द्वारा दी जाने वाली फीस सेवा शुल्क नहीं होती। शिक्षा का अर्थ सामान्य अध्ययन में किसी को प्रशिक्षित करना है। न्यायालय ने अपने निर्णय में और भी स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल विद्यालयों में निर्देशों तक सीमित नहीं है। उसका क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक विकास भी आते हैं इससे स्पष्ट है कि शिक्षक उपभोक्ता नहीं और शिक्षकों के विरुद्ध फोरम में परिवाद सन्धार्य नहीं होगा।
उत्तर- ( 5 ) प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा (Prohibited Trade Practice) [ धारा 2 (41) ] – प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा से तात्पर्य ऐसी व्यापारिक प्रथा से है जिसकी प्रवृत्ति मामलों या सेवाओं से सम्बन्धित बाजार में ऐसी रीति में कीमत की हेराफेरी या परिदान में इसकी शर्तों में परिवर्तन करने वाली हो या आपूर्ति के बहाव को प्रभावित करने वाली हो ताकि उपभोक्ताओं पर उचित कीमतें या प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जा सके और उसमें निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित होंगी –
(क) उस अवधि से अधिक विलम्ब जिस पर ऐसे मालों की आपूर्ति में या सेवाओं को प्रदान करने में व्यापारी द्वारा करार किया गया है जिससे कीमत में वृद्धि हो गई या होने की सम्भावना है;
(ख) ऐसी कोई व्यापार प्रथा जो किसी माल या सेवा को क्रय करने या उपयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में अन्य माल या सेवा कम करने या उपयोग करने की अपेक्षा करती है।
इस परिभाषा के अनुसार ऐसे मामले आयेंगे जहाँ व्यापारी ऐसे माल को बेचता है जो विक्रय लायक नहीं है या जिनकी माँग बाजार में बहुत नहीं है। ऐसे मामलों का निपटारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा।
उदाहरण- एक रसोई चूल्हा विक्रय करने वाला व्यापारी यह पूर्ववर्ती शर्त लगाता है। कि वह गैस कनेक्शन तभी देगा जब क्रेता गैस का चूल्हा भी खरीदेगा।
उत्तर- (6) सेवा पदावली (Term Service) – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का लाभ उठाने के लिए किसी परिवादी को यह साबित करना होगा कि (1) वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (7) के अन्तर्गत परिभाषित उपभोक्ता पदावली को सन्तुष्ट करता है, (2) वह जिसके विरुद्ध शिकायत कर रहा है वह ‘सेवा’ पदावली को सन्तुष्ट करता तथा (3) यह कि विपक्षी द्वारा प्रदान की गई सेवा में कमी या त्रुटि की गई जिसके फलस्वरूप उसे कोई क्षति उठानी पड़ी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (42) में ‘सेवा’ पदावली को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार ‘सेवा’ से तात्पर्य किसी ऐसी सेवा से है जो सम्भावित प्रयोग कर्ताओं को उपलब्ध करायी जाती है तथा सेवा के अन्तर्गत बैंककार्य (Banking), वित्तपोषण (financing), बीमा (insurance). परिवहन (transportation), प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय बोर्ड या विकास, मनोरंजन, गृह निर्माण, आमोद-प्रमोद, समाचार तथा अन्य जानकारी उपलब्ध कराने वाली सुविधा सम्मिलित है।
परन्तु ‘सेवा’ के अन्तर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का किया जाना नहीं है विभिन्न वादों में विभिन्न लोक सेवाओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा माना गया है।
चीफ जनरल मैनेजर महानगर टेलीफोन निगम बनाम वी० एम० नादकर्णी, (1992) सी० पी० जे० 321 राष्ट्रीय आयोग के बाद में दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने के कारण सड़कों के टूट-फूट जाने से क्षति हुई। दूर संचार विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत नहीं करायी गयी थी। राष्ट्रीय आयोग ने निर्णय दिया कि परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता तथा परिवाद निरस्त कर दिया गया।
ए० आर० नारायण बनाम यू० को० बैंक, (1992) सी० पी० जे० 286 राष्ट्रीय आयोग के बाद में भारत सरकार तथा रिवर्ज बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बैंकों को ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें मात्र निर्देशक रेखा (Guide Line) माना गया है। बैंकों को ऋण सुविधा देते समय साख योग्यता, ऋण पुनर्भुगतान को देखना होता है। परिवादी ने बैंक को अपना ऋण नहीं चुकाया था। राष्ट्रीय आयोग ने निर्णय दिया कि बैंक द्वारा परिवादी के ऋण प्राप्त करने हेतु दिये गए आवेदन पत्र को निरस्त कर देना सेवा की कमी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता।
डिविजनल मैनेजर भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम श्री भावनम श्री निवास रेड्डी, (1991) 2 सौ० पी० जे० 144 राष्ट्रीय आयोग के बाद में बीमा कम्पनी के विरुद्ध सेवा में कमी के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय आयोग ने यह निर्णय दिया कि वीमा सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सेवा मानो जाएगी।
मंजू सिंह बनाम म० प्र० विद्युत परिषद, (1992) सी० पी० जे० 73 राष्ट्रीय आयोग के बाद में परिवादों के विरुद्ध विद्युत बिल बकाया था। परिवादी को इस बिल का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया। इस अतिरिक्त समय में भी परिवादी विद्युत बिल जमा नहीं कर सका। इस कारण परिवादी का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। राष्ट्रीय आयोग ने यह निर्णय दिया कि विद्युत परिषद् का यह कार्य उचित था।
प्रश्न 28. संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
Write short notes.
(1) अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice)
(2) सेवा में कमी (Deficiency of Service)
(3) माल में त्रुटि (Defect in Goods)
उत्तर – (1) अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) [ धारा 2 ( 47 ) ] – “अनुचित व्यापार प्रथा” के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा किये गये मामलों का सारभूत तत्व यह है कि यह सिद्ध किया जाना अनिवार्य है कि ऐसे अनुचित व्यापार से उपभोक्ता को क्षति पहुंची है। मात्र अनुचित व्यापार प्रथा का सबूत प्रतिकर प्रदान किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है जब तक कि उससे हुई क्षति को सिद्ध न कर दिया जाय। (जनरल मोटर्स (इण्डिया) प्रा० लि० बनाम अशोक रमणिक लाल (2015) 1 एस० सी० सी० 429]
परिवाद व्यापारी के अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप परिवादी को क्षति या हानि पहुँची हो।
धारा 2 (47) के अनुसार “अनुचित व्यापार प्रथा” से तात्पर्य किसी माल की बिक्री, प्रयोग या आपूर्ति की वृद्धि के लिए अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए निम्न को शामिल करते हुए अपनाया गया कोई अनुचित तरीका या अनुचित धोखाधड़ी, नामत:
मौखिक रूप से या लिखित रूप से या प्रकट अभिवेदन की प्रथा द्वारा जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हों –
(i) यह झूठा प्रतिनिधान (represent) की कोई माल विशिष्ट मानक, गुण, संरचना, किस्म या प्रतिमान का है,
(ii) ऐसा झूठा प्रतिनिधान है कि सेवाएँ विशिष्ट स्तर, गुण या श्रेणी की हैं;
(ili) ऐसा झूठा प्रतिनिधान है कि पुन:निर्मित, पुरानी, नवीकृत, पुन: अनुकूलित वस्तु नयी है;
(iv) यह प्रतिनिधान करता है कि वस्तु अथवा सेवाओं को किसी के द्वारा प्रायोजित, अनुमोदित, निर्मित किया गया है या उसमें विशेष उपकरण, उपयोग या लाभ है जब कि वे ऐसी वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में न हों;
(v) यह प्रतिनिधान करता है कि ऐसी वस्तु या सेवा का कोई प्रयोजन, अनुमोदन या सम्बद्धता प्राप्त है जबकि विक्रेता या प्रदायकर्ता को वह वास्तव में प्राप्त न हो;
(vi) किसी वस्तु या सेवाओं के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकता व उपयोगिता के बाबत गलत या भ्रामक प्रतिनिधान करता है;
(vii) उत्पाद या किसी वस्तु के निष्पादन कार्यक्षमता तथा टिकाऊपन के सम्बन्ध में जनता को ऐसी गारण्टी देना जो कि उसकी पर्याप्त या उचित जाँच पर आधारित नहीं है;
(viii) जन साधारण के समक्ष ऐसे प्रारूप में निरूपण प्रस्तुत करता है जिसका तात्पर्य है- (i) किसी उत्पाद या वस्तु या सेवा की गारण्टी या (ii) वस्तु या उसके भाग (part) को बदलने, अनुरक्षण करने या मरम्मत करने या जब तक कि कोई विशेष परिणाम प्राप्त न हो सेवा की पुनरावृत्ति या जारी रखना; यदि ऐसी वारण्टी या गारण्टी या वायदा सारवान रूप से भ्रमित करने वाला है या उसके क्रियान्वयन के समुचित आधार नहीं हैं;
(ix) जनता को सारवान रूप से मूल्य के बारे में भ्रम पैदा करता है जिस पर उत्पाद या मिलता-जुलता उत्पाद या वस्तुएँ या सेवायें बेची गयी हैं या आमतौर पर विक्रय की जाती है तथा इस उद्देश्य के लिए, मूल्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधान उसको मूल्य संदर्भित करने वाला समझा जायेगा जिस उत्पाद या माल या सेवाओं को संगत बाजार में सामान्यतः विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है या प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह विहित न हो कि किस मूल्य पर उस व्यक्ति द्वारा उत्पाद को विक्रय या सेवाओं का प्रदाय किया गया है, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से प्रतिनिधान किया जाता है:
(x) दूसरे व्यक्ति को वस्तु या सेवा या व्यापार के सम्बन्ध में भ्रामक या मिथ्या तथ्य देता है,
(xi) समाचार पत्र या अन्य किसी रूप में उन वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या प्रदाय को सौदा मूल्य पर देने के लिए, किसी विज्ञापन के प्रकाशन की स्वीकृति देता है जो सौदा मूल्य पर विक्रय या प्रदाय करने के लिए अभिप्रेत नहीं है या उस अवधि के लिए या उस मात्रा में दिया जाना, उस बाजार जिसमें व्यवसाय किया जाता है, के स्वरूप व व्यवसाय के स्वरूप व आकार व विज्ञापन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेत नहीं है;
(xii) जनसाधारण को भेंट, पुरस्कार या अन्य सामग्री देने का प्रस्ताव जबकि अभिप्राय ऐसा करने का नहीं है अथवा निःशुल्क प्रदाय करने का प्रस्ताव जबकि वास्तव में सौदे के अन्तर्गत अंशत: या पूर्णतः उसके मूल्य की वसूली पहले कर ली जाती है;
(xiii) उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए अभिप्रेत है या प्रयोग के लिए सम्भावित वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति की अनुमति यह जानकर या समझकर भी देता है कि निष्पादन, संगठन, अन्तर्वस्तु, डिजाइन, संरचना, परिष्करण (finishing) या पैकिंग के मामले में यह वस्तुएँ;
(xiv) वस्तुओं की जमाखोरी या विनष्टीकरण की अनुमति देता है या वस्तुओं की बिक्री करने में या बिक्री के लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराने से इन्कार करता है, यदि ऐसी जमाखोरी, विनष्टीकरण या इन्कार से उन वस्तुओं या उनसे मिलती-जुलती वस्तुओं या सेवाओं की लागत में वृद्धि हो या वृद्धि की प्रवृत्ति हो।
प्रभारमुक्त उपहारों, पुरस्कारों या अन्य मदों का प्रस्ताव करने वाले किसी योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों से योजना के अन्तिम परिणाम के विषय में सूचना के प्रकट होने पर अपने पास रोक लेना।
जनरल मोटर्स (इण्डिया) प्रा० लि० बनाम अशोक रमणिक लाल, (2015) 1 एस० सी० सी० 429 के मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि प्रतिपक्षी/परिवादकर्ता ने 14,00,000 रुपये में एक कार का क्रय किया था। उसने कार एक विज्ञापन को देखकर खरीदी थी जिसमें कि कार को रोड पर एवं बिना रोड के कच्चे रास्तों पर एवं धूल भरे रास्तों पर भी चलने के अनुकूल (एस० यू० वी०) सुविधायुक्त प्रदर्शित किया गया था किन्तु कार चलाने के बाद परिवादकर्ता ने पाया कि वह कार एक साधारण यात्री कार थी और जैसा कि विज्ञापन में दावा किया गया था वह एस० यू० वी० क्षमता से युक्त नहीं थी और कार में गड़बड़ी थी अपीलार्थी कार कम्पनी के इस कृत्य को “अनुचित व्यापार प्रथा” के अन्तर्गत प्रतिपक्षी कार क्रेता ने वाहन के मूल्य को ब्याज समेत लौटाये जाने व 50,000 रुपये मुआवजे व खर्चा-हर्जा दिलाये जाने हेतु अपीलार्थी कार कम्पनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया। जिलापीठ ने 9% वार्षिक ब्याज की दर से कार मूल्य को लौटाये जाने एवं 5,000 रुपये मानसिक त्रास हेतु व 2,000 रुपये वाद व्यय हेतु परिवादकर्ता को दिये जाने का निर्देश दिया, जिसे राज्य आयोग ने बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया और राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के निष्कर्षों को उचित माना।
(2) सेवा में कमी– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (11) के अनुसार ‘कमी’ से ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाये रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के सम्बन्ध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किये जाने का वचन भंग किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है।
“सेवा” शब्द से तात्पर्य बैंकिंग, फाइनेन्सिग, इन्श्योरेन्स, ट्रान्सपोर्ट, संसाधन, विद्युत आपूर्ति या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, छात्रावास, भोजनालय, चिकित्सा, आवास, गृहनिर्माण, मनोरन्जन व सूचना से सम्बन्धित सेवा प्रदान करना है। किन्तु इसमें शुल्क रहित सेवा या निजी सेवा की संविदा सम्मिलित नहीं है। “सेवा” शब्द का अर्थ अत्यन्त व्यापक है और इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सेवा आ जाती है। अपवाद- अधिनियम में दी गयी परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित सेवाएँ”सेवा” के अन्तर्गत नहीं आयेंगी
(क) शुल्क या प्रभार अथवा मूल्य रहित सेवा
(ख) वैयक्तिक अथवा निजी सेवा की संविदा के अधीन दी गयी सेवा।
चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाम अवतार सिंह, ए० आई० आर० (2011) सुप्रीम कोर्ट 130 के मामले में आवासीय परिषद द्वारा समितियों को उनके सदस्यों के लिये आवास निर्माण हेतु भूमि आवण्टित की गयी थी। इसके लिये सदस्यों से पेशगी की राशि जमा कर ली गयी थी। किन्तु आवास आवण्टन से पूर्व ही सदस्यों ने आवास में अरुचि दिखाते हुए अपना धन वापस किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया। परिषद ने पेशगी की रकम में से 10 से 25% तक की राशि की कटौती करने के पश्चात् ही धन वापस करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि समिति आवास आवण्टन से पूर्व ही अपनी माँग को रद्द कर देती है तो वह बिना कटौती के पूर्ण अग्रिम धन पाने की अधिकारी है। इस प्रकार की कटौती अवैध है और यदि परिषद पूर्ण धनराशि लौटाने में असफल रहता है तो यह सेवा में कमी माना जायेगा।
अपोलो हास्पिटल, विक्रमपुरी बनाम टी० एस० आनन्द कुमार, ए० आई० आर० (2011) (NOC) 155 आन्ध्र प्रदेश के मामले में चिकित्सकों के बीमाकर्ता को परिवाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु “सेवा में कमी” के आधार पर न्यायालय में आवेदन दिया गया था। किन्तु परिवादकर्ताओं की शिकायत बीमाकर्ता के विरुद्ध नहीं थी। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि जब तक कि परिवाद पत्र में बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई वाद कारण न हो, उसे आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।
मेसर्स स्प्रिंग मेदास हास्पिटल बनाम हरजोल अहलूवालिया, ए० आई० आर० (1988) सु० को० 130 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा अत्यन्त व्यापक अर्थों में है अत: उपभोक्ता के अन्तर्गत न केवल सेवा लेने अथवा उसका क्रयकर्ता व्यक्ति आता है बल्कि उसके सभी लाभभोगी व्यक्ति आ जाते हैं। इसलिये चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती हुए बच्चे के साथ-साथ उसके अभिभावक भी उपभोक्ता माने जायेंगे।
हरियाणा अर्बन डेवलपमेन्ट अथारिटी बनाम वीरेश संगवन, (2012) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 256 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पर अतिक्रमण हो गया है तो इसके लिये प्राधिकरण दायी नहीं होगा और यह “सेवा में कमी” नहीं मानी जायेगी।
यदि कोई वकील जो कि किसी मुवक्किल द्वारा पूर्व से ही नियुक्त कर दिया गया है, तस मुवक्किल के विरोधी पक्ष के लिए ऐसा कार्य करता है जो उस पूर्व मुवक्किल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो वह वकील अपने व्यावसायिक दायित्व के प्रति कर्त्तव्य भंग, वचन-भंग व कदाचार का दोषी होगा। एक वकील ने जो क के लिए नियुक्त किया गया। था, के विरोधी पक्ष की ओर से ही क के विरुद्ध उसी सम्पत्ति के लिए वाद दाखिल कर दिया था जिसके लिए क की ओर से उसे नियुक्त किया गया था जिसके लिए वकील को कर्त्तव्य भंग व वचनभंग का दोषी माना गया। [चनु प्रकाश त्यागी बनाम बनारसी, (2015) 8 सु० को० 506]
वड़ोदरा म्युनिसिपल कार्पोरेशन बनाम पुरुषोत्तम वी० मुरुजनी, (2015) 3 सु० को० के० के मामले में बड़ोदरा नगर निगम के प्रबन्धन के अधीन एक सार्वजनिक झील में नौका-विहार के दौरान एक नौका दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 22 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गयी। नौका की क्षमता 20 यात्री की थी जबकि उसमें 38 यात्री थे। नगर-निगम द्वारा नौका-विहार सुविधा की परिचालन व्यवस्था अनुबन्ध के अधीन ठेकेदारों को दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने दुर्घटना हेतु नगर-निगम व अनुबन्धित ठेकेदारों को दायित्वाधीन माना और निर्णय दिया कि नौका यात्री “उपभोक्ता” और नगर निगम के अनुबन्धकर्मी “व्यापारी सेवा प्रबन्धक” के अन्तर्गत माने जायेंगे। नगर निगम और उसके संविदाकर्मी द्वारा की गयी नौका-विहार प्रबन्धन में उपेक्षा, लापरवाही व उचित सावधानी न बरतने का कर्त्तव्य भंग “सेवा में कमी” की परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा।
(3) माल में त्रुटि– धारा 2 (10) के अनुसार ‘त्रुटि’ से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अन्तर्गत या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाये रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी माल के सम्बन्ध में किसी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है, कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है।
सी० एन० अनन्तराम बनाम मेसर्स फियेट इण्डिया लि०, ए० आई० आर० (2011) सु० को० 523 के मामले में याची, जो कि मूलत: वादी था, ने प्रत्यर्थी से एक फियेट सियेना डीजल कार खरीदी थी। वाहन चलाने पर गियर बाक्स व इंजन में शोर सम्बन्धी दोष पाया गया। याची के परिवाद पर वाहन के इंजन सहित अनेक पूजें बदल दिये गये किन्तु याची सन्तुष्ट नहीं हुआ था। उसने जिला फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जो कि स्वीकृत हो गया और फोरम ने याची को वाहन का सम्पूर्ण मूल्य 7,69,187/ रुपये लौटा देने का आदेश दिया। व्यथित होकर प्रत्यर्थी राज्य आयोग जहाँ आयोग ने निर्णय दिया कि याची वाहन में विनिर्माण सम्बन्धी त्रुटि दिखा समक्ष गया पाने में असफल रहा है। अतः वाहन के डीलर व निर्माता को आदेशित किया गया कि यदि वाहन में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करके वाहन पुन: याची को लौटा दिया जाय। इस आदेश के विरुद्ध याची उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि डीजल इंजन के चलने पर कुछ घरघराहट अथवा खड़खड़ाहट होती है जो कि पेट्रोल इंजन में नहीं होती अतः वाहन में कोई विनिर्माण सम्बन्धी त्रुटि नहीं है जैसा कि याची का परिवाद है। गिअर-पेटिका व इंजन से शोर आने के अतिरिक्त परिवाद में अन्य कोई भारी दोष उल्लिखित नहीं है जो कि वाहन को चलाने हेतु अक्षम सिद्ध करता हो अतः राज्य आयोग का आदेश युक्तियुक्त है।
प्रश्न 29. निम्न में अन्तर स्पष्ट करें –
(1) हमला तथा प्रहार,
(2) मानहानि तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजन,
(3) अपलेख तथा अपवचन,
(4) निजी उपताप तथा लोक उपताप,
(5) दैवी कृत्य तथा अवश्यमभावी दुर्घटना,
(6) अतिचार तथा उपताप,
( 7 ) सहमति से क्षति नहीं तथा योगदायी उपेक्षा,
(8) सेवक तथा स्वतन्त्र ठेकेदार।
Distinguish the followings –
(1) Assualt and Battery
(2) Defamation and Malicious Prosecution
(3) Libel and Slander
(4) Private Nuisance and Public Nuisance
(5) Act of God and inevitable accident
(6) Trespass and Nuisance
(7) Volenti non fit Injuria and Contributory Negligence
(8) Servant and Independent Contractor
उत्तर- (1) हमला तथा प्रहार में अन्तर (Distinction between Assault and Bettery)
हमला (Assault) आक्रमण
(1) किसी के मन में प्रहार का युक्तियुक्त भय या आशंका उत्पन्न करना आक्रमण या हमला है
(2) आमतौर पर प्रहार से पूर्व हमला या आक्रमण अवश्य होता है सिवाय उन मामलों में जहाँ प्रहार पीछे से किया जाय या प्रहार सोने की अवस्था (sleeping position) में किया गया हो।
(3) हमले में शरीर स्पर्श आवश्यक तत्व नहीं है।
(4) हमला या आक्रमण को भा० द० सं० की धारा 351 में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रहार (Battery)
(1) किसी के शरीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना किसी विधिक औचित्य के स्पर्श करना प्रहार है
(2) प्रहार, आक्रमण के बाद की प्रक्रिया है। पहले आक्रमण होता है तब प्रहार होता है।
(3) प्रहार में शरीर स्पर्श आवश्यक तत्व होता है।
(4) प्रहार को भा० द० सं० की धारा 350 में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
(2) मानहानि तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजन में अन्तर (Distinction between Defamation and Malicious Prosecution)
मानहानि (Defamation)
(1) मानहानि उस अपलेख का प्रकाशन है जिससे वादी की प्रतिष्ठा को क्षति होती है।
(2) मानहानि के अपकृत्य में वादी को यह साबित करना होता है कि वादी द्वारा अपमानजनक कथन का प्रकाशन किया गया था।
(3) मानहानि या अपमान के वाद में विद्वेष आवश्यक तत्व नहीं है आवश्यक यह है कि कथन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची है।
(4) मानहानि में प्रतिकर का आधार वादी की प्रतिष्ठा होता है।
(5) मानहानि में आर्थिक नुकसान साबित करना आवश्यक नहीं है तथा अपलेख स्वतः अनुयोज्य है।
विद्वेष पूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution)
(1) विद्वेषपूर्ण अभियोजन विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसमें वादी को विद्वेषता के अन्तर्गत अभियोजन कर परेशान करने का आशय होता है।
(2) विद्वेषपूर्ण अभियोजन में सफल होने के लिए वादी को यह साबित करना होता है कि वादी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम अपील के पश्चात् तथा यदि अपील नहीं की गई है तो सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।
(3) विद्वेषपूर्ण अभियोजन में विद्वेषता के अन्तर्गत वादी को परेशान करने के आशय से उसका अभियोजन किया गया था यह साबित करना आवश्यक है।
(4) विद्वेषपूर्ण अभियोजन में प्रतिकर का आधार वादी को हुई आर्थिक क्षति तथा मानसिक एवं शारीरिक परेशानी है।
(5) विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद में नुकसानी (damage) साबित करना आवश्यक है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अपकृत्य स्वतः अनुयोज्य (Actionable per se) नहीं है।
(3) अपवचन तथा अपलेख में अन्तर (Distinction between Slander and Libel)
अपवचन (Slander)
(1) अपवचन मौखिक कंथन है जो वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है ।
(2) अपवचन अस्थायी प्रकृति का होता है।
(3) अपवचन कानों को सम्बोधित होता है।
(4) इंग्लैण्ड में अपवचन अपराध नहीं है परन्तु अपलेख अपराध है।
(5) अपवचन कुछ अपवादित मामलों को छोड़कर स्वतः अनुयोज्य नहीं हैं।
अपलेख (Libel)
(1) अपलेख प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित लिखित कथन है जो वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है।
(2) अपलेख स्थायी प्रकृति का होता है।
(3) अपलेख आँखों को सम्बोधित होता है।
(4) भारत में अपवचन तथा अपलेख दोनों अपराध हैं।
(5) अपलेख सदा स्वतः अनुयोज्य है अर्थात् उसमें सफल होने के लिए नुकसानी (damage) तथा आशय साबित करना आवश्यक है।
(4) निजी उपताप तथा लोक उपताप में अन्तर (Distinction between Private Nuisance and Public Nuisance)
निजी उपताप (Private Nuisance)
(1) निजी उपताप एक अपकृत्य है।
(2) यदि उपतापजनक कार्य से सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति को परेशानी होती है तो यह निजी उपताप है।
(3) निजी उपताप में क्षतिग्रस्त पक्षकार को प्रतिकर प्राप्त होता है।
(4) निजी उपताप में क्षतिग्रस्त पक्षकार वाद ला सकता है।
लोक उपताप (Public Nuisance)
(1) लोक उपताप एक अपराध है।
(2) लोक उपतापजनक कार्य से समाज का वर्ग विशेष प्रभावित होता है।
(3) लोक उपताप के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है
(4) लोक उपताप के लिए राज्य वाद लाता है। लोक उपताप में एक विशिष्ट व्यक्ति तभी वाद ला सकता है जब वह सफलतापूर्वक यह साबित कर दे कि उसे उस लोक उपताप से विशेष तौर पर क्षति हुई है।
(5) दैवी कृत्य तथा अपरिहार्य दुर्घटना में अन्तर (Distinction between Act of God and inevitable accident)
दैवी कृत्य (Act of God)
(1) दैवी कृत्य से तात्पर्य प्राकृतिक तथा दैवी बलों के कारण हुई क्षति से है।
अपरिहार्य दुर्घटना (Inevitable accident)
(1) अपरिहार्य दुर्घटना में मानवीय कारक निहित होते हैं परन्तु ऐसी दुर्घटना वादी की सावधानी तथा सतर्कता के बावजूद निवारित नहीं की जा सकती है।
(6) अतिचार तथा उपताप में अन्तर (Distinction between Trespass and Nuisance)
अतिचार (Trespass)
(1) किसी भी भूमि, भवन या परिसर में बिना किसी विधिक औचित्य के प्रवेश ही अतिचार या अपकृत्य है।
(2) अतिचार प्रत्यक्ष होता है जैसे किसी की भूमि में प्रवेश करना या किसी की भूमि में पौधा लगाना ।
(3) अतिचार स्वतः अनुयोज्य है अर्थात् उसमें सफल होने के लिए नुकसानी, आशय या जानकारी साबित करना आवश्यक नहीं है।
(4) अतिचार एक व्यक्ति के विरुद्ध अपकृत्य है।
(5) अतिचार में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं है।
(6) अतिचार कब्जे के प्रति क्षति है।
(7) अतिचार सदैव मूर्त पदार्थ के माध्यम से होता है।
उपताप (Nuisance)
(1) किसी भी भूमि, भवन या परिसर के उपयोग या उपभोग में अविधिपूर्ण हस्तक्षेप ही उपताप का अपकृत्य है।
(2) उपताप परिणामजनक (consequen tial) होता है। जैसे अपनी भूमि पर पौधा (पेड़) लगाया जाय परन्तु उसकी डाली दूसरे की भूमि पर छाया या कूड़ा उत्पन्न करे।
(3) उपताप के मामले में नुकसानी या क्षति (damage) साबित किया जाना आवश्यक है।
(4) उपताप कुछ परिस्थितियों में अपराध भी हो सकता है।
(5) उपताप निजी या लोक हो सकता है।
(6) उपताप कब्जे के किसी अधिकार के प्रति क्षति है।
(7) उपताप अदृश्य पदार्थ जैसे शोर, कम्पन, दुर्गन्ध या धूम्र के हो सकता है। माध्यम से
(7) सहमति से क्षति नहीं तथा योगदायी उपेक्षा में अन्तर (Distinction between Volenti non fit Injuria and Contributory Negligence)
सहमति से क्षति नहीं (Volunti non fit Injuria)
(1) सहमति से क्षति नहीं पूर्ण बचाव है। प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होता है।
(2) सहमति वादी की सहमति होती है परन्तु वह अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क होता है।
(3) सहमति में वादी तथा प्रतिवादी दोनों स्वयं के खतरों से भिज्ञ (जानकार) रहते हैं।
(4) सहमति में प्रतिवादी की उपेक्षा को बचाव के रूप में समाप्त कर देते हैं।
योगदायी उपेक्षा (Contributory negligence)
(1) योगदायी उपेक्षा में दोनों क्षति के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा प्रतिकर की राशि उनके दोष के अनुपात में समायोजित होती है।
(2) योगदायी उपेक्षा में वादी तथा प्रतिवादी दोनों उपेक्षा के दोषी होते हैं।
(3) योगदायी उपेक्षा में वादी अपने खतरों से अनजान या अनभिज्ञ हो सकता है। यद्यपि उसे उनसे भिन्न होना चाहिए।
(4) योगदायी उपेक्षा में प्रतिवादी की उपेक्षा भी एक प्रमुख कारक होती है।
(8) सेवक तथा स्वतन्त्र ठेकेदार में अन्तर (Distinction between Servant and Independent Contractor)
सेवक (Servant)
(1) सेवक वह है जो पारिश्रमिक या पुरस्कार के लिए नियोजित होता है।
(2) सेवक स्वामी के नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण में काम करता है।
(3) सेवक के कार्यों के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है।
(4) सेवक को यह बताया जाता है कि कार्य कैसे (How) किया जाना है।
स्वतन्त्र ठेकेदार (Independent Contractor)
(1) स्वतन्त्र ठेकेदार वह है जो किसी एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त होता है तथा प्रयोजन पूरा होते ही, उसके तथा स्वामी के मध्य सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं।
(2) स्वतन्त्र ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर स्वामी का प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण नहीं होता।
(3) स्वतन्त्र ठेकेदार के अपकृत्यात्मक कार्यों के लिए आमतौर पर अपवादित परिस्थितियों को छोड़ कर स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा।
(4) स्वतन्त्र ठेकेदार को सिर्फ यही बताना होता है कि क्या (What) कार्य किया जाना है। कार्य कैसे किया जाना है उस पर स्वामी का कोई नियन्त्रण नहीं होता।