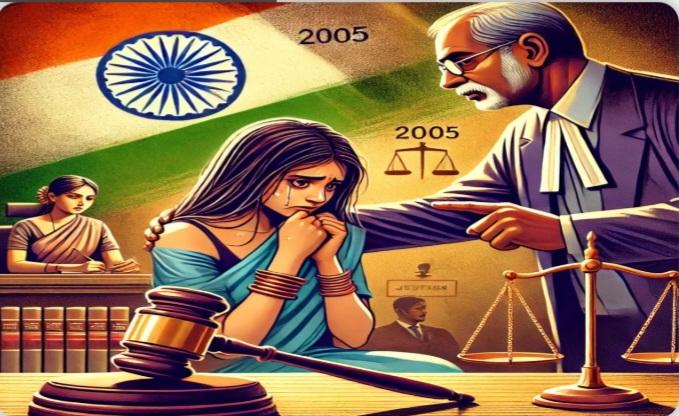घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) : विस्तृत लेख
1. प्रस्तावना
घरेलू हिंसा (Domestic Violence) केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण, आर्थिक नियंत्रण, और भावनात्मक प्रताड़ना भी शामिल होती है। भारत में लंबे समय तक घरेलू हिंसा को “निजी मामला” माना गया और कानून के दायरे में लाने में देरी हुई। महिलाओं के प्रति हिंसा की बढ़ती घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों (विशेषकर CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) में भारत की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप “घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005” पारित किया गया, जो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ।
2. अधिनियम की पृष्ठभूमि
- संवैधानिक आधार – अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान), और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) इस कानून का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।
- पूर्व की स्थिति – पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A में केवल पति या ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता को दंडित किया जाता था, लेकिन यह प्रावधान सीमित था और महिलाओं को तुरंत राहत नहीं देता था।
- CEDAW और संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएँ ने भारत पर यह दबाव डाला कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक व्यापक नागरिक कानून बनाया जाए।
3. अधिनियम का उद्देश्य
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करना।
- शारीरिक, मानसिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण को रोकना।
- पीड़िता को उसके निवास स्थान से बेदखल होने से बचाना।
- अपराधी को पुनर्वास और सुधार की दिशा में लाना।
4. घरेलू हिंसा की परिभाषा
अधिनियम में घरेलू हिंसा को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं –
- शारीरिक उत्पीड़न (Physical Abuse) – मारपीट, चोट, जलाना, हानि पहुँचाना।
- यौन उत्पीड़न (Sexual Abuse) – इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध, अश्लील टिप्पणी, यौन क्रियाओं के लिए मजबूर करना।
- भावनात्मक/मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न (Emotional or Psychological Abuse) – अपमान, धमकी, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, बच्चों से अलग करना।
- आर्थिक उत्पीड़न (Economic Abuse) – धन रोकना, संपत्ति पर रोक, रोजगार करने से रोकना, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति न करना।
5. अधिनियम के लाभार्थी (Aggrieved Person)
- कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में है (पत्नी, बहन, माँ, बेटी, महिला लिव-इन पार्टनर)।
- यह कानून केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो घरेलू संबंध में रहते हुए हिंसा का शिकार हुई हों।
6. प्रतिवादी (Respondent)
- कोई भी वयस्क पुरुष जो पीड़िता के साथ घरेलू संबंध में है।
- 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानून महिलाओं के खिलाफ महिलाओं द्वारा की गई हिंसा पर भी लागू हो सकता है (यदि महिला घरेलू संबंध में प्रभुत्वशाली स्थिति में हो)।
7. अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- निवास का अधिकार (Right to Reside)
- महिला को वैवाहिक घर या साझा घर में रहने का अधिकार है, भले ही वह उसकी मालिक न हो।
- सुरक्षा आदेश (Protection Orders)
- अदालत आरोपी को हिंसा करने, संपर्क करने या पीड़िता के पास आने से रोक सकती है।
- निवास आदेश (Residence Orders)
- आरोपी को पीड़िता को घर से बेदखल करने से रोका जा सकता है।
- आर्थिक राहत (Monetary Relief)
- पीड़िता को चिकित्सा खर्च, भरण-पोषण, आय की क्षति आदि के लिए आर्थिक सहायता।
- अंतरिम और अंतिम आदेश (Interim & Final Orders)
- त्वरित राहत के लिए अदालत अंतरिम आदेश दे सकती है।
- परामर्श और सहायता (Counselling & Assistance)
- पीड़िता को आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
8. संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की भूमिका
- राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करती है।
- उनकी जिम्मेदारियाँ:
- पीड़िता की शिकायत दर्ज करना।
- अदालत में याचिका दायर करना।
- चिकित्सा, आश्रय और कानूनी सहायता की व्यवस्था करना।
- मामले की प्रगति की रिपोर्ट देना।
9. दंड प्रावधान
- संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास और ₹20,000 तक का जुर्माना।
- यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।
10. न्यायालय की प्रक्रिया
- मामला महिला मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में सुना जाता है।
- याचिका पर 3 दिनों के भीतर सुनवाई प्रारंभ और 60 दिनों के भीतर निर्णय का प्रावधान।
11. अधिनियम की सीमाएँ और चुनौतियाँ
- कम जागरूकता – ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाएँ कानून की जानकारी से वंचित।
- कार्यान्वयन की कमजोरी – संरक्षण अधिकारियों की संख्या और संसाधन सीमित।
- समाज में कलंक (Social Stigma) – पीड़िता शिकायत करने से डरती है।
- झूठे मामलों का आरोप – कभी-कभी प्रतिशोध के रूप में शिकायतें दर्ज की जाती हैं।
12. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
- Indra Sarma v. V.K.V. Sarma (2013) – सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशन में महिलाओं को भी संरक्षण का अधिकार दिया।
- Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora (2016) – प्रतिवादी के दायरे का विस्तार किया, अब महिलाएँ भी प्रतिवादी हो सकती हैं।
13. निष्कर्ष
घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 ने महिलाओं को केवल दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक और पुनर्वासात्मक अधिकार प्रदान किए हैं। इसका दायरा व्यापक है और यह महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हालाँकि, इसे प्रभावी बनाने के लिए जन-जागरूकता, शीघ्र न्याय, पीड़ित सहायता तंत्र, और सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है।