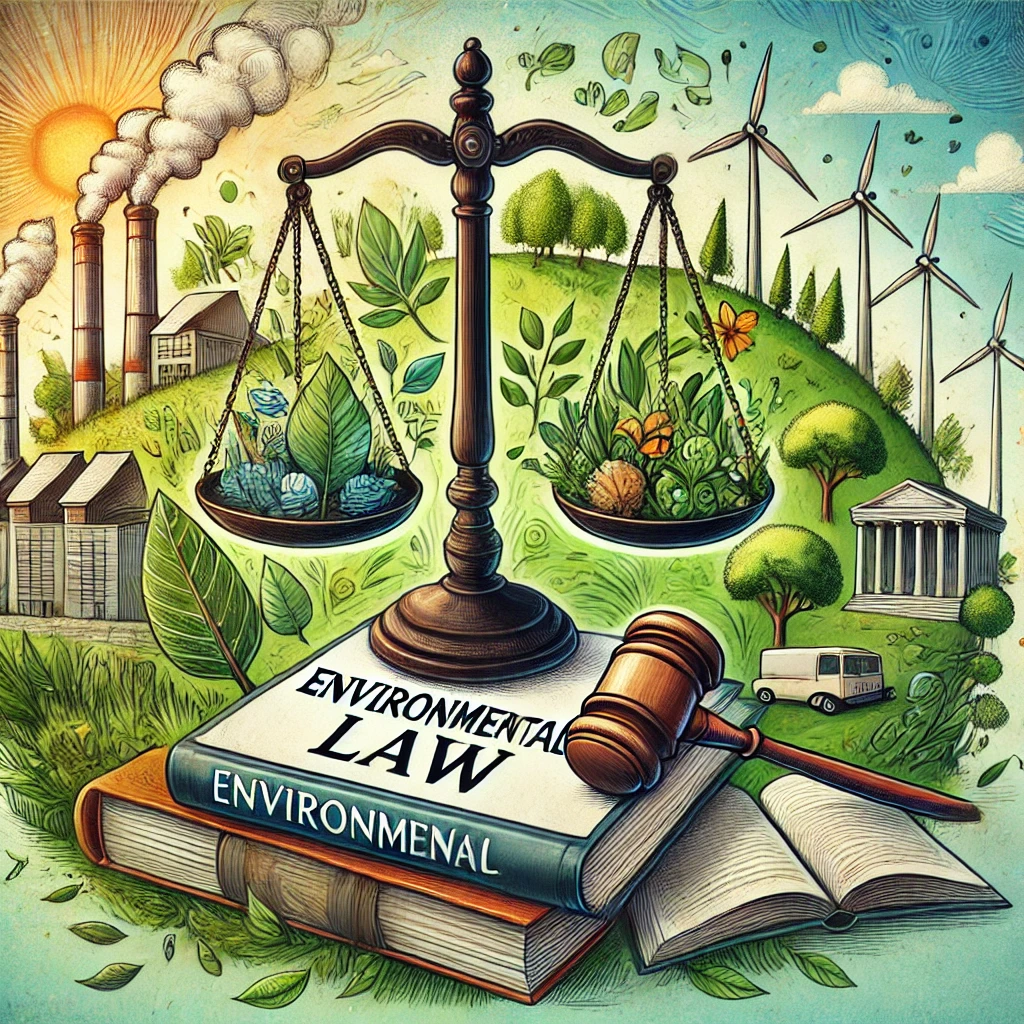पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) : विस्तृत लेख
1. प्रस्तावना
पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि और जैव विविधता केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की अनिवार्यता हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों का क्षय तीव्र गति से बढ़ा, जिससे न केवल पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा बल्कि मानव स्वास्थ्य और जीव-जंतुओं के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हुआ।
भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कानून पहले से थे, जैसे – जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, लेकिन 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के बाद एक व्यापक और समग्र कानून की आवश्यकता महसूस हुई। इसी पृष्ठभूमि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA, 1986) अस्तित्व में आया।
2. अधिनियम की पृष्ठभूमि
- अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ – 1972 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन ने सदस्य देशों को व्यापक पर्यावरण कानून बनाने की अनुशंसा की।
- राष्ट्रीय संदर्भ – भोपाल गैस आपदा (3 दिसंबर 1984) ने भारत में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और रासायनिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून की आवश्यकता को उजागर किया।
- संवैधानिक आधार – संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार का निर्देश और अनुच्छेद 51A(g) में प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य बताया गया है।
3. अधिनियम का उद्देश्य
EPA, 1986 के मुख्य उद्देश्य हैं –
- पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और संरक्षण।
- प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय।
- पर्यावरणीय खतरों से मानव, जीव-जंतु और संपत्ति की सुरक्षा।
- पर्यावरण प्रबंधन के लिए नीतिगत और कानूनी ढांचा प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना।
4. अधिनियम की परिभाषाएँ
- पर्यावरण (Environment) – जल, वायु, भूमि, और इनमें विद्यमान जीव-जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा पारस्परिक संबंध।
- पर्यावरण प्रदूषक (Environmental Pollutant) – कोई भी ठोस, तरल या गैस रूपी पदार्थ जो पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।
- पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution) – किसी भी पर्यावरणीय घटक में हानिकारक प्रदूषकों की उपस्थिति।
5. अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- केंद्रीय सरकार को व्यापक अधिकार –
- पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक तय करना।
- विभिन्न पदार्थों और रासायनिक अपशिष्टों के निष्कासन की सीमा तय करना।
- प्रदूषण स्रोतों की पहचान और नियंत्रण उपाय।
- पर्यावरणीय दुर्घटनाओं की रोकथाम और आपदा प्रबंधन।
- सूचना और निरीक्षण के अधिकार – अधिकृत अधिकारी किसी भी परिसर में प्रवेश कर निरीक्षण कर सकते हैं और नमूने ले सकते हैं।
- निषिद्ध गतिविधियाँ – ऐसे औद्योगिक कार्य, प्रक्रियाएँ या पदार्थों का उपयोग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, रोके जा सकते हैं।
- दंड प्रावधान –
- उल्लंघन पर 5 वर्ष तक कारावास, या ₹1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों।
- लगातार उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना।
6. पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम और अधिसूचनाएँ
EPA, 1986 के तहत केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ जारी कीं, जैसे –
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 – किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन।
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989 – hazardous waste का सुरक्षित निपटान।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 – कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण के दिशा-निर्देश।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2021) – सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध।
- ओजोन परत क्षयकारी पदार्थ नियम, 2000 – CFCs और अन्य हानिकारक गैसों का नियंत्रण।
7. अधिनियम का क्रियान्वयन ढांचा
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) – नीतियां, मानक और निगरानी।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) – राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण और निरीक्षण।
- पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) – राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों का निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन।
8. अधिनियम के अंतर्गत शक्तियाँ
EPA, 1986 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह –
- किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया पर रोक लगा सके।
- मानक तय कर सके और उनका पालन सुनिश्चित कर सके।
- प्रदूषण फैलाने वालों पर आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई कर सके।
- आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई कर सके।
9. अधिनियम के लाभ
- समग्र कानून – जल, वायु, भूमि और जैव विविधता सभी को कवर करता है।
- तेज़ कार्रवाई की शक्ति – आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय।
- औद्योगिक उत्तरदायित्व – उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार बनाता है।
- जन भागीदारी – सार्वजनिक शिकायतों और सुझावों को शामिल करना।
10. अधिनियम की सीमाएँ और चुनौतियाँ
- क्रियान्वयन में कमी – कई बार सख्त प्रावधान होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं होता।
- औद्योगिक दबाव – आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कठिन।
- जन जागरूकता की कमी – ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की जानकारी सीमित।
- निगरानी तंत्र की कमजोरी – प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास पर्याप्त संसाधन और तकनीक नहीं।
11. प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ – सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध कई ऐतिहासिक निर्णय दिए।
- भोपाल गैस पीड़ित संगठन बनाम भारत संघ – पीड़ितों के पुनर्वास और सुरक्षा नियमों को सख्त करने के निर्देश।
12. निष्कर्ष
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत में पर्यावरण सुरक्षा का आधारभूत कानून है। इसने न केवल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सशक्त ढांचा प्रदान किया बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को जिम्मेदार बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन भागीदारी, तकनीकी सुधार, सख्त निगरानी, और राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है।
भविष्य में, यह अधिनियम तभी सार्थक होगा जब विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन साधते हुए हम “सतत विकास” के लक्ष्य को अपनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित हो सके।