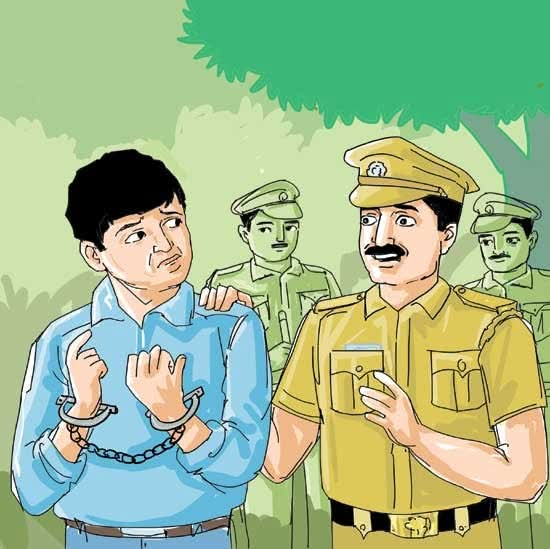बाल अधिकार और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015)
✨ प्रस्तावना:
भारत एक युवा राष्ट्र है, जहां बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। संविधान ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु कई उपबंध प्रदान किए हैं। इसी उद्देश्य को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए “किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015” को पारित किया गया। यह अधिनियम विशेष रूप से उन बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण हेतु बनाया गया है जो या तो अपराध में लिप्त हैं या जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।
📜 अधिनियम का इतिहास और पृष्ठभूमि:
भारत में किशोर न्याय प्रणाली की शुरुआत 1986 में हुई थी। उसके बाद 2000 में “किशोर न्याय अधिनियम, 2000” अस्तित्व में आया। परंतु 2012 के निर्भया कांड के बाद, समाज में यह मांग तेज हुई कि गंभीर अपराधों में संलिप्त 16–18 वर्ष के किशोरों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के चलते Juvenile Justice Act, 2015 अस्तित्व में आया, जिसने पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया।
🎯 अधिनियम के उद्देश्य:
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना।
- अपराध करने वाले बच्चों को सुधार और पुनर्वास की सुविधा देना।
- परित्यक्त, अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों को संरक्षण प्रदान करना।
- न्याय प्रणाली को बालमनोविज्ञान आधारित बनाना।
- बच्चों को पुनः समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।
🏛️ प्रमुख विशेषताएं:
1. परिभाषाएँ (Section 2):
- बालक (Child): 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
- कानून के विरुद्ध बालक (Child in Conflict with Law): ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो।
- संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक: जो अनाथ, परित्यक्त, शोषित, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो।
2. किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board):
- इसमें एक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।
- यह बोर्ड यह निर्धारित करता है कि किशोर अपराधी की सुनवाई किस रूप में होगी—किशोर या वयस्क के रूप में (विशेषतः जघन्य अपराध में)।
3. बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee – CWC):
- प्रत्येक जिले में CWC की स्थापना अनिवार्य है।
- यह समिति परित्यक्त और संकट में पड़े बच्चों के पुनर्वास, देखभाल और संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है।
4. जघन्य अपराधों में प्रावधान:
- यदि 16 से 18 वर्ष का किशोर कोई जघन्य अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक आदि) करता है, तो बोर्ड तय करेगा कि उसकी सुनवाई वयस्क न्यायालय में हो या नहीं।
- यह प्रावधान काफी विवादास्पद रहा, लेकिन इसे न्याय और सुरक्षा के संतुलन के रूप में देखा गया।
5. दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया (Adoption Procedure):
- यह अधिनियम Central Adoption Resource Authority (CARA) को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- अनाथ या परित्यक्त बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
6. सुधारात्मक और पुनर्वास उपाय:
- बच्चों को खुला घर, विशेष गृह, देखरेख गृह आदि में रखा जाता है।
- शिक्षा, प्रशिक्षण, मानसिक सलाह और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।
⚖️ न्यायिक दृष्टिकोण और आलोचना:
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोर अपराधियों को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह परिपक्व नहीं होता।
- कई विशेषज्ञों ने इस अधिनियम की यह कहकर आलोचना की है कि 16–18 वर्ष के किशोरों को वयस्क के रूप में दंडित करना उनके सुधार की संभावना को नष्ट कर सकता है।
🧠 बाल अधिकारों की सुरक्षा:
यह अधिनियम बच्चों के निम्नलिखित अधिकारों की रक्षा करता है:
- जीवन और गरिमा का अधिकार
- शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार
- शोषण से सुरक्षा का अधिकार
- पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण का अधिकार
🌐 अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:
- भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) को स्वीकार किया है, और यह अधिनियम उसी के अनुरूप तैयार किया गया है।
- UNCRC के चार प्रमुख सिद्धांत—गैर-भेदभाव, बाल हित सर्वोपरि, जीवन और विकास का अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—इस अधिनियम में परिलक्षित होते हैं।
✅ निष्कर्ष:
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 भारत में बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और उनके पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम न केवल अपराध करने वाले बच्चों को दंडित करता है, बल्कि उन्हें समाज के उपयोगी नागरिक के रूप में पुनः स्थापित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि इसमें कुछ विवादास्पद प्रावधान हैं, फिर भी यह अधिनियम भारतीय विधि प्रणाली में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।