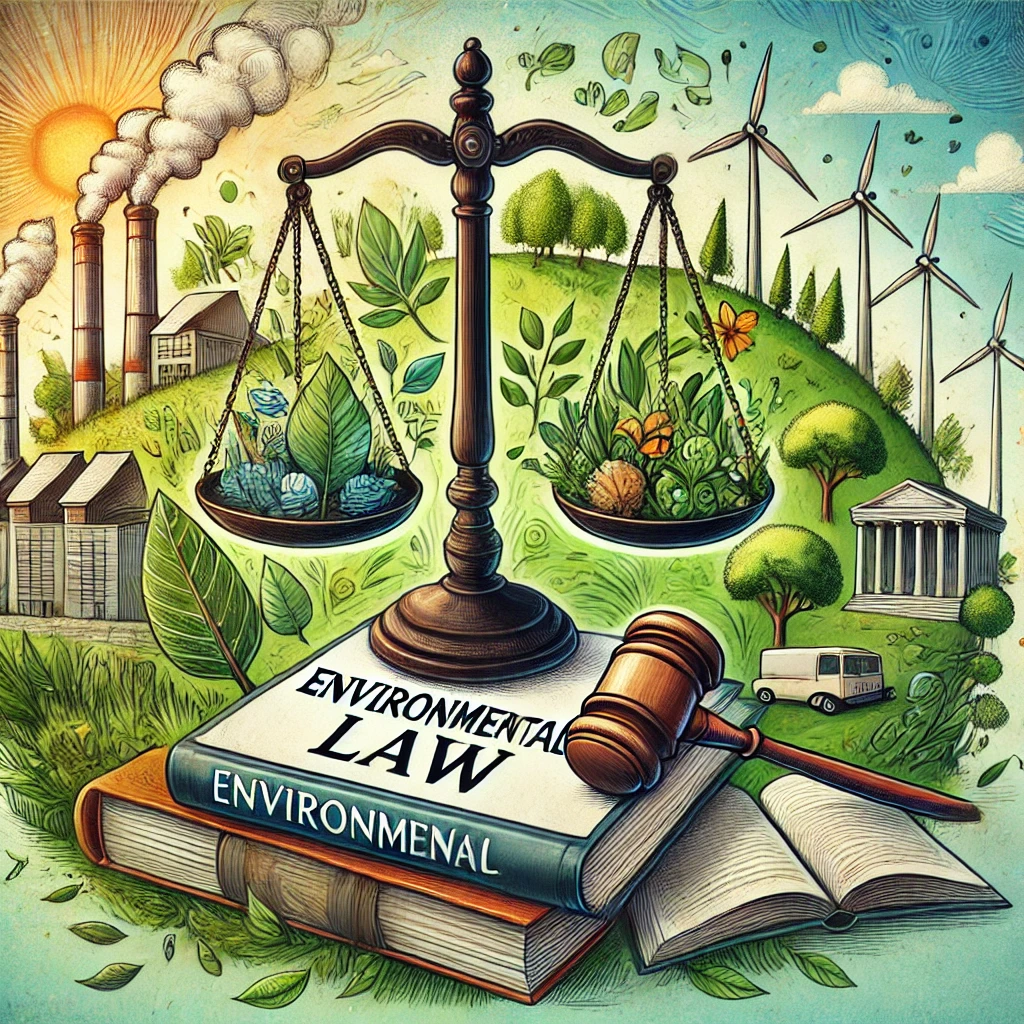The Environment (Protection) Act, 1986: व्यापक अवलोकन
परिचय
The Environment (Protection) Act, 1986, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) के बाद बनाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को मान्यता दी गई। भारत सरकार ने इस अधिनियम को 1986 में पारित किया और इसे “umbrella legislation” कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य पर्यावरण कानूनों के कार्यान्वयन में सहायक है और एक समग्र ढांचा प्रदान करता है।
इस अधिनियम का उद्देश्य न केवल पर्यावरण की रक्षा करना है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानूनी आधार प्रदान करना है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, ताकि विभिन्न प्रदूषणों और पर्यावरणीय खतरों से निपटा जा सके।
प्रमुख विशेषताएँ
- Umbrella Legislation:
यह अधिनियम अन्य पर्यावरण कानूनों जैसे कि The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 और The Wildlife Protection Act, 1972 के कार्यान्वयन में सहायक है। इसका अर्थ यह है कि यह सभी पर्यावरण कानूनों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करने का अवसर प्रदान करता है। - केंद्र सरकार की शक्तियाँ:
अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह निर्देश, नियम और मानक तय कर सकती है, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसमें उद्योगों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर निगरानी रखने की शक्ति शामिल है। - परिभाषाएँ और दायरा:
अधिनियम में पर्यावरण के व्यापक अर्थ को शामिल किया गया है। इसमें वायु, जल, भूमि, और जैविक विविधता शामिल है। यह प्रदूषण के सभी प्रकार—वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण—के नियंत्रण का प्रावधान करता है। - आपातकालीन शक्तियाँ:
किसी भी पर्यावरणीय खतरे या दुर्घटना की स्थिति में, केंद्र सरकार तात्कालिक उपाय कर सकती है। इसमें संपत्ति पर कब्जा, निरीक्षण, आदेश और रोकथाम की शक्तियाँ शामिल हैं।
धारा-वार विवरण
धारा 1: शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार
यह अधिनियम भारत में “The Environment (Protection) Act, 1986” के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत में लागू होता है।
धारा 2: परिभाषाएँ
- “Environment”: जल, वायु, भूमि, और जैविक विविधता।
- “Pollution”: पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश।
- “Hazardous Substance”: वह पदार्थ जो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक हो।
धारा 3: केंद्र सरकार की शक्तियाँ
- केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह निर्देश, नियम और आदेश जारी कर सके।
- यह शक्तियाँ संपत्ति, उद्योग और परियोजनाओं पर लागू होती हैं।
धारा 4: नियम बनाने की शक्ति
- केंद्र सरकार उद्योगों और परियोजनाओं के लिए मानक निर्धारित कर सकती है।
- इसमें प्रदूषण के स्रोत, नियंत्रण तकनीक और निगरानी विधियाँ शामिल हैं।
धारा 5: प्रदूषण नियंत्रण
- अधिनियम प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निर्देश जारी करने की अनुमति देता है।
- इसमें ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण के लिए सीमाएं और उपाय शामिल हैं।
धारा 6: आपातकालीन कार्रवाई
- किसी प्राकृतिक आपदा या प्रदूषण दुर्घटना की स्थिति में तत्काल कदम उठाने की शक्ति।
- इसमें उद्योगों को बंद करना, पर्यावरणीय क्षति रोकना शामिल है।
धारा 7: अनुवर्ती निरीक्षण और निगरानी
- केंद्र सरकार संपत्तियों, उद्योगों और परियोजनाओं का निरीक्षण कर सकती है।
- उल्लंघन की स्थिति में सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा 8: अनुसंधान और शिक्षा
- केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान, अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का अधिकार।
- इससे सामाजिक जागरूकता और विज्ञान आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा मिलता है।
धारा 9: रिपोर्टिंग
- अधिनियम उद्योगों और संस्थाओं को निर्देश देता है कि वे पर्यावरणीय डेटा और रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्र सरकार को दें।
धारा 10: सजा और दंड
- अधिनियम के उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास की सजा दी जा सकती है।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
महत्त्वपूर्ण प्रावधान और नियम
- वायु प्रदूषण नियंत्रण:
- औद्योगिक इकाइयों और परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए मानक निर्धारित।
- एयर क्वालिटी इन्डेक्स (AQI) और वायु गुणवत्ता नियंत्रण बोर्डों का निर्माण।
- जल प्रदूषण नियंत्रण:
- नदियों, तालाबों और जलस्रोतों में औद्योगिक अपशिष्ट का परीक्षण।
- जल शोधन संयंत्रों के संचालन और निगरानी के नियम।
- ध्वनि प्रदूषण:
- शहरी क्षेत्रों, धार्मिक स्थल और औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर के मानक।
- शोर नियंत्रण के लिए सीमा निर्धारित और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना।
- रेडियोधर्मी और hazardous substances:
- रेडियोधर्मी अपशिष्ट और खतरनाक रसायनों के भंडारण और निपटान के लिए विशेष नियम।
महत्त्वपूर्ण कोर्ट के निर्णय
- MC Mehta vs. Union of India: सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू किया।
- Indian Council for Enviro-Legal Action vs. Union of India: केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने और प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के निर्देश।
ये निर्णय अधिनियम के केंद्र सरकार को दी गई शक्तियों और पर्यावरणीय संरक्षण के गंभीर दृष्टिकोण को प्रमाणित करते हैं।
निष्कर्ष
The Environment (Protection) Act, 1986, भारत में पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त कानूनी साधन है। यह अधिनियम केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण, और समाज में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
यह अधिनियम केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ देता है, जिससे कि प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इसके तहत लागू किए गए नियम, दिशा-निर्देश और मानक आधुनिक भारत में पर्यावरण संरक्षण का मूल आधार बन गए हैं।
Umbrella legislation के रूप में, यह अधिनियम अन्य पर्यावरण कानूनों को मजबूती और एकीकृत दृष्टिकोण देता है, जिससे भारत में सतत और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में मजबूत कानूनी ढांचा तैयार होता है।
1. Environment (Protection) Act, 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। यह केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है ताकि वायु, जल, भूमि और जैविक विविधता की सुरक्षा की जा सके। अधिनियम के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने, उद्योगों और परियोजनाओं का निरीक्षण करने, और नियम एवं मानक निर्धारित करने की क्षमता दी गई है। यह अन्य पर्यावरण कानूनों के कार्यान्वयन में सहायक “umbrella legislation” के रूप में कार्य करता है।
2. यह अधिनियम कब और किसके प्रभाव में आया?
The Environment (Protection) Act, 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) के बाद बनाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। भारत सरकार ने इसे 1986 में पारित किया ताकि देश में पर्यावरणीय खतरे और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित किया जा सके।
3. Environment Act को “umbrella legislation” क्यों कहा जाता है?
इस अधिनियम को “umbrella legislation” इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य पर्यावरण कानूनों जैसे कि Water Act 1974, Air Act 1981, और Wildlife Protection Act 1972 के कार्यान्वयन को एकीकृत करता है। यह एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सभी प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं।
4. अधिनियम केंद्र सरकार को किन शक्तियों से लैस करता है?
अधिनियम केंद्र सरकार को उद्योगों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की निगरानी, नियम और मानक तय करने, पर्यावरणीय दिशा-निर्देश जारी करने, और प्रदूषण रोकने के लिए आपातकालीन कार्रवाई करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यह सजा और जुर्माने का प्रावधान भी करता है।
5. Environment Act के तहत आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं?
धारा 6 के तहत, यदि किसी औद्योगिक दुर्घटना या पर्यावरणीय खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार तत्काल कदम उठा सकती है। इसमें उद्योगों को बंद करना, संपत्ति पर कब्जा करना, प्रदूषण को रोकना और प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा शामिल है।
6. अधिनियम में प्रदूषण की परिभाषा क्या है?
प्रदूषण का अर्थ है—“पर्यावरण में हानिकारक या अवांछित पदार्थों का प्रवेश जो स्वास्थ्य, जीव-जंतु और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाता है।” इसमें वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं।
7. यह अधिनियम किन पर्यावरणीय घटकों की रक्षा करता है?
अधिनियम मुख्य रूप से वायु, जल, भूमि और जैविक विविधता की सुरक्षा करता है। इसके तहत औद्योगिक, कृषि और शहरी प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाता है। यह रेडियोधर्मी और hazardous substances के भंडारण एवं निपटान के नियम भी निर्धारित करता है।
8. अधिनियम में अनुसंधान और शिक्षा का क्या प्रावधान है?
धारा 8 के तहत केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान, अध्ययन, प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम चलाने की शक्ति रखती है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्माण और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है।
9. अधिनियम में उल्लंघन करने पर दंड क्या है?
अधिनियम के उल्लंघन करने पर जुर्माना, कारावास या दोनों की सजा दी जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है।
10. इस अधिनियम के महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन-कौन से हैं?
- MC Mehta vs. Union of India: प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू।
- Indian Council for Enviro-Legal Action vs. Union of India: प्रदूषण रोकने और प्रभावित क्षेत्रों के पुनरुद्धार के निर्देश।
ये निर्णय अधिनियम की शक्तियों और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं।
1. The Environment (Protection) Act, 1986 का उद्देश्य क्या है?
A) केवल जल संरक्षण
B) केवल वायु प्रदूषण नियंत्रण
C) सम्पूर्ण पर्यावरण की रक्षा
D) केवल वन्यजीव संरक्षण
Answer: C
2. यह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
A) 1972
B) 1981
C) 1986
D) 1991
Answer: C
3. इस अधिनियम को “umbrella legislation” क्यों कहा जाता है?
A) क्योंकि यह सिर्फ वायु प्रदूषण पर लागू होता है
B) क्योंकि यह अन्य पर्यावरण कानूनों को लागू करने में सहायक है
C) क्योंकि यह केवल केंद्र सरकार के लिए है
D) क्योंकि यह राज्य सरकार को शक्तियाँ देता है
Answer: B
4. Environment Act के तहत केंद्र सरकार को कौन-सी शक्ति नहीं है?
A) नियम और मानक तय करना
B) उद्योगों का निरीक्षण करना
C) आपातकालीन कार्रवाई करना
D) राज्य कानूनों को रद्द करना
Answer: D
5. अधिनियम की धारा 6 क्या संबोधित करती है?
A) अनुसंधान और शिक्षा
B) आपातकालीन कार्रवाई
C) प्रदूषण की परिभाषा
D) सजा और दंड
Answer: B
6. Environment Act के तहत पर्यावरण में “प्रदूषण” की परिभाषा क्या है?
A) केवल जल में हानिकारक पदार्थ
B) केवल वायु में हानिकारक गैसें
C) पर्यावरण में हानिकारक या अवांछित पदार्थ
D) केवल औद्योगिक अपशिष्ट
Answer: C
7. अधिनियम किन पर्यावरणीय घटकों की रक्षा करता है?
A) वायु, जल, भूमि, जैविक विविधता
B) केवल वन्य जीव
C) केवल जल स्रोत
D) केवल औद्योगिक क्षेत्रों
Answer: A
8. अधिनियम के तहत अनुसंधान और शिक्षा किस धारा में निर्दिष्ट है?
A) धारा 4
B) धारा 6
C) धारा 8
D) धारा 10
Answer: C
9. इस अधिनियम के तहत उल्लंघन करने पर क्या दंड हो सकता है?
A) केवल चेतावनी
B) केवल जुर्माना
C) जुर्माना और/या कारावास
D) कोई दंड नहीं
Answer: C
10. अधिनियम के तहत “hazardous substances” का क्या अर्थ है?
A) केवल जहर
B) कोई भी पदार्थ जो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक हो
C) केवल रेडियोधर्मी पदार्थ
D) केवल औद्योगिक अपशिष्ट
Answer: B
11. Environment Act का प्रावधान किस सम्मेलन के प्रभाव में आया?
A) रियो सम्मेलन 1992
B) स्टॉकहोम सम्मेलन 1972
C) क्योटो प्रोटोकॉल 1997
D) पेरिस समझौता 2015
Answer: B
12. अधिनियम केंद्र सरकार को किन उद्योगों पर लागू होता है?
A) केवल सार्वजनिक उद्योग
B) केवल निजी उद्योग
C) सभी सार्वजनिक और निजी उद्योग
D) केवल सरकारी परियोजनाएँ
Answer: C
13. धारा 5 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) अनुसंधान करना
B) प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम
C) सजा देना
D) रिपोर्टिंग
Answer: B
14. केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना है?
A) अनिवार्य
B) वैकल्पिक
C) केवल राज्य सरकारों के लिए
D) केवल निजी संस्थाओं के लिए
Answer: A
15. अधिनियम में जल प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?
A) केवल कानून द्वारा
B) औद्योगिक अपशिष्ट परीक्षण और शोधन संयंत्र
C) केवल शिक्षा द्वारा
D) केवल NGO द्वारा
Answer: B
16. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम किसे जिम्मेदार ठहराता है?
A) केवल उद्योग
B) केवल शहरी निवासी
C) सभी स्रोत: उद्योग, शहरी, धार्मिक
D) केवल सरकार
Answer: C
17. Environment Act में आपातकालीन कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है?
A) राज्य सरकार
B) केंद्र सरकार
C) न्यायपालिका
D) NGO
Answer: B
18. MC Mehta vs. Union of India किस मामले से संबंधित है?
A) वन्यजीव संरक्षण
B) प्रदूषण नियंत्रण उपाय
C) जल अधिकार
D) ध्वनि प्रदूषण
Answer: B
19. Indian Council for Enviro-Legal Action vs. Union of India में क्या निर्देश दिया गया?
A) प्रदूषण रोकने और प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार
B) केवल शिक्षा कार्यक्रम
C) केवल औद्योगिक निरीक्षण
D) केवल वायु गुणवत्ता माप
Answer: A
20. Environment Act का दायरा किस स्तर तक है?
A) केवल राज्य स्तर
B) केवल नगर स्तर
C) पूरे भारत
D) केवल औद्योगिक क्षेत्र
Answer: C