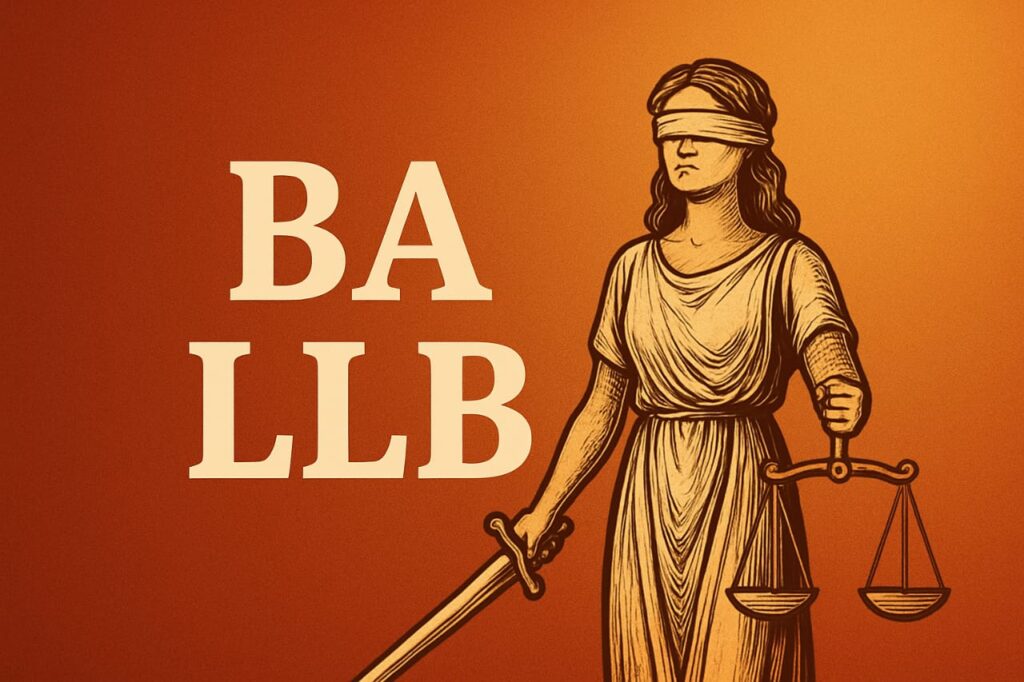भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध : एक विस्तृत अध्ययन
भूमिका
राजनीति विज्ञान (Political Science) का अध्ययन केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संविधान, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे व्यापक विषयों को भी समेटे हुए है। भारतीय संदर्भ में संविधान वह आधारशिला है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है, शासन व्यवस्था वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ और कार्यक्रम लागू होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह क्षेत्र है जिसमें भारत अन्य देशों के साथ कूटनीति, सहयोग और प्रतिस्पर्धा करता है।
इस निबंध में हम इन तीनों पहलुओं का विश्लेषण करेंगे—
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ और महत्व,
- शासन व्यवस्था का स्वरूप और चुनौतियाँ,
- भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उनकी बदलती प्रकृति।
भाग – 1 : भारतीय संविधान
संविधान की परिभाषा और महत्व
संविधान किसी भी राष्ट्र की मूलभूत विधि होती है। यह राज्य की संरचना, शक्तियों के वितरण और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
- लिखित और विस्तृत संविधान – भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ (मूल स्वरूप में) थीं, जो समय-समय पर संशोधनों द्वारा और भी विस्तृत हो गया है।
- संघात्मक ढाँचा (Federal Structure) और एकात्मक प्रवृत्ति (Unitary Bias) – भारत एक संघ है, परंतु यहाँ केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।
- मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, जीवन और शिक्षा जैसे मूल अधिकार देता है।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) – ये सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए राज्य को दिशा देते हैं।
- मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और पर्यावरण की रक्षा करेगा।
- स्वतंत्र न्यायपालिका – संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया है।
- संशोधन प्रक्रिया – संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों का समन्वय है।
संविधान का महत्व
भारतीय संविधान ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया है। यह समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देता है, समानता स्थापित करता है और शासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
भाग – 2 : भारतीय शासन व्यवस्था (Governance System)
शासन व्यवस्था की परिभाषा
शासन व्यवस्था (Governance) का अर्थ केवल सरकार नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नीतियों का निर्माण, उनका कार्यान्वयन और समाज में न्याय व विकास सुनिश्चित किया जाता है।
भारत की शासन व्यवस्था की संरचना
- विधायिका (Legislature) – संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करते हैं।
- कार्यपालिका (Executive) – राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी नीतियों को लागू करते हैं।
- न्यायपालिका (Judiciary) – संविधान की रक्षा और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करती है।
भारतीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ
- लोकतांत्रिक प्रणाली – जनता ही सर्वोच्च है और सरकार जनता की इच्छानुसार चुनी जाती है।
- संसदीय शासन प्रणाली – भारत में ब्रिटिश पद्धति के अनुसार संसदीय शासन है जहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है।
- नागरिक सेवाएँ (Civil Services) – नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- नियंत्रण एवं जवाबदेही – संसद, न्यायपालिका और मीडिया सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं।
शासन व्यवस्था की चुनौतियाँ
- भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी
- प्रशासनिक जटिलता और लालफीताशाही
- सामाजिक असमानता और गरीबी
- राजनीतिक दलों में दलबदल और धनबल का प्रभाव
सुधार के प्रयास
ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता अधिनियम (RTI Act, 2005), पंचायती राज प्रणाली और लोकपाल जैसी संस्थाएँ शासन व्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रयास हैं।
भाग – 3 : भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)
अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा
अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR) राज्यों के बीच कूटनीति, युद्ध, सहयोग, व्यापार और वैश्विक संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन है।
भारत की विदेश नीति के सिद्धांत
- असंपृक्त नीति (Non-Alignment Movement – NAM) – शीत युद्ध के समय भारत ने किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति अपनाई।
- पंचशील सिद्धांत – चीन के साथ 1954 में पंचशील समझौता किया गया जिसमें आपसी सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई।
- विश्व शांति और निरस्त्रीकरण – भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों की होड़ का विरोध किया।
- विकासशील देशों के साथ सहयोग – अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग भारत की विदेश नीति का अंग है।
भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंध
- पड़ोसी देश – पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव, जबकि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ सहयोगात्मक संबंध।
- चीन के साथ संबंध – आर्थिक साझेदारी के बावजूद सीमा विवाद बना हुआ है।
- अमेरिका के साथ संबंध – 21वीं सदी में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) ने नया आयाम लिया है।
- रूस के साथ संबंध – रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में पारंपरिक सहयोग।
- संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन – भारत ने शांति स्थापना बलों में योगदान दिया है और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
भारत की विदेश नीति की चुनौतियाँ
- सीमा विवाद और आतंकवाद
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट
- आर्थिक असमानता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
- तकनीकी और साइबर सुरक्षा खतरे
निष्कर्ष
भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तीनों ही भारतीय राजनीति विज्ञान के केंद्रीय स्तंभ हैं। संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है, शासन व्यवस्था उसका संचालन तंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं।
आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो न केवल अपने नागरिकों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि विश्व शांति, विकास और सहयोग में भी योगदान दे रहा है। इस दृष्टि से भारतीय राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक महत्व भी रखता है।
BA LL.B. Political Science – Constitution, Governance and International Relations
प्रश्न 1 : भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ और महत्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
संविधान किसी भी राष्ट्र का आधारभूत दस्तावेज होता है। यह राज्य की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है।
प्रमुख विशेषताएँ –
- लिखित और विस्तृत संविधान – 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ (मूल स्वरूप में)।
- संघात्मक ढाँचा और एकात्मक प्रवृत्ति – केंद्र को अधिक शक्तियाँ।
- मौलिक अधिकार – समानता, स्वतंत्रता, जीवन, शिक्षा आदि।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व – सामाजिक-आर्थिक न्याय हेतु मार्गदर्शन।
- मौलिक कर्तव्य – एकता, अखंडता और पर्यावरण रक्षा का दायित्व।
- स्वतंत्र न्यायपालिका – संविधान एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा।
- संशोधन प्रक्रिया – कठोर और लचीलेपन का मिश्रण।
महत्व –
भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को मजबूती दी, समाज में समानता और न्याय की नींव रखी, और शासन व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया।
प्रश्न 2 : भारतीय शासन व्यवस्था की संरचना और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
शासन व्यवस्था का अर्थ केवल सरकार से नहीं है, बल्कि नीति-निर्माण, क्रियान्वयन और न्याय-व्यवस्था की संपूर्ण प्रक्रिया से है।
संरचना –
- विधायिका (Legislature) – संसद और राज्य विधानमंडल।
- कार्यपालिका (Executive) – राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी।
- न्यायपालिका (Judiciary) – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान और अधिकारों की रक्षा करते हैं।
विशेषताएँ –
- लोकतांत्रिक प्रणाली
- संसदीय शासन
- सिविल सेवाओं की भूमिका
- नियंत्रण एवं जवाबदेही की व्यवस्था
चुनौतियाँ –
- भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी
- लालफीताशाही और प्रशासनिक जटिलता
- गरीबी और सामाजिक असमानता
- राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव
सुधार के प्रयास –
ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005), पंचायती राज और लोकपाल जैसी संस्थाएँ।
प्रश्न 3 : भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) का अर्थ राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों से है। भारत की विदेश नीति कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है –
- असंपृक्त आंदोलन (NAM) – शीत युद्ध के समय किसी गुट में शामिल न होना।
- पंचशील सिद्धांत (1954) – आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।
- विश्व शांति और निरस्त्रीकरण – परमाणु हथियारों की दौड़ का विरोध।
- विकासशील देशों के साथ सहयोग – एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका – शांति स्थापना और वैश्विक विकास में योगदान।
प्रश्न 4 : भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों, महाशक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध विशेष महत्व रखते हैं।
- पड़ोसी देश –
- पाकिस्तान : सीमा विवाद और आतंकवाद के कारण तनावपूर्ण संबंध।
- बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका : सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग।
- चीन – आर्थिक सहयोग के बावजूद सीमा विवाद और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।
- अमेरिका – 21वीं सदी में रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership)।
- रूस – रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में पारंपरिक सहयोगी।
- संयुक्त राष्ट्र – भारत शांति स्थापना बलों में सक्रिय और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
प्रश्न 5 : भारतीय विदेश नीति के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं?
उत्तर:
भारत की विदेश नीति अनेक वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर रही है –
- सीमा विवाद और आतंकवाद।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक असमानता।
- तकनीकी और साइबर सुरक्षा खतरे।
- ऊर्जा संसाधनों और समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण की होड़।
प्रश्न 6 : संविधान, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आपसी संबंध स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारतीय राजनीति विज्ञान के तीनों स्तंभ—संविधान, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध—एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
- संविधान शासन को वैधता देता है और विदेश नीति निर्माण का आधार तय करता है।
- शासन व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार नीतियों को लागू करती है और विदेश नीति संचालित करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत की आंतरिक नीतियों और लोकतांत्रिक मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करते हैं।
इस प्रकार ये तीनों पहलू मिलकर भारत को एक लोकतांत्रिक, संगठित और वैश्विक शक्ति बनाने का कार्य करते हैं।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव है, शासन व्यवस्था उसका संचालन तंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका तय करते हैं। आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो आंतरिक रूप से सामाजिक-आर्थिक न्याय और बाहरी रूप से विश्व शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।