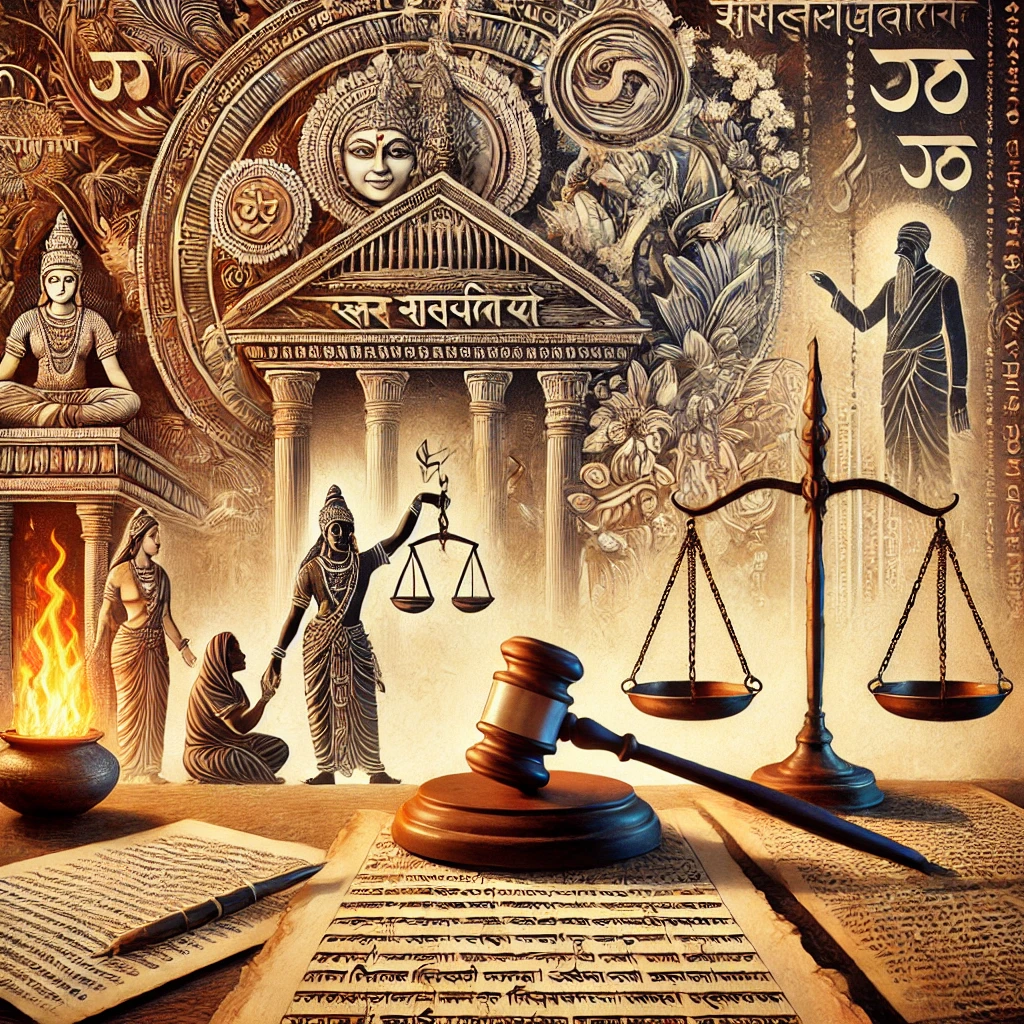हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 – विस्तृत लेख
भूमिका
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) भारत में हिन्दू समुदाय के विवाह संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में कदम उठाया, जिसमें विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना और संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्थाओं को एक समान और न्यायपूर्ण रूप देने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य न केवल विवाह को एक कानूनी मान्यता प्रदान करना था, बल्कि इसे सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण के अनुरूप बनाना भी था।
यह अधिनियम मुख्य रूप से हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है और इसमें समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं, ताकि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुरूप रहे।
लागू क्षेत्र और दायरा
धारा 2 के अनुसार यह अधिनियम लागू होता है:
- हिन्दू धर्म के अनुयायियों पर।
- बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर।
- ऐसे व्यक्ति जो हिन्दू धर्म के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह इसके अनुयायी जन्म से हों या धर्म परिवर्तन द्वारा।
- यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो हिन्दू धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं।
यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है (अब 2019 के बाद यह राज्य भी इसमें सम्मिलित हो चुका है)।
विवाह की आवश्यक शर्तें (धारा 5)
हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह को वैध मानने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:
- एकपत्नी/एकपति प्रथा – विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।
- स्वेच्छा और मानसिक क्षमता – विवाह के समय दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए और वे मानसिक रूप से सक्षम हों।
- विवाह योग्य आयु –
- वर (लड़का) की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
- वधू (लड़की) की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- प्रतिबंधित संबंध में विवाह नहीं – जब तक कि प्रथा या रीति-रिवाज इसकी अनुमति न दें।
- सगोत्र/सपिंडा संबंध में विवाह नहीं – जब तक प्रचलित परंपरा इसकी अनुमति न दे।
विवाह की पंजीकरण व्यवस्था (धारा 8)
हालांकि हिन्दू विवाह में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न विवाह मान्य होते हैं, लेकिन अधिनियम ने विवाह पंजीकरण की भी व्यवस्था दी है।
- पंजीकरण से विवाह का प्रमाण मिल जाता है, जो तलाक, संपत्ति विवाद या अन्य कानूनी मामलों में साक्ष्य के रूप में उपयोगी होता है।
- कई राज्यों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
शून्य और शून्ययोग्य विवाह
हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह को दो श्रेणियों में अमान्य घोषित किया जा सकता है:
- शून्य विवाह (Void Marriages) – प्रारंभ से ही अमान्य विवाह, जैसे:
- पहले से विवाहित व्यक्ति से विवाह।
- प्रतिबंधित संबंध में विवाह।
- सगोत्र/सपिंडा विवाह (जहाँ प्रथा अनुमति न दे)।
- शून्ययोग्य विवाह (Voidable Marriages) – ऐसे विवाह जिन्हें अदालत के आदेश से रद्द किया जा सकता है, जैसे:
- जब विवाह किसी पक्ष की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो।
- जब विवाह के समय मानसिक अस्वस्थता हो।
- जब विवाह के समय पति/पत्नी किसी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हों।
पति-पत्नी के अधिकार और कर्तव्य
अधिनियम के अंतर्गत विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच निम्न अधिकार और कर्तव्य स्थापित होते हैं:
- एक-दूसरे के साथ रहना और वैवाहिक संबंध निभाना।
- एक-दूसरे के प्रति निष्ठा और सहयोग का कर्तव्य।
- भरण-पोषण का अधिकार और दायित्व।
- वैवाहिक संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार।
न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) – धारा 10
यदि पति-पत्नी के बीच संबंध इतने बिगड़ जाएं कि साथ रहना कठिन हो जाए, तो वे न्यायालय से न्यायिक पृथक्करण का आदेश प्राप्त कर सकते हैं।
- यह तलाक नहीं होता, बल्कि अलग रहने की कानूनी अनुमति होती है।
- इसमें विवाह कायम रहता है, परंतु सहवास का दायित्व समाप्त हो जाता है।
भरण-पोषण और गुजारा भत्ता (धारा 24, 25)
- धारा 24 – कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण (Interim Maintenance) की व्यवस्था।
- धारा 25 – स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) का आदेश दिया जा सकता है।
- पति और पत्नी दोनों इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
तलाक के प्रावधान
हिन्दू विवाह अधिनियम ने पहली बार हिन्दू समाज में तलाक की कानूनी व्यवस्था दी।
तलाक के आधार (धारा 13)
- व्यभिचार (Adultery)।
- क्रूरता (Cruelty)।
- परित्याग (Desertion) – कम से कम 2 वर्ष।
- धर्म परिवर्तन।
- मानसिक विकार।
- संक्रामक रोग।
- संन्यास ग्रहण करना।
- मृत्यु का अनुमान – 7 वर्ष से अधिक समय से कोई सूचना न मिलना।
आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce – धारा 13B)
- पति-पत्नी यदि एक वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे हों और विवाह जारी रखना संभव न हो, तो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं।
संशोधन और बदलाव
- 1976 का संशोधन – तलाक के आधारों का विस्तार किया गया और आपसी सहमति से तलाक की व्यवस्था जोड़ी गई।
- 2005 का संशोधन – बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला।
- हालिया संशोधन प्रस्ताव – तलाक के लिए “Cooling-off Period” को कम करने या समाप्त करने का विचार।
महिला सशक्तिकरण में भूमिका
हिन्दू विवाह अधिनियम ने महिला अधिकारों को मजबूत किया है:
- एकपत्नी प्रथा को अनिवार्य बनाया।
- तलाक और भरण-पोषण का अधिकार दिया।
- विवाह के समय और बाद में महिला के समान अधिकार सुनिश्चित किए।
- मानसिक और शारीरिक क्रूरता के खिलाफ कानूनी संरक्षण।
न्यायिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायालयों ने इस अधिनियम की व्याख्या करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जैसे:
- Smt. Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha (1984) – सहवास का पुनःस्थापन वैवाहिक संबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- Naveen Kohli v. Neelu Kohli (2006) – वैवाहिक संबंधों के टूटने पर “Irretrievable Breakdown of Marriage” को तलाक का आधार बनाने की सिफारिश।
निष्कर्ष
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिन्दू विवाह को धार्मिक अनुष्ठान से आगे बढ़ाकर एक कानूनी संस्था का दर्जा दिया है। इसने विवाह संबंधों में समानता, न्याय और आधुनिकता का समावेश किया है। हालांकि, बदलते समय और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप इसमें और सुधार की आवश्यकता बनी हुई है, जैसे तलाक की प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाना, पंजीकरण को पूरी तरह अनिवार्य करना, और लैंगिक समानता को और सुदृढ़ करना।