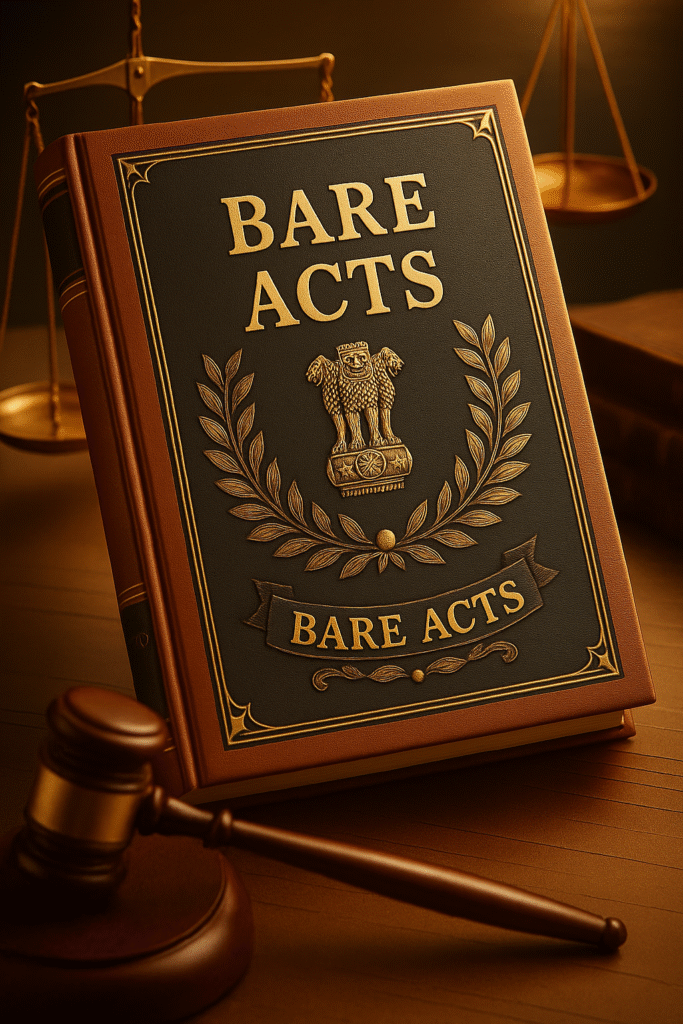सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005)
प्रस्तावना
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल आधार पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) है। यदि नागरिकों को यह पता ही न हो कि सरकार उनके नाम पर क्या नीतियाँ बना रही है और संसाधनों का उपयोग कैसे कर रही है, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में शासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना का अधिकार (Right to Information) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया, जिसने नागरिकों को सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी पाने का कानूनी अधिकार प्रदान किया।
अधिनियम की पृष्ठभूमि
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य – लोकतंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न देशों में सूचना तक पहुँच का अधिकार पहले से मौजूद था। स्वीडन (1766), अमेरिका (1966) और ब्रिटेन (2000) में सूचना का अधिकार कानून के रूप में लागू किया गया।
- भारतीय संदर्भ –
- संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” को सूचना पाने के अधिकार से जोड़ा गया।
- 1990 के दशक में राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने इस अधिकार को जन-आंदोलन का रूप दिया।
- 2002 में केंद्र सरकार ने “सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम” पारित किया, परंतु वह प्रभावी नहीं था।
- अंततः 15 जून 2005 को संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया और यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
अधिनियम का उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य है:
- सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता लाना।
- नागरिकों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- भ्रष्टाचार को कम करना और लोकहित में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना।
- नागरिकों को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर देना।
- लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना।
अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ
- सूचना (Information): किसी भी रूप में उपलब्ध दस्तावेज, रिकॉर्ड, आदेश, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, अनुबंध, रिपोर्ट, ई-मेल, डेटा सामग्री आदि।
- सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority): केंद्र या राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, और सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ।
- लोक सूचना अधिकारी (PIO): प्रत्येक विभाग में नियुक्त अधिकारी जो सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होता है।
- आवेदक (Applicant): कोई भी भारतीय नागरिक जो सूचना माँगता है।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- सूचना पाने का अधिकार – प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना माँगने का अधिकार है।
- समय सीमा –
- सामान्य स्थिति में 30 दिन के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।
- यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे में देना अनिवार्य है।
- लोक सूचना अधिकारी (PIO) – हर विभाग में PIO नियुक्त किया गया है।
- आवेदन शुल्क – मामूली शुल्क लेकर सूचना उपलब्ध कराई जाती है।
- अपील की व्यवस्था – यदि आवेदक को समय पर या संतोषजनक सूचना नहीं मिलती तो वह प्रथम अपील (विभागीय अधिकारी के पास) और द्वितीय अपील (सूचना आयोग के पास) कर सकता है।
- सूचना आयोग –
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) की स्थापना की गई है।
- इन आयोगों के पास सुनवाई, जांच और दंड देने का अधिकार है।
किन सूचनाओं का खुलासा नहीं किया जा सकता
अधिनियम की धारा 8 और 9 में कुछ अपवाद बताए गए हैं, जैसे–
- राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित सूचना।
- विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव डालने वाली सूचना।
- न्यायालय की अवमानना से जुड़ी सूचना।
- व्यापारिक गोपनीयता और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित सूचना।
- संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाली सूचना।
- व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी सूचना, जब तक कि यह लोकहित में न हो।
दंडात्मक प्रावधान
यदि लोक सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता या गलत सूचना देता है तो:
- 250 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 25,000 रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- आयोग अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकता है।
अधिनियम का महत्व
- पारदर्शिता – सरकारी कामकाज जनता के लिए खुला हुआ।
- भ्रष्टाचार में कमी – लोकहित में नीतियों और खर्चों की जानकारी मिलने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
- जनसशक्तिकरण – नागरिक शासन से संबंधित निर्णयों में सक्रिय भागीदारी करने लगे।
- लोकतंत्र की मजबूती – सूचना तक पहुँच से जनता और सरकार के बीच विश्वास मजबूत हुआ।
- प्रशासनिक सुधार – अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया।
अधिनियम की आलोचना
- सूचना न देने की प्रवृत्ति – कई विभाग जानबूझकर सूचना देने में टालमटोल करते हैं।
- दंड का कमजोर प्रवर्तन – दंड प्रावधान होने के बावजूद कई मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती।
- सूचना आयोग की कमजोरी – आयोगों में स्टाफ और संसाधनों की कमी रहती है, जिससे मामलों का निपटारा देर से होता है।
- दुरुपयोग – कभी-कभी लोग व्यक्तिगत या दुर्भावनापूर्ण कारणों से RTI का प्रयोग करते हैं।
- संशोधन विवाद – 2019 के संशोधन द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की कार्यावधि और वेतन केंद्र सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया, जिससे इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठे।
न्यायालयों की भूमिका
भारतीय न्यायपालिका ने RTI को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना।
- राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी पाने का अधिकार है।
- एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) – न्यायालय ने सूचना के अधिकार को लोकतंत्र की नींव बताया।
- अनुराधा भसीन केस (2019) – अदालत ने कहा कि सूचना तक पहुँच लोकतांत्रिक अधिकार है।
निष्कर्ष
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जिसने नागरिकों को सशक्त बनाया और सरकार को अधिक पारदर्शी बनाया। इस अधिनियम ने सामान्य नागरिक को सरकारी नीतियों और खर्चों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देकर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को चुनौती दी है।
हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ हैं। आयोगों की स्वतंत्रता, अधिकारियों की जवाबदेही और नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि इस अधिनियम को सही भावना से लागू किया जाए तो यह शासन को अधिक जिम्मेदार, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बना सकता है।