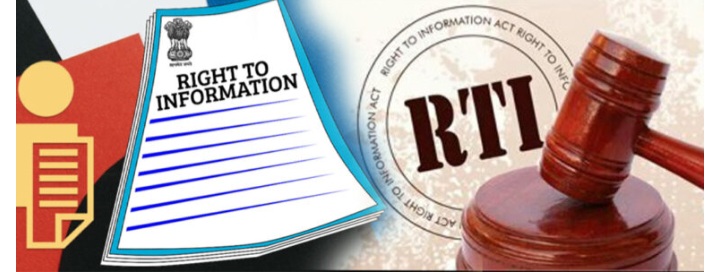सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम
(Right to Information Act, 2005 – A Landmark Legislation for Transparency and Accountability in Governance)
प्रस्तावना
लोकतंत्र में सूचना का अधिकार नागरिकों का सबसे सशक्त हथियार है। यह अधिकार जनता को शासन में सहभागी बनाता है और सरकारी कामकाज पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 – RTI Act) एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जिसने “सरकार के रहस्यों की दीवार” को तोड़कर नागरिकों को सच्ची लोकतांत्रिक शक्ति दी।
इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक यह पूछ सकता है कि —
सरकारी निर्णय कैसे लिए गए?
पैसा कहाँ खर्च हुआ?
कौन अधिकारी जिम्मेदार है?
और क्या जनता के हित में निर्णय लिए गए या नहीं?
इस प्रकार, RTI केवल एक कानून नहीं बल्कि जन-सशक्तिकरण (Empowerment of People) का माध्यम है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
सूचना तक पहुँच का अधिकार किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में यह विचार स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही उभरने लगा था।
महत्वपूर्ण घटनाक्रम:
- 1975 – राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला:
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी गतिविधियों में पारदर्शिता लोकतंत्र की आवश्यकता है।
न्यायालय ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है। - 1982 – S.P. Gupta बनाम भारत संघ (Judge Transfer Case):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा — “जानने का अधिकार (Right to Know) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।” - 1990s – जन आंदोलनों का उदय:
राजस्थान के “मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)” ने गाँव स्तर पर भ्रष्टाचार और फर्जी भुगतान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने “सूचना का अधिकार” को जन आंदोलन बना दिया। - 2002 – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 पारित हुआ, परन्तु इसे लागू नहीं किया गया।
- 2005 – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित हुआ, जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
यह कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) से सूचना प्राप्त कर सके।
उद्देश्य (Objectives of the Act)
RTI Act का मुख्य उद्देश्य है —
- सरकार के कामकाज में पारदर्शिता (Transparency) लाना।
- प्रशासन में जवाबदेही (Accountability) बढ़ाना।
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाना।
- नागरिकों को जानकारी तक पहुँच का अधिकार देना।
- लोकतंत्र को भागीदारी आधारित शासन में बदलना।
“सूचना का अधिकार नागरिक को सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि उसे शासन में भागीदारी का अधिकार देता है।”
सूचना का अधिकार : संवैधानिक आधार (Constitutional Basis)
RTI Act सीधे संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) से व्युत्पन्न है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा —
“जानने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवश्यक घटक है।”
अर्थात, यदि व्यक्ति को जानकारी तक पहुँच नहीं है, तो वह अपनी राय स्वतंत्र रूप से नहीं बना सकता।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Act)
- हर नागरिक को सूचना का अधिकार है।
- सूचना देने की अधिकतम समय सीमा — 30 दिन।
- 24 घंटे में सूचना देनी होगी यदि मामला जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है।
- सूचना के लिए केवल ₹10 शुल्क।
- यदि अधिकारी ने जानकारी देने में देरी की, तो ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का जुर्माना।
- केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग (Information Commissions) की स्थापना।
- लोक प्राधिकरण (Public Authority) की परिभाषा में सभी सरकारी कार्यालय, PSUs, और वे NGOs शामिल हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं।
- कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
‘सूचना’ की परिभाषा (Definition of Information – Section 2(f))
सूचना का अर्थ है —
“किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री – जैसे दस्तावेज, ई-मेल, आदेश, अनुबंध, रिपोर्ट, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, नमूने, डेटा आदि।”
सूचना में वह सामग्री भी शामिल है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संग्रहीत है।
‘लोक प्राधिकरण’ (Public Authority – Section 2(h))
लोक प्राधिकरण में शामिल हैं —
- सरकार (केंद्र या राज्य)
- संसद या विधानमंडल
- न्यायपालिका (सीमित दायरे में)
- स्थानीय निकाय (नगर निगम, पंचायत)
- वे NGOs या संस्थान जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो।
अधिकार प्राप्त व्यक्ति (Right Holders)
भारत का प्रत्येक नागरिक (Citizen of India) इस अधिनियम के तहत सूचना मांग सकता है। विदेशी नागरिक इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते।
सूचना मांगने की प्रक्रिया (Procedure to Obtain Information)
- आवेदन (Application):
- किसी भी Public Information Officer (PIO) को लिखित या ऑनलाइन आवेदन भेजा जा सकता है।
- ₹10 शुल्क जमा किया जाता है।
- समय सीमा:
- सामान्य मामले में 30 दिन।
- अन्य विभागों से सूचना माँगने पर 35 दिन।
- जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे।
- अपील:
- यदि सूचना न मिले या अधूरी मिले, तो पहली अपील (First Appeal) 30 दिन में की जा सकती है।
- दूसरी अपील (Second Appeal) राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के पास की जाती है।
सूचना आयोग (Information Commissions)
दो स्तर पर आयोग बनाए गए हैं —
| स्तर | आयोग का नाम | प्रमुख अधिकारी |
|---|---|---|
| केंद्र स्तर | केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) | मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) |
| राज्य स्तर | राज्य सूचना आयोग (SIC) | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) |
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति:
- राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (केंद्र के लिए)।
- राज्यपाल द्वारा की जाती है (राज्य के लिए)।
कार्यकाल:
पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक था, परंतु 2019 संशोधन अधिनियम ने इसे केंद्र सरकार द्वारा तय की जाने वाली अवधि बना दिया है।
अपवाद (Exemptions – Section 8 & 9)
कुछ सूचनाएँ सार्वजनिक हित में नहीं दी जा सकतीं।
Section 8 के अंतर्गत अपवाद:
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति से जुड़ी सूचना।
- विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना।
- न्यायालय में लंबित मामलों से जुड़ी सूचना।
- किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी (यदि सार्वजनिक हित न हो)।
- जांच या अभियोजन को प्रभावित करने वाली सूचना।
- व्यापारिक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से जुड़ी जानकारी।
परंतु यदि जनहित (Public Interest) ज्यादा है, तो ऐसी सूचना भी दी जा सकती है।
दंड का प्रावधान (Penalty Provisions – Section 20)
यदि कोई PIO –
- सूचना देने में असफल रहता है,
- जानबूझकर गलत जानकारी देता है, या
- समय पर उत्तर नहीं देता,
तो उसे निम्न दंड दिया जा सकता है:
- ₹250 प्रति दिन का जुर्माना (अधिकतम ₹25,000)।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही।
महत्वपूर्ण संशोधन (RTI Amendment Act, 2019)
2019 में RTI अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत —
- मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा।
- उनका वेतन और भत्ता भी सरकार तय करेगी।
- इससे पहले इनका दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त के समान था।
इस संशोधन की आलोचना यह कहकर की गई कि इससे सूचना आयोग की स्वतंत्रता कम हो सकती है।
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Important Case Laws)
- Raj Narain v. State of U.P. (1975):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा — “लोकतंत्र में जनता को जानने का अधिकार है।” - S.P. Gupta v. Union of India (1982):
कोर्ट ने कहा — “जानने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।” - People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India (2004):
कोर्ट ने माना कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की जानकारी जानने का अधिकार है। - CBSE v. Aditya Bandopadhyay (2011):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा कॉपियाँ भी RTI के तहत मांगी जा सकती हैं। - Girish Ramchandra Deshpande v. CIC (2013):
कोर्ट ने कहा — “व्यक्तिगत सूचना को तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक जनहित स्पष्ट न हो।”
सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता का अधिकार (RTI vs Right to Privacy)
गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy), Puttaswamy v. Union of India (2017) में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया।
RTI और गोपनीयता के बीच संतुलन आवश्यक है —
“जहाँ जनहित प्रमुख है, वहाँ गोपनीयता सीमित होगी;
जहाँ व्यक्तिगत हित प्रमुख है, वहाँ गोपनीयता को प्राथमिकता मिलेगी।”
RTI का सामाजिक प्रभाव (Impact of RTI Act)
- भ्रष्टाचार में कमी: कई विभागों में पारदर्शिता बढ़ी।
- जन-जागरूकता में वृद्धि: ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जानकारी मांगने लगे।
- शासन में जवाबदेही: अधिकारी अब निर्णयों को रिकॉर्ड पर लाने लगे।
- सिविल सोसाइटी की सशक्त भूमिका: NGOs और कार्यकर्ता नीतिगत बदलाव लाने में सक्षम हुए।
- मीडिया की मजबूती: पत्रकारों को सूचना के लिए आधिकारिक स्रोत मिला।
सीमाएँ और चुनौतियाँ (Limitations and Challenges)
- सूचना अधिकारियों की कमी और प्रशिक्षण की समस्या।
- देरी से सूचना उपलब्ध होना।
- राजनीतिक हस्तक्षेप।
- आवेदकों को धमकियाँ या हिंसा का खतरा।
- कई विभाग RTI के अपवाद का दुरुपयोग करते हैं।
- 2019 संशोधन के बाद आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न।
सुधार हेतु सुझाव (Suggestions for Improvement)
- सूचना आयोगों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
- सभी सरकारी विभागों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो।
- RTI आवेदकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- अधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व और प्रशिक्षण बढ़ाया जाए।
- Proactive Disclosure यानी सरकार स्वयं सूचना सार्वजनिक करे।
निष्कर्ष (Conclusion)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने वाला कानून है। इसने आम नागरिक को यह शक्ति दी कि वह सरकार से सवाल पूछ सके, जवाब मांग सके और जवाबदेही तय कर सके।
“लोकतंत्र में सच्ची शक्ति बैलेट बॉक्स में नहीं, बल्कि जानकारी तक पहुँच में निहित होती है।”
हालांकि इस कानून के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसकी आत्मा अब भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में गहराई से बस चुकी है। RTI ने शासन को “राज्य के रहस्यों के शासन” से “जनता के पारदर्शी शासन” की दिशा में अग्रसर किया है।
“सूचना का अधिकार — जनता की आँखें और लोकतंत्र की आत्मा है।”
– न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर