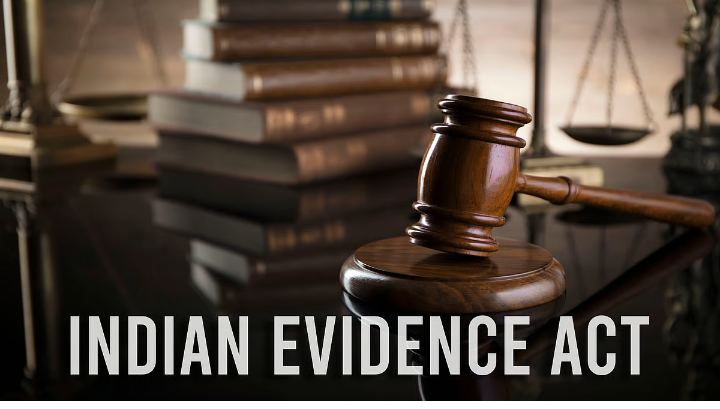न्यायालय में प्रतिपरीक्षण (Cross-Examination) की मर्यादा और शक्ति: साक्ष्य अधिनियम, 2011 की धारा 226 का विश्लेषण
परिचय:
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2011 (Evidence Act, 2011) के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिपरीक्षण (Cross-Examination) एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रतिपक्ष वकील गवाह की विश्वसनीयता, साक्ष्य की सच्चाई और कथन की दृढ़ता को परखता है। परंतु, इस प्रक्रिया का उपयोग केवल सत्य की खोज के लिए किया जाना चाहिए, न कि प्रताड़ना या अनुचित लाभ के लिए। इस संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 226 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अधिवक्ता अपनी सीमा से बाहर जाकर या बिना युक्तिसंगत कारण के प्रश्न न पूछे।
धारा 226 साक्ष्य अधिनियम, 2011 का सार:
धारा 226 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई अधिवक्ता प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछता है जो न केवल असंगत हैं, बल्कि जिनके पीछे कोई उचित कारण नहीं है, तो न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उस अधिवक्ता की रिपोर्ट महान्यायवादी (Attorney-General of the Federation) या संबंधित प्राधिकरण को भेज सके।
यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे और अदालत में अनुशासन एवं मर्यादा का पालन किया जाए।
प्रतिपरीक्षण का उद्देश्य:
प्रतिपरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी गवाह के बयान की सच्चाई का परीक्षण करना होता है। इसके द्वारा यह देखा जाता है कि:
- गवाह का कथन विरोधाभासी है या नहीं।
- उसके पास दी गई जानकारी प्रत्यक्ष है या सुनी-सुनाई (hearsay) है।
- गवाह किसी पक्ष विशेष से प्रभावित तो नहीं।
- क्या उसका कथन तर्कसंगत और विश्वसनीय है।
प्रतिपरीक्षण न्याय की खोज का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। यह न्यायालय को यह समझने में सहायता करता है कि कौन-सी गवाही सच्चाई के निकट है और कौन-सी मात्र कल्पना या झूठ पर आधारित।
प्रतिपरीक्षण की सीमाएं और न्यायाधीश की भूमिका:
न्यायाधीश का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया की निगरानी करे ताकि कोई भी प्रश्न अशोभनीय, अपमानजनक या असंगत न पूछा जाए। यदि कोई अधिवक्ता बिना उचित कारण के व्यक्तिगत, अशिष्ट या असंगत प्रश्न पूछता है, तो न्यायाधीश उसे रोक सकता है।
साथ ही, धारा 226 यह भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों में न्यायाधीश निष्क्रिय न रहे — वह उस अधिवक्ता की रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकरण को भेज सकता है ताकि भविष्य में ऐसे आचरण पर रोक लग सके।
प्रतिपरीक्षण का नैतिक और विधिक पक्ष:
वकालत केवल तर्क की कला नहीं, बल्कि एक नैतिक पेशा भी है। अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे न्याय की खोज में सहायता करें, न कि उसे भटकाएं।
यदि कोई अधिवक्ता प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उद्देश्य गवाह को अपमानित करना या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करना है, तो यह पेशेवर आचरण (Professional Misconduct) की श्रेणी में आता है।
अतः अधिवक्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि:
- हर प्रश्न का एक युक्तिसंगत आधार हो।
- प्रश्न मामले के तथ्यों से संबंधित हो।
- किसी गवाह की निजी गरिमा का उल्लंघन न हो।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की दृष्टि:
भारतीय न्यायपालिका ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि प्रतिपरीक्षण की स्वतंत्रता असीमित नहीं है।
State of Punjab v. Gurmit Singh (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि “प्रतिपरीक्षण का उद्देश्य सत्य की खोज है, न कि गवाह की गरिमा को ठेस पहुँचाना।”
इसी प्रकार Zahira Habibullah Sheikh v. State of Gujarat (2004) में कहा गया कि “यदि प्रतिपरीक्षण का उपयोग भय, दबाव या बदनामी के हथियार के रूप में किया जाए, तो यह न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।”
“When there is no need to ask questions in cross-examination, don’t ask” – इस टिप का अर्थ:
यह वाक्य न्यायिक अभ्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार अधिवक्ता प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यधिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे गवाह का बयान स्पष्ट होने के बजाय उलझ जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, एक सक्षम वकील वही प्रश्न पूछता है जो आवश्यक हों, और जो उसके मुकदमे की दिशा तय कर सकें।
अनावश्यक प्रश्न पूछना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि गवाह को सताने या अदालत के धैर्य की परीक्षा लेने जैसा भी हो सकता है।
प्रतिपरीक्षण एक “दो-धारी तलवार”:
प्रतिपरीक्षण को अक्सर “a double-edged sword” कहा जाता है — अर्थात यह न्याय की खोज में मदद भी कर सकता है और दुरुपयोग होने पर न्याय में बाधा भी बन सकता है।
यदि अधिवक्ता इस प्रक्रिया का उपयोग गवाह की झूठी गवाही को उजागर करने में करते हैं, तो यह न्याय के लिए लाभकारी है।
लेकिन यदि इसका प्रयोग मात्र अपमानजनक या भ्रामक प्रश्नों के लिए किया जाए, तो यह न्याय के मार्ग में रुकावट है।
न्यायालय की सुरक्षा-व्यवस्था और अधिवक्ता की जिम्मेदारी:
अदालत एक गरिमामय स्थान है। यहाँ हर व्यक्ति—चाहे वह अभियुक्त हो, गवाह हो या अधिवक्ता—को मर्यादा का पालन करना आवश्यक है।
साक्ष्य अधिनियम की धारा 226 इस गरिमा को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। यह न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह अनुचित व्यवहार करने वाले अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकरण को सूचित करे।
इस प्रकार, यह प्रावधान न केवल न्यायिक अनुशासन को सुदृढ़ करता है, बल्कि अधिवक्ताओं के लिए एक चेतावनी भी है कि वे अपने पेशे की प्रतिष्ठा बनाए रखें।
व्यावहारिक उदाहरण:
मान लीजिए किसी आपराधिक मुकदमे में एक महिला गवाह है, और प्रतिपक्ष के वकील उससे ऐसे व्यक्तिगत या अपमानजनक प्रश्न पूछते हैं जिनका मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।
ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उन प्रश्नों को रोक दे, और यदि अधिवक्ता बार-बार ऐसा करता है, तो उसके विरुद्ध रिपोर्ट तैयार करके उसे Bar Council या Attorney-General के पास भेज दे।
न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा का संरक्षण:
धारा 226 का असली उद्देश्य यही है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का अनावश्यक तनाव, अपमान या अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
वकील का कार्य न्यायालय की सहायता करना है, न कि उसे नियंत्रित करना। इसलिए उसे अपने प्रश्नों में संयम और विवेक का परिचय देना चाहिए।
निष्कर्ष:
प्रतिपरीक्षण न्याय की नींव में रखी गई एक महत्वपूर्ण ईंट है। यह गवाह के कथनों की सच्चाई को परखने और वास्तविक तथ्यों को सामने लाने का सशक्त उपकरण है। परंतु, यह उपकरण तभी प्रभावी होता है जब उसका प्रयोग जिम्मेदारी और संयम के साथ किया जाए।
साक्ष्य अधिनियम, 2011 की धारा 226 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अधिवक्ता इस शक्ति का दुरुपयोग न करे।
इसलिए, जब प्रतिपरीक्षण में कोई आवश्यक प्रश्न न हो, तब प्रश्न पूछना अनावश्यक और जोखिमपूर्ण हो सकता है।
एक सच्चा अधिवक्ता वही होता है जो न्यायालय की मर्यादा बनाए रखते हुए अपने मुवक्किल के हित में युक्तिसंगत प्रश्न पूछे — क्योंकि अंततः न्याय का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना करना है।
अंतिम टिप्पणी:
धारा 226 एक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों का कार्य करती है। यह हमें यह सिखाती है कि वकालत केवल कानून का ज्ञान नहीं, बल्कि न्याय, नैतिकता और सम्मान का संतुलन है।
अतः प्रत्येक अधिवक्ता को यह याद रखना चाहिए कि —
“प्रतिपरीक्षण की शक्ति न्याय की सेवा में है, न कि उसके दुरुपयोग में।”