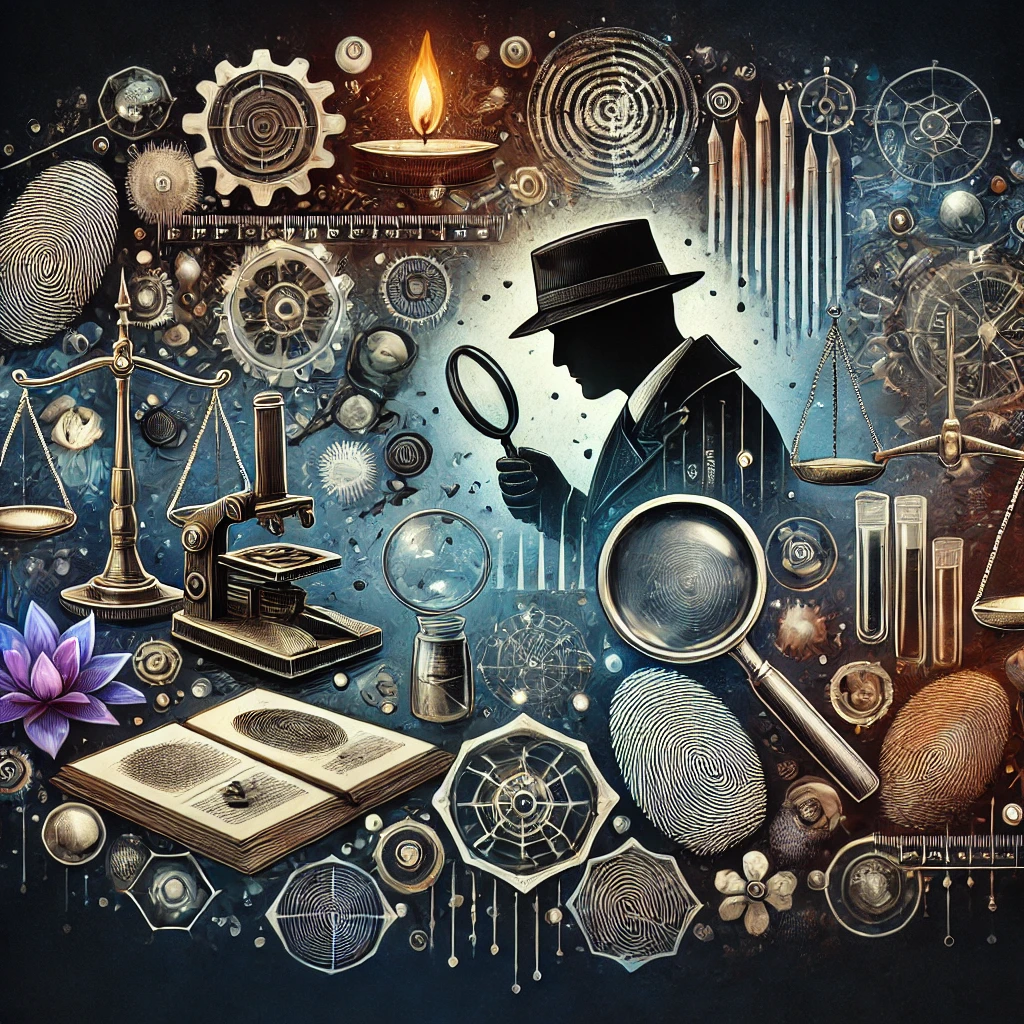शीर्षक: साइबर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून: डिजिटल युग में भारत की विधिक और सुरक्षा चुनौतियाँ
भूमिका:
इक्कीसवीं सदी में जैसे-जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, वैसे-वैसे सुरक्षा के समक्ष नए प्रकार की चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism) ऐसी ही एक आधुनिक चुनौती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है। भारत में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए विभिन्न विधिक प्रावधान, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय दंड संहिता, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) प्रभावी हैं।
1. साइबर आतंकवाद की परिभाषा:
साइबर आतंकवाद वह आपराधिक गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण संरचनाओं या नागरिक जीवन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है।
उदाहरण:
- सरकारी वेबसाइटों या रक्षा नेटवर्क पर हैकिंग
- बैंकिंग सिस्टम या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को बाधित करना
- सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और आतंक फैलाना
- वायरस, मैलवेयर या स्पाइवेयर के माध्यम से संवेदनशील डेटा चुराना
2. भारत में साइबर आतंकवाद के विरुद्ध लागू प्रमुख कानून:
(क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):
- धारा 66F – साइबर आतंकवाद से संबंधित विशेष प्रावधान
- यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, तो अजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
(ख) भारतीय दंड संहिता (IPC):
- धारा 121 से 124A – देशद्रोह, युद्ध छेड़ने, और असंतोष भड़काने से संबंधित
- साइबर माध्यम से किए गए कृत्य यदि इन प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं तो दंडनीय हैं।
(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act, 1980):
- केंद्र और राज्य सरकारों को संदेहास्पद व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति
- साइबर माध्यम से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर लागू हो सकता है।
(घ) यूएपीए अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act):
- आतंकवादी गतिविधियों में शामिल वेबसाइट, संगठन, या व्यक्ति पर प्रतिबंध
- साइबर माध्यम से आतंक फैलाने वाले ग्रुप्स पर कार्रवाई
3. साइबर आतंकवाद के प्रकार:
- DDoS (Distributed Denial of Service) हमले
- क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैकिंग (जैसे पावर ग्रिड, रेलवे नेटवर्क)
- डेटा लीक और साइबर जासूसी
- फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग द्वारा सैन्य या वैज्ञानिक जानकारी चुराना
- डार्क वेब पर आतंकवादी संचार और फंडिंग
4. भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था:
- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)
- डिफेंस साइबर एजेंसी (DCA)
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013)
- साइबर क्राइम सेल्स और NIA द्वारा जांच एवं निष्पादन
5. साइबर आतंकवाद से जुड़ी प्रमुख घटनाएँ:
- 2008 मुंबई हमलों से पूर्व आतंकी ईमेल भेजे गए
- पाकिस्तान स्थित हैकर्स द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट्स हैक करने के प्रयास
- चीन से जुड़े APT ग्रुप्स द्वारा साइबर जासूसी
- बिजली ग्रिड पर साइबर हमला (माना गया 2020 में मुंबई ब्लैकआउट)
6. चुनौतियाँ और जटिलताएँ:
- तकनीकी साक्ष्य एकत्र करना कठिन
- अज्ञात स्रोतों से हमलों की पहचान करना मुश्किल
- क्रॉस-बॉर्डर साइबर अपराधों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी
- साइबर कानूनों की सीमित जागरूकता और क्रियान्वयन
- डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन
7. सुधार के सुझाव और भविष्य की रणनीति:
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2024 को सशक्त बनाना
- साइबर अपराध के लिए विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना
- साइबर फोरेंसिक लैब्स और प्रशिक्षण संस्थान का विकास
- 5G और AI आधारित साइबर सुरक्षा तंत्र
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डेटा-शेयरिंग समझौते
- शिक्षण संस्थानों में साइबर शिक्षा अनिवार्य करना
निष्कर्ष:
साइबर आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित खतरों में से एक बन चुका है। भारत ने विधिक और तकनीकी स्तर पर इस खतरे से निपटने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, किंतु एक समन्वित, आधुनिक और सक्रिय रणनीति ही इस डिजिटल युद्ध में जीत सुनिश्चित कर सकती है। भविष्य की सुरक्षा अब केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि स्क्रीन और सर्वरों के पीछे भी तय होगी।