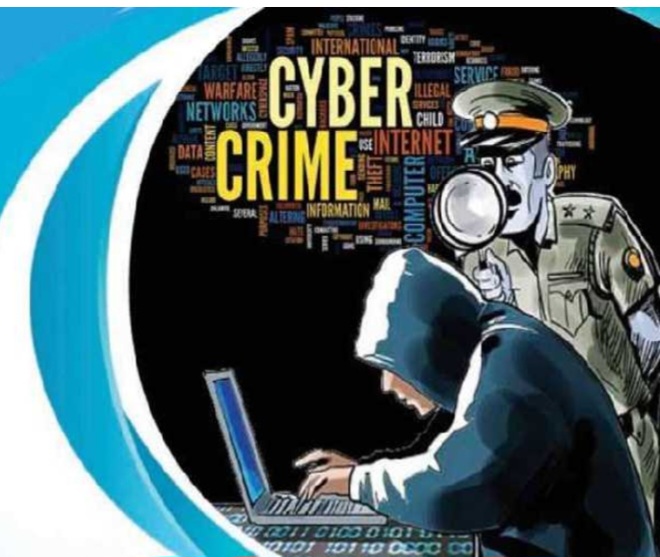साइबर अपराधों में नाबालिगों की भूमिका: क्या कानून तैयार है?
भूमिका
वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट न केवल जानकारी और संचार का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक गतिविधियों का मुख्य आधार बन चुका है। इसी के साथ साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, और चिंता की बात यह है कि अब इन अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता भी देखने को मिल रही है। कुछ नाबालिग मज़ाक या अज्ञानता में अपराध कर बैठते हैं, तो कुछ जानबूझकर संगठित साइबर अपराधों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे परिदृश्य में यह प्रश्न उठता है—क्या हमारा कानूनी ढांचा ऐसे मामलों से निपटने के लिए तैयार है?
नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले सामान्य साइबर अपराध
- हैकिंग और डाटा ब्रीच – कुछ किशोर शौकिया तौर पर वेबसाइट हैक कर देते हैं।
- साइबर बुलिंग – सोशल मीडिया पर धमकी देना, मजाक उड़ाना या मानसिक प्रताड़ना देना।
- फेक प्रोफाइल बनाना – दूसरों की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी प्रोफाइल बनाना।
- पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री का वितरण – विशेष रूप से किशोरों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में।
- ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी – जैसे इन-गेम खरीददारी में क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग।
- डार्क वेब तक पहुंच – नाबालिग कभी-कभी गैरकानूनी प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंच बना लेते हैं।
भारतीय कानून में नाबालिग साइबर अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को ‘किशोर’ मानता है। अगर नाबालिग द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है (जैसे साइबर आतंकवाद, गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी), तो 16 से 18 आयु वर्ग के किशोर को वयस्क की तरह ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसा आदेश दे। - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- IT Act में कोई विशेष खंड नाबालिग अपराधियों के लिए नहीं है, लेकिन नाबालिगों द्वारा की गई हैकिंग, अश्लील सामग्री का प्रेषण, साइबर स्टॉकिंग आदि अपराधों के लिए दंड निर्धारित है।
- धारा 66E, 67, 67B, 72 आदि के अंतर्गत नाबालिग भी उत्तरदायी हो सकते हैं।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023)
- IPC की कई धाराएं जैसे धारा 419, 420 (धोखाधड़ी), 500 (मानहानि), 507 (गुमनाम धमकी) साइबर अपराधों पर लागू होती हैं।
- हालांकि IPC में नाबालिगों के लिए दंड की अलग व्यवस्था नहीं है, इसलिए JJB कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।
चुनौतियाँ और कानूनी कमियाँ
- डिजिटल समझ की कमी – कानून प्रवर्तन एजेंसियों में साइबर फॉरेंसिक या डिजिटल जांच का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।
- मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा – नाबालिग के मनोविज्ञान को समझना और सुधार की प्रक्रिया को प्राथमिकता देना जरूरी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव – IT Act या JJ Act में साइबर अपराधों में नाबालिगों की भूमिका को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है।
- शिक्षा संस्थानों की निष्क्रियता – स्कूल-कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता की कमी और साइबर नैतिकता की शिक्षा न होना एक बड़ी कमी है।
क्या कानून तैयार है?
कहना गलत न होगा कि भारत का कानूनी ढांचा आंशिक रूप से तैयार है, लेकिन पूरी तरह सुसज्ज नहीं।
- किशोर न्याय अधिनियम का संशोधित संस्करण गंभीर मामलों में कड़े निर्णय की अनुमति देता है।
- लेकिन IT Act में नाबालिगों के लिए अलग से पुनर्वास आधारित न्याय व्यवस्था का अभाव है।
- साइबर अपराधों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझकर समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
समाधान और सुझाव
- विशेष साइबर अपराध सुधार गृह – जहां नाबालिगों को तकनीकी शिक्षा और साइबर नैतिकता सिखाई जा सके।
- स्कूल स्तर पर साइबर कानूनी शिक्षा अनिवार्य हो।
- पुलिस, शिक्षक और अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- डेटा संरक्षण कानून में नाबालिगों के लिए विशेष प्रावधान।
- जुवेनाइल बोर्ड में तकनीकी और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की भागीदारी।
निष्कर्ष
डिजिटल युग में जहां तकनीक नाबालिगों की पहुंच में है, वहीं उनका अपराध की ओर झुकाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के कानूनों को सिर्फ दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक और संरक्षणात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि हम भविष्य की पीढ़ी को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हमें कानून, शिक्षा और सामाजिक संरचना—तीनों को एक साथ सशक्त करना होगा।