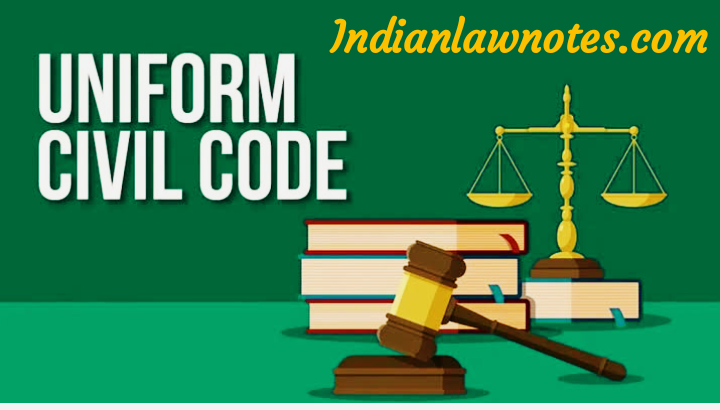समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code): भारतीय न्याय व्यवस्था, संवैधानिक सिद्धांत और सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श का व्यापक विश्लेषण
भूमिका: एक राष्ट्र, एक कानून — क्या यह समय की मांग है?
भारतीय संविधान की आत्मा समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। इसके बावजूद आज भी देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दहेज, संरक्षकता, गोद लेना आदि निजी कानूनी क्षेत्र धर्म-धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों से संचालित होते हैं। यही कानून व्यवस्था के क्षेत्र में विविधता और कभी-कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसे में “समान नागरिक संहिता” अर्थात Uniform Civil Code (UCC) का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
UCC का मूल उद्देश्य देश के सभी नागरिकों—चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के हों—को समान नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करना है। यह विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उल्लेखित है। परंतु इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना भारतीय समाज, राजनीति और न्याय-व्यवस्था के लिए सबसे संवेदनशील प्रश्नों में से एक है।
समान नागरिक संहिता का इतिहास और संवैधानिक पृष्ठभूमि
भारत में UCC का विचार कोई नया नहीं है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। संविधान निर्माताओं का मत था कि एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में व्यक्तिगत कानूनों का विभाजन लंबी अवधि में न्याय और सामाजिक एकता के लिए चुनौती बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, UCC के प्रबल समर्थक थे। उनका विश्वास था कि व्यक्तिगत कानूनों की असमानता समाज में भेदभाव, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ उत्पन्न करती है।
हालाँकि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, न कि मौलिक अधिकार में। संविधान सभा ने माना कि विविध धार्मिक पृष्ठभूमि वाले भारतीय समाज में तत्काल UCC लागू करने से सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती थी।
व्यक्तिगत कानूनों का स्वरूप: क्यों ज़रूरी है एकरूपता?
भारत में वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों के अलग-अलग निजी कानून लागू हैं:
| धर्म / समुदाय | संबंधित व्यक्तिगत कानून |
|---|---|
| हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख | हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक अधिनियम आदि |
| मुस्लिम | मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 |
| ईसाई | भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 |
| पारसी | पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 |
| विशेष विवाह अधिनियम | धर्म-निरपेक्ष विवाह कानून |
इस विभाजन के कारण न्याय के सिद्धांत और अधिकार अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग अर्थ प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए—तलाक का प्रावधान, गोद लेने का अधिकार, बहुविवाह की स्थिति, पैतृक संपत्ति में महिला का अधिकार, इत्यादि कई क्षेत्रों में असमानता दिखाई देती है।
धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से UCC का महत्व
धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ राज्य और धर्म के बीच समान दूरी बनाए रखना है। जब राज्य अलग-अलग धर्मों के आधार पर नागरिक अधिकार तय करता है, तो यह सिद्धांत कमजोर हो जाता है। UCC लागू होने से—
- कानून सभी नागरिकों के लिए बराबर होगा
- धार्मिक पहचान से ऊपर राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता मिलेगी
- समानता और न्याय के संविधानिक सिद्धांत मजबूत होंगे
- महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में UCC की भूमिका
भारत में कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उदाहरण रहे हैं। जैसे—
- मुस्लिम कानून में पहले तीन तलाक की व्यवस्था (अब समाप्त)
- कई धर्मों में पुत्रों को अधिक संपत्ति अधिकार
- हज़ारों वर्षों तक हिंदू उत्तराधिकार में स्त्रियों को सीमित अधिकार
- गोद लेने के अधिकार में धार्मिक प्रतिबंध
UCC इन असमानताओं को दूर कर समान अधिकार स्थापित करता है। इसका मूल उद्देश्य परिवार व्यवस्था को न्याय तथा आधुनिक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाना है।
धार्मिक स्वतंत्रता बनाम UCC: एक संवैधानिक संतुलन
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि UCC धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन शैली के अधिकार का उल्लंघन करेगा। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसलिए जब व्यक्तिगत कानून नागरिक अधिकारों में असमानता पैदा करते हैं, तो राज्य का कर्तव्य न्याय सुनिश्चित करना बन जाता है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य और न्यायालयों की भूमिका
भारतीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर UCC की आवश्यकता पर टिप्पणी की है।
शाह बानो मामला (1985) महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत कानून टकराव का प्रमुख उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि समान नागरिक संहिता न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है।
इसके बाद सरला मुद्गल केस (1995) एवं पायल शर्मा बनाम नितिन कुमार (2003) जैसे प्रकरणों में भी न्यायालय ने कहा कि एक समान कानून विवाहों और पारिवारिक विवादों के न्यायपूर्ण समाधान में सहायक होगा।
गोवा मॉडल: क्या यह UCC का आदर्श उदाहरण है?
भारत में गोवा राज्य पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करता है। इसमें सभी धर्मों पर समान विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं। यह मॉडल दर्शाता है कि विविध समाज में भी एक समान नागरिक कानून व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है।
UCC से जुड़ी चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
UCC लागू करने में निम्न प्रमुख चुनौतियाँ सामने आती हैं:
- धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताएँ
- सामाजिक विविधता और परंपराओं के संरक्षण का प्रश्न
- राजनीतिक ध्रुवीकरण और वोट-बैंक राजनीति
- जन जागरूकता और व्याख्या का अभाव
- कानूनों का व्यावहारिक एकीकरण
कुछ आलोचकों का तर्क है कि कानून का उद्देश्य केवल समानता नहीं, बल्कि न्याय और विविधता का सम्मान भी होना चाहिए। इसलिए UCC को कठोर कानून की जगह “परामर्श, संवाद और चरणबद्ध सुधार” के रूप में लागू किया जाना चाहिए।
UCC लागू करने के संभावित तरीके
समान नागरिक संहिता के लिए निम्न रणनीतियाँ व्यवहारिक मानी जा सकती हैं—
- चरणबद्ध रूप से लागू करने की नीति
- महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता
- धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों से संवाद
- जन-जागरण और संवैधानिक शिक्षा
- गोवा मॉडल का विस्तार
- Special Marriage Act को सरल और लोकप्रिय बनाना
UCC के लाभों का सार
| क्षेत्र | संभावित लाभ |
|---|---|
| सामाजिक न्याय | सभी वर्गों को समान अधिकार |
| महिला सशक्तिकरण | विवाह, तलाक, विरासत में समानता |
| राष्ट्रीय एकता | राष्ट्रीय पहचान को मजबूती |
| धर्मनिरपेक्षता | कानून और धर्म का स्पष्ट विभाजन |
| न्यायिक प्रणाली | पारिवारिक विवादों में पारदर्शिता |
निष्कर्ष: समानता, न्याय और आधुनिक भारत की दिशा में निर्णायक कदम
समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के मूल मूल्य—समानता, न्याय और मानव गरिमा—का प्राकृतिक विस्तार है। UCC का उद्देश्य किसी धर्म को चुनौती देना नहीं, बल्कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को समान रूप से सुनिश्चित करना है। यह केवल कानून सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है।
भारत की लोकतांत्रिक और बहुलतावादी व्यवस्था में UCC को लागू करना चुनौतीपूर्ण अवश्य है, मगर असंभव नहीं। संवाद, शिक्षा और संवेदनशील दृष्टिकोण से यह कदम नए भारत की दिशा में महान सामाजिक-न्यायिक परिवर्तन सिद्ध हो सकता है।
एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समान नागरिक संहिता केवल कानून नहीं— बल्कि समान मानव अधिकारों की आवाज है।