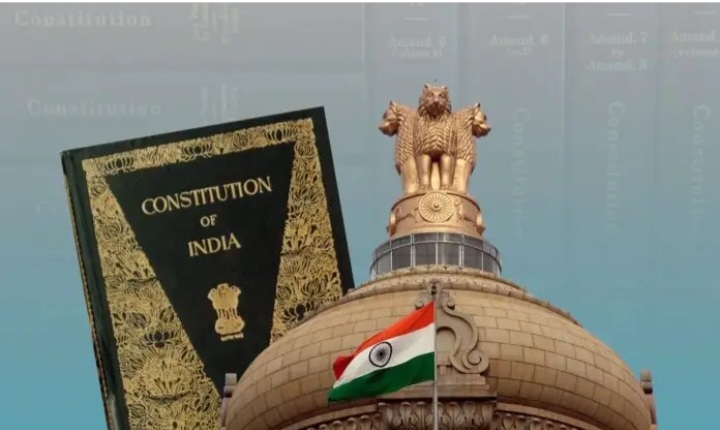समानता का अधिकार: भारतीय संदर्भ में व्याख्या
(Right to Equality: Interpretation in Indian Context)
परिचय:
भारतीय संविधान का मूल आधार “समानता” है। यह सिद्धांत न केवल सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में लोकतंत्र की आत्मा भी है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत है। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर और छुआछूत की समाप्ति का आश्वासन देता है।
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि राज्य न तो अनुचित भेदभाव करेगा और न ही विशेष वर्ग को अनुचित लाभ देगा।
हालांकि, यह समानता “समान व्यवहार” नहीं बल्कि “समान परिस्थितियों में समान व्यवहार” की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि समानता का अर्थ यह नहीं कि हर किसी के साथ एक-सा व्यवहार हो, बल्कि जो समान हैं उनके साथ समान व्यवहार हो और जो अलग हैं उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जा सकता है यदि उसका औचित्य हो।
अनुच्छेद 15: भेदभाव के विरुद्ध प्रतिबंध
यह अनुच्छेद राज्य को इस बात से रोकता है कि वह केवल धर्म, जाति, जाति समूह, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करे।
हालांकि, इसमें कुछ सकारात्मक छूट दी गई हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यह सामाजिक न्याय की ओर एक कदम है।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
यह प्रावधान सरकारी नौकरियों और पदों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसमें भी राज्य को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सके।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन
यह एक क्रांतिकारी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे कानूनन दंडनीय बनाता है। यह भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन
यह अनुच्छेद भारत में “समानता” की भावना को प्रोत्साहित करता है, जहां किसी भी नागरिक को सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियों (जैसे “सर”, “लॉर्ड”) का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, जिससे समाज में उच्च-नीच की भावना न उत्पन्न हो।
न्यायपालिका की भूमिका:
भारतीय न्यायपालिका ने समानता के अधिकार की व्याख्या समय-समय पर की है। मनु भाई शाह बनाम गुजरात राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (मंडल आयोग मामला), के.सी. वासवानी बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार न केवल नकारात्मक अधिकार (भेदभाव से संरक्षण) है, बल्कि यह सकारात्मक दायित्व भी है जो राज्य पर समान अवसर सृजित करने के लिए लगाया गया है।
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और विधिक समता का मूल आधार है। यह न केवल नागरिकों को एक-दूसरे के समकक्ष खड़ा करता है, बल्कि राज्य को भी यह निर्देश देता है कि वह सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए सकारात्मक उपाय अपनाए। समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है और इसके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी केवल राज्य की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है।