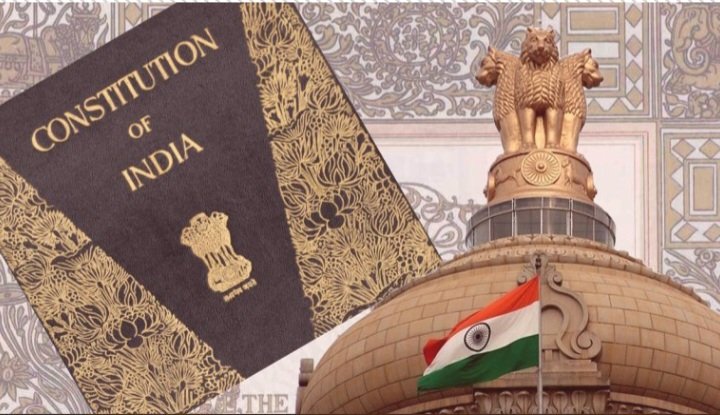-
संविधान क्या है? (What is Constitution?) संविधान एक लिखित या मौखिक दस्तावेज है, जिसमें किसी देश या राज्य का शासन ढांचा, संस्थाओं के अधिकार, कर्तव्य, और क़ानूनी प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी भी देता है।
- सांविधानिक विधि की परिभाषा दीजिये। (Define Constitutional Law.) सांविधानिक विधि वह कानून है जो किसी राज्य या देश के संविधान से संबंधित होता है। यह संविधान के तहत सरकारी संस्थाओं, उनके अधिकार, कर्तव्य और राज्य की नागरिकों के साथ संबंधों को नियंत्रित करता है।
- संविधानिक विधि तथा सामान्य विधि में क्या अन्तर है? (What is difference between Constitutional Law and General Law?) संविधानिक विधि संविधान से संबंधित होती है और यह राज्य के संगठन और संचालन के लिए नियम निर्धारित करती है, जबकि सामान्य विधि वह कानून है जो व्यक्तिगत मामलों जैसे अपराध, अनुबंध, संपत्ति आदि से संबंधित होता है।
- संविधान की प्रस्तावना। (Preamble of Constitution.) संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक भाग है, जो संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को व्यक्त करती है। इसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, और न्याय के सिद्धांतों का उल्लेख है।
- (क) क्या उद्देशिका संविधान का भागं है? (Whether the Preamble is the part of the Constitution?) हां, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, हालांकि इसे संविधान के विभिन्न भागों में से एक संशोधन योग्य भाग नहीं माना जाता है, लेकिन यह संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है।(ख) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों का वर्णन कीजिये। (Discuss the objects set out in the Preamble of Indian Constitution.) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, और न्याय के सिद्धांतों का समावेश है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है।
- संविधान की रचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (Write a short note on the making of Constitution.) भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में हुआ था, और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसकी रचना में भारतीय संविधान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रमुख रचनाकार माना जाता है।
- संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व क्या हैं? (What are the essential elements of Federal Constitution?) संघात्मक संविधान के मुख्य तत्वों में संघीय शासन, विभाजित सत्ता, साझा शक्तियाँ, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल हैं। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण होता है।
- प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं? (What do you understand by delegated legislation?) प्रत्यायोजित विधान वह कानून है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी अन्य संस्था (जैसे कि कार्यकारी) को बनाने की शक्ति दी जाती है। इसे प्रधान विधान से अलग किया जाता है और यह कुछ विशेष मामलों में लागू होता है।
- अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं? स्पष्ट करें। (What is Residuary Legislative Powers? Explain.) अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जो संविधान में केंद्रीय और राज्य विधानमंडल के बीच विभाजित नहीं की गईं, और जिन्हें संसद को अधिग्रहण करने का अधिकार होता है। यह शक्तियाँ सामान्यत: केंद्रीय सरकार को मिलती हैं।
- “सहकारी परिसंघवाद” के विषय में बतलाइये। (Explain Co-operative Federalism.) सहकारी परिसंघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, और उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यह साझा निर्णय लेने और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है।
- परिसंघवाद को परिभाषित कीजिये। (Define Federalism.) परिसंघवाद एक शासन प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें, जैसे केंद्रीय और राज्य सरकारें, एक साथ काम करती हैं और उनके अधिकारों का वितरण संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें सत्ता का विभाजन होता है और दोनों स्तरों के सरकारों के बीच स्वतंत्रता होती है।
- आच्छादन का सिद्धान्त क्या है? (What is the Doctrine of Eclipse?) आच्छादन का सिद्धान्त भारतीय संविधान में उस स्थिति को व्यक्त करता है जब कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ होता है, लेकिन संविधान की एक अस्थायी शिथिलता के कारण वह कानून अस्तित्व में रहता है। यह तब लागू होता है जब कोई विधि किसी मौलिक अधिकार से टकराती है, लेकिन इस पर अदालत द्वारा आक्षेप नहीं किया गया हो। जब यह शिथिलता समाप्त हो जाती है, तो वह कानून फिर से अप्रभावी हो जाता है।
- धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अन्तर है? (What is the difference between Money Bills and Finance Bills?)
- धन विधेयक (Money Bill): यह विधेयक केवल संसद के निम्न सदन (लोक सभा) में प्रस्तुत किया जाता है और यह सरकार की धन संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि कर संग्रह, राजस्व, और सरकारी खर्च।
- वित्त विधेयक (Finance Bill): यह विधेयक आमतौर पर केंद्रीय बजट के बाद प्रस्तुत किया जाता है और इसमें सरकार के विभिन्न वित्तीय मामलों का प्रस्ताव किया जाता है। इसमें करों, राजस्व या अन्य वित्तीय नीतियों में बदलाव की परिकल्पना होती है।
- सदन के सदस्यों की संयुक्त बैठक (Joint sitting of both Houses): जब दोनों सदन, लोक सभा और राज्य सभा, किसी विधेयक पर सहमति नहीं बना पाते हैं, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में दोनों सदन के सदस्य मिलकर विधेयक पर मतदान करते हैं, और यह मतदान निर्णय लेने के लिए अंतिम होता है।
- संसद को सदस्यता के लिये अर्हता क्या है? (What is qualification for membership of Parliament?)
- लोक सभा: उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- राज्य सभा: उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इसके अलावा, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होना चाहिए।
- (क) न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिये। (Define Judicial Activism?) न्यायिक सक्रियता वह सिद्धांत है जिसमें न्यायपालिका सरकार की नीतियों या विधायिका द्वारा पारित कानूनों के खिलाफ सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रही है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है।
(ख) धर्म-निरपेक्षता (Secularism): धर्म-निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है और न ही किसी धर्म के आधार पर नागरिकों के अधिकारों में भेदभाव करता है। भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता की पुष्टि की गई है, जिससे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? (What is Judicial Review?) न्यायिक पुनर्विलोकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून, आदेश, या सरकारी निर्णय को संविधान के अनुकूल या संविधान के खिलाफ जांच सकते हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकार के कार्यों की वैधता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- संसद की संरचना (Composition of Parliament): भारतीय संसद दो सदनों में बटी हुई है:
- लोक सभा (Lower House): सदस्य 545 होते हैं (जिनमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 सांसद राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं)।
- राज्य सभा (Upper House): सदस्य 250 होते हैं, जिनमें से कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
- लोक सभा (Lok Sabha): लोक सभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। लोक सभा का मुख्य कार्य कानून बनाना, बजट पास करना, और सरकार की नीतियों की निगरानी करना है।
- लोक सभा का स्पीकर (Speaker of Lok Sabha): लोक सभा का स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो लोक सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। वह सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का उत्तरदायी होता है और मतदान में निर्णय लेने में भी भूमिका निभाता है।
- सार-तत्व का सिद्धान्त (Doctrine of Pith and Substance): यह सिद्धांत यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई विधायिका कानून किस हद तक केंद्रीय या राज्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि कोई कानून केंद्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में आता है, तो उसके उद्देश्य और वास्तविक पदार्थ का विश्लेषण किया जाता है, और उसी के आधार पर उसका अधिकार क्षेत्र तय किया जाता है।
- राष्ट्रपति की विधायी शक्ति (Legislative power of the President): राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि विधेयकों को स्वीकृति देना, उन्हें खारिज करना या उन्हें संसद में पुनः भेजना। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को अनुमोदित करने से पहले उन्हें अपनी सहमति दे सकते हैं।
- राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का संक्षेप में उल्लेख करें (Discuss briefly the judicial powers of President): राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेना, सजा माफ करना, या किसी विशेष मामले में सजा को कम करना। राष्ट्रपति न्यायिक आदेशों की सिफारिश करने का अधिकार भी रखते हैं।
- भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President of India): भारतीय राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ होती हैं। वह सरकार के प्रमुख होते हुए राज्यपालों की नियुक्ति, कानूनों पर हस्ताक्षर करने, और संसद को बुलाने या सत्र को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं।
- राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख कीजिये (Discuss the executive powers of the President): राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ विभिन्न कार्यों को लागू करने से संबंधित होती हैं, जैसे कि मंत्रियों की नियुक्ति, सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करना, और अन्य कार्यकारी कार्यों की निगरानी करना। वह सरकार के प्रमुख के रूप में निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- राष्ट्रपति की अर्हताएँ क्या हैं? (What are qualifications of President?) भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होती हैं:
- वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- वह किसी राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य बनने के लिए अर्हतापूर्ण होना चाहिए।
- वह किसी अन्य पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरकारी अधिकारी या राज्य के प्रमुख का पद।
- भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्तियों का उल्लेख करें (Discuss the powers of President of India related to grant of Pardon.) भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय दंड संहिता के तहत दया, क्षमा, माफी और सजा में छूट देने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, खासकर उन मामलों में जहां मृत्यु दंड दिया गया हो।
- राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया (Procedure for impeachment of the President): राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद में निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम होते हैं:
- महाभियोग का प्रस्ताव लोक सभा या राज्य सभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- प्रस्ताव को दोनों सदनों में 14 दिन तक चर्चा के लिए रखा जाता है।
- अगर दोनों सदन प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी देते हैं, तो राष्ट्रपति को महाभियोग से दोषी ठहराया जा सकता है और उसे पद से हटा दिया जाता है।
- राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? (When the President can issue an ordinance?) राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, जब संसद का सत्र नहीं होता और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना यह समाप्त हो जाता है।
- संसद सदस्यों के लिये क्या निरर्हताएँ होती हैं? (What are the disqualifications to be a member of Parliament?) संसद सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित निरर्हताएँ हो सकती हैं:
- कोई व्यक्ति मानसिक विकृति से पीड़ित होना।
- चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार।
- वह सरकार या किसी सार्वजनिक कार्यालय में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- अपराधी होना या गंभीर दंड की सजा प्राप्त होना।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। (Discuss about procedure of election of President.) भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को अपनी वोट का मूल्य होता है, जो उनके राज्य या क्षेत्र के आधार पर तय किया जाता है। राष्ट्रपति का चयन वैकल्पिक मतदान प्रणाली के तहत होता है, जिसमें बहुमत प्राप्त उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है।
- छद्म विधायन के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? (What do you understand with doctrine of colourable legislation?) छद्म विधायन का सिद्धांत यह कहता है कि यदि एक विधान निर्माता अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग करके किसी अन्य संस्था या क्षेत्र के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो वह “छद्म विधायन” के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि अगर राज्य किसी विषय पर कानून बनाते हुए केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो वह असंवैधानिक होगा।
- क्षेत्रीय संबंध का सिद्धान्त (Territorial Nexus): क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि किसी विशेष कानून या कानून की शक्ति को उस स्थान के आधार पर माना जाता है, जिसके साथ उसका संबंध है। इसका मतलब है कि यदि किसी राज्य या क्षेत्र का कानून उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो वह वहां लागू हो सकता है।
- प्रसाद पर्यन्त का सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure): यह सिद्धांत कहता है कि सरकार के अधिकारी, विशेषकर राष्ट्रपति और राज्यपाल, अपनी नियुक्ति के दौरान “प्रसाद पर्यन्त” यानी अपनी खुशी के आधार पर सेवा में रह सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी समय, बिना किसी कारण के, इन्हें हटा सकती है।
- उप-राष्ट्रपति कौन होता है? उप-राष्ट्रपति के मुख्य कार्य क्या हैं? (Who is Vice-President? What are the main functions of Vice-President?) उप-राष्ट्रपति भारतीय संसद का अध्यक्ष होता है, और उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। वे राष्ट्रपति के अभाव में उनके कार्यों का निर्वाह भी कर सकते हैं। उप-राष्ट्रपति की भूमिका संसद की कार्यवाही को नियंत्रित करना और उसे सुव्यवस्थित रखना होती है।
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India): भारत का महान्यायवादी सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह केंद्रीय सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार को कानूनी सलाह देता है।
- लेखानुदान (Votes of Account): लेखानुदान एक अस्थायी वित्तीय व्यवस्था है जो संसद के अगले बजट सत्र के दौरान सरकारी खर्च को जारी रखने के लिए होती है, जब तक कि पूरे बजट को स्वीकृति नहीं मिल जाती। यह प्रक्रिया बजट के पारित होने से पहले कुछ आवश्यक खर्चों के लिए अनुमति देती है।
- मंत्रि परिषद् में प्रधानमंत्री की स्थिति तथा उसकी शक्तियाँ (Position and powers of the Prime Minister in Council of Ministers): प्रधानमंत्री भारतीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और उसे सरकार के सभी कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। वह मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों का आवंटन और उनके कर्तव्यों की निगरानी करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की सलाह पर निर्णय लेने की शक्तियाँ होती हैं।
- वित्त विधेयक (Finance Bill): वित्त विधेयक वह विधेयक है जो केंद्रीय सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जैसे कि बजट, करों और राजस्व के बारे में प्रस्ताव। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए और यह सरकार के वित्तीय योजना और नीतियों को लागू करने के लिए जरूरी होता है।
- धन विधेयक (Money Bill): धन विधेयक वह विधेयक है जो केवल वित्तीय मामलों जैसे कि कर, राजस्व संग्रह, या सरकारी खर्च से संबंधित होता है। यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों के भीतर अपनी राय प्रस्तुत कर सकती है। यदि राज्यसभा इसे पारित नहीं करती, तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है।
- विनियोग विधेयक से क्या अभिप्रेत है? (What is meant by Appropriation Bills?) विनियोग विधेयक वह विधेयक होता है जिसके माध्यम से संसद सरकार को उसके निर्धारित बजट के तहत धन आवंटित करने की अनुमति देती है। यह विधेयक सरकार को उस धन का उपयोग करने के लिए मंजूरी प्रदान करता है, जो संसद द्वारा बजट के रूप में तय किया गया है।
- धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया (Procedure of passing of Money Bill): धन विधेयक की प्रक्रिया में सबसे पहले यह लोकसभा में प्रस्तुत होता है। यदि राज्यसभा इसे 14 दिन में पारित नहीं करती, तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा केवल संशोधन या सलाह दे सकती है, लेकिन यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद ही कानून बनता है।
- लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? (How is Speaker of Lok Sabha elected?) लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चुनाव में सभी सदस्य वोट करते हैं और जिनमें से जो अधिकतम वोट प्राप्त करता है, वह अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना और सदन के व्यवहार को सुव्यवस्थित रखना होता है।
- मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective responsibility of the Council of Ministers): मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहता है कि मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि सरकार को संसद में बहुमत का समर्थन नहीं मिलता, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। इसके तहत मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य सरकार की नीतियों और निर्णयों के लिए collectively उत्तरदायी होता है।
- मंत्रि परिषद् (Council of Ministers): मंत्रि परिषद केंद्रीय सरकार के उन सभी मंत्रियों का समूह होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों का समावेश होता है। मंत्रि परिषद सरकार की नीतियाँ तय करती है और कार्यपालिका को संचालित करती है।
- संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया (Procedure to pass a Bill in Parliament): विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल होते हैं:
- विधेयक का प्रस्ताव (First Reading).
- विधेयक पर चर्चा और संशोधन (Second Reading).
- तीसरी पढ़ाई और अंतिम मतदान (Third Reading).
- सदन में पारित होने के बाद, विधेयक दूसरे सदन (राज्यसभा) में प्रस्तुत होता है।
- यदि राज्यसभा में यह पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है।
46. राज्यसभा और लोकसभा की संरचना क्या है? (What is the Composition of the Council of States and the House of the People?)
- लोकसभा (House of the People): इसमें अधिकतम 545 सदस्य होते हैं, जिनमें 543 सदस्य सीधे चुनाव से चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
- राज्यसभा (Council of States): इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से कुछ सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और कुछ राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
47. राज्यसभा का सभापति (Chairman of the Council of States): राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और सदन के भीतर व्यवधान या असहमति से बचने के लिए कार्यवाही को नियंत्रित करता है।
48. अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ (Residuary powers of legislation): अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वह शक्तियाँ हैं जो भारतीय संसद को संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत दी गई हैं, जिसके द्वारा संसद को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है जो संघ और राज्य सूची में नहीं आते हैं। यह शक्तियाँ संसद को किसी भी नए क्षेत्र में कानून बनाने की अनुमति देती हैं।
49. संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बनाया जा सकता है? (When Parliament can make law on state subject?) संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि:
- जब राष्ट्रपति की अनुमति हो।
- राज्य में संविधानिक संकट की स्थिति हो।
- जब राज्य सरकार की अनुशंसा हो।
50. लोकसभा का विघटन (Dissolution of Lok Sabha): लोकसभा का विघटन तब होता है जब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे अगले आम चुनाव की आवश्यकता होती है। यह सामान्यतः पाँच वर्षों के बाद होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी कर सकते हैं यदि उन्हें उपयुक्त लगता है।
51. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा (Proclamation of emergency in case of failure of constitutional machinery in any state): यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस स्थिति में राज्य सरकार की कार्यवाही केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है।
52. आपात-उद्घोषणाकालिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? (Discuss the effects of declaration of emergency on fundamental rights): आपातकाल (Emergency) की स्थिति में भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषकर, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने से निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:
- निवारक निरुद्ध (Preventive Detention): आपातकाल के दौरान, व्यक्ति को बिना न्यायिक आदेश के भी हिरासत में लिया जा सकता है।
- मौलिक अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता।
- रक्षा के विशेष उपाय: आपातकाल के दौरान सरकार को अपने निर्णय लेने के लिए अधिक शक्ति मिल जाती है, और कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में। हालांकि, कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 20 और 21 (जो व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं) आपातकाल में भी नहीं रद्द किए जा सकते।
53. वित्तीय आपातकाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये (Write a short note on financial emergency): वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जा सकता है। यह तब लागू होता है जब केंद्र सरकार को लगता है कि भारत की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि देश की आर्थिक स्थिरता पर खतरा आ सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे राज्यों को वित्तीय सहायता पर नियंत्रण रखना और उन्हें सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए आदेश देना। यह स्थिति विशेष रूप से तब लागू होती है जब वित्तीय संकट का सामना किया जा रहा हो, जैसे आर्थिक मंदी या असाधारण वित्तीय परिस्थितियां।
- भारत के संविधान में क्षेत्रीय आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। स्पष्ट कीजिये (Discuss about the distribution of powers on the territorial basis in Indian Constitution): भारतीय संविधान में क्षेत्रीय आधार पर विधायी शक्तियाँ तीन सूची में विभाजित की गई हैं:
- संघ सूची (Union List): इसमें उन विषयों का विवरण है जो केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे रक्षा, विदेश नीति, और परमाणु ऊर्जा।
- राज्य सूची (State List): इसमें उन विषयों का विवरण है जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे पुलिस, शिक्षा, और स्वास्थ्य।
- संयुक्त सूची (Concurrent List): इसमें विषयों का विवरण है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे आपराधिक कानून, व्यापार और श्रम। यदि कोई कानून इन तीन सूचियों के अनुसार बनता है, तो संविधान के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण के अधिकार तय होते हैं।
55. संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों का क्या विस्तार है? (What is the extent of laws made by Parliament and Legislature of State?):
- संसद (Parliament): संसद द्वारा बनाए गए कानून संघ सूची, राज्य सूची (कुछ मामलों में) और संयुक्त सूची से संबंधित हो सकते हैं। संसद देश के पूरे क्षेत्र में कानून बना सकती है।
- राज्य विधानमंडल (State Legislature): राज्य विधानमंडल केवल राज्य सूची और संयुक्त सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, और यह कानून राज्य के भीतर लागू होता है। यदि राज्य की शक्ति संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वह संघीय कानूनों के अनुरूप कानून बना सकता है।
56. वित्त आयोग (Finance Commission): वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए अनुशंसा करता है। यह आयोग राज्य सरकारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और अनुदानों को तय करता है, और इसे हर पाँच साल में गठित किया जाता है।
- शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? (What do you understand by separation of power?): शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि शासन की शक्तियाँ (कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका) अलग-अलग संस्थाओं के बीच वितरित की जानी चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत, प्रत्येक शाखा अपने कार्यों में स्वतंत्र होती है और अन्य शाखाओं के हस्तक्षेप से बचती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी शाखा अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए और लोकतंत्र में संतुलन बना रहे।
- भारतीय संविधान में आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं? (How many kinds of emergency provisions in Indian Constitution?): भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल उपबंध हैं:
- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency): जब देश की सुरक्षा को खतरा हो, जैसे युद्ध या आंतरिक अशांति।
- राज्य आपातकाल (President’s Rule): जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए।
- वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency): जब देश की वित्तीय स्थिति गंभीर हो और केंद्र को विशेष शक्तियाँ मिलनी चाहिए।
- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक पद है। इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का लेखा-जोखा रखना है और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी खर्च और राजस्व का सही तरीके से हिसाब रखा जा रहा है।
- राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor): राज्यपाल को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का कार्य राज्य सरकार की कार्यवाही की निगरानी करना और राज्य में राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करना होता है।
- अपवादानुदान (Exceptional grants): अपवादानुदान विशेष प्रकार की वित्तीय सहायता होती है जिसे सरकार विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को देती है। यह आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों में दिया जाता है।
- विधान परिषद (Legislary Council): विधान परिषद राज्य की द्व chambers प्रणाली का दूसरा सदन होता है, जो राज्य विधानसभा के साथ होता है। इसका कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विधायकों पर चर्चा करना होता है। यह सदन केवल कुछ राज्यों में होता है और इसके सदस्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं।
- संसद में चर्चा पर निर्बंधन (Restrictions on discussion in Parliament): भारतीय संसद में चर्चा पर कुछ विधिक और संवैधानिक प्रतिबंध होते हैं। उदाहरण के लिए, संसद में न्यायिक मामलों, संवैधानिक मुद्दों या राष्ट्रपति के कार्यों पर चर्चा करने से रोक लगाई जा सकती है।
-
समस्याएँ (Problems): यह सामान्य प्रश्न है जिसमें विभिन्न संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का संदर्भ हो सकता है।