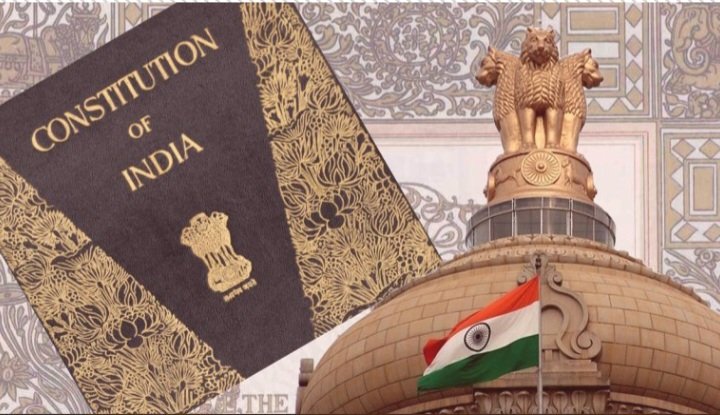- विधि के समक्ष समता का अर्थ
विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधिक अधिकारों का समान रूप से पालन किया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति से हो। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को न्यायपालिका के समक्ष समान व्यवहार प्राप्त होगा। - न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है?
न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि न्यायालय, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों या निर्णयों की वैधता की समीक्षा कर सकता है। यदि कोई क़ानून संविधान के खिलाफ है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। - युक्तियुक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं?
युक्तियुक्त वर्गीकरण का मतलब है कि राज्य कुछ वर्गों या व्यक्तियों को विशेष अधिकार दे सकता है, जब ऐसा वर्गीकरण तर्कसंगत हो और समानता के सिद्धांत के खिलाफ न हो। - आधारभूत ढाँचा से आप क्या समझते हैं?
आधारभूत ढाँचा का सिद्धांत भारतीय संविधान में उन मूलभूत सिद्धांतों को संदर्भित करता है जिन्हें संविधान के परिवर्तन के लिए छेड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि संविधान की संरचना में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिन्हें बदलने का अधिकार नहीं है। - अभित्यजन के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?
अभित्यजन का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष अधिकार का प्रयोग या त्याग करने के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वह अपने अधिकारों का त्याग स्वेच्छा से करे। - भारतीय संविधान के तहत ‘राज्य’ से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लेख कीजिए।
भारतीय संविधान में ‘राज्य’ से संबंधित उपबन्ध मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जो राज्य के अधिकार, कार्य, और नागरिकों के खिलाफ राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करते हैं। - क्या निम्नलिखित ‘राज्य’ शब्द के अन्तर्गत सम्मिलित हैं?
- उच्च न्यायालय (High Court) – हाँ
- नगर पालिका (Municipal) – नहीं
- भारतीय खाद्य निगम (IFC) – हाँ
- विश्वविद्यालय (University) – हाँ
- जीतेन्द्र उपाध्याय (Jeetendra Upadhyay) – नहीं
- जीवन बीमा निगम (LIC) – हाँ
- संविधानोत्तर विधियाँ क्या हैं?
संविधानोत्तर विधियाँ वे विधियाँ हैं जो भारतीय संविधान की स्थापना के बाद, संविधान के भीतर प्रावधानों के तहत बनाई जाती हैं और संविधान के उद्देश्य से मेल खाती हैं। - विधि का शासन की व्याख्या कीजिए।
विधि का शासन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सत्ताधारी हो या सामान्य नागरिक, सभी को संविधान और कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकता।
Here are the short answers to the remaining questions:
- मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अन्तर
- मौलिक अधिकार: ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं, जो नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता, और समानता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन्हें संविधान में विशेष रूप से अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित किया गया है।
- मानव अधिकार: ये सार्वभौमिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुनिश्चित होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा।
- न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए।
न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि न्यायालय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए गलत या असंवैधानिक कार्यों पर हस्तक्षेप करता है। इसका उद्देश्य संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। - शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं?
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि सरकार की तीन प्रमुख शाखाओं (विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका) को एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग रखा जाना चाहिए, ताकि किसी एक शाखा का अत्यधिक प्रभाव न हो और सत्ता का संतुलन बना रहे। - अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं?
अस्पृश्यता का मतलब है समाज में कुछ वर्गों को, विशेषकर दलितों या अनुसूचित जातियों को, अपवित्र या नीचा समझना और उन्हें सामाजिक, धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से भेदभाव करना। भारतीय संविधान ने इसे समाप्त किया है। - उपाधियों के अन्त पर टिप्पणी लिखें।
भारतीय संविधान ने संविधान के 18वें संशोधन के तहत “उपाधियों” या “सैन्य या सामंती उपाधियों” को समाप्त कर दिया। इसका उद्देश्य जातिवाद और समाज में असमानताओं को समाप्त करना था। - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।
वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई एक मौलिक स्वतंत्रता है, जो नागरिकों को विचारों, विचारधाराओं और सूचनाओं को व्यक्त करने का अधिकार देती है, हालांकि इस पर कुछ सीमाएं भी हैं। - भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार एवं उन पर प्रतिबन्धों की विवेचना करें।
भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, लेकिन इसे कुछ विशेष प्रतिबंधों के तहत रखा गया है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, द्वेष, अशांति, और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कारणों से। - मौलिक अधिकारों की उपलब्धता राज्य के विरुद्ध है या सामान्य व्यक्तित्व के विरुद्ध है।
मौलिक अधिकारों की उपलब्धता मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ होती है, न कि सामान्य व्यक्तियों के खिलाफ। इन अधिकारों का उद्देश्य राज्य द्वारा किए गए किसी भी असंवैधानिक कार्यों या भेदभाव को चुनौती देना है। - क्या मूल अधिकार पूर्ण हैं।
नहीं, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर कुछ उचित प्रतिबंध और सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आपातकाल के दौरान। - दोहरे दण्ड के विरुद्ध संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत यह अधिकार दिया गया है। - आत्म-अभिशंसन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
आत्म-अभिशंसन का सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में इसे सुरक्षित किया गया है। - प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण।
यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जो प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, सिवाय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के। - शिक्षा का अधिकार।
यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत दिया गया है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। - एक गिरफ्तार व्यक्ति के कौन से अधिकार हैं?
गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के कारण और उसकी अधिकारों की जानकारी दी जाए, उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए उचित कारण हो, और उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द न्याय मिल सके। - सम्यक् विधि प्रक्रिया क्या है?
सम्यक् विधि प्रक्रिया का मतलब है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करते समय उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। - प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के कुछ आयामों का उल्लेख करें।
इसमें जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार या बंदी बनाए जाने से बचाना शामिल है। इसके तहत, किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
Here are the short answers to the remaining questions:
- मरने का अधिकार
भारतीय संविधान में “मरने का अधिकार” विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि आत्महत्या के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता। हालांकि, “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” के अधिकार के अंतर्गत, कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या से बचने के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता हो सकती है। - फर्जी मुठभेड़ तथा अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 के तहत, हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। फर्जी मुठभेड़ में, जब पुलिस या अन्य सुरक्षा बल किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन बिना उचित प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। - बलात् श्रम क्या है?
बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दबाव के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत, बलात् श्रम निषिद्ध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। - शोषण के विरुद्ध अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम के खिलाफ और अनुच्छेद 24 बच्चों से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से किसी भी प्रकार के शोषण को रोकता है। - धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचारित करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, साथ ही राज्य को धर्मनिरपेक्ष होने की आवश्यकता है। - चकमा माइग्रेन्ट क्या है?
चकमा माइग्रेन्ट मामले में चकमा जनजाति के लोग, जो म्यांमार से भारत में आए थे, उनकी पहचान और अधिकारों के बारे में विवाद था। इन लोगों को भारत में शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन उनका स्थायी नागरिकता status विवादास्पद था। - धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं?
धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और न ही किसी एक धर्म को दूसरों से ऊपर रखेगा। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। - अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है?
अल्पसंख्यक का मतलब उन समूहों से है जिनकी संख्या किसी समाज में अन्य समूहों के मुकाबले कम होती है। यह समूह जाति, धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर हो सकते हैं, और संविधान इन्हें विशेष अधिकार प्रदान करता है। - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत याचिकाएँ अथवा उपचारात्मक याचिका
अनुच्छेद 32 के तहत, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय से उपचारात्मक याचिका (Writs) दायर कर सकते हैं। इसमें Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, और Quo Warranto जैसी याचिकाएं शामिल हैं। - बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख
यह एक याचिका है जो एक व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के अवैध तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ दायर की जाती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने से बचाना है। - परमादेश लेख
यह एक याचिका है जो अदालत को यह आदेश देने के लिए दायर की जाती है कि किसी सरकारी अधिकारी या निकाय को अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। - प्रतिषेध लेख क्या है?
यह याचिका तब दायर की जाती है जब किसी न्यायालय या प्राधिकरण को किसी कार्य को करने से रोका जाता है, जो उसे करने का अधिकार नहीं है। - उत्प्रेषण लेख क्या है?
यह याचिका तब दायर की जाती है जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, निचले न्यायालय से दस्तावेज़ या रिकॉर्ड प्राप्त करने का आदेश देता है, ताकि उसे किसी विशेष मामले में समीक्षा किया जा सके। - अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 में प्रमुख अन्तर क्या हैं?
अनुच्छेद 32 का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 226 व्यापक अधिकार देता है। - लोकहित वाद क्या है?
लोकहित वाद (PIL) का उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए जनहित में याचिका दायर करना है। इसके तहत, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक भलाई के लिए चिंता करता हो, वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। - राज्य के उन नीति निदेशक तत्वों को वर्णित कीजिए जिन्हें मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है?
संविधान के कुछ नीति निदेशक तत्व, जैसे कि समान वेतन, बच्चों की शिक्षा, और श्रमिकों के अधिकारों को बाद में अदालतों के निर्णयों द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में माना गया है।
Here are the short answers to the remaining questions:
- भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान किया गया है? स्पष्ट करें।
अनुच्छेद 41 में राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह अपने सीमित संसाधनों के भीतर नागरिकों को जीवन यापन के लिए आवश्यक सेवाएँ और अधिकार प्रदान करेगा। यह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में है, जैसे बेरोजगारी, वृद्धावस्था, या बीमारी के समय सहायता देना। - नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
एक समान सिविल संहिता का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना चाहिए, जो धर्म, जाति, या लिंग के आधार पर भेदभाव न करता हो। इसका उद्देश्य समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। - बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह शिक्षा का अधिकार क़ानून के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। - कृषि और पशुपालन संगठन।
कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है (अनुच्छेद 48) और इसका उद्देश्य किसानों के कल्याण, कृषि सुधारों, और पशुपालन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है, और अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में योगदान करे। - क्या निःशुल्क विधिक सहायता मूल अधिकार है?
हां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत राज्य यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए विधिक सहायता प्राप्त कर सकें। - कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण।
कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की स्वतंत्रता देना है, ताकि सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप न हो। - अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह निर्देशित किया गया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में सहयोग करेगा। - सामाजिक न्याय क्या है?
सामाजिक न्याय का अर्थ है, समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होना, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को। इसका उद्देश्य हर नागरिक को सम्मान और बराबरी की स्थिति में लाना है। - काम पाने के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
काम पाने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, ताकि वह अपनी जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारतीय संविधान में इसे एक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि नीति निदेशक तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अनुच्छेद 41)। - भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है। इनमें संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना आदि शामिल हैं। - क्या स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है?
हां, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। - सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं?
सूचना का अधिकार (Right to Information, RTI) नागरिकों को सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसे 2005 में लागू किया गया था। - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
उच्चतम न्यायालय को “अभिलेख न्यायालय” (Court of Record) माना जाता है, इसका अर्थ है कि इसकी सभी कार्यवाही, निर्णय और आदेशों का एक स्थायी और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएँ।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में 5 साल तक कार्य कर चुका हो।
- या वह विधि के अभ्यास में 10 साल तक अनुभव रखता हो।
Here are the short answers to the remaining questions:
- सर्वोच्च न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय का आरम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) वह अधिकार है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष मामले को सीधे पहली बार सुन सकता है, बिना मामले के पहले निचली अदालतों में जाने के। उदाहरण के लिए, संघीय विवाद, राज्यों के बीच विवाद, और अन्य संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार होता है (अनुच्छेद 131)। - न्यायपालिका की स्वतन्त्रता।
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का मतलब है कि न्यायालय को किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 50 और अन्य प्रावधानों के तहत सुनिश्चित किया गया है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान कर सके और कार्यपालिका या विधायिका के प्रभाव से बच सके। - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत है। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी या संवैधानिक मामलों में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जिनका समाधान अन्यथा संभव नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार अनिवार्य नहीं होता, बल्कि सलाह देने के रूप में होता है। - भारत में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को समझाइए।
उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction) के तहत यह सर्वोच्च न्यायालय अपीलों को सुनता है जो निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ दायर की जाती हैं। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 के तहत है और इसमें नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अंतिम अवसर मिलता है। - सम्पत्ति का अधिकार।
सम्पत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 से 32 के तहत एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रखा गया, बल्कि यह अब संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य केवल विधिक प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। - संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्ति।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। इसमें दो तरह के संशोधन होते हैं – एक साधारण बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत से। कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है, जबकि अन्य मामलों में संसद का विशेष बहुमत ही पर्याप्त होता है। - क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है?
हां, भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि उद्देशिका का मूल ढांचा या उसकी बुनियादी संरचना अपरिवर्तनीय है, लेकिन उसमें कुछ शब्दों को संशोधित किया जा सकता है यदि यह संविधान के मूल उद्देश्य को प्रभावित न करे। - निवारक निरोध पदावली को स्पष्ट कीजिए।
निवारक निरोध (Preventive Detention) वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए, केवल भविष्य में अपराध करने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। यह निरोध अवधि आम तौर पर तीन महीने होती है, लेकिन इसे बिना अदालत में पेश किए लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते यह संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उचित तरीके से किया जाए। -
तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में बतलाइये।
तदर्थ न्यायाधीश (Ad Hoc Judges) वे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी होती है। इन न्यायाधीशों को विशेष परिस्थितियों में नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल सीमित होता है। वे नियमित न्यायाधीशों के साथ न्यायिक कार्यों को करते हैं।