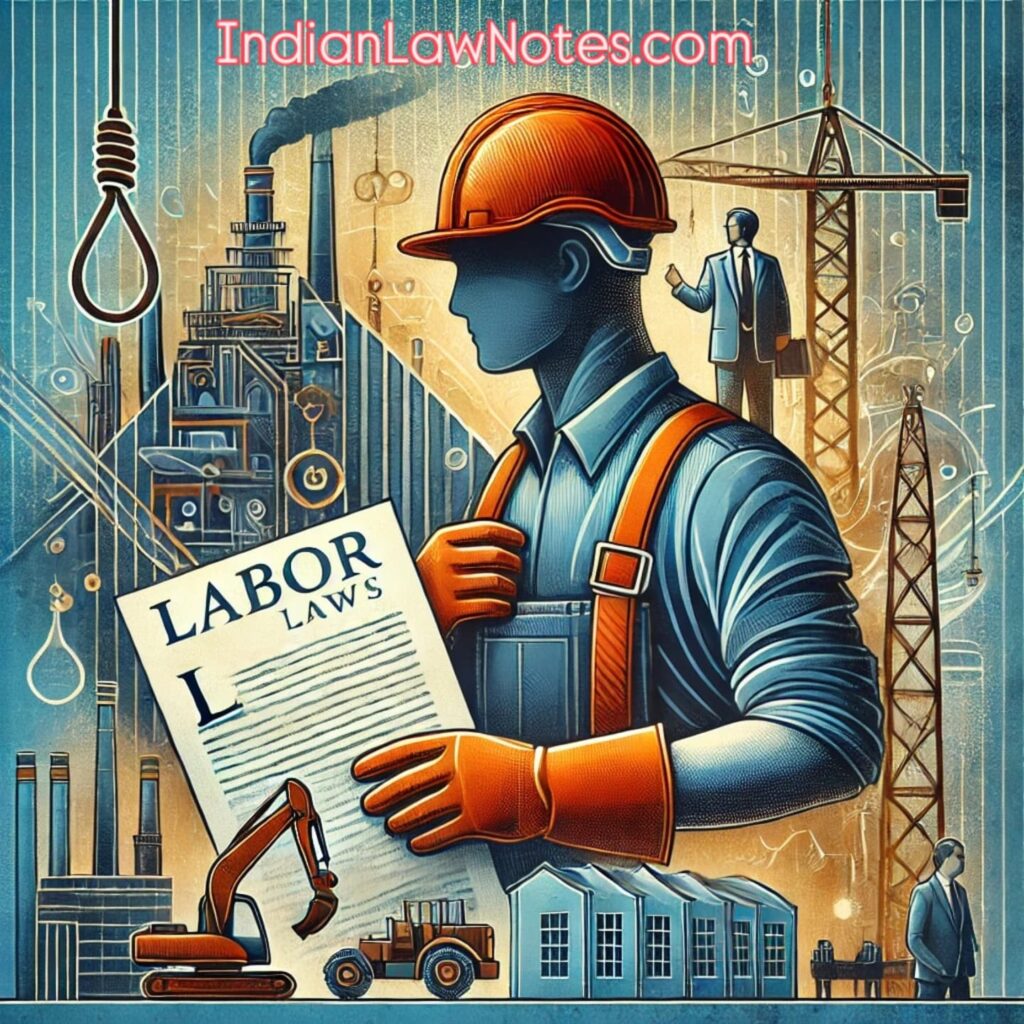श्रमिकों के अधिकारः जानिए मजदूरों के लिए लागू प्रमुख कानून
परिचय
भारत एक विकासशील देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों और मजदूरों के परिश्रम पर आधारित है। ये श्रमिक हमारे समाज की रीढ़ हैं, जो उद्योगों, खेतों, निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों और अन्य क्षेत्रों में अपने श्रम से देश को आगे बढ़ाते हैं। परंतु, इतिहास गवाह है कि मजदूरों का शोषण अक्सर होता रहा है — जैसे कम वेतन, अधिक घंटे काम, खराब कार्य स्थितियाँ, सुरक्षा की कमी, और सामाजिक सुरक्षा लाभों की अनुपलब्धता। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने समय-समय पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं।
यह लेख इन प्रमुख कानूनों, अधिकारों और उनके प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
1. श्रमिकों के मौलिक अधिकार
श्रमिकों को भारतीय संविधान और श्रम कानूनों के तहत निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं:
- समान वेतन का अधिकार (Equal Pay for Equal Work): पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
- शोषण से संरक्षण: बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, और जबरन श्रम पर कानूनी प्रतिबंध है।
- सम्मानजनक कार्य स्थिति का अधिकार: सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल की व्यवस्था अनिवार्य है।
- संघ बनाने का अधिकार: श्रमिक यूनियन (Trade Union) बनाने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी का अधिकार।
- न्याय पाने का अधिकार: अगर कोई श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित होता है तो वह अदालत में न्याय की मांग कर सकता है।
2. भारत में लागू प्रमुख श्रम कानून
भारत में अनेक श्रम कानून हैं, लेकिन 2020 में सरकार ने इन कानूनों को सरल और संगठित रूप में प्रस्तुत करने के लिए चार प्रमुख श्रम संहिताएँ (Labour Codes) पारित कीं:
(1) वेतन संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019)
यह कोड निम्नलिखित चार पुराने कानूनों को मिलाकर बना है:
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- भुगतान वेतन अधिनियम, 1936
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
मुख्य प्रावधान:
- न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू होगा।
- समय पर वेतन भुगतान अनिवार्य।
- समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना।
(2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (The Industrial Relations Code, 2020)
यह कोड तीन पुराने कानूनों को मिलाकर बना है:
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
मुख्य प्रावधान:
- ट्रेड यूनियन की पहचान और मान्यता।
- कर्मचारियों को निष्कासित करने के लिए प्रक्रिया और अनुमति।
- हड़ताल की प्रक्रिया को विनियमित करना।
(3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020)
यह कोड सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों को मिलाकर बना है, जैसे:
- कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (EPF)
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI)
- मातृत्व लाभ अधिनियम, आदि
मुख्य प्रावधान:
- सभी श्रमिकों के लिए पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ, बेरोजगारी भत्ता जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी कवर करने का प्रयास।
(4) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)
यह कोड 13 पुराने कानूनों को समाहित करता है, जैसे कि:
- फैक्ट्री अधिनियम, 1948
- खान अधिनियम, 1952
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, आदि
मुख्य प्रावधान:
- सभी कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रावधान।
- मजदूरों के लिए विश्राम, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था।
- कार्य के घंटे निर्धारित करना और ओवरटाइम के नियम।
3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार
भारत में एक बहुत बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है — जैसे कि घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, खेतिहर मजदूर आदि। इनके लिए सरकार ने कई योजनाएँ और कानून बनाए हैं:
- ई-श्रम पोर्टल: श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस जिससे योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना: वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- अटल पेंशन योजना
- मातृत्व लाभ योजनाएँ
4. श्रमिकों के अधिकारों से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ
- कई मजदूरों को कानूनों की जानकारी नहीं होती।
- असंगठित क्षेत्र में कानूनी अनुपालन की कमी।
- श्रम विभाग की निगरानी सीमित है।
- ट्रेड यूनियन की ताकत में कमी आई है।
5. समाधान और सुधार की दिशा
- मजदूरों में जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।
- श्रम कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन।
- डिजिटल पंजीकरण और पोर्टल का उपयोग।
निष्कर्ष
भारत जैसे विशाल देश में जहाँ श्रमिकों की संख्या करोड़ों में है, वहाँ उनके अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। कानूनों की उपस्थिति तब ही प्रभावी हो सकती है जब उनका सही से कार्यान्वयन हो और मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। सरकार, समाज और उद्योग जगत की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे श्रमिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण कार्य वातावरण प्रदान करें।