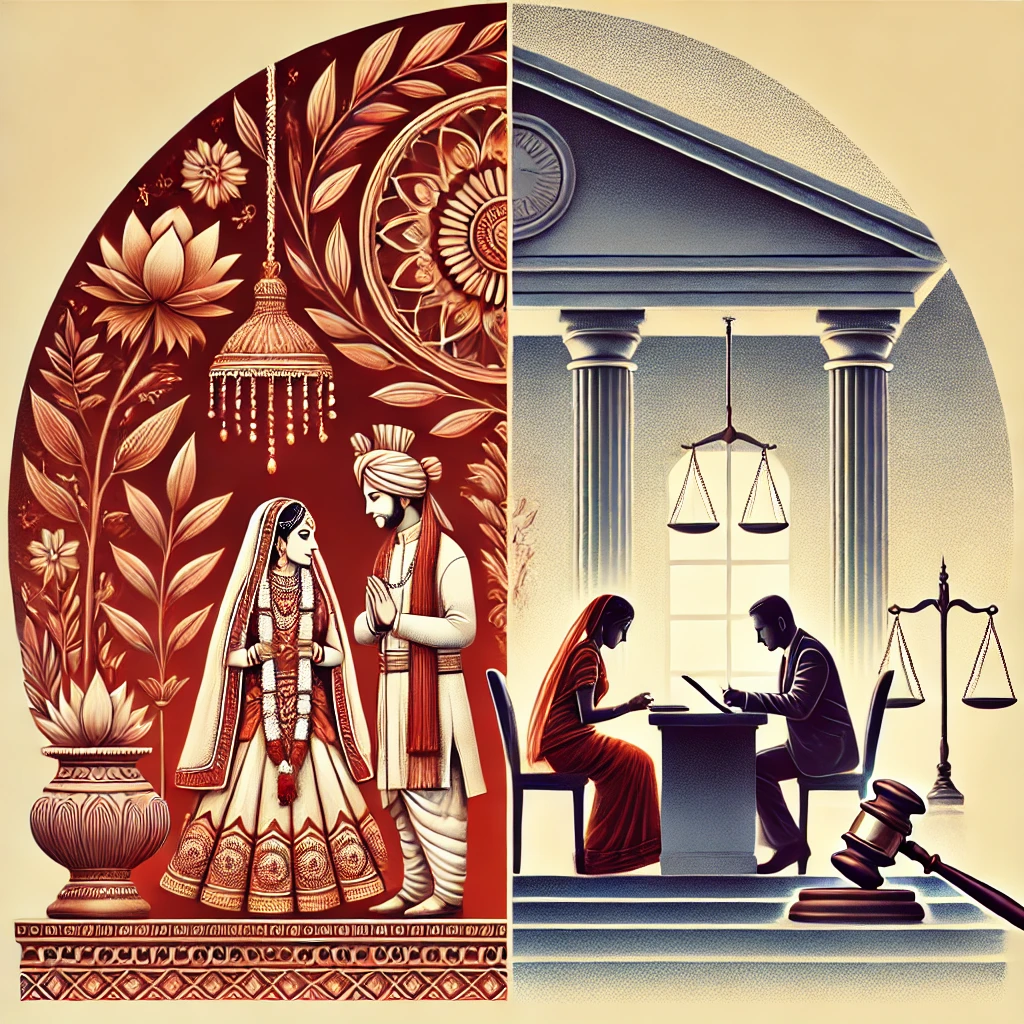“विवाह-समान संबंध” की अवधारणा: महिलाओं की सुरक्षा हेतु विधिक ढांचे में एक क्रांतिकारी समावेश
🔷 प्रस्तावना:
भारतीय समाज में पारंपरिक विवाह संस्था को एक पवित्र सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता रहा है। किंतु आधुनिक समय में सामाजिक संरचना, जीवन शैली और संबंधों की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन आया है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूकता ने ऐसे संबंधों को जन्म दिया है, जो विवाह के कानूनी बंधन में बंधे बिना सहमति से साथ रहने पर आधारित होते हैं। ऐसे संबंधों को ही न्यायपालिका ने “विवाह-समान संबंध” (Relationship in the Nature of Marriage) के रूप में परिभाषित किया है।
इस अवधारणा को विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा (से महिलाओं का संरक्षण) अधिनियम, 2005 के तहत विधिक मान्यता दी गई है, ताकि उन महिलाओं को भी संरक्षण मिले जो पारंपरिक विवाह में न होते हुए भी दीर्घकालिक, स्थायी और विवाह-जैसे संबंधों में रहती हैं।
🔷 विवाह-समान संबंध: विधिक परिभाषा और महत्व
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) में “घरेलू संबंध” (Domestic Relationship) की परिभाषा दी गई है:
“दो व्यक्तियों के बीच संबंध, जो रिश्तेदारी, विवाह, या विवाह के समान संबंध के कारण, एक साझा घरेलू जीवन व्यतीत करते हैं।”
यह परिभाषा “विवाह-समान संबंध” को विधिक संरक्षण देने का आधार बनती है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी महिला सिर्फ इस कारण विधिक सुरक्षा से वंचित न हो कि वह एक गैर-पारंपरिक सहवास संबंध में रह रही थी।
🔷 न्यायपालिका का योगदान:
भारतीय न्यायपालिका ने कई निर्णयों के माध्यम से “विवाह-समान संबंध” को मान्यता देते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है।
1. इंदिरा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013) 15 SCC 755
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संबंध निम्न मानकों को पूरा करता है, तो उसे विवाह-समान संबंध माना जा सकता है:
- दोनों वयस्क हों और उनके बीच सहमति हो
- दीर्घकालिक सहवास
- एक साझा घरेलू जीवन
- सामाजिक पहचान एक विवाहित जोड़े की तरह
- आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता
2. ललिता टोप्पो बनाम राज्य (2013, झारखंड HC)
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त हो सकता है।
3. डॉ. ए. इदप्पन बनाम सुषमा (Madras HC, 2022)
यह माना गया कि यदि संबंध की प्रकृति विवाह के समरूप है, तो महिला को भरण-पोषण और संरक्षण प्राप्त हो सकता है।
🔷 “विवाह-समान संबंध” के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार:
- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण:
यदि महिला विवाह के समान संबंध में है, तो वह घरेलू हिंसा की शिकार होने पर शिकायत दर्ज कर सकती है। - भरण-पोषण (Maintenance):
यदि यह प्रमाणित हो जाए कि महिला लंबे समय तक विवाह-जैसे संबंध में रही है, तो वह भरण-पोषण की पात्र हो सकती है। - आवासीय अधिकार:
महिला को साझा घर में रहने का अधिकार प्राप्त होता है, भले ही वह कानूनी पत्नी न हो। - गोपनीयता और गरिमा की रक्षा:
ऐसे संबंधों को सार्वजनिक रूप से कलंकित करना महिला की निजता और गरिमा के उल्लंघन के समान है, जिसे अदालतों ने अस्वीकार किया है।
🔷 विधिक चुनौतियाँ और सीमाएं:
- साक्ष्य की कठिनाई:
विवाह-समान संबंध को प्रमाणित करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, विशेषकर तब जब कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध न हो। - सामाजिक अस्वीकार्यता:
समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी ऐसे संबंधों को नैतिक रूप से स्वीकार नहीं करता, जिससे महिलाओं को कलंक और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। - उत्तराधिकार संबंधी अस्पष्टता:
विवाह-समान संबंध में रह रही महिला को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। - कानूनी व्याख्याओं में असंगति:
विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस अवधारणा की अलग-अलग व्याख्या की गई है, जिससे एकरूपता का अभाव है।
🔷 विधिक सुधार की आवश्यकता:
- “विवाह-समान संबंध” की स्पष्ट परिभाषा और मानदंडों को कानून में सम्मिलित करना
- ऐसे संबंधों की रजिस्ट्री की वैकल्पिक व्यवस्था, जिससे प्रमाणन की सुविधा हो
- महिला और बच्चों को संपत्ति व उत्तराधिकार संबंधी अधिकार प्रदान करना
- जनजागृति अभियान चलाकर सामाजिक कलंक को समाप्त करना
🔷 निष्कर्ष:
“विवाह-समान संबंध” की अवधारणा को विधिक रूप से स्वीकार करना भारतीय न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता और यथार्थपरक दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह न केवल महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना को भी पुष्ट करता है। हालाँकि इस दिशा में अभी भी कई विधिक और सामाजिक चुनौतियाँ शेष हैं, परंतु यह अवधारणा महिलाओं को एक ऐसा कानूनी ढाँचा उपलब्ध कराती है, जो उन्हें असुरक्षा, त्याग और शोषण से बचाता है।
🔷 समापन कथन:
“विवाह-समान संबंध” के विधिक समावेशन ने यह सुनिश्चित किया है कि रिश्तों की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, महिला की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है — यही संवैधानिक न्याय का मूल स्वर है।