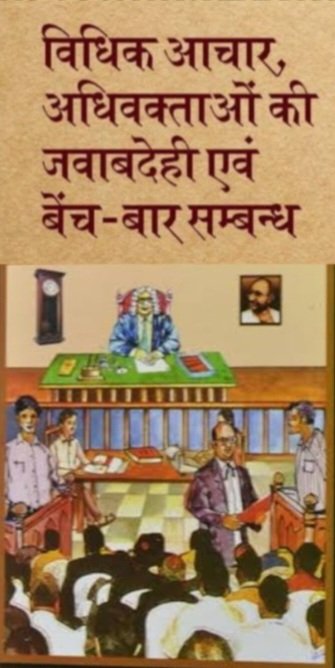लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर
1. अधिवक्ता (Advocates):
अधिवक्ता वे व्यक्ति होते हैं जो विधि (कानून) की पढ़ाई पूरी करने के बाद विधिक व्यवसाय में प्रविष्ट होते हैं और न्यायालयों में अपने मुवक्किलों की ओर से पैरवी करते हैं।
2. मूलभूत ढांचे का सिद्धान्त (Principle of Basic Structure):
यह सिद्धांत भारतीय संविधान के उन मौलिक तत्वों को संरक्षित करने के लिए विकसित किया गया है जिन्हें संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
3. अधिवक्ता के पंजीकरण के लिए अर्हताएँ (Qualifications for Enrolment as an Advocate):
- भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि (LL.B.) की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
- किसी भी प्रकार की नैतिक या आपराधिक दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए।
4. वाक् की स्वतंत्रता एवं न्यायालय की अवमानना (Freedom of Speech and Contempt of Court):
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह पूर्णतः निर्बाध नहीं है। न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) अधिनियम, 1971 के अनुसार, यदि कोई अभिव्यक्ति न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचाती है या उसके कामकाज में बाधा डालती है, तो इसे अवमानना माना जा सकता है।
5. एक राज्य सूची से दूसरे राज्य सूची में अधिवक्ता पंजीकरण के स्थानांतरण की प्रक्रिया (Procedure of Transfer of Advocate from One State Roll to Another):
- अधिवक्ता को अपने मौजूदा राज्य की बार काउंसिल को आवेदन देना होगा।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुमति आवश्यक होगी।
- नए राज्य की बार काउंसिल में पुनः नामांकन करवाना होगा।
6. राज्य विधिज्ञ परिषदों के कृत्य (Functions of State Bar Councils):
- अधिवक्ताओं का पंजीकरण और अनुशासन बनाए रखना।
- अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- कानूनी शिक्षा के विकास में योगदान देना।
- अधिवक्ताओं की शिकायतों का निवारण करना।
7. अधिवक्ता का पारिश्रमिक (Advocate’s Fee):
अधिवक्ता को उनके मुवक्किलों द्वारा दिए गए पारिश्रमिक (Fees) के आधार पर भुगतान किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा न्यूनतम फीस निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच स्वतंत्र रूप से शुल्क तय किया जाता है।
8. नामांकन समिति (Enrolment Committee):
यह समिति अधिवक्ताओं के पंजीकरण (Enrolment) की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह राज्य विधिज्ञ परिषद के अधीन कार्य करती है और अधिवक्ताओं की पात्रता की समीक्षा करती है।
9. अधिवक्ता के समाज के प्रति कर्तव्य (Duties of an Advocate Towards Society):
- न्याय और सत्य की रक्षा करना।
- गरीबों और असहाय लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देना।
- कानूनी जागरूकता फैलाना।
- पेशे में नैतिकता बनाए रखना।
10. पूर्व सुनवाई का अधिकार (Right of Pre-audience):
पूर्व सुनवाई का अधिकार का अर्थ है कि कुछ विशेष अधिवक्ताओं को न्यायालय में अन्य अधिवक्ताओं की तुलना में पहले सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं, महाधिवक्ता (Attorney General), सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को दिया जाता है।
11. अधिवक्ता एवं मुवक्किल के संबंध (Relationship of an Advocate and Client):
- यह विश्वास और गोपनीयता पर आधारित संबंध होता है।
- अधिवक्ता को मुवक्किल की पूरी निष्ठा से सहायता करनी चाहिए।
- मुवक्किल के मामलों को न्यायालय में उचित ढंग से प्रस्तुत करना अधिवक्ता का कर्तव्य होता है।
- अधिवक्ता को मुवक्किल की जानकारी बिना अनुमति के किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए।
12. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का उद्देश्य (Object of Advocate Act, 1961):
- पूरे भारत में एक समान विधिक व्यवसाय की संरचना करना।
- अधिवक्ताओं के पंजीकरण और अनुशासन को नियंत्रित करना।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल की स्थापना करना।
- अधिवक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करना।
13. अधिवक्ता की पोशाक (Dress of an Advocate):
- अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित पोशाक अनिवार्य है।
- पुरुष अधिवक्ताओं को काले कोट के साथ सफेद बैंड और सफेद शर्ट पहननी होती है।
- महिला अधिवक्ता काले कोट के साथ सफेद साड़ी या सफेद सलवार-कुर्ता पहन सकती हैं।
14. व्यावसायिक अवचार (Professional Misconduct):
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, अधिवक्ता के अनुचित आचरण को व्यावसायिक अवचार कहा जाता है।
- इसमें धोखाधड़ी, मुवक्किल से अनुचित धन लेना, न्यायालय में अनुचित व्यवहार करना आदि शामिल हैं।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।
15. विधिज्ञ परिषदें (Bar Councils):
- भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) और राज्य विधिज्ञ परिषदें (State Bar Councils) होती हैं।
- यह अधिवक्ताओं के पंजीकरण, अनुशासन और उनके अधिकारों की सुरक्षा करती हैं।
16. अधिवक्ता नामावली में परिवर्तन (Alteration in Roll of an Advocates):
- यदि किसी अधिवक्ता की पंजीकरण जानकारी में बदलाव करना हो (जैसे नाम, पता, राज्य), तो वह संबंधित राज्य बार काउंसिल को आवेदन दे सकता है।
17. अधिवक्ता लेखांकन (Advocate Accountancy):
- अधिवक्ता को अपने मुवक्किलों से प्राप्त धन का उचित लेखा-जोखा रखना चाहिए।
- उसे अपने व्यक्तिगत और मुवक्किल के धन को अलग-अलग रखना आवश्यक है।
18. वरिष्ठता के बारे में विवाद (Dispute about Seniority):
- अधिवक्ताओं की वरिष्ठता उनकी नामांकन तिथि, अनुभव और उनके द्वारा प्राप्त विशेष पदों के आधार पर तय होती है।
- यदि वरिष्ठता को लेकर विवाद होता है, तो बार काउंसिल या उच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है।
19. वरिष्ठ अधिवक्ता कौन है? (Who is Senior Advocate?):
- भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिवक्ता को “वरिष्ठ अधिवक्ता” का दर्जा प्रदान कर सकता है।
- वरिष्ठ अधिवक्ता सामान्य अधिवक्ताओं की तरह सीधे मुवक्किल से फीस नहीं ले सकते, बल्कि किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से ही केस लड़ सकते हैं।
20. विधिक व्यवसाय का महत्व (Importance of Legal Profession):
- यह न्यायपालिका का अभिन्न अंग है और समाज में न्याय की रक्षा करता है।
- नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी और सुरक्षा प्रदान करता है।
- लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने में सहायता करता है।
21. व्यावसायिक आचार (Professional Ethics):
- यह अधिवक्ताओं के आचरण और नैतिकता से संबंधित नियमों का एक समूह है।
- इसमें मुवक्किलों, न्यायालय और समाज के प्रति उनके कर्तव्य शामिल होते हैं।
- अधिवक्ताओं को न्यायालय और कानून के प्रति पूर्ण ईमानदारी रखनी चाहिए।
22. न्यायालय अवमानना संबंधी सांविधानिक उपबंध (Constitutional Provisions Relating to Contempt of Court):
- अनुच्छेद 129 और 215 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना के मामलों में कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए लागू किया गया था।
23. भारतीय विधिज्ञ परिषद की शक्तियाँ (Powers of Indian Bar Council):
- अधिवक्ताओं के नामांकन और अनुशासन पर नियंत्रण रखना।
- कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखना।
- अधिवक्ताओं की व्यावसायिक नैतिकता सुनिश्चित करना।
- विधिक सहायता सेवाओं का संचालन करना।
24. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court):
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, कोई भी कार्य या शब्द जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए या उसके आदेशों की अवहेलना करे, उसे न्यायालय की अवमानना माना जाता है।
- यह दो प्रकार की होती है: सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना।
25. आपराधिक अवमान (Criminal Contempt):
- जब कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करता है या न्यायालय की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है, तो यह आपराधिक अवमान कहलाती है।
- इसमें न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले शब्दों, कृत्यों या लेखों को भी शामिल किया जाता है।
26. बार-बेंच संबंध (Bar-Bench Relation):
- बार (अधिवक्ता) और बेंच (न्यायाधीश) न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं।
- दोनों के बीच अच्छा संबंध न्याय की निष्पक्षता और प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक है।
- अधिवक्ता को न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए, और न्यायाधीशों को अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए।
27. अधिवक्ता का मुवक्किल के प्रति कर्तव्य (Duties of an Advocate towards Client):
- मुवक्किल के हितों की रक्षा करना और सही कानूनी परामर्श देना।
- मुवक्किल की सूचना गोपनीय रखना।
- न्यायालय में मुवक्किल के मामले को पूरी निष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ प्रस्तुत करना।
- मुवक्किल से उचित और पारदर्शी फीस लेना।
28. राज्य विधिज्ञ परिषद (State Bar Council):
- यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह राज्य में अधिवक्ताओं के पंजीकरण और अनुशासन को नियंत्रित करता है।
- यह कानूनी शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने का कार्य करता है।
29. व्यावसायिक कदाचार के लिए दंड (Punishment for Professional Misconduct):
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल किसी भी अधिवक्ता के व्यावसायिक कदाचार की स्थिति में निम्नलिखित दंड दे सकती हैं:
- चेतावनी (Warning)
- अस्थायी रूप से नामांकन निलंबन (Suspension)
- स्थायी रूप से नामांकन रद्द करना (Disbarment)
30. अधिवक्ताओं द्वारा अवमानना (Contempt by Advocates):
- यदि कोई अधिवक्ता न्यायालय के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, न्यायाधीशों को धमकाता है, या उनके आदेशों की अवहेलना करता है, तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाती है।
31. न्यायाधीशों द्वारा अवमानना (Contempt by Judges):
- यदि कोई न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है या अनुचित व्यवहार करता है, तो उस पर भी न्यायालय की अवमानना का मामला चल सकता है।
- न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
32. भारतीय विधिज्ञ परिषद की अपीलीय शक्तियाँ (Appellate Powers of the Bar Council of India):
- यह राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है।
- अधिवक्ताओं के अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति रखती है।
33. अनुशासन समिति की शक्तियाँ (Powers of Disciplinary Committee):
- यह अधिवक्ताओं द्वारा किए गए व्यावसायिक कदाचार की जांच करती है।
- दोषी पाए जाने पर अधिवक्ता को चेतावनी, निलंबन या नामांकन रद्द करने का आदेश दे सकती है।
34. विधिक सहायता समिति (Legal Aid Committee):
- यह गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए गठित की जाती है।
- संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सरकार यह सेवा प्रदान करती है।
35. अनुशासन समिति (Disciplinary Committee):
- यह बार काउंसिल द्वारा गठित एक समिति होती है जो अधिवक्ताओं के आचरण से संबंधित शिकायतों की जांच करती है।
- दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।
36. विधिक शिक्षा समिति (Legal Education Committee):
- यह समिति कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और विधि विश्वविद्यालयों की मान्यता तय करने का कार्य करती है।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करती है।
37. सिविल अवमानना (Civil Contempt):
- यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता या उसकी अवज्ञा करता है, तो इसे सिविल अवमानना कहा जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय के आदेशों को लागू कराना होता है।
38. सिविल अवमान में प्रतिरक्षाएँ (Defences in Civil Contempt):
निम्नलिखित प्रतिरक्षाएँ (defences) सिविल अवमान में उपलब्ध होती हैं:
- आज्ञाकारी प्रयास (Bonafide Attempt): यदि व्यक्ति ने न्यायालय के आदेश का पालन करने का पूरा प्रयास किया हो।
- असंभवता (Impossibility): यदि आदेश का पालन करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो।
- गलत व्याख्या (Misinterpretation): यदि आदेश की गलत व्याख्या के कारण पालन नहीं हुआ हो।
- निष्क्रियता (Lack of Knowledge): यदि व्यक्ति को आदेश की जानकारी न हो।
39. न्यायालय अवमान के लिए दंड (Punishment for Contempt of Court):
- अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत, न्यायालय की अवमानना के लिए निम्न दंड हो सकते हैं:
- अधिकतम छह महीने की कारावास।
- अधिकतम ₹2,000 का जुर्माना।
- न्यायालय चाहे तो माफी स्वीकार कर सकता है और दंड को समाप्त कर सकता है।
40. विधि स्नातक (Law Graduates):
- वे व्यक्ति जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. (LL.B.) की डिग्री प्राप्त की हो।
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, विधि स्नातक बार काउंसिल में नामांकन के बाद अधिवक्ता बन सकते हैं।
41. राज्य नामावली (State Roll):
- प्रत्येक राज्य बार काउंसिल द्वारा उस राज्य में पंजीकृत अधिवक्ताओं की सूची।
- अधिवक्ता अपने राज्य की सूची में पंजीकरण के बाद ही न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
42. नामांकन प्रमाण पत्र (Certificate of Enrolment):
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र, जो किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत करता है।
43. विधि का शासन (Rule of Law):
- इसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और सभी नागरिकों (सामान्य व्यक्ति से लेकर शासक तक) को कानून का पालन करना आवश्यक है।
- यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) में निहित है।
44. क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश अपील योग्य होता है? (Is the Order Passed by the Disciplinary Committee of Bar Council of India Appealable?):
- हाँ, भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य होता है।
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 38 के तहत यह प्रावधान दिया गया है।
45. क्या भारत के महान्यायवादी को अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार है? (Does the Attorney General of India Have the Right of Pre-audience Over All Other Advocates?):
- हाँ, भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) को सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
- यह विशेषाधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) में उल्लिखित है।
46. क्या किसी अधिवक्ता के लिए अपना विज्ञापन करना प्रतिबंधित है? (Is Self-Advertisement for a Lawyer Forbidden?):
- हाँ, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत अधिवक्ताओं को स्वयं का विज्ञापन करने की अनुमति नहीं है।
- यह प्रतिबंध अधिवक्ता की गरिमा बनाए रखने और पेशेवर नैतिकता (Professional Ethics) की रक्षा के लिए लगाया गया है।
47. किन मामलों में अवमानना दंडनीय नहीं होती है? (What Are the Cases Where Contempt Is Not Punishable?):
निम्नलिखित मामलों में अवमानना दंडनीय नहीं होती:
- सत्य का प्रतिपादन (Truth as a Defence): यदि बयान सत्य है और लोकहित में दिया गया है।
- इच्छाकृत न होना (Unintentional Act): यदि अवमानना अनजाने में हुई हो।
- अच्छे आचरण के साथ माफी (Apology with Good Conduct): यदि अवमानना करने वाला न्यायालय से ईमानदारीपूर्वक माफी मांग ले।
48. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee):
- यह समिति राज्य बार काउंसिल और भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रशासनिक कार्यों को संभालती है।
- यह वित्तीय मामलों, कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती है।
49. विशेष समिति का गठन (Constitution of Special Committee):
- किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित अस्थायी समिति।
- उदाहरण: यदि राज्य बार काउंसिल भंग कर दी जाए, तो विशेष समिति का गठन कर उसका कार्यभार संभाला जाता है।
50. विधिक परामर्श (Legal Advice):
- विधिक परामर्श का अर्थ है किसी अधिवक्ता या कानूनी विशेषज्ञ द्वारा दिए गए कानूनी सुझाव या मार्गदर्शन।
- यह परामर्श विभिन्न कानूनी मामलों जैसे संविदा, संपत्ति विवाद, आपराधिक मामले, दीवानी मामले, कर कानून, परिवार कानून आदि से संबंधित हो सकता है।
- अधिवक्ता को अपनी विधिक परामर्श सेवाओं में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और मुवक्किल के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
51. नामांकन के लिए निरर्हता (Disqualification for Enrolment):
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत, निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हो सकता:
- अपराध का दोषी (Convicted for a Crime): यदि किसी व्यक्ति को नैतिक पतन (Moral Turpitude) से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
- मानसिक अयोग्यता (Mental Incapacity): यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है और न्यायालय ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया हो।
- सरकारी नौकरी में होना (Engaged in Other Profession): यदि व्यक्ति किसी अन्य लाभ के पद (Government Job) पर कार्यरत हो, सिवाय इसके कि बार काउंसिल ने उसे अनुमति दी हो।
- अन्यायपूर्ण आचरण (Misconduct): यदि व्यक्ति पर गंभीर व्यावसायिक कदाचार (Professional Misconduct) के आरोप सिद्ध हो चुके हों।
- न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित (Declared Insolvent): यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित किया गया हो और अभी तक पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त न की हो।