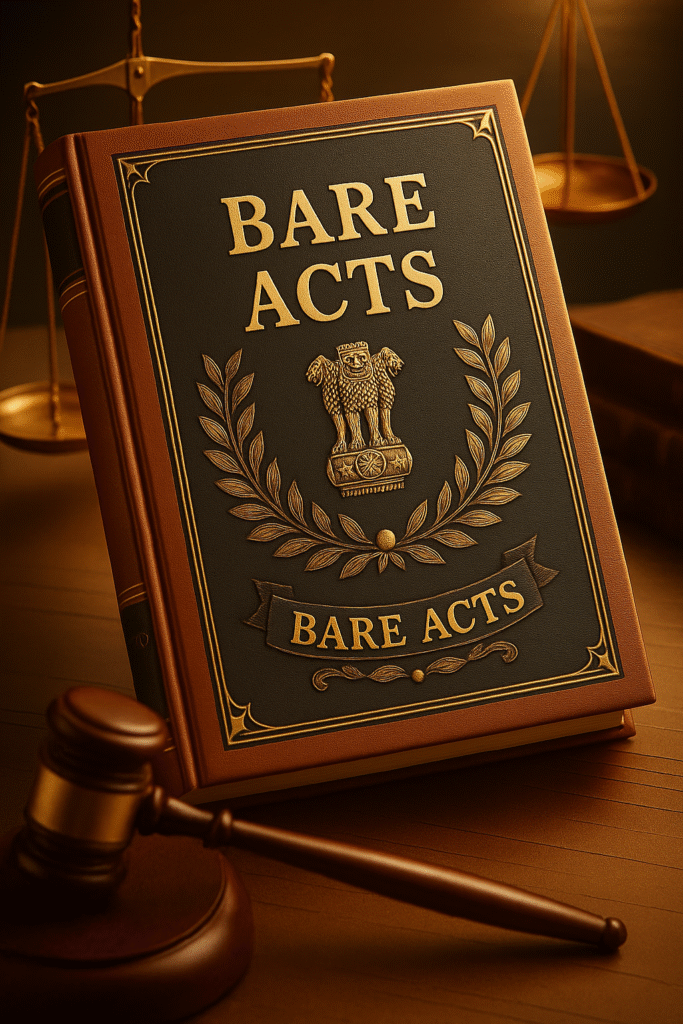वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
प्रस्तावना
वायु मानव जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी जल और भोजन। शुद्ध वायु के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। परंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन साधनों की वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण वायु प्रदूषण आज सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुका है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या और उद्योग दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, वायु प्रदूषण स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और जलवायु पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 बनाया।
अधिनियम की पृष्ठभूमि
- वैश्विक संदर्भ – 1972 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया गया। भारत भी इस सम्मेलन में सहभागी था और उसने वायु प्रदूषण रोकने के लिए विशेष कानून बनाने का वचन दिया।
- राष्ट्रीय संदर्भ – 1970 के दशक में भारत में औद्योगिक प्रदूषण तेजी से बढ़ा। विशेषकर बड़े नगरों में वायु गुणवत्ता लगातार गिरती गई।
- संवैधानिक आधार – 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 48A में राज्य को और अनुच्छेद 51A(g) में नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा का दायित्व सौंपा गया।
- नियामक ढाँचा – जल प्रदूषण रोकने के लिए पहले से जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 था। उसी की तर्ज पर वायु प्रदूषण रोकने हेतु यह अधिनियम बनाया गया।
अधिनियम का उद्देश्य
वायु अधिनियम, 1981 का मुख्य उद्देश्य है:
- वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी करना।
- वायु गुणवत्ता मानक (Air Quality Standards) निर्धारित करना।
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और वाहनों को नियंत्रित करना।
- केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सशक्त बनाना।
- नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना।
अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ
- वायु (Air): इसमें वायुमंडल के समस्त परतें आती हैं।
- वायु प्रदूषण (Air Pollution): वायु में किसी प्रदूषक पदार्थ की उपस्थिति जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- प्रदूषक (Pollutant): ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो वायु की संरचना को बिगाड़कर जीवन एवं पर्यावरण को हानि पहुँचाए।
- प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र (Air Pollution Control Area): वह क्षेत्र जिसे राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित करती है।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना –
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)।
ये बोर्ड वायु गुणवत्ता बनाए रखने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र –
राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को “वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र” घोषित कर सकती हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों और वाहनों पर कड़े मानक लागू होते हैं। - औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण –
किसी भी औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लिए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। - वायु गुणवत्ता मानक –
बोर्डों को वायु प्रदूषण की सीमा तय करने और नियमित निगरानी करने का अधिकार है। - निरीक्षण और नमूना लेने की शक्ति –
बोर्डों को कारखानों, वाहनों और प्रदूषण स्रोतों का निरीक्षण करने और नमूने लेने का अधिकार है। - प्रदूषण नियंत्रण उपकरण –
उद्योगों को प्रदूषण कम करने हेतु उपकरण लगाने और उनका नियमित रखरखाव करने का दायित्व दिया गया।
अधिनियम के तहत बोर्डों के कार्य
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):
- वायु गुणवत्ता मानक तैयार करना।
- राज्यों को मार्गदर्शन देना।
- अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की तकनीक विकसित करना।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB):
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करना।
- उद्योगों और कारखानों से अनुमति लेना और उनका निरीक्षण करना।
- स्थानीय स्तर पर प्रदूषण रोकने के उपाय करना।
- जनता को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करना।
दंडात्मक प्रावधान
- अधिनियम का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- अपराध जारी रहने पर अतिरिक्त दंड लगाया जाता है।
- यदि उद्योग या व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करता, तो सरकार उद्योग बंद भी कर सकती है।
अधिनियम का महत्व
- पहला व्यापक वायु कानून – भारत में यह पहला बड़ा कानून है जिसने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान दिए।
- कानूनी ढाँचा – इस अधिनियम ने CPCB और SPCB को कानूनी अधिकार प्रदान किए।
- स्वास्थ्य संरक्षण – शुद्ध वायु सुनिश्चित कर यह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है।
- सतत विकास – औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन लाने का प्रयास।
- न्यायिक सहयोग – न्यायालयों ने भी इस अधिनियम को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
अधिनियम की आलोचना
- कार्यान्वयन की कमजोरी – कई बार बोर्ड उद्योगों और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती नहीं कर पाते।
- राज्यों की सीमित क्षमता – राज्य प्रदूषण बोर्डों के पास संसाधनों और तकनीक की कमी रहती है।
- जनसहभागिता का अभाव – नागरिकों की प्रत्यक्ष भूमिका अधिनियम में बहुत कम है।
- वाहनों से होने वाला प्रदूषण – अधिनियम मुख्यतः उद्योगों पर केंद्रित है, जबकि वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका सीमित है।
न्यायालयों की भूमिका
भारतीय न्यायपालिका ने इस अधिनियम की व्याख्या करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं:
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) – दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए।
- सुब्रमण्यम बालाजी केस – न्यायालय ने वायु प्रदूषण को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जोड़ा।
- ताज त्रेपेजियम केस – ताजमहल क्षेत्र में प्रदूषण रोकने हेतु उद्योगों को गैस आधारित ईंधन अपनाने का आदेश।
निष्कर्ष
वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 भारत में पर्यावरणीय कानूनों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्डों को अधिकार दिए। हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे संसाधनों की कमी, जनसहभागिता का अभाव और प्रशासनिक ढिलाई। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए इस अधिनियम को और मजबूत करने, जनसहभागिता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि उद्योग, नागरिक और न्यायपालिका तीनों को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि भावी पीढ़ियों को शुद्ध वायु मिल सके।