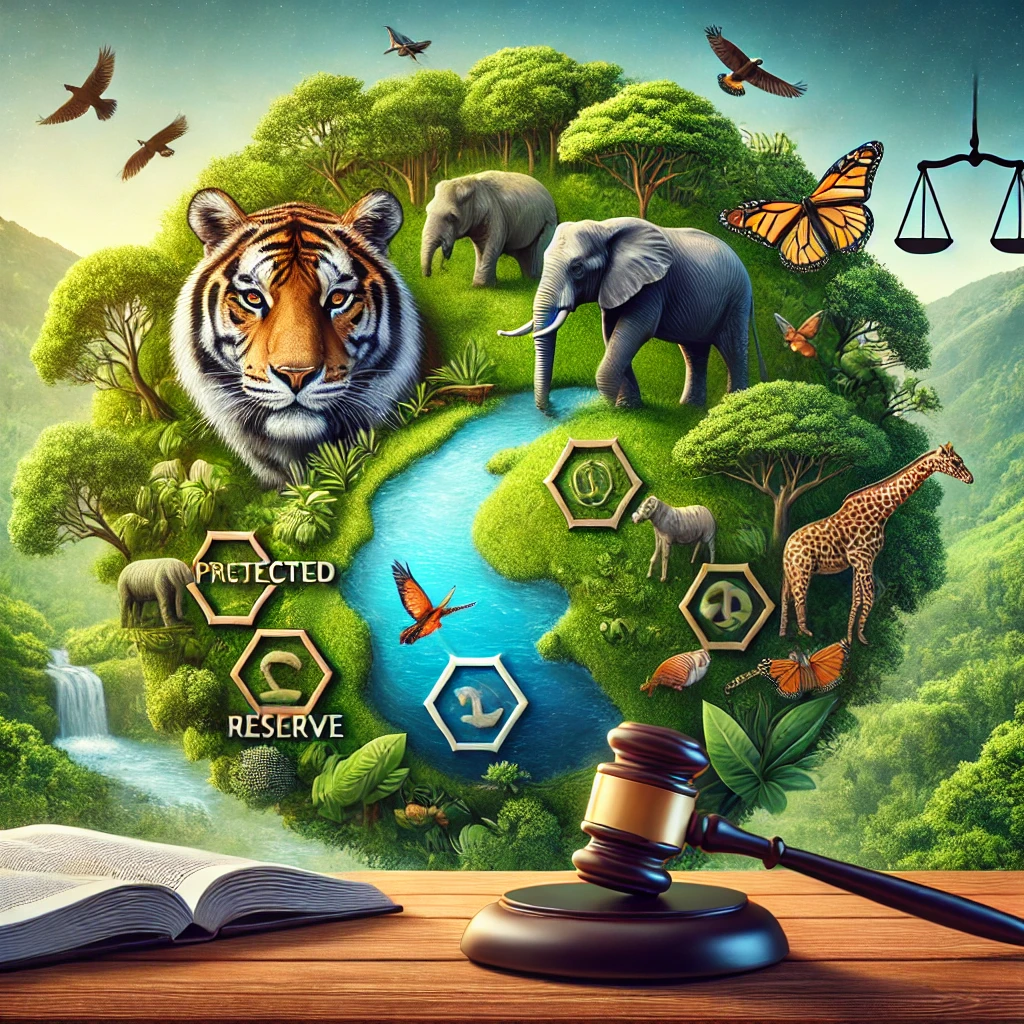वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) : विस्तृत लेख
1. प्रस्तावना
वन्यजीव (Wildlife) केवल जंगलों में रहने वाले पशु-पक्षी ही नहीं, बल्कि वनस्पतियाँ, सूक्ष्म जीव, जलीय जीव और प्राकृतिक आवास का वह पूरा तंत्र है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। इनका संरक्षण न केवल जैव विविधता (Biodiversity) के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक अस्तित्व से भी जुड़ा है।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शिकार, अवैध व्यापार, वन कटाई और औद्योगिक विस्तार के कारण वन्यजीवों की संख्या में भारी गिरावट आई। कई प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर पहुँच गईं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 लागू किया, जो आज भी देश में वन्यजीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए मुख्य कानून है।
2. अधिनियम की पृष्ठभूमि
- संवैधानिक आधार – संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य को पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा करने का निर्देश और अनुच्छेद 51A(g) में प्रत्येक नागरिक को इसका कर्तव्य बताया गया है।
- 1960 और 1970 के दशक में शिकार के कारण बाघ, हाथी, गैंडा और कई पक्षी प्रजातियों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुँच गई।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) जैसे समझौते में भारत की भागीदारी ने वन्यजीव संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता को बल दिया।
3. अधिनियम का उद्देश्य
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के मुख्य उद्देश्य हैं –
- देश के वन्यजीवों और वनस्पतियों की रक्षा करना।
- जैव विविधता का संरक्षण।
- अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार पर रोक।
- राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और अभयारण्य क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन।
- अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण दायित्वों का पालन।
4. अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- संपूर्ण भारत में लागू – जम्मू-कश्मीर (अब केंद्रशासित प्रदेश) में भी संशोधन के बाद लागू।
- वन्यजीव संरक्षण के छह अनुसूचियाँ (Schedules) –
- अनुसूची I और II (भाग II) – अति संरक्षित प्रजातियाँ, इनके शिकार पर सबसे सख्त दंड।
- अनुसूची III और IV – संरक्षित प्रजातियाँ, दंड थोड़ा कम।
- अनुसूची V – हानिकारक मानी जाने वाली प्रजातियाँ, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।
- अनुसूची VI – संरक्षित वनस्पतियाँ, जिनका उन्मूलन या व्यापार वर्जित है।
- राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य –
- केंद्र और राज्य सरकार को अधिकार कि वे विशेष क्षेत्रों को National Park, Wildlife Sanctuary, Conservation Reserve या Community Reserve घोषित कर सकें।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) – अवैध वन्यजीव व्यापार की रोकथाम और जांच के लिए।
5. अधिनियम के अंतर्गत दंड प्रावधान
- अनुसूची I और II (भाग II) की प्रजातियों का शिकार – पहली बार अपराध पर 3 से 7 वर्ष का कारावास और ₹10,000 या उससे अधिक जुर्माना।
- बार-बार अपराध पर दंड और अवधि और बढ़ सकती है।
- संरक्षित वनस्पतियों के विनाश पर भी कठोर सजा।
6. अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित क्षेत्र
- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) – पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र, मानव गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण।
- वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) – कुछ नियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ अनुमत।
- अभयारण्य आरक्षित (Conservation Reserves) – स्थानीय समुदाय और सरकार के संयुक्त प्रबंधन में।
- सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र (Community Reserves) – स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित।
7. संशोधन
- 1991 संशोधन – पर्यावरण और वन्यजीव अपराधों के दंड को कठोर बनाया।
- 2002 संशोधन – संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व की अवधारणा जोड़ी।
- 2006 संशोधन – बाघ संरक्षण के लिए National Tiger Conservation Authority (NTCA) की स्थापना।
- 2022 संशोधन – अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप और अधिक सख्ती, वन्यजीव व्यापार पर नियंत्रण।
8. अधिनियम के लाभ
- शिकार और अवैध व्यापार में कमी।
- बाघ, गैंडा, मगरमच्छ जैसी प्रजातियों की संख्या में सुधार।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता मजबूत हुई।
- संरक्षित क्षेत्रों की संख्या और क्षेत्रफल में वृद्धि।
9. अधिनियम की सीमाएँ और चुनौतियाँ
- मानव-वन्यजीव संघर्ष – गाँवों और जंगलों की सीमाओं पर बढ़ते टकराव।
- शिकार और तस्करी के नए तरीके – आधुनिक हथियार और तकनीक से अपराध।
- जन भागीदारी की कमी – कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को साथ नहीं लिया जाता।
- अपर्याप्त संसाधन – वन रक्षकों के पास तकनीकी और वित्तीय कमी।
10. प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप
- सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल लॉ, WWF बनाम भारत संघ – सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्रों में खनन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई।
- गोदावर्मन थिरुमुलपद केस – वन क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश।
11. निष्कर्ष
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 ने भारत में वन्यजीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया है। इसने न केवल कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया बल्कि जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई।
हालाँकि, इसे और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, तकनीकी संसाधनों का उपयोग, सख्त प्रवर्तन और सतत विकास की नीति अपनाना आवश्यक है।