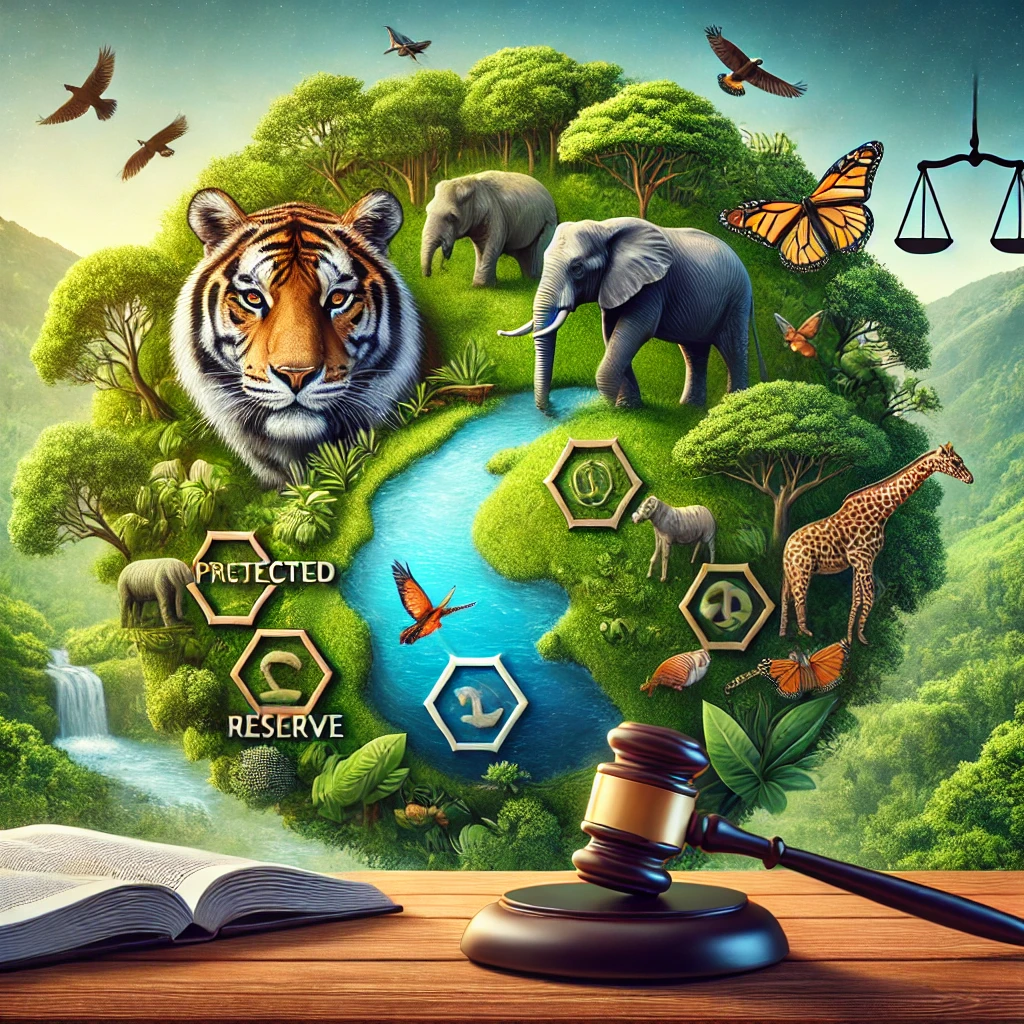वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 : जैव विविधता की सुरक्षा और संवैधानिक दायित्व
प्रस्तावना
भारत प्राचीन काल से ही जैव विविधता और वन्यजीवों का धनी देश रहा है। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर समुद्री तटों तक, यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु, पक्षी, सरीसृप और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। किंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों की अंधाधुंध कटाई तथा शिकार के कारण कई प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर पहुँच गईं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (The Wildlife Protection Act, 1972) लागू किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों का विकास तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।
अधिनियम की पृष्ठभूमि
1972 से पूर्व भारत में अलग-अलग राज्यों के पास अपने-अपने शिकार और वन्यजीव कानून थे। इनके अंतर्गत सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी और कई राज्यों में कठोर दंड प्रावधान भी नहीं थे। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। इसी के बाद भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 को पारित किया। यह अधिनियम प्रारंभ में केवल 5 अनुसूचियों (Schedules) के साथ आया था, लेकिन बाद में इसमें कई संशोधन किए गए।
अधिनियम के उद्देश्य
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा करना।
- संरक्षित क्षेत्रों – राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व – का गठन।
- शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण।
- लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान।
- केंद्र और राज्य सरकारों को संरक्षण संबंधी अधिकार प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों (जैसे CITES) के अनुरूप वन्यजीवों की रक्षा करना।
अधिनियम की संरचना
यह अधिनियम 66 धाराओं और 6 अनुसूचियों (Schedules) में विभाजित है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
1. परिभाषाएँ (धारा 2)
इस धारा में ‘अभयारण्य’, ‘राष्ट्रीय उद्यान’, ‘वन्य जीव’, ‘शिकार’, ‘ट्रॉफी’, ‘आयुध’, आदि की विस्तृत परिभाषाएँ दी गई हैं।
2. शिकार पर प्रतिबंध (धारा 9 से 12)
- किसी भी अनुसूची I या II के पशु का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- अनुसूची III और IV के पशुओं का शिकार केवल विशेष परिस्थितियों (मानव जीवन की सुरक्षा, फसलों की हानि आदि) में अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।
- अनुसूची V में उल्लिखित प्रजातियाँ ‘हानिकारक जीव’ मानी जाती हैं, जिनका शिकार किया जा सकता है।
- अनुसूची VI में कुछ दुर्लभ वनस्पतियाँ आती हैं जिनका उखाड़ना या नष्ट करना निषिद्ध है।
3. संरक्षित क्षेत्र
अधिनियम में निम्न संरक्षित क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है –
- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) – जहाँ वनस्पति और जीवों को पूर्ण सुरक्षा मिलती है और कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की जा सकती।
- अभयारण्य (Sanctuaries) – इनमें अनुसंधान, शिक्षा और सीमित पर्यटन की अनुमति दी जा सकती है।
- संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व – 2002 संशोधन द्वारा जोड़े गए, जिनमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संरक्षण किया जाता है।
4. व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधि पर प्रतिबंध (धारा 39 से 49)
- वन्यजीवों की खाल, हड्डी, दाँत, सींग आदि का व्यापार अवैध है।
- किसी भी ट्रॉफी, शिकार वस्तु या जंगली जानवर की खरीद-बिक्री पर रोक।
- अपराधियों पर कड़ा दंड और कारावास।
5. दंड प्रावधान (धारा 51)
- प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तक की कैद और ₹25,000 तक का जुर्माना।
- लुप्तप्राय प्रजातियों के मामले में 7 वर्ष तक की कैद और ₹25,000 से अधिक का जुर्माना।
- पुनरावृत्ति पर और भी कठोर दंड।
अनुसूचियाँ (Schedules) का महत्व
- अनुसूची I एवं II – अति दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियाँ (जैसे शेर, बाघ, गैंडा, हाथी)। इन पर सर्वाधिक सुरक्षा।
- अनुसूची III एवं IV – अन्य संरक्षित जीव, जिन पर भी कुछ सुरक्षा दी गई है।
- अनुसूची V – हानिकारक जीव (जैसे चूहा, कौआ, चमगादड़), जिनका शिकार किया जा सकता है।
- अनुसूची VI – संरक्षित वनस्पतियाँ (जैसे लोटस, ब्लू पीपर)।
अधिनियम के संशोधन
- 1991 संशोधन – शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध और अनुसूचियों का पुनर्गठन।
- 2002 संशोधन – ‘राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड’ एवं ‘राज्य वन्यजीव बोर्ड’ का गठन। साथ ही संरक्षण एवं सामुदायिक रिज़र्व की स्थापना।
- 2006 संशोधन – ‘राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण’ और ‘बाघ संरक्षण रिज़र्व’ की स्थापना।
- 2022 संशोधन – अंतर्राष्ट्रीय समझौतों (CITES) के अनुरूप और अधिक कड़े प्रावधान।
राष्ट्रीय और राज्य वन्यजीव बोर्ड
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह नीति निर्माण, योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करता है।
- राज्य वन्यजीव बोर्ड राज्य स्तर पर संरक्षण गतिविधियों का संचालन करता है।
न्यायालयीन दृष्टांत
- T.N. Godavarman v. Union of India (1997) – सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों के महत्व पर बल दिया।
- Centre for Environmental Law v. Union of India (2013) – विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु सरकार को कड़े कदम उठाने का निर्देश।
- K.M. Chinnappa v. Union of India (2002) – अदालत ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है।
महत्व और प्रभाव
- भारत में लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान और 564 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित हो चुके हैं।
- बाघ, गैंडा, मगरमच्छ और शेर जैसी प्रजातियों की संख्या में सुधार हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार पर्यावरणीय राष्ट्र के रूप में उभरी है।
चुनौतियाँ
- अवैध शिकार (Poaching) और वन्यजीव तस्करी।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष।
- वनों की कटाई और आवास का विनाश।
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी का अभाव।
- कानून के क्रियान्वयन में ढिलाई और भ्रष्टाचार।
निष्कर्ष
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत के पर्यावरणीय कानूनों की नींव है। इसने न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। यद्यपि चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन जन-जागरूकता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और कड़े कानून प्रवर्तन के माध्यम से भारत अपने समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रख सकता है। यह अधिनियम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को स्वस्थ प्रकृति देने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
प्रश्न 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 कब और क्यों लागू किया गया?
उत्तर: यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। इसका मुख्य कारण वन्यजीवों की तेजी से हो रही हानि, अवैध शिकार और वनों की कटाई था। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों के अपने-अपने कानून थे, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इसी के परिणामस्वरूप भारत ने एक केंद्रीय कानून बनाया। अधिनियम का उद्देश्य वन्यजीवों और वनस्पतियों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना तथा जैव विविधता को संरक्षित करना है।
प्रश्न 2. इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
उत्तर: अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य वन्यजीवों और उनके आवास की रक्षा करना है। इसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को सुरक्षित रखना, शिकार पर नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रों का गठन और अवैध व्यापार पर रोक लगाना शामिल है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को संरक्षण संबंधी अधिकार दिए गए हैं। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे CITES के अनुरूप भी है। मूल रूप से इसका मकसद जैव विविधता का संरक्षण करके पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना और भावी पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना है।
प्रश्न 3. अधिनियम में शिकार पर क्या प्रावधान हैं?
उत्तर: अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अनुसूची I और II में सूचीबद्ध जीवों का शिकार पूर्णतः निषिद्ध है। केवल विशेष परिस्थितियों में – जैसे मानव जीवन की रक्षा, फसलों को नुकसान या बीमारी फैलाने पर – राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। अनुसूची III और IV के जीवों के शिकार पर भी नियंत्रण है। केवल अनुसूची V के जीव (हानिकारक प्रजातियाँ जैसे चूहा, कौआ आदि) शिकार योग्य हैं। इस प्रकार कानून ने शिकार पर कठोर नियंत्रण लगाया है ताकि प्रजातियों का संरक्षण हो सके।
प्रश्न 4. राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है?
उत्तर: राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्यजीवों और वनस्पतियों की रक्षा हेतु किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि, शिकार या वनों की कटाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ पूर्ण सुरक्षा दी जाती है। अभयारण्य भी संरक्षित क्षेत्र हैं, परंतु इनमें कुछ सीमित गतिविधियाँ जैसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा अनुमति से हो सकती हैं। दोनों का उद्देश्य संरक्षण है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान अधिक कठोर और सुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं।
प्रश्न 5. अनुसूचियों (Schedules) का क्या महत्व है?
उत्तर: अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची I और II में लुप्तप्राय प्रजातियाँ (जैसे शेर, बाघ, गैंडा) शामिल हैं, जिनको सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। अनुसूची III और IV में अन्य संरक्षित जीव हैं। अनुसूची V में हानिकारक जीव सूचीबद्ध हैं, जिनका शिकार किया जा सकता है। अनुसूची VI में संरक्षित वनस्पतियाँ (जैसे कुछ दुर्लभ पौधे) हैं। अनुसूचियों का महत्व यह है कि इनके आधार पर प्रत्येक प्रजाति की सुरक्षा का स्तर तय होता है।
प्रश्न 6. इस अधिनियम के तहत कौन-से बोर्ड गठित किए गए हैं?
उत्तर: अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) और राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Boards for Wildlife) गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करता है। राज्य बोर्ड राज्य स्तर पर संरक्षण योजनाओं को लागू करता है। 2006 संशोधन द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी गठित किया गया, जो विशेष रूप से बाघों की रक्षा के लिए काम करता है।
प्रश्न 7. दंड प्रावधान क्या हैं?
उत्तर: अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष तक की कैद और ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि अपराध लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है तो सजा 7 वर्ष तक की कैद और ₹25,000 से अधिक जुर्माना हो सकता है। पुनरावृत्ति पर दंड और भी कठोर किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अवैध शिकार और व्यापार को रोकना है।
प्रश्न 8. 2002 और 2006 संशोधनों का महत्व क्या है?
उत्तर: 2002 संशोधन द्वारा संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व की व्यवस्था की गई। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य वन्यजीव बोर्डों का गठन हुआ। 2006 संशोधन में ‘राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण’ और ‘बाघ संरक्षण रिज़र्व’ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को बचाना था। इन संशोधनों ने अधिनियम को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी महत्व दिया।
प्रश्न 9. सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की व्याख्या में क्या भूमिका निभाई है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिनियम की व्याख्या की है। T.N. Godavarman v. Union of India (1997) मामले में कोर्ट ने कहा कि वन्यजीव और वन संरक्षण अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जुड़ा है। K.M. Chinnappa v. Union of India (2002) में भी कोर्ट ने संरक्षण को मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना। Centre for Environmental Law (2013) केस में कोर्ट ने सरकार को विलुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा हेतु सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया।
प्रश्न 10. इस अधिनियम के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?
उत्तर: अधिनियम के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अवैध शिकार और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सबसे बड़ी समस्या है। मानव-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है, जिससे दोनों को नुकसान होता है। वनों की कटाई और शहरीकरण से आवास नष्ट हो रहे हैं। स्थानीय समुदायों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से योजनाएँ विफल होती हैं। साथ ही कानून का सही क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रवर्तन भी बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटना वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक है।