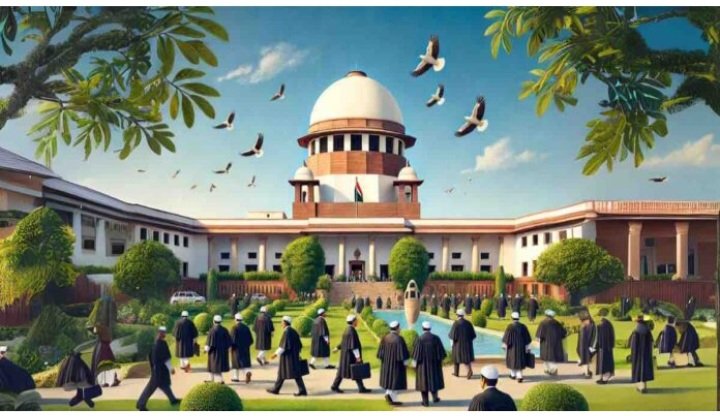वकीलों की हड़ताल : न्याय प्रणाली के भविष्य पर मंडराता खतरा
देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा असंतोष उभरकर सामने आया है। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आम जनता को न्याय की प्राप्ति में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वह तो दिख ही रही हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण कहीं अधिक गहरा और गंभीर है। यह केवल वकीलों का पुलिस के खिलाफ आंदोलन नहीं है, बल्कि न्याय प्रणाली की आत्मा को सुरक्षित रखने का संघर्ष है।
विवाद की जड़ : नया नोटिफिकेशन
दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अब पुलिसकर्मियों को अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे थाने या किसी निर्धारित स्थान से बैठकर तकनीकी माध्यमों के जरिए गवाही दे सकेंगे। पहली दृष्टि में यह कदम आधुनिक तकनीक को न्याय प्रणाली में शामिल करने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो इसके परिणाम न्याय के मूल सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हैं।
कानून की मंशा : क्यों पुलिस की गवाही को सीमित किया गया था?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की मूल भावना यह रही है कि पुलिस के समक्ष दिए गए बयान कोर्ट में admissible evidence नहीं माने जाएंगे। CrPC की धारा 161 (अब नए कानून BNSS की धारा 180) स्पष्ट करती है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
इसका कारण ऐतिहासिक है। ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस का गठन जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार के हितों को बनाए रखने के लिए किया गया था। पुलिस को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वह झूठे मुकदमे बनाकर, झूठी गवाहियाँ जुटाकर किसी भी निर्दोष को दोषी साबित कर सकती थी। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं और कानून निर्माताओं ने इस खतरे को भांपते हुए पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को अदालत में स्वीकार्य नहीं माना।
तकनीक के नाम पर खतरनाक प्रयोग
आज तकनीकी क्रांति का दौर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल सबूतों का महत्व बढ़ चुका है। इसी के बहाने सरकार ने पुलिस को भी सुविधा देने का प्रयास किया है। यदि पुलिसकर्मी थाने में ही बैठकर गवाही देंगे तो यह एक “आरामदायक विकल्प” उनके लिए अवश्य हो सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के लिए यह आत्मघाती कदम है।
समस्या कहाँ है?
- क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन की कमजोरी – अदालत में जब पुलिसकर्मी को वकील सवाल-जवाब करते हैं तो उसकी शारीरिक भाषा, उसकी हिचकिचाहट, उसकी आँखें चुराना या विरोधाभासी उत्तर सामने आ जाते हैं। लेकिन यदि वह सुरक्षित स्थान (थाने) में बैठकर बयान दे रहा है, तो उस पर वही दबाव नहीं होगा।
- सत्यता पर प्रश्न – कोर्ट का वातावरण गवाह को सच बोलने के लिए बाध्य करता है। वहीं थाने में बैठकर गवाही देना वैसा ही है जैसे किसी को किताब खोलकर मौखिक परीक्षा देने की छूट मिल जाए।
- निष्पक्षता पर चोट – पुलिस स्वयं ही अभियोजन पक्ष का अंग होती है। यदि वही अपने “आरामदायक माहौल” में गवाही देने लगे तो अभियुक्त के अधिकारों का हनन होगा।
न्याय प्रणाली पर संभावित प्रभाव
- निर्दोष व्यक्ति को सज़ा का खतरा – जब पुलिस की गवाही पर पर्याप्त शक किया ही नहीं जा सकेगा, तो निर्दोष व्यक्ति भी दोषी सिद्ध हो सकता है।
- विश्वसनीयता का संकट – न्यायालय की छवि समाज में तभी मजबूत रहती है जब वह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। यदि अदालतें केवल तकनीकी साधनों पर निर्भर होकर पुलिस के शब्दों को ही अंतिम मान लेंगी, तो लोगों का विश्वास टूटेगा।
- असमानता की खाई – अभियोजन पक्ष (Prosecution) के पास पहले से ही पर्याप्त साधन होते हैं, लेकिन अभियुक्त और उसके वकील सीमित संसाधनों में लड़ते हैं। नया प्रावधान अभियुक्त के अधिकारों को और कमजोर कर देगा।
वकीलों की हड़ताल : गलतफहमी का निवारण
यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वकीलों की यह हड़ताल पुलिसकर्मियों के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इस व्यवस्था का विरोध करना है, जिसके तहत न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन इसे वकील बनाम पुलिस का विवाद बताकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यह लड़ाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अभियुक्त के मौलिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है।
न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका : टकराव का नया आयाम
भारतीय संविधान के तीन स्तंभ—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए काम करते हैं। लेकिन जब कार्यपालिका (सरकार) न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है, तब टकराव अपरिहार्य हो जाता है। यह नोटिफिकेशन भी न्यायपालिका की स्वायत्तता पर एक आघात की तरह देखा जा रहा है।
समाधान क्या हो सकता है?
- नोटिफिकेशन पर पुनर्विचार – सरकार को इस निर्णय को वापस लेकर विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिए।
- तकनीक का संतुलित उपयोग – तकनीक का प्रयोग वहाँ होना चाहिए जहाँ न्याय की पारदर्शिता बनी रहे, जैसे गवाहों की सुरक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन पुलिस की गवाही हमेशा कोर्ट में प्रत्यक्ष होनी चाहिए।
- सुधार, न कि समझौता – यदि पुलिसकर्मियों का समय बचाना है तो अदालतों में “समर्पित गवाही दिवस” तय किए जा सकते हैं।
- जन-जागरूकता – आम जनता को यह समझना चाहिए कि यह केवल वकीलों का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न है।
निष्कर्ष : न्याय से समझौता नहीं
वकीलों की हड़ताल के पीछे जो असली वजह है, वह लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत गंभीर चेतावनी है। यह संघर्ष न तो केवल पुलिस के खिलाफ है और न ही केवल वकीलों का स्वार्थ। यह उस “न्याय की आत्मा” को बचाने की लड़ाई है, जहाँ निर्दोष को सज़ा न मिले और दोषी को कानून के मुताबिक दंड मिले।
यदि अदालतों में पुलिसकर्मी केवल थाने से बैठकर गवाही देंगे तो यह न्यायिक प्रक्रिया की नींव को ही हिला देगा। ऐसे में यह आंदोलन हमारे लोकतंत्र के लिए चेतावनी है कि तकनीकी सुविधा के नाम पर न्याय के सिद्धांतों से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।