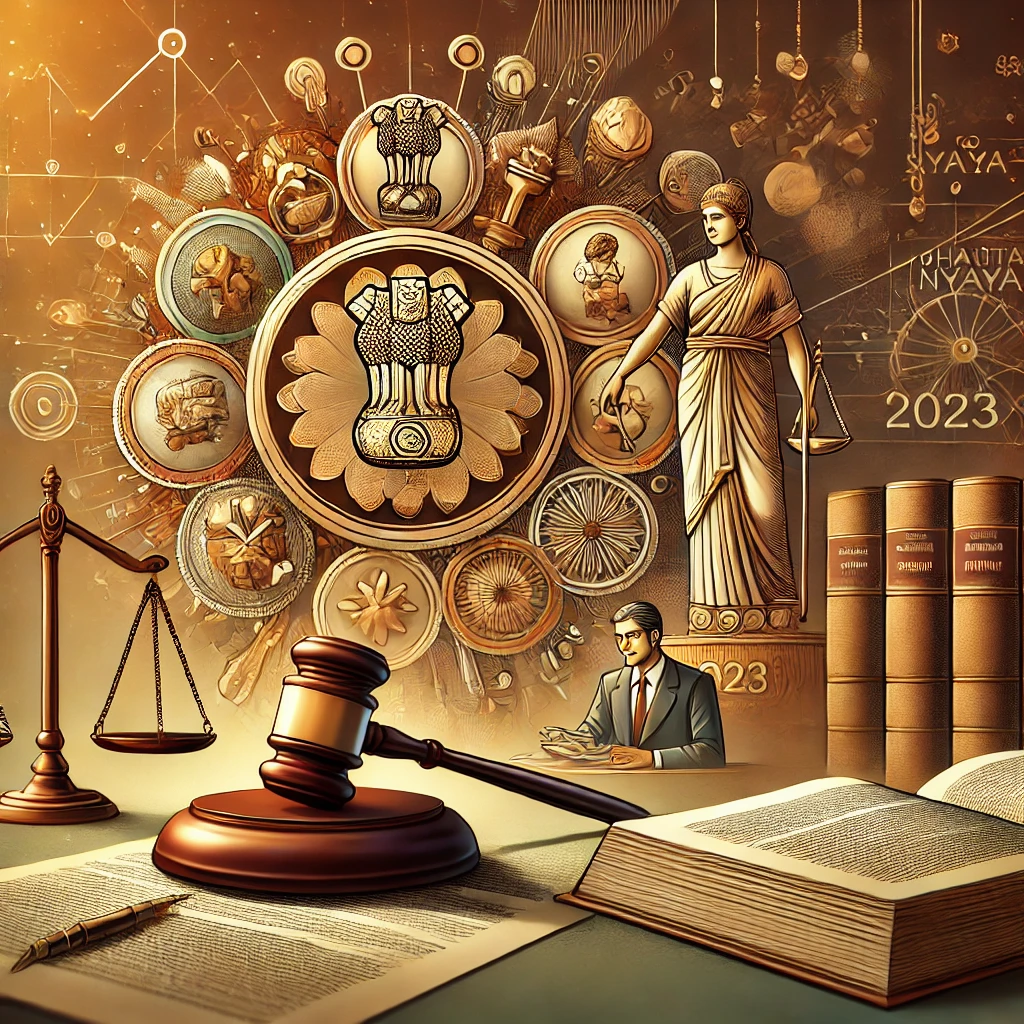लिव-इन रिलेशनशिप का कानूनी दृष्टिकोण: एक व्यापक विश्लेषण
परिचय:
भारतीय समाज में परंपरागत रूप से विवाह को ही सहवास का एकमात्र वैध और नैतिक रूप माना गया है। परंतु सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रभाव से जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है, जिसके फलस्वरूप “लिव-इन रिलेशनशिप” की अवधारणा धीरे-धीरे उभरकर सामने आई है। यह संबंध दो वयस्कों के बीच बिना विवाह के साथ रहने की व्यवस्था है, जो सहमति और स्वतंत्रता पर आधारित होती है। यद्यपि यह अवधारणा सामाजिक रूप से विवादित रही है, परंतु भारतीय न्यायपालिका ने इसे कुछ सीमाओं के भीतर कानूनी स्वीकृति प्रदान की है।
लिव-इन रिलेशनशिप की परिभाषा:
लिव-इन रिलेशनशिप को किसी विशेष अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय न्यायालयों ने इसे निम्न रूप में व्याख्यायित किया है:
“एक ऐसा संबंध जिसमें एक पुरुष और एक महिला, बिना विवाह किए, एक विवाहित दंपत्ति की तरह सहमति से एक साथ रहते हैं।”
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:
- इंदिरा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013) 15 SCC 755:
सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि लिव-इन रिलेशनशिप ‘घरेलू संबंध’ (domestic relationship) की परिभाषा में आ सकती है यदि संबंध दीर्घकालिक, सहमति पर आधारित और विवाह के समान प्रतीत हो। इस निर्णय में कोर्ट ने विभिन्न प्रकार के लिव-इन संबंधों को वर्गीकृत किया। - धनवल्ली बनाम राज्य (2010):
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है और यदि संबंध दीर्घकालिक हो तो महिला को ‘कानूनी पत्नी’ के समान संरक्षण मिल सकता है। - ललिता टोप्पो बनाम राज्य (2013, झारखंड HC):
कोर्ट ने माना कि लिव-इन में रह रही महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण प्राप्त हो सकता है। - सुभाष चंद्र बनाम भारती देवी (AIR 2016 SC):
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लिव-इन पार्टनर्स लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहते हैं तो उस महिला को वैवाहिक पत्नी के कुछ अधिकार मिल सकते हैं।
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में लिव-इन रिलेशनशिप:
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) में ‘घरेलू संबंध’ की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:
“एक ऐसा संबंध जिसमें दो लोग एक साथ एक साझा घरेलू जीवन व्यतीत करते हैं और वे रिश्तेदारी, विवाह, या विवाह के समान संबंध में रहते हैं।”
इस परिभाषा में ‘विवाह के समान संबंध’ (relationship in the nature of marriage) को शामिल किया गया है, जो लिव-इन रिलेशनशिप के कानूनी संरक्षण की आधारशिला रखता है।
लिव-इन रिलेशनशिप के मानदंड (Supreme Court द्वारा निर्धारित):
सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सरमा केस में निम्नलिखित बिंदुओं को विवाह के समान संबंध को मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण बताया:
- दोनों वयस्कों की सहमति।
- दीर्घकालिक सहवास।
- एक साझा घरेलू जीवन।
- सामाजिक स्वीकार्यता या प्रतीकात्मक मान्यता (जैसे पति-पत्नी की तरह रहना)।
- आर्थिक और सामाजिक निर्भरता।
लिव-इन रिलेशनशिप में उत्पन्न कानूनी प्रश्न:
- संतानों की वैधता:
सुप्रीम कोर्ट ने Tulsa & Ors. v. Durghatiya (2008) में स्पष्ट किया कि यदि माता-पिता दीर्घकालिक लिव-इन में रहे हैं, तो उस संबंध से उत्पन्न संतान को वैध माना जाएगा। - उत्तराधिकार अधिकार:
लिव-इन पार्टनर को उत्तराधिकार अधिनियमों में स्वत: पत्नी या पति के अधिकार नहीं मिलते, परंतु यदि संबंध विवाह के समान माना जाए, तो कुछ अधिकार मिल सकते हैं। - पालन-पोषण और भरण-पोषण:
यदि महिला को साबित होता है कि वह विवाह के समान संबंध में थी, तो वह भरण-पोषण की मांग कर सकती है। - धोखाधड़ी या दूसरी शादी की प्रकृति:
यदि पुरुष पहले से विवाहित है और किसी महिला से लिव-इन में रहता है, तो उसे ‘कन्याभग’ या धोखा देने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है।
लिव-इन रिलेशनशिप पर सामाजिक दृष्टिकोण:
यद्यपि कानून ने लिव-इन संबंधों को कुछ हद तक सुरक्षा दी है, फिर भी भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग इसे अनैतिक या अस्वीकार्य मानता है। परिवार, जाति, संस्कृति और धर्म जैसे कारकों के कारण इस संबंध को सार्वजनिक स्वीकार्यता अब भी सीमित है।
निष्कर्ष:
लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय कानून में एक जटिल, परंतु उभरती हुई अवधारणा है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक जीवनशैली को प्रतिबिंबित करता है, परंतु इसे सामाजिक और कानूनी रूप से पूरी तरह स्वीकार करने में अभी भी समय लगेगा। न्यायपालिका ने जिस संवेदनशीलता के साथ लिव-इन संबंधों को “विवाह के समान” मानते हुए कुछ सुरक्षा प्रदान की है, वह महिला अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रस्तावना:
लिव-इन रिलेशनशिप का कानूनन मान्यता प्राप्त करना भारत जैसे परंपरावादी देश में सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है।