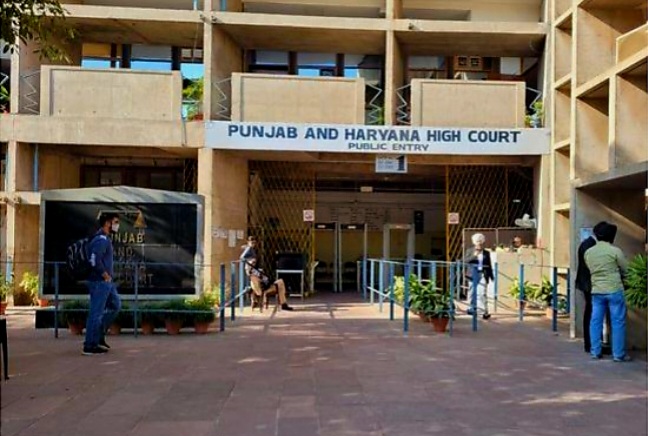‘यह संदिग्ध है कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति के आरोपियों पर लागू होता है’: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय और नियमित ज़मानत की स्वीकृति का विस्तृत विश्लेषण
भारत में जातिगत भेदभाव और उससे जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक सशक्त विधिक औजार है। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना और उनके साथ होने वाले अत्याचारों को कठोर दंड के माध्यम से रोकना है। लेकिन हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय इस कानून की प्रयोज्यता और सीमाओं पर गंभीर सवाल उठाता है।
22 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने एक ऐसे आरोपी को नियमित ज़मानत प्रदान की जो स्वयं अनुसूचित जाति (वंचित श्रेणी) से संबंध रखता है। अदालत ने माना कि जब आरोपी स्वयं एक अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है, तब यह विचारणीय है कि क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम उसके खिलाफ लागू हो सकता है।
यह निर्णय न केवल ज़मानत संबंधी सिद्धांतों बल्कि अत्याचार निवारण अधिनियम की व्याख्या से जुड़े जटिल प्रश्नों को सामने लाता है। इस लेख में हम इस मामले की पृष्ठभूमि, उच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ, बचाव एवं अभियोजन पक्ष के तर्क, अधिनियम की विधिक स्थिति और इस निर्णय के व्यापक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक प्राथमिकी से उपजा जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल बुंदेला उर्फ़ राहुल नामक युवक ने अपने सह-आरोपियों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, जातिसूचक गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ी गईं।
लेकिन इस प्राथमिकी से जुड़े दो महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने आए—
- गिरफ्तारी में देरी: प्राथमिकी दर्ज होने के 425 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
- अस्पष्ट आरोप: प्राथमिकी में सीधे तौर पर आरोपी पर जाति-आधारित अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया।
इन परिस्थितियों ने अदालत को मामले की गंभीरता और अभियोजन पक्ष के दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने को विवश किया।
आरोपी की जातिगत स्थिति और अधिनियम की प्रयोज्यता पर प्रश्न
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि आरोपी खटीक जाति से ताल्लुक रखता है जिसे हरियाणा सरकार ने वंचित अनुसूचित जाति घोषित किया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जब आरोपी स्वयं अनुसूचित जाति का सदस्य है तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएँ उसके खिलाफ लागू नहीं हो सकतीं।
न्यायालय ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए कहा:
“वैसे भी, वह वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में आता है और इस तरह, यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान उसके खिलाफ लागू होते हैं या नहीं?”
इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि अदालत ने कानून की विधिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई व्याख्या का द्वार खोला है।
विशिष्ट चोट और हथियार का अभाव
अभियोजन पक्ष की दलीलों का एक और कमजोर पहलू यह था कि आरोपी पर न तो किसी विशेष चोट पहुँचाने का आरोप था और न ही उसके पास किसी हथियार का होना सिद्ध हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि घटना में उसकी भूमिका सामान्य धारणाओं और सामूहिक आरोपों तक ही सीमित रही।
न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में उसे लगातार हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा।
हिरासत की अवधि और ज़मानत का अधिकार
याचिकाकर्ता 05 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने माना कि लंबी अवधि तक हिरासत में रखना, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और जब आरोपी की जातिगत स्थिति अधिनियम की प्रयोज्यता पर प्रश्न खड़े करती है, तो न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।
निचली अदालत की चूक
बचाव पक्ष के अधिवक्ता हर्ष जैन ने यह भी तर्क दिया कि निचली अदालत ने ज़मानत याचिका खारिज करते समय आरोपी की जातिगत स्थिति को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस चूक को गंभीर माना और कहा कि जातिगत स्थिति इस मामले का एक प्रमुख तत्व थी जिस पर विचार आवश्यक था।
न्यायालय का निर्णय
सभी तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को नियमित ज़मानत प्रदान की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि—
- यह ज़मानत मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना दी जा रही है।
- निर्णय केवल जातिगत स्थिति, हिरासत की अवधि, और आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
- ट्रायल जारी रहेगा और अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
विधिक विश्लेषण: क्या अधिनियम अनुसूचित जाति आरोपियों पर लागू हो सकता है?
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 मुख्यतः इन समुदायों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य इन वर्गों को संरक्षण प्रदान करना है, न कि इन्हीं वर्गों के सदस्यों को दंडित करना।
यदि कोई अनुसूचित जाति का सदस्य स्वयं अपने ही समुदाय के अन्य सदस्य पर जाति-आधारित अपमान करता है, तो क्या यह अधिनियम लागू होगा? इस प्रश्न का उत्तर विधायिका द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, और यही कारण है कि अदालत ने इसे “संदिग्ध” माना।
कानून की भाषा और उद्देश्य को देखते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि अधिनियम का मूल भाव अनुसूचित जातियों को सुरक्षा देना है, न कि उन्हीं पर लागू करना। हालांकि, यदि किसी अनुसूचित जाति सदस्य द्वारा अन्य अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य पर गंभीर अत्याचार किया जाता है, तो यह व्याख्या जटिल हो सकती है।
इस निर्णय के व्यापक प्रभाव
- कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता: यह मामला अधिनियम की प्रयोज्यता से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है। विधायिका या उच्चतम न्यायालय को भविष्य में इस मुद्दे पर स्पष्टता लानी होगी।
- ज़मानत संबंधी दृष्टिकोण: अदालत ने एक बार फिर यह दोहराया कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद। बिना ठोस साक्ष्यों और लंबे समय की हिरासत को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।
- सामाजिक प्रभाव: यह निर्णय अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर उत्पन्न होने वाले विवादों और झगड़ों में अधिनियम की सीमाओं को उजागर करता है।
- ट्रायल अदालतों के लिए संकेत: निचली अदालतों को ज़मानत अर्जी पर निर्णय देते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों, विशेषकर आरोपी की जातिगत स्थिति, पर गंभीरता से विचार करना होगा।
निष्कर्ष
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का यह निर्णय केवल एक आरोपी को ज़मानत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की व्याख्या और उसकी सीमाओं पर एक गहन बहस की ओर इशारा करता है।
जब आरोपी स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय से हो, तो क्या यह अधिनियम लागू होगा—यह प्रश्न अब विधिक विमर्श का विषय बन गया है। अदालत ने ज़मानत देते समय सावधानी बरतते हुए स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रही, बल्कि केवल आरोपी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राहत दे रही है।
यह निर्णय न्यायपालिका के उस दृष्टिकोण को रेखांकित करता है जिसमें न्याय केवल सख्त दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी के संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी को भी समान महत्व दिया जाता है।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णय
1. सुप्रीम कोर्ट – State of M.P. v. Ram Krishna Balothia (1995)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को विशेष संरक्षण देना है।
- इसमें स्पष्ट किया गया कि यह अधिनियम केवल उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर केंद्रित है।
- इस केस में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया।
👉 संबंध: यह केस बताता है कि अधिनियम का मूल उद्देश्य सुरक्षा है, न कि इन्हीं समुदायों पर दंड लगाना।
2. सुप्रीम कोर्ट – Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra (2018)
- अदालत ने माना कि अधिनियम का दुरुपयोग भी संभव है और इसलिए गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जाँच आवश्यक होनी चाहिए।
- हालाँकि बाद में संसद ने संशोधन करके इस फ़ैसले को आंशिक रूप से पलट दिया।
👉 संबंध: इस फैसले ने दिखाया कि न्यायपालिका अधिनियम की सीमाओं को लेकर पहले भी चिंतित रही है।
3. दिल्ली उच्च न्यायालय – Hitesh Verma v. State of Uttarakhand (2020, बाद में SC में)
- यहाँ प्रश्न था कि यदि दोनों पक्ष SC समुदाय से हैं, तो क्या अधिनियम लागू होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातिसूचक गालियाँ यदि सार्वजनिक स्थान पर हों और अपमान जातिगत कारणों से हो, तभी अधिनियम लागू होगा।
- यदि विवाद सिविल प्रकृति का है (जैसे ज़मीन-जायदाद) तो मात्र झगड़े में गाली देना स्वतः SC/ST Act के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।
👉 संबंध: यह सीधे उस बिंदु से जुड़ा है जिसे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उठाया—जब आरोपी भी SC समुदाय से है तो अधिनियम की प्रयोज्यता संदिग्ध हो जाती है।
4. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय – Kailash v. State of M.P. (2019)
- यहाँ आरोपी और पीड़ित दोनों SC समुदाय से थे।
- अदालत ने कहा कि केवल जाति का उल्लेख कर देने से SC/ST Act लागू नहीं हो जाता।
- यह देखना होगा कि अपमान का कारण जातिगत द्वेष था या केवल निजी विवाद।
👉 संबंध: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हालिया निर्णय इसी सोच को आगे बढ़ाता है।
5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय – Shyam Babu v. State of U.P. (2021)
- आरोपी भी SC समुदाय से था।
- अदालत ने कहा कि SC/ST Act केवल तब लागू होगा जब आरोपी की मंशा जातिगत अपमान की हो।
- यदि विवाद व्यक्तिगत दुश्मनी या सामान्य झगड़े का हो तो अधिनियम लागू नहीं होगा।
📌 तुलनात्मक विश्लेषण
- समानता: सभी अदालतों ने माना कि SC/ST Act का उद्देश्य जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देना है, और यदि आरोपी भी उसी जाति का है तो अधिनियम की प्रयोज्यता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।
- फर्क: सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक दिशा-निर्देश दिए (जैसे Hitesh Verma केस) जबकि उच्च न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों में तथ्यात्मक आधार पर निर्णय दिए।
- नवीनता (2025 का निर्णय): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मानत देते समय स्पष्ट कहा कि “यह संदिग्ध है कि अधिनियम आरोपी पर लागू होता भी है या नहीं”। यह टिप्पणी भविष्य में बड़े संवैधानिक विमर्श का कारण बन सकती है।
✅ निष्कर्ष
इस तुलना से यह स्पष्ट है कि:
- यदि आरोपी स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से है, तो अधिनियम की स्वचालित प्रयोज्यता संदिग्ध हो जाती है।
- न्यायालय मंशा (intention) और परिस्थिति (circumstances) पर ध्यान देता है—क्या सचमुच जातिगत द्वेष से अपराध हुआ, या केवल निजी विवाद था।
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय इस श्रृंखला की कड़ी है, लेकिन इसमें एक नई दृष्टि है कि लंबी हिरासत + अस्पष्ट आरोप + आरोपी की जातिगत स्थिति—इन सबका संयुक्त मूल्यांकन ज़मानत में निर्णायक है।