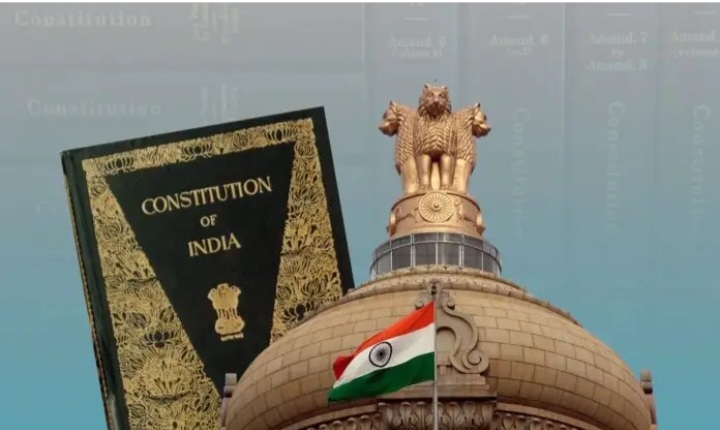मौलिक अधिकार बनाम राज्य की शक्तियाँ
परिचय
भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और साथ ही राज्य को इन अधिकारों की रक्षा और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक शक्तियाँ भी देता है। लेकिन इन दोनों के बीच एक स्वाभाविक टकराव (Conflict) की स्थिति भी उत्पन्न होती है। एक ओर नागरिक अपने अधिकारों की स्वतंत्रता चाहता है, वहीं दूसरी ओर राज्य समाज में अनुशासन, सुरक्षा, न्याय और विकास सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाता है, जो कभी-कभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। अतः यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन कैसे बना रहे।
मौलिक अधिकारों की प्रकृति
भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार लोकतंत्र की आत्मा हैं, जो हर व्यक्ति को स्वतंत्र और गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देते हैं। इन अधिकारों में प्रमुख हैं:
- समता का अधिकार (Art. 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Art. 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art. 23–24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Art. 25–28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Art. 29–30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (Art. 32)
इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, अर्थात कोई भी नागरिक इनकी अवहेलना होने पर अदालत की शरण ले सकता है।
राज्य की शक्तियाँ: एक विवेचना
संविधान के विभिन्न भागों में राज्य को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे:
- कानून निर्माण की शक्ति (संविधान की अनुसूचियों में सूचीबद्ध विषयों पर)
- न्याय प्रशासन
- लोक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता की रक्षा
- आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन
- आपातकालीन शक्तियाँ (भाग-XVIII, अनुच्छेद 352–360)
राज्य का मुख्य उद्देश्य है – “सार्वजनिक हित में शांति, सुरक्षा, नैतिकता, और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना।” कभी-कभी यही उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का कारण बन जाता है।
मौलिक अधिकार बनाम राज्य की शक्ति: टकराव के उदाहरण
1. अनुच्छेद 19 और प्रतिबंध
अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को अभिव्यक्ति, आंदोलन, संघ बनाने, निवास और पेशा चुनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन अधिकारों पर “युक्तियुक्त प्रतिबंध” लगाए जा सकते हैं यदि वे:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता,
- राज्य की सुरक्षा,
- लोक व्यवस्था,
- नैतिकता या शिष्टाचार,
- अपराधों की रोकथाम,
- या अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हों।
उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति भाषण में हिंसा भड़काता है, तो राज्य उसे रोक सकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच संघर्ष का उदाहरण है।
2. आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन
अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं।
1975-77 की इमरजेंसी के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएँ बहुत हद तक सीमित कर दी गई थीं, जो मौलिक अधिकार बनाम राज्य शक्ति का प्रमुख उदाहरण है।
3. अनुच्छेद 21 बनाम सार्वजनिक हित
अनुच्छेद 21: “किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।”
लेकिन राज्य यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, या सामाजिक व्यवस्था हेतु कोई प्रतिबंध लगाता है (जैसे COVID-19 महामारी में लॉकडाउन), तो यह एक सीमा तक अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है।
न्यायपालिका की भूमिका: संतुलन का रक्षक
भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, इस संघर्ष में न्याय का संतुलन बनाए रखने वाली संस्था है। समय-समय पर कोर्ट ने इन मामलों में निर्णय दिए हैं जो संविधान की मूल भावना की रक्षा करते हैं:
1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) को नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकार इसी मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
यह फैसला राज्य की शक्तियों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की बात करता है और कहता है कि “संविधान में शक्ति और स्वतंत्रता का संतुलन जरूरी है।”
3. मानवेन्द्र सिंह बनाम भारत संघ (2005)
कोर्ट ने कहा कि लोक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर किसी निर्दोष नागरिक की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता।
वर्तमान संदर्भ में मौलिक अधिकार बनाम राज्य शक्ति
आज के समय में डिजिटल निगरानी, इंटरनेट शटडाउन, मीडिया नियंत्रण, विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध जैसे मामलों में मौलिक अधिकारों और राज्य की शक्तियों के टकराव की स्थिति बार-बार सामने आती है।
उदाहरण के लिए:
- शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन बनाम सार्वजनिक मार्गों की बाधा
- पेगासस जासूसी मामला बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा
- धारा 144 के बार-बार प्रयोग द्वारा सभा की स्वतंत्रता पर प्रभाव
निष्कर्ष
मौलिक अधिकार और राज्य की शक्तियाँ दोनों ही आवश्यक हैं — अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं, जबकि राज्य की शक्तियाँ समाज में व्यवस्था और सामूहिक कल्याण की गारंटी देती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता है। अतः न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वे अधिकार और शक्ति के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाए रखें। संविधान न तो निरंकुश स्वतंत्रता की अनुमति देता है और न ही निरंकुश शासन की। यही भारतीय संविधान की सुंदरता और महानता है।