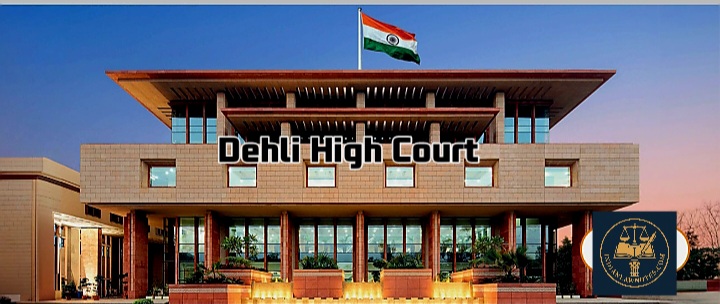“मेडिकल सेल्स रिप्रजेंटेटिव ‘वर्कमैन’ नहीं हैं”: दिल्ली उच्च न्यायालय का विस्तृत विश्लेषणात्मक निर्णय
1. प्रस्तावना (Introduction)
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) भारत में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों के समाधान का प्रमुख विधिक ढांचा है। इसका उद्देश्य ‘वर्कमैन’ को संरक्षण प्रदान करना है, ताकि वे मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, अन्यायपूर्ण व्यवहार, या अनुचित श्रम-प्रथाओं के विरुद्ध कानूनी राहत पा सकें।
परंतु प्रश्न तब उठता है — क्या प्रत्येक कर्मचारी को ‘वर्कमैन’ कहा जा सकता है?
इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि “वर्कमैन” की परिभाषा स्वयं क़ानून में सीमित और तकनीकी है।
इसी संदर्भ में, दिल्ली उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय – Sh. Samarendra Das v. M/s Win Medicare Pvt. Ltd. – अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने यह स्पष्ट किया कि Medical Sales Representative (MSR), जिन्हें आम बोलचाल में Medical Representative कहा जाता है, Industrial Disputes Act की धारा 2(s) के तहत ‘वर्कमैन’ की परिभाषा में नहीं आते।
2. मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)
अर्ज़ीकर्ता (Petitioner) Win Medicare Pvt. Ltd. में मेडिकल सेल्स रिप्रजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था।
उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत “अवैध बर्खास्तगी” (illegal termination) का मामला दायर किया।
उसका तर्क था कि:
- वह कंपनी में नियमित कर्मचारी था,
- उसके कार्य कंपनी के लिए आवश्यक थे,
- उसे अनुचित रूप से नौकरी से निकाला गया,
- और इसलिए उसे Industrial Disputes Act के तहत “वर्कमैन” माना जाना चाहिए।
कंपनी ने प्रतिवाद किया कि:
- मेडिकल रिप्रजेंटेटिव का कार्य बिक्री-प्रचार (sales promotion) का होता है, न कि मैनुअल या क्लेरिकल;
- वह डॉक्टरों से मिलकर उत्पाद की जानकारी देता है, रिपोर्ट तैयार करता है, और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है;
- इसलिए उसे “वर्कमैन” नहीं कहा जा सकता।
लेबर कोर्ट ने कंपनी के तर्क को स्वीकार किया और यह कहा कि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव “वर्कमैन” नहीं है।
इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
3. कानूनी प्रश्न (Legal Issue)
मुख्य प्रश्न था:
क्या एक “Medical Sales Representative” को Industrial Disputes Act, 1947 की धारा 2(s) के तहत “वर्कमैन” माना जा सकता है?
4. प्रासंगिक कानूनी प्रावधान (Relevant Legal Provision)
धारा 2(s), Industrial Disputes Act, 1947 के अनुसार:
“वर्कमैन” वह व्यक्ति है जो किसी उद्योग में नियोजित है और किसी नियोक्ता के अधीन मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, या सुपरवाइजरी कार्य करता है, लेकिन वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्य करता हो।
स्पष्ट है कि “वर्कमैन” की परिभाषा कार्य के प्रकार (nature of duties) पर निर्भर करती है, न कि पदनाम (designation) पर।
5. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क (Arguments before the Court)
(A) याचिकाकर्ता के तर्क:
- मेडिकल रिप्रजेंटेटिव कंपनी की ओर से कार्य करता है और उसके ऊपर प्रबंधकीय नियंत्रण है, अतः वह ‘वर्कमैन’ है।
- उसका वेतन और कार्य-घंटे कंपनी द्वारा तय किए जाते थे।
- Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 के तहत, मेडिकल रिप्रजेंटेटिव को “सेल्स प्रमोशन कर्मचारी” के रूप में मान्यता दी गई है; अतः उसे श्रमिक संरक्षण मिलना चाहिए।
(B) प्रतिवादी कंपनी के तर्क:
- मेडिकल रिप्रजेंटेटिव का कार्य मैनुअल या क्लेरिकल नहीं है;
- वह स्वतंत्र रूप से डॉक्टरों से बातचीत करता है, उत्पाद का प्रचार करता है, बिक्री रणनीति अपनाता है — यह सब बौद्धिक कार्य हैं;
- इसलिए उसे ‘वर्कमैन’ नहीं कहा जा सकता।
6. दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय (Judgment of the Delhi High Court)
दिल्ली उच्च न्यायालय (जस्टिस तारा वितस्ता गंजू) ने याचिका को खारिज करते हुए निम्नलिखित प्रमुख बिंदु रखे:
(i) कार्य का स्वभाव महत्वपूर्ण है, न कि पदनाम
अदालत ने कहा कि यह देखना आवश्यक है कि कर्मचारी का कार्य क्या है, न कि उसका पदनाम क्या है।
मेडिकल रिप्रजेंटेटिव का कार्य बिक्री-प्रचार (sales promotion) है, जो कि औद्योगिक-कानूनी परिभाषा में “मैनुअल, क्लेरिकल या तकनीकी” नहीं है।
(ii) स्वतंत्र निर्णय-शक्ति और पेशेवर भूमिका
मेडिकल रिप्रजेंटेटिव को डॉक्टरों, अस्पतालों, और फार्मासिस्ट्स से मिलकर दवाइयों की जानकारी देनी होती है, नए उत्पाद प्रस्तुत करने होते हैं और व्यापार बढ़ाने की रणनीति अपनानी होती है।
यह कार्य स्वतंत्र पेशेवर निर्णय-शक्ति (independent discretion) पर आधारित है, जो किसी भी मैनुअल कार्य से भिन्न है।
(iii) सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों पर निर्भरता
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले H.R. Adyanthaya v. Sandoz (India) Ltd., (1994 5 SCC 737) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था:
“Sales Promotion Employees, including Medical Representatives, do not fall under the definition of ‘workman’ under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act.”
इस निर्णय में स्पष्ट किया गया था कि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव की जिम्मेदारियां मैनुअल, क्लेरिकल, या टेक्निकल कार्य से भिन्न हैं।
(iv) Sales Promotion Employees Act का सीमित प्रभाव
SPE Act, 1976 कुछ सेवाओं को श्रम संरक्षण देता है, परंतु यह Industrial Disputes Act की परिभाषा को स्वतः नहीं बदल देता।
अर्थात् — SPE Act के अंतर्गत आने वाला हर व्यक्ति “वर्कमैन” नहीं बन जाता।
(v) निष्कर्ष (Conclusion)
अदालत ने कहा कि अर्ज़ीकर्ता का कार्य “बिक्री-प्रचार और विपणन” से संबंधित था, जो बौद्धिक और स्वतंत्र था। अतः वह “वर्कमैन” नहीं कहा जा सकता।
इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।
7. प्रासंगिक पूर्व-निर्णय (Precedent Cases)
| क्रम | केस का नाम | निर्णय |
|---|---|---|
| 1 | May & Baker (India) Ltd. v. Their Workmen, AIR 1967 SC 678 | मेडिकल रिप्रजेंटेटिव “वर्कमैन” नहीं क्योंकि उसका कार्य बिक्री-प्रचार का है। |
| 2 | Burmah Shell Oil Storage v. Burmah Shell Management Staff Assn., (1971) 2 SCC 706 | कर्मचारी का कार्य-स्वभाव निर्णायक है, पदनाम नहीं। |
| 3 | H.R. Adyanthaya v. Sandoz (India) Ltd., (1994) 5 SCC 737 | सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव ‘वर्कमैन’ नहीं। |
| 4 | Glaxo India Ltd. v. Presiding Officer, Labour Court, 2011 LLR 1177 | मेडिकल रिप्रजेंटेटिव का कार्य बिक्री-वर्धन का है, इसलिए वह ID Act की धारा 2(s) में नहीं आता। |
8. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 का प्रभाव
यह अधिनियम औषधि-विक्रय कर्मचारियों के सेवा-नियमों को नियंत्रित करने के लिए पारित हुआ था।
इसका उद्देश्य था कि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव जैसे कर्मचारियों को कुछ श्रम-सुरक्षा (जैसे अवकाश, वेतन, कार्य-घंटे) दी जा सके।
परंतु इसकी धारा 6(2) स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम Industrial Disputes Act की परिभाषा को विस्तारित नहीं करता, बल्कि केवल उन मामलों में लागू होगा जहाँ अन्य अधिनियमों में पहले से सुरक्षा न हो।
अतः SPE Act के तहत “सेल्स प्रमोशन कर्मचारी” होने का अर्थ यह नहीं कि वह स्वचालित रूप से “वर्कमैन” बन जाएगा।
9. निर्णय के निहितार्थ (Implications of the Judgment)
(A) कंपनियों के लिए प्रभाव
- फार्मा कंपनियां अब यह कह सकती हैं कि उनके मेडिकल रिप्रजेंटेटिव “वर्कमैन” नहीं हैं,
अतः Industrial Disputes Act के तहत वे औद्योगिक विवाद नहीं उठा सकते। - इससे कंपनियों को अनुशासन और सेवा-समाप्ति संबंधी मामलों में अधिक लचीलापन मिलता है।
(B) कर्मचारियों के लिए प्रभाव
- मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स को ID Act की सुरक्षा (जैसे पुनर्नियुक्ति, अवैध बर्खास्तगी पर राहत) नहीं मिल पाएगी।
- उनके पास विकल्प के रूप में सिविल कोर्ट या सेवा-संविदा (employment contract) के उल्लंघन का दावा बचता है।
(C) श्रम-कानून की सीमाएँ उजागर
यह निर्णय बताता है कि ID Act की परिभाषा समय-सापेक्ष नहीं रही है।
1950-60 के दशक की औद्योगिक परिस्थितियों में गढ़ी गई यह परिभाषा आधुनिक “सेल्स-प्रमोशन”, “बिज़नेस डेवलपमेंट” और “कॉर्पोरेट मार्केटिंग” जैसे पेशों पर लागू नहीं होती।
10. तुलनात्मक दृष्टिकोण (Comparative Perspective)
(i) अन्य देशों में स्थिति
- यूके और ऑस्ट्रेलिया में “वर्कर” की परिभाषा व्यापक है — जिसमें वे व्यक्ति भी आते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं पर नियंत्रण के अधीन हैं।
- भारत में, “वर्कमैन” की परिभाषा संकीर्ण (narrow) है और केवल परंपरागत श्रमिक वर्ग पर केंद्रित है।
(ii) भारत में न्यायिक विविधता
कुछ हाईकोर्ट्स (जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, Dr. R. R. Pillai v. HMM Ltd., 2003 LLR 208) ने मेडिकल रिप्रजेंटेटिव को “वर्कमैन” माना है, पर दिल्ली हाईकोर्ट का नवीनतम निर्णय इस मत को सीमित करता है।
11. आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Evaluation)
- कानूनी अस्पष्टता: Industrial Disputes Act की धारा 2(s) में “वर्कमैन” की परिभाषा अत्यंत पुरानी है। आधुनिक कार्य-संरचनाओं (marketing, communication, digital sales) को वह कवर नहीं करती।
- समानता का अभाव: एक क्लेरिकल स्टाफ को ‘वर्कमैन’ माना जाता है, परंतु अधिक मेहनती, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त मेडिकल रिप्रजेंटेटिव को नहीं — यह विरोधाभासी लगता है।
- सामाजिक न्याय का सवाल: ID Act का उद्देश्य श्रमिकों की रक्षा करना है। यदि उच्च शिक्षित या प्रशिक्षित सेल्स प्रमोशन कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वैकल्पिक सुरक्षा-तंत्र आवश्यक है।
- संभावित विधायी सुधार: भविष्य में संसद इस पर विचार कर सकती है कि “वर्कमैन” की परिभाषा को संशोधित कर “knowledge-based workers” को भी शामिल किया जाए।
12. निष्कर्ष (Conclusion)
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय श्रम-विधि में एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि “वर्कमैन” का दर्जा कार्य-स्वभाव से तय होगा, न कि पद या योग्यता से।
मेडिकल सेल्स रिप्रजेंटेटिव, जो स्वतंत्र रूप से बिक्री-प्रचार का कार्य करते हैं, Industrial Disputes Act के अंतर्गत वर्कमैन नहीं हैं।
हालांकि, यह निर्णय न्यायिक दृष्टि से तर्कसंगत है, पर सामाजिक-दृष्टि से यह प्रश्न उठाता है कि आधुनिक पेशों के कर्मचारियों को श्रम-कानूनी सुरक्षा कैसे दी जाए।
भविष्य में संभवतः इस क्षेत्र में विधायी सुधार या सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार-याचिका से नई दिशा मिलेगी।
संदर्भ (References):
- Sh. Samarendra Das v. Win Medicare Pvt. Ltd., Delhi High Court, 2025.
- H.R. Adyanthaya v. Sandoz (India) Ltd., (1994) 5 SCC 737.
- May & Baker (India) Ltd. v. Their Workmen, AIR 1967 SC 678.
- Burmah Shell Oil Storage v. Burmah Shell Management Staff Assn., (1971) 2 SCC 706.
- Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
- Articles: LiveLaw, Indian Kanoon, Verdictum & Casemine.