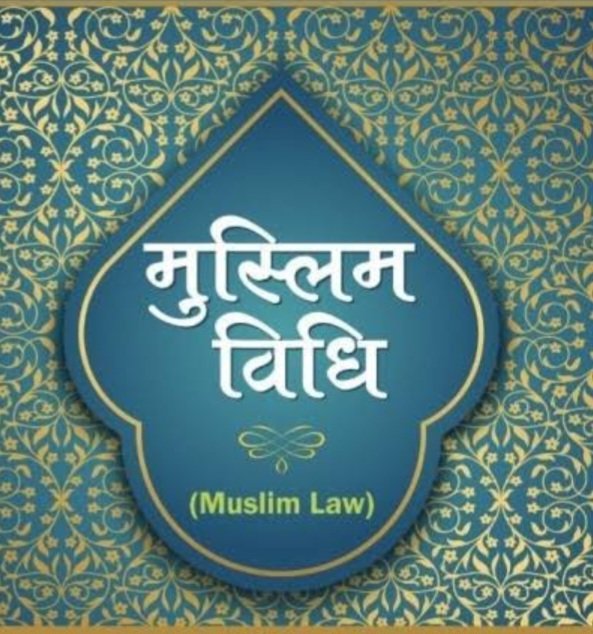1. मुस्लिम विधि के विकास की रूपरेखा (Outline of Development of Mohammedan Law)
मुस्लिम विधि का विकास मुख्य रूप से चार चरणों में हुआ:
- प्रारंभिक चरण (610-632 ई.) – इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद के समय में, कुरान और सुन्नत (मुहम्मद की शिक्षाएँ और कार्य) मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत बने।
- खलीफा काल (632-661 ई.) – चार खलीफाओं के शासन में, इस्लामी न्याय प्रणाली को संगठित किया गया।
- फिक़्ह (Jurisprudence) का विकास (661-1258 ई.) – इस काल में विभिन्न इस्लामी विद्वानों ने हदीस, इज्मा और कियास के आधार पर विधि का विकास किया।
- आधुनिक काल – ब्रिटिश शासन और आधुनिक मुस्लिम देशों में विधान के माध्यम से मुस्लिम विधि में बदलाव हुए।
2. मुसलमान कौन हैं? (Who is a Muslim?)
मुसलमान वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम धर्म को मानता है, अल्लाह की एकता (तौहीद) और पैगंबर मुहम्मद को अंतिम पैगंबर स्वीकार करता है।
3. सुन्नी एवं शिया सम्प्रदाय (Sunni and Shia Sampraday)
- सुन्नी – जो चार खलीफाओं को वैध शासक मानते हैं और चार इमामों (अबू हनीफा, शाफ़ई, मालिक, हंबल) के फिक़्ह का पालन करते हैं।
- शिया – जो मानते हैं कि पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकारी अली और उनके वंशज हैं।
4. कुरान का महत्व (Importance of Quran as a Primary Source of Muslim Law)
- कुरान इस्लामी विधि का मुख्य स्रोत है।
- इसमें इस्लामिक जीवन, विवाह, उत्तराधिकार, अपराध आदि से संबंधित नियम हैं।
- यह ईश्वरीय आदेशों का संकलन है और इस्लामी न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है।
5. सुन्नत तथा हदीस (Sunnat and Hadis as Source of Muslim Law)
- सुन्नत – पैगंबर मुहम्मद के कार्य और आदतें।
- हदीस – पैगंबर के कथनों और कार्यों का संग्रह।
- मुस्लिम विधि में सुन्नत और हदीस कुरान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं।
6. इज्मा (Ijma) की व्याख्या
- इज्मा का अर्थ इस्लामी विद्वानों की सर्वसम्मति से दी गई राय है।
- जब किसी नए मामले में कुरान और सुन्नत में स्पष्ट नियम नहीं होते, तब इज्मा का सहारा लिया जाता है।
7. मुस्लिम विधि में विधायन (Legislation) का महत्व
- आधुनिक समय में विभिन्न मुस्लिम देशों में विधान (Legislation) द्वारा मुस्लिम कानून में संशोधन किया गया है।
- जैसे – पाकिस्तान, भारत और अन्य देशों में मुस्लिम विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर कानून बनाए गए हैं।
8. निकाह (Marriage) का अर्थ
- निकाह का अर्थ मुस्लिम विवाह से है। यह एक वैधानिक और धार्मिक अनुबंध होता है जिसमें पति-पत्नी के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं।
9. वैध विवाह की आवश्यक शर्तें (Essentials of a Valid Marriage in Muslim Law)
- प्रस्ताव (Ijab) और स्वीकार (Qubool)।
- दो गवाहों की उपस्थिति।
- दूल्हा और दुल्हन का मुस्लिम होना।
- मेहर (दहेज) की तयशुदा राशि।
- विवाह के लिए योग्य उम्र (बालिग़ होना)।
10. इद्दत (Iddat) और उसके नियम
- परिभाषा: इद्दत वह अवधि है जब तलाकशुदा या विधवा महिला को दोबारा विवाह करने से पहले प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- अवधि:
- तलाकशुदा महिला – 3 मासिक धर्म (यदि गर्भवती न हो)।
- गर्भवती महिला – बच्चे के जन्म तक।
- विधवा – 4 महीने 10 दिन।
11. इद्दत के उद्देश्य (Objects of Iddat)
- यह सुनिश्चित करना कि महिला गर्भवती नहीं है।
- पति-पत्नी को पुनर्मिलन का अवसर देना।
- विधवा के मामले में, पति के प्रति शोक व्यक्त करना।
12. वयस्कता या ख्यारूल बुलूग (Option of Puberty)
- यदि किसी नाबालिग का विवाह कर दिया जाता है, तो बालिग होने पर उसे विवाह को जारी रखने या तोड़ने का अधिकार होता है। इसे ख्यारूल बुलूग कहते हैं।
13. बातिल विवाह (Batil Marriage)
- वह विवाह जो पूरी तरह से अमान्य हो और वैध न हो।
- जैसे – निकट संबंधियों (माँ-बेटा, भाई-बहन) के बीच विवाह, पांचवें पति से विवाह आदि।
14. फासिद विवाह (Fasid Marriage) क्या है?
फासिद विवाह वह विवाह है जिसमें कुछ खामियां होती हैं, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता है। यदि कोई शर्त पूरी नहीं होती, तो विवाह अस्थायी रूप से अमान्य रहता है, लेकिन बाद में उसे वैध बनाया जा सकता है। उदाहरण:
- बिना गवाहों के विवाह
- निषिद्ध समय (इद्दत) के दौरान विवाह
15. सहीह (Valid) विवाह क्या है?
सहीह विवाह वह विवाह होता है जो इस्लामी कानून की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे:
- दोनों पक्षों की सहमति
- मेहर का निर्धारण
- गवाहों की उपस्थिति
16. मेहर (Dower) क्या है?
मेहर वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के समय या बाद में पत्नी को देता है। यह मुस्लिम विवाह का एक अनिवार्य तत्व है।
17. मेहर के विभिन्न प्रकार (Types of Dower)
- मुसम्मा मेहर (Specified Dower) – विवाह के समय तय किया गया मेहर।
- महर-मिस्ल (Proper Dower) – यदि मेहर तय न हो, तो पत्नी के परिवार की महिलाओं के आधार पर तय किया जाता है।
18. तत्काल एवं विलंबित मेहर का अंतर (Prompt vs. Deferred Dower)
तत्काल और विलंबित मेहर का अंतर
तत्काल (Prompt) मेहर वह होता है जिसे पति को पत्नी के मांगने पर तुरंत अदा करना होता है। यह विवाह संपन्न होते ही या निकाह के तुरंत बाद किसी भी समय पत्नी की मांग पर दिया जा सकता है। यदि पति मेहर का भुगतान नहीं करता, तो पत्नी को पति से अलग रहने और न्यायालय में दावा करने का अधिकार होता है।
विलंबित (Deferred) मेहर वह होता है जिसे भविष्य में किसी निश्चित समय पर या पति की मृत्यु के बाद अदा किया जाता है। यह अक्सर तलाक या पति की मृत्यु के बाद पत्नी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा जाता है। जब तक विलंबित मेहर का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक पत्नी इसे प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखती है और इसे पति की संपत्ति से वसूल किया जा सकता है।
इस प्रकार, तत्काल मेहर तुरंत अदा किया जाता है, जबकि विलंबित मेहर को भविष्य के लिए टाला जाता है, लेकिन दोनों ही पत्नी का अधिकार होते हैं।
19. मेहर न मिलने पर पत्नी के अधिकार (Rights of Wife on Non-Payment of Dower)
- पति से मेहर की मांग कर सकती है।
- अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है।
- पति से अलग होने का अधिकार।
- यदि पति की मृत्यु हो जाए, तो उसकी संपत्ति से मेहर प्राप्त कर सकती है।
20. बातिल और फासिद निकाह में अंतर (Void vs. Invalid Marriage)
बातिल और फासिद निकाह में अंतर
बातिल निकाह पूरी तरह से अवैध (Void) होता है और इसका कोई कानूनी या धार्मिक मान्यता प्राप्त प्रभाव नहीं होता। इसमें पति-पत्नी के बीच कोई वैध संबंध स्थापित नहीं होता, और इससे उत्पन्न संतान को अवैध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विवाह निकट संबंधियों (माँ-बेटा, भाई-बहन) के बीच हो, किसी विवाहित महिला से किया जाए, या इस्लामी विवाह की बुनियादी शर्तों को पूरा न करे, तो वह बातिल निकाह कहलाता है।
फासिद निकाह अस्थायी रूप से अमान्य (Irregular) होता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद इसे वैध (Valid) बनाया जा सकता है। यह पूरी तरह अवैध नहीं होता, बल्कि कुछ त्रुटियों के कारण अमान्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, बिना गवाहों के विवाह, निषिद्ध समय (इद्दत) के दौरान विवाह, या असमान धर्म के व्यक्ति से विवाह फासिद निकाह हो सकता है। यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाए, तो विवाह को वैध माना जा सकता है।
इस प्रकार, बातिल निकाह को किसी भी स्थिति में वैध नहीं बनाया जा सकता, जबकि फासिद निकाह को आवश्यक सुधारों के बाद वैध किया जा सकता है।
21. निश्चित मेहर (Fixed Dower) क्या है?
निश्चित मेहर (Fixed Dower) क्या है?
निश्चित मेहर (Mahr Musamma) वह मेहर होता है जिसे विवाह के समय पति और पत्नी (या उनके अभिभावकों) द्वारा पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है। यह राशि या संपत्ति निकाह के अनुबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसे विवाह के दौरान या बाद में किसी भी समय अदा किया जा सकता है।
यदि निश्चित मेहर तय कर लिया जाता है, तो पति को इसे अनिवार्य रूप से पत्नी को देना होता है, चाहे वह तुरंत (तत्काल मेहर) हो या बाद में (विलंबित मेहर)। यह मेहर पत्नी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे विवाह में अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जाता है।
22. उचित मेहर (Proper Dower) क्या है?
उचित मेहर (Proper Dower) क्या है?
उचित मेहर (Mahr-e-Misl) वह मेहर होता है जो तब लागू होता है जब विवाह के समय मेहर की राशि निर्धारित नहीं की गई हो। ऐसी स्थिति में, पत्नी को उतनी ही मेहर दी जाती है जितनी उसके परिवार की अन्य महिलाओं (जैसे उसकी बहन, मौसी, बुआ, आदि) को उनके विवाह में दी गई थी।
उचित मेहर तय करने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:
- पत्नी का पारिवारिक दर्जा – उसके परिवार की अन्य महिलाओं को कितना मेहर मिला था।
- पति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति – उसकी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।
- पत्नी की व्यक्तिगत योग्यताएँ – उसकी शिक्षा, उम्र, रूप-रंग, और चरित्र को भी ध्यान में लिया जाता है।
उचित मेहर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी को विवाह में न्यायोचित और सम्मानजनक मेहर प्राप्त हो, भले ही इसे विवाह के समय तय न किया गया हो।
23. सुन्नी और शिया विवाह में अंतर
सुन्नी और शिया विवाह में अंतर
सुन्नी विवाह में दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि शिया विवाह में गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। सुन्नी निकाह आमतौर पर स्थायी विवाह होता है, जबकि शिया संप्रदाय में मुत’आ विवाह (अस्थायी विवाह) की अनुमति होती है, जिसमें विवाह एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और अवधि समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाता है।
सुन्नी विवाह में तलाक देने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सरल होती है, और तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) मान्य होता है। शिया विवाह में तीन तलाक तुरंत प्रभावी नहीं होता, बल्कि इसे एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।
मेहर के संदर्भ में, सुन्नी विवाह में इसे तुरंत या बाद में दिया जा सकता है, जबकि शिया विवाह में मेहर का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त होती है।
उत्तराधिकार कानून में भी अंतर देखा जाता है। शिया विधि में केवल रक्त-संबंधी रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सुन्नी विधि में रिश्तेदारों के अलावा दत्तक और अन्य रिश्तेदारों को भी संपत्ति में अधिकार मिल सकता है।
इस प्रकार, सुन्नी और शिया विवाह की प्रक्रिया, गवाहों की अनिवार्यता, तलाक की विधि, मेहर की शर्तें और उत्तराधिकार के नियमों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है।
24. खर्च-ए-पानदान (Kharch-i-Pandan) क्या है?
यह मुस्लिम विवाह में पत्नी को मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता है, जो उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए दिया जाता है।
25. मुत’आ विवाह (Muta Marriage) क्या है?
यह एक अस्थायी विवाह है, जो शिया संप्रदाय में प्रचलित है। इसमें विवाह एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और समय समाप्त होते ही स्वतः खत्म हो जाता है।
अनिवार्य शर्तें:
- विवाह की अवधि तय होनी चाहिए।
- मेहर तय होना चाहिए।
- केवल शिया पुरुष और शिया महिला के बीच मान्य।
26. मुत’आ विवाह के विधिक प्रभाव (Legal Effects of Muta Marriage)
- पत्नी को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होता।
- केवल पति को विवाह तोड़ने का अधिकार होता है।
- संतान को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है।
27. मुस्लिम और हिंदू विवाह में अंतर
मुस्लिम और हिंदू विवाह में अंतर
मुस्लिम विवाह एक नागरिक अनुबंध (Contract) है, जबकि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार (Sacrament) माना जाता है। मुस्लिम विवाह में पति और पत्नी के अधिकार और कर्तव्य कानूनी सहमति और मेहर पर आधारित होते हैं, जबकि हिंदू विवाह धार्मिक अनुष्ठानों और सप्तपदी जैसी रस्मों द्वारा संपन्न होता है।
मुस्लिम कानून के तहत बहुविवाह (Polygamy) की अनुमति होती है, जहां एक मुस्लिम पुरुष चार पत्नियाँ रख सकता है, जबकि हिंदू विवाह में एकपत्नीवाद (Monogamy) लागू है और पति-पत्नी दोनों को एक ही विवाह तक सीमित रहना पड़ता है।
तलाक की प्रक्रिया में भी अंतर है। मुस्लिम विवाह में तलाक (Talak) एक स्वीकृत प्रक्रिया है, जिसमें पति एक निश्चित प्रक्रिया के तहत विवाह को समाप्त कर सकता है। वहीं, हिंदू विवाह में तलाक कठिन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और इसे विवाह विच्छेद के अंतिम उपाय के रूप में माना जाता है, जिसके लिए कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है।
उत्तराधिकार के मामलों में भी अंतर देखा जाता है। मुस्लिम विधि के तहत पति-पत्नी को एक-दूसरे की संपत्ति में पूर्व निर्धारित हिस्सेदारी मिलती है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संपत्ति का बंटवारा विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है।
इस प्रकार, मुस्लिम और हिंदू विवाह की प्रकृति, तलाक की प्रक्रिया, बहुविवाह की अनुमति और उत्तराधिकार के नियमों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है।
28. तलाक (Talak) क्या है?
तलाक का अर्थ पति द्वारा विवाह को समाप्त करना है। इसके प्रकार:
- तलाक-ए-अहसन (सर्वश्रेष्ठ रूप)
- तलाक-ए-हसन (अच्छा रूप)
- तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक, सुन्नियों में प्रचलित)
29. मुस्लिम महिला न्यायिक विच्छेद (Judicial Divorce) किन आधारों पर प्राप्त कर सकती है?
- पति की अनुपस्थिति (चार साल से अधिक)।
- पति द्वारा परित्याग (दो साल से अधिक)।
- पति का क्रूर व्यवहार।
- पति का पागलपन या गंभीर बीमारी।
- पति द्वारा मेहर का भुगतान न करना।
- “दिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939” के तहत दिए गए अधिकार।
30. विवाह विच्छेद के बाद मुस्लिम पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार (Maintenance of Muslim Wife after Divorce)
विवाह विच्छेद (तलाक) के बाद मुस्लिम पत्नी को कुछ विशेष भरण-पोषण अधिकार प्राप्त होते हैं।
- इद्दत की अवधि के दौरान भरण-पोषण – पति को तलाक के बाद पत्नी के इद्दत (तीन माह) की अवधि तक उसका भरण-पोषण करना अनिवार्य होता है।
- मेहर की अदायगी – पति को तलाक के समय तक बकाया मेहर का भुगतान करना होता है।
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 – इसके तहत, यदि पत्नी स्वयं जीविका चलाने में असमर्थ हो, तो वह अपने माता-पिता या वक्फ बोर्ड से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
- न्यायिक दावा – यदि पति भरण-पोषण देने से इनकार करता है, तो पत्नी अदालत में दावा कर सकती है।
31. लियान (Lian) क्या है?
यदि पति बिना किसी प्रमाण के अपनी पत्नी पर व्यभिचार (व्यभिचार/अविवेकपूर्ण आचरण) का आरोप लगाता है और पत्नी इसे अस्वीकार करती है, तो इस्लामी कानून में इसे लियान कहा जाता है। इस स्थिति में, पत्नी को तलाक लेने और पति से अलग होने का अधिकार मिल जाता है।
32. हिज़ानत (Hizanat) या संरक्षकता (Guardianship) क्या है?
हिज़ानत का अर्थ है माता-पिता या अन्य संरक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण करना। मुस्लिम कानून के अनुसार, बच्चे की संरक्षकता पहले माँ को मिलती है, जब तक कि वह कुछ परिस्थितियों में अयोग्य न मानी जाए। पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है, लेकिन माँ की भूमिका पालन-पोषण में महत्वपूर्ण होती है।
33. अभिस्वीकृति (Acknowledgment) क्या है?
अभिस्वीकृति का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा यह मान लेना कि कोई विशेष व्यक्ति उसका वैध उत्तराधिकारी या पुत्र है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो, तो उसका पिता या संरक्षक उसे अपनी संतान के रूप में मान्यता देकर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है।
34. तलाक के विभिन्न रूप (Different Forms of Talaq)
- तलाक-ए-अहसन – एक बार तलाक कहा जाता है, फिर इद्दत की अवधि के दौरान संबंध फिर से स्थापित किया जा सकता है।
- तलाक-ए-हसन – तीन बार तलाक कहा जाता है, प्रत्येक माह में एक बार, और इसे वापस लिया जा सकता है।
- तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) – सुन्नी समुदाय में मान्य, जहां पति एक साथ तीन बार तलाक कहकर विवाह समाप्त कर सकता है।
- खुला – पत्नी द्वारा तलाक मांगा जाता है, जिसमें उसे मेहर लौटाना पड़ सकता है।
- मुबारत – आपसी सहमति से तलाक।
35. इला और खुला में अंतर (Difference between Ila and Khula)
इला – जब पति शपथ लेता है कि वह अपनी पत्नी से चार महीने या अधिक समय तक संबंध नहीं बनाएगा, तो यह इला कहलाता है। यदि वह इस अवधि के बाद भी पत्नी से संबंध नहीं बनाता, तो तलाक स्वतः हो जाता है।
खुला – यह पत्नी द्वारा तलाक की प्रक्रिया है, जिसमें वह अपने पति से विवाह समाप्त करने की मांग करती है और बदले में कुछ संपत्ति (जैसे मेहर) लौटाने के लिए सहमत होती है।
36. हिबा (Hiba) क्या है?
हिबा का अर्थ मुस्लिम कानून में दान (Gift) से है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के देता है।
37. हिबा के प्रकार (Kinds of Hiba)
- साधारण हिबा (Hiba) – बिना किसी शर्त के दान।
- हिबा-बिल-एवज – बदले में कुछ लेने की शर्त पर दिया गया दान।
- हिबा-बह-शर्त-उल-इवज – दान करने के बाद दाता बदले में कुछ पाने का हकदार होता है।
38. हिबा के आवश्यक तत्व (Essential Ingredients of Gifts)
- दाता (Donor) – जिसे संपत्ति देने का अधिकार है।
- प्राप्तकर्ता (Donee) – जिसे संपत्ति प्राप्त हो रही है।
- संपत्ति (Subject Matter) – दान की जाने वाली वस्तु।
- स्वेच्छा (Free Will) – दानकर्ता की स्वतंत्र इच्छा से दिया जाना चाहिए।
- स्वामित्व का हस्तांतरण (Delivery of Possession) – संपत्ति पर अधिकार दूसरे को सौंपना आवश्यक है।
39. वसीयत (Will) की परिभाषा
वसीयत वह कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण का आदेश देता है।
40. एक वसीयतकर्ता की योग्यता (Qualification of a Testator)
- वह अक्लमंद और बालिग होना चाहिए।
- वह अपनी संपत्ति का अधिकतम 1/3 भाग ही वसीयत कर सकता है (उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना)।
- उसकी वसीयत किसी अनुचित दबाव या धोखे से मुक्त होनी चाहिए।
41. मर्ज-उल-मौत (मृत्यु शैय्या दान) क्या है?
यदि कोई व्यक्ति मृत्युशय्या पर रहते हुए हिबा (दान) करता है, तो इसे मर्ज-उल-मौत या Death-Bed Gift कहा जाता है। यह केवल तब मान्य होता है जब मृतक के उत्तराधिकारियों को कोई अन्याय न हो।
42. हिबा-बिल-एवज (Hiba Bil Ewaz) क्या है?
जब कोई व्यक्ति हिबा के बदले में कुछ धन या संपत्ति प्राप्त करता है, तो इसे हिबा-बिल-एवज कहा जाता है। यह हिबा और बिक्री (Sale) के बीच का एक रूप होता है।
43. वसीयत और हिबा में अंतर (Difference between Will and Hiba)
हिबा जीवनकाल में किया गया स्वैच्छिक दान होता है, जबकि वसीयत मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण का आदेश होता है। हिबा तत्काल प्रभावी होता है, जबकि वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के बाद लागू होती है।
44. वसीयत को रद्द करने के तरीके (Modes of Revocation of Will)
- वसीयतकर्ता स्वयं वसीयत को निरस्त कर सकता है।
- नई वसीयत बनाकर पुरानी वसीयत को अमान्य किया जा सकता है।
- वसीयत की गई संपत्ति को बेचकर या दान करके वसीयत रद्द की जा सकती है।
45. दाय के अवतरण (Devolution of Inheritance) के प्रकार
- फरायज (Sharers) – वे रिश्तेदार जिन्हें निश्चित भाग मिलता है।
- आसबा (Residuaries) – जिन्हें शेष संपत्ति दी जाती है।
- जिन्हें कोई निश्चित हिस्सा नहीं (Distant Kindred) – यदि कोई फरायज या आसबा न हो, तो अन्य दूर के रिश्तेदारों को संपत्ति मिलती है।
46. वक्फ के प्रकार (Kinds of Wakf)
- वक्फ-लिल्लाह (Religious Wakf) – धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान।
- वक्फ-अल-अलद (Family Wakf) – परिवार के भरण-पोषण के लिए संपत्ति का दान।
- वक्फ-खैराती (Charitable Wakf) – गरीबों, अनाथों या समाज कल्याण के लिए संपत्ति दान।
(ख) वक्फ-अलल-औलाद (Wakf-Alal-Aulad) क्या है?
वक्फ-अलल-औलाद वह वक्फ होता है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने परिवार और वंशजों (औलाद) के लाभ के लिए दान करता है। यह एक प्रकार का पारिवारिक वक्फ होता है, जिसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यदि वंशज समाप्त हो जाते हैं, तो संपत्ति धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है।
47. आरियत और सदका (Areeat and Sadaqa) क्या है?
- आरियत (Areeat) – किसी वस्तु या संपत्ति को अस्थायी रूप से उपयोग के लिए बिना किसी शुल्क के देना। यह पूर्ण स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता।
- सदका (Sadaqa) – यह एक स्थायी दान होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति गरीबों, जरूरतमंदों, या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बिना किसी प्रत्याशा के देता है।
48. हक-शुफा (Haq-Shuffaa) या पूर्व-क्रयाधिकार (Pre-Emption) की परिभाषा
हक-शुफा का अर्थ है किसी संपत्ति के निकटतम पड़ोसी, सह-मालिक, या साझेदार को उस संपत्ति को खरीदने का प्राथमिक अधिकार होना, यदि उसका मालिक उसे बेचता है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने से रोकना और समुदाय या परिवार की सुरक्षा बनाए रखना है।
49. मुस्लिम विधि में शुफा (पूर्व-क्रयाधिकार) का दावा कौन कर सकता है?
मुस्लिम कानून में तीन प्रकार के व्यक्ति शुफा का दावा कर सकते हैं:
- साझेदार (Sharik) – जो संपत्ति में सह-स्वामी है।
- अंशधारी पड़ोसी (Khalit) – जो समान परिसीमा (सीमावर्ती भूमि) का मालिक है।
- निकटतम पड़ोसी (Jar) – जो संपत्ति के निकट रहता है।
50. मुशा (Musha) का सिद्धांत क्या है?
मुशा का अर्थ है किसी संपत्ति में बिना विभाजन के साझा स्वामित्व। मुस्लिम कानून के अनुसार, यदि कोई साझा संपत्ति दी जा रही है, तो इसे स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, अन्यथा हिबा (दान) अमान्य हो सकता है। हालांकि, अविभाजित संपत्ति को उत्तराधिकार में साझा किया जा सकता है।
51. मुतवल्ली (Mutawalli) कौन बन सकता है?
मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करता है। मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार वक्फ बनाने वाले व्यक्ति (वाकिफ), उत्तराधिकारी, या अदालत के पास होता है। मुतवल्ली कोई भी बुद्धिमान, ईमानदार और प्रबंधन में सक्षम व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह वक्फ की संपत्ति का मालिक नहीं होता, केवल उसका संरक्षक होता है।
52. जिना (Zina) और इसके परिणाम
जिना इस्लामी कानून में अवैध यौन संबंध (व्यभिचार) को कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है:
- व्यभिचार (Adultery) – जब विवाहित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाता है।
- व्यभिचार के बिना संभोग (Fornication) – जब अविवाहित पुरुष और महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं।
परिणाम:
- यदि जिना साबित हो जाता है, तो शरीयत के अनुसार कठोर दंड (हद) लगाया जाता है, जैसे पत्थर मारना या कोड़े मारना।
- सामाजिक बदनामी और पारिवारिक कलह हो सकती है।
- कानूनी रूप से संतान का उत्तराधिकार प्रभावित हो सकता है।
53. मुस्लिम विधि में प्राकृतिक संरक्षकों (Natural Guardians) के अधिकार
मुस्लिम कानून में प्राकृतिक संरक्षक बच्चे के पालन-पोषण, शिक्षा, और संपत्ति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- पिता (Father) – प्राथमिक संरक्षक होता है और बच्चे की शिक्षा व संपत्ति का ध्यान रखता है।
- दादा (Paternal Grandfather) – यदि पिता जीवित नहीं है, तो दादा संरक्षक बनता है।
- माता (Mother) – माँ को हिज़ानत के तहत बच्चे की देखभाल का प्राथमिक अधिकार होता है, लेकिन वह कानूनी संरक्षक नहीं होती।
54. माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी (Maintenance of Parents under Muslim Law)
मुस्लिम कानून के अनुसार, माता-पिता का भरण-पोषण उनके पुत्रों पर अनिवार्य होता है। यदि पुत्र सक्षम नहीं हैं, तो यह दायित्व उनकी बेटियों पर आता है। यदि कोई संतान नहीं है, तो अन्य निकटतम रिश्तेदारों को माता-पिता की देखभाल करनी होती है।
55. वास्तविक संरक्षक (De Facto Guardian) क्या है?
वास्तविक संरक्षक (De Facto Guardian) वह व्यक्ति होता है जो कानूनी रूप से नियुक्त नहीं होने के बावजूद किसी नाबालिग की देखभाल और संपत्ति प्रबंधन करता है। यह व्यक्ति बच्चे के भले के लिए कार्य कर सकता है, लेकिन उसे कानूनी अधिकार नहीं होते।
56. वास्तविक संरक्षक और विधितः (वैधानिक) संरक्षक में अंतर
- वास्तविक संरक्षक (De Facto Guardian) – यह व्यक्ति बिना किसी कानूनी नियुक्ति के बच्चे की देखभाल करता है, लेकिन उसके पास कानूनी अधिकार नहीं होते।
- विधितः (Legal Guardian) – यह व्यक्ति अदालत, वसीयत, या कानून द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे कानूनी रूप से संपत्ति और बच्चे की देखभाल का अधिकार होता है।