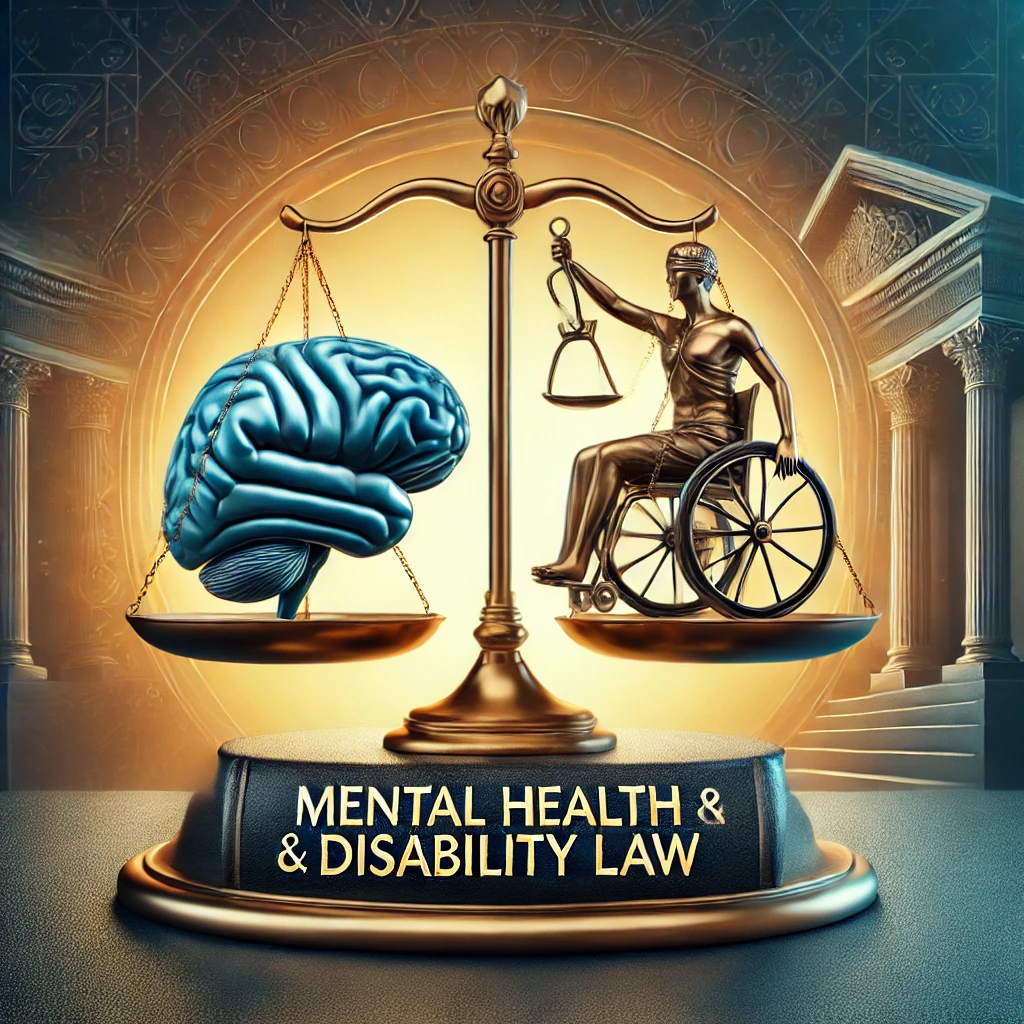मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 : रोगियों की कानूनी सुरक्षा
प्रस्तावना
मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण कल्याण का अनिवार्य अंग है। यदि मानसिक स्वास्थ्य उपेक्षित रह जाए, तो न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन-शैली प्रभावित होती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। भारत में लंबे समय तक मानसिक रोगियों को लेकर पूर्वाग्रह, भेदभाव और सामाजिक उपेक्षा का वातावरण रहा है। मानसिक बीमारियों को प्रायः कलंकित दृष्टि से देखा गया और रोगियों को समाज से अलग-थलग कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) का अधिनियमन एक मील का पत्थर है, जिसने न केवल मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का संवैधानिक और कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया।
अधिनियम का उद्देश्य
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को 7 अप्रैल 2017 को पारित किया गया और यह 29 मई 2018 से प्रभावी हुआ। इसके मुख्य उद्देश्यों को निम्न रूप में समझा जा सकता है–
- मानसिक रोगियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना।
- रोगियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न और असम्मानजनक व्यवहार को रोकना।
- रोगियों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि उनके उपचार और जीवन दोनों में गरिमा बनी रहे।
- आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर, उसे स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से देखना।
अधिकार आधारित दृष्टिकोण
यह अधिनियम अधिकार आधारित दृष्टिकोण (Rights Based Approach) पर आधारित है। अर्थात् मानसिक रोगियों को ‘बीमार’ या ‘अक्षम’ समझने की बजाय उन्हें एक अधिकार प्राप्त नागरिक माना गया है, जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
रोगियों की कानूनी सुरक्षा : प्रमुख प्रावधान
1. स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार
- प्रत्येक मानसिक रोगी को सरकार से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है।
- सरकार पर यह दायित्व है कि वह पर्याप्त संख्या में अस्पताल, पुनर्वास केंद्र और क्लिनिक स्थापित करे।
- सेवाएँ न केवल उपलब्ध हों बल्कि किफायती और समान रूप से सुलभ हों।
2. भेदभाव से संरक्षण
- रोगियों के साथ जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- किसी भी रोगी को मानसिक बीमारी के आधार पर समाज से अलग करने या रोजगार से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है।
3. उपचार में गरिमा और सम्मान का अधिकार
- रोगी को सम्मानजनक भाषा और व्यवहार के साथ उपचार प्राप्त करने का अधिकार है।
- उसे मजबूरन बंधक बनाकर या असम्मानजनक तरीके से अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता।
- परिवार और मित्रों से मिलने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
4. सूचना का अधिकार
- रोगी को अपनी बीमारी, उपचार की प्रकृति, औषधियों के दुष्प्रभाव तथा वैकल्पिक उपचारों की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।
- यह अधिकार रोगी के संरक्षक या अभिभावक को भी प्राप्त है।
5. पूर्व-निर्देश (Advance Directive)
- रोगी को यह अधिकार है कि वह पहले से लिखित रूप में यह निर्देश दे सके कि भविष्य में यदि उसे मानसिक बीमारी हो तो किस प्रकार का उपचार लिया जाए या किस प्रकार का उपचार नहीं लिया जाए।
- यह निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाएगा और चिकित्सक को उसका पालन करना होगा।
6. नामित प्रतिनिधि का अधिकार
- रोगी अपनी पसंद का नामित प्रतिनिधि (Nominated Representative) नियुक्त कर सकता है।
- यह प्रतिनिधि रोगी की ओर से चिकित्सीय निर्णय लेने और उसके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करेगा।
7. निरोध और पृथक्करण पर प्रतिबंध
- रोगियों को अनुचित रूप से बंधक बनाना, जंजीरों से बाँधना या अत्यधिक पृथक्करण में रखना पूरी तरह निषिद्ध है।
- केवल असाधारण परिस्थितियों में और चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक होने पर ही नियंत्रित निरोध किया जा सकता है।
8. आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना
- पूर्व में आत्महत्या का प्रयास भारतीय दंड संहिता (IPC की धारा 309) के अंतर्गत अपराध माना जाता था।
- इस अधिनियम ने स्पष्ट किया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव या बीमारी का शिकार है और उसे सजा की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है।
9. निगरानी और न्यायिक उपाय
- अधिनियम ने स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी (State Mental Health Authority) और सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी (Central Mental Health Authority) की स्थापना का प्रावधान किया।
- इन संस्थाओं का कार्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और रोगियों की शिकायतों का समाधान करना है।
10. न्यायिक संरक्षण
- रोगी को अपने अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड (Mental Health Review Board) में अपील करने का अधिकार है।
- यह बोर्ड रोगियों की शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित राहत प्रदान कर सकता है।
संवैधानिक दृष्टिकोण
यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 और 15 (समानता और भेदभाव निषेध) की मूल भावना को मूर्त रूप देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में मानसिक रोगियों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अंग माना है।
न्यायालयों का दृष्टिकोण
भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर मानसिक रोगियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं –
- शिवकुमार बनाम राज्य, 2017: अदालत ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं, बल्कि परामर्श और चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है।
- शीला बरसे केस: सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में मानसिक रोगियों के अमानवीय व्यवहार को असंवैधानिक ठहराया।
चुनौतियाँ और व्यावहारिक कठिनाइयाँ
यद्यपि अधिनियम में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, फिर भी कार्यान्वयन स्तर पर अनेक कठिनाइयाँ हैं –
- संसाधनों की कमी – देश में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अस्पतालों की संख्या अत्यंत सीमित है।
- सामाजिक कलंक – आज भी मानसिक रोगियों को परिवार और समाज में ‘पागल’ कहकर अलग-थलग किया जाता है।
- वित्तीय बाधाएँ – गरीब रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँचना कठिन है।
- जागरूकता का अभाव – अधिकांश लोग इस अधिनियम और इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अनभिज्ञ हैं।
सुधार की संभावनाएँ
- सरकार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित करना चाहिए।
- सामुदायिक स्तर पर परामर्श केंद्र, हेल्पलाइन और पुनर्वास योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए।
- मीडिया और शिक्षा के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है।
- न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को रोगियों की कानूनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 भारत में मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम न केवल मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार देता है, बल्कि उन्हें पूर्व-निर्देश, नामित प्रतिनिधि, भेदभाव से संरक्षण, और न्यायिक उपाय जैसे अधिकार प्रदान करता है। आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर इस अधिनियम ने मानसिक रोगियों के प्रति समाज की सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।
हालाँकि चुनौतियाँ अब भी शेष हैं, लेकिन यदि इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो यह न केवल मानसिक रोगियों को सम्मानजनक जीवन दे सकता है बल्कि भारत को एक संवेदनशील और समावेशी समाज बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।