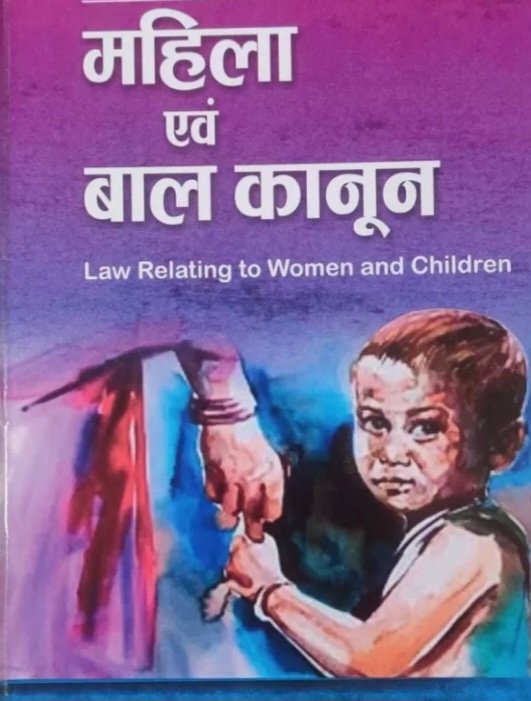-
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1979 की विशेषताएँ:
- यह अभिसमय महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- इसके तहत 186 देशों ने हस्ताक्षर किए और यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ बन गया।
- यह अभिसमय महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देता है।
- इसमें महिलाओं के साथ समानता, कार्यस्थल में भेदभाव से बचाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- बदलते समाज में महिलाओं की स्थिति:
- बदलते समाज में महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन भेदभाव और उत्पीड़न अब भी मौजूद है।
- शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लेकिन पारंपरिक विचारधाराएँ और सांस्कृतिक मान्यताएँ महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधक बनी हुई हैं।
- समाज में महिलाओं की स्थिति में समानता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु पूर्ण समानता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
- बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में उल्लिखित अधिकार:
- इस अभिसमय में बच्चों के जीवन, विकास, और सुरक्षा के अधिकारों पर जोर दिया गया है।
- बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन, और शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- यह अभिसमय यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाए।
- बच्चों को भाषण, विचार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलता है।
- महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों की संक्षिप्त समीक्षा:
- महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय हैं, जिनमें CEDAW (महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की समाप्ति का अनुबंध), ICESCR (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध) शामिल हैं।
- ये अभिसमय महिलाओं के लिए समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और हिंसा से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं।
- इन अभिसमयों के माध्यम से महिलाओं के लिए विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय स्तरों पर नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
- बालक के अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1989 पर समीक्षात्मक चर्चा:
- बालक के अधिकारों पर यह अभिसमय बालकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लागू हुआ।
- इसमें बच्चों के अधिकारों की व्यापक सूची दी गई है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और शोषण से सुरक्षा।
- हालांकि यह अभिसमय बच्चों के हित में है, लेकिन कई देशों में इसे प्रभावी रूप से लागू करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। गरीबी, युद्ध, और असमानताओं के कारण बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है।
- बच्चों के सन्दर्भ में भारतीय संविधान में दिये गये प्रावधानों पर निबन्ध:
- भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- अनुच्छेद 15 (3) के तहत राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 24 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के श्रम निषेध का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 39 (e) और (f) बच्चों के लिए उचित देखभाल और शिक्षा की गारंटी देते हैं।
- इसके अलावा, बालकों की शिक्षा और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा लागू किए गए हैं।
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी:
(1) महिलाओं की प्रांस्थित पर आयोग: यह आयोग महिलाओं के मुद्दों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव, हिंसा, और शोषण को रोकना है।
(2) राष्ट्रीय महिला आयोग: यह आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उपाय सुझाता है। यह महिलाओं के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान देता है और उनके न्यायाधिकार की सख्ती से निगरानी करता है।
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी:
(क) शिक्षा का अधिकार (Right to Education):
- यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।
- यह कानून 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है, जिससे बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिलता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलता है।
(ख) रैगिंग से रक्षा (Protection from Ragging):
- रैगिंग को छात्रों के शोषण और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है, और इसके खिलाफ कड़े कानून हैं।
- विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ विशेष नियम और कानूनी प्रावधान हैं, जो छात्रों को सुरक्षित और आदर्श शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
(ग) समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code):
- समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने आदि को नियंत्रित करता है।
- यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है, जो राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
(घ) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण:
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे महिलाओं को स्थानीय सरकारों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।
- यह कदम महिलाओं को राजनीति में सशक्त बनाने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों की विवेचना:
- भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में बालकों के कल्याण के लिए कई प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 39(e) और (f) के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बच्चों का शोषण न हो, और उनकी शिक्षा और कल्याण के लिए उचित उपाय किए जाएं।
- अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है।
- इसके अलावा, राज्य को बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी कार्य करने का आदेश है।
- महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबन्ध जो लिंग विभेद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं:
- संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- अनुच्छेद 16(2) के तहत महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोकने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे 1989 में बालकों के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और CEDAW (महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की समाप्ति का अनुबंध)।
- क्या राज्य लिंग के आधार पर नागरिकों में विभेद कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में?
- संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने से मना किया गया है।
- हालांकि, राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है यदि इसका उद्देश्य महिलाओं और अन्य उपेक्षित समूहों के लिए विशेष उपायों के माध्यम से उनके कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हो, जैसा कि अनुच्छेद 15(3) में उल्लेखित है।
- भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को सुरक्षा:
- भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कई प्रावधान हैं, जैसे दुष्कर्म (धारा 375), पीछा करना (धारा 354), स्त्री की असम्मानजनक छवि बनाना (धारा 509) और घरेलू हिंसा (धारा 498A)।
- ये प्रावधान महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को सुरक्षा:
- दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं, जैसे महिलाओं के लिए अलग से महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विशेष सुनवाई, और उनके बयान सुरक्षित स्थानों पर लेने का प्रावधान।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं को हिंसा और शोषण के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतें भी बनाई गई हैं।
- महिलाओं के अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत और सम्बन्धित अपराधों का प्रतिषेध:
- महिलाओं के अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है महिलाओं का अवमानना, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण, और उन्हें एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना।
- भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से संबंधित अपराधों के लिए कड़े प्रावधान हैं, जैसे अश्लील चित्रण (धारा 292) और इंटरनेट पर अशिष्ट सामग्री साझा करना (धारा 67)।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं के अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए विभिन्न कानूनी उपायों और नीतियों को लागू किया गया है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 के उद्देश्यों और लक्ष्यों की व्याख्या:
- उद्देश्य: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के बीच विवाह को अवैध बनाना था।
- लक्ष्य: इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य बालकों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना था, क्योंकि बाल विवाह के परिणामस्वरूप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती थीं। यह कानून बाल विवाह को रोकने और किशोरों की शिक्षा और मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए था।
बाल विवाह के बावजूद अधिनियम का प्रभाव:
- भारत में बाल विवाह की समस्या का प्रभावी रूप से समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि यह प्रथा सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जड़ पकड़ चुकी है।
- कई स्थानों पर पारंपरिक मान्यताएँ, गरीबी, शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता बाल विवाह को बढ़ावा देती हैं।
- इसके अलावा, कानून की पूरी जानकारी का अभाव और प्रभावी निगरानी की कमी के कारण बाल विवाह को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है।
- ‘सती’ शब्द की परिभाषा और सती (निवारण) अधिनियम के उद्देश्य:
- सती: सती का अर्थ है उस प्रथा से है जिसमें एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में कूदकर आत्महत्या करती थी।
- सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के उद्देश्य:
- सती प्रथा को समाप्त करना और इसे कानूनी रूप से दंडनीय बनाना।
- सती के मामलों में आरोपी व्यक्तियों को दंडित करना, जिनमें प्रोत्साहन देने वाले और सती करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति शामिल थे।
- समाज में सती प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाना और महिलाओं के सम्मान और जीवन की रक्षा करना।
- सती होने के लिए दुष्प्रेरित करना और सती विषयक अन्य निषेधित कार्यों का वर्णन:
- सती के लिए दुष्प्रेरित करना: किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को यह उकसाना या प्रेरित करना कि वह अपने पति के साथ सती हो जाए।
- सती विषयक निषेधित कार्य: इसमें सती की कोशिश करने वाली महिला की मदद करना, उसे इसके लिए उकसाना या उसके परिवार के सदस्य द्वारा यह निर्णय लेने में सहयोग देना शामिल है।
- जिला मजिस्ट्रेटों या जिलाधीश की शक्तियाँ:
- सती प्रथा से संबंधित किसी भी कार्य में प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होती है।
- जिलाधीश को यह अधिकार है कि वह सती होने के प्रयासों को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में त्वरित कार्रवाई करें और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करें।
- महिलाओं के दृष्टिकोण से अपराधों की व्याख्या:
(क) लज्जा भंग (Outrage of Modesty):
- यह अपराध तब होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा महिला की शारीरिक या मानसिक असम्मानजनक स्थिति उत्पन्न की जाती है, जैसे कि उसे गंदे या अपमानजनक तरीके से छेड़ना।
(ख) बलात्कार (Rape):
- बलात्कार एक गंभीर अपराध है, जिसमें किसी महिला के साथ उसके सहमति के बिना यौन शोषण किया जाता है। यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत दंडनीय है।
(ग) अप्राकृतिक अपराध (Unnatural Offence):
- अप्राकृतिक अपराध तब होते हैं जब यौन संबंध सामान्य शारीरिक संबंधों से बाहर होते हैं, जैसे कि समलैंगिक संबंध या जानवरों के साथ यौन संबंध। इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 में अपराध माना गया है।
(घ) लज्जा का अनादर (Insult of Modesty):
- लज्जा का अनादर तब होता है जब किसी महिला का शारीरिक या मानसिक सम्मान खोला जाता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना, उसके कपड़े खींचना या उसका शारीरिक शोषण करना।
- “अनैतिक व्यापार” क्या है? स्पष्ट करें।
- अनैतिक व्यापार (Immoral Traffic) का मतलब है, वह व्यापार जिसमें शारीरिक शोषण या यौन शोषण किया जाता है, जैसे वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी आदि। यह व्यापार महिलाओं और बच्चों के शोषण और उत्पीड़न से जुड़ा होता है और इसे रोकने के लिए कई कानूनी उपाय किए गए हैं।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति चलाने या वेश्यागृह के रूप में परिसरों को प्रयुक्त करने देने के लिये दण्ड की व्यवस्था:
- इस अधिनियम के तहत, वेश्यावृत्ति चलाने और वेश्यागृह के रूप में परिसरों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
- वेश्यावृत्ति के संचालन और वेश्यागृह चलाने के लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति के निवारण हेतु निवारक व्यवस्थाएँ:
- इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों की तस्करी और उनका यौन शोषण रोकने के लिए निवारक उपाय किए गए हैं।
- इसमें पीड़ित महिलाओं और बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजने, उनके पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने और उन्हें शारीरिक और मानसिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
- इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत, वेश्यावृत्ति में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न की समस्या की विवेचना:
- कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न की समस्या गंभीर है और इसमें शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं। यह अपराध विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे अश्लील टिप्पणियाँ, छेड़छाड़, शारीरिक शोषण, और काम का अनुचित दबाव डालना।
- इस प्रकार के उत्पीड़न से महिलाओं की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिससे उनकी कार्यकुशलता और सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- इसके समाधान के लिए विभिन्न कानूनों जैसे ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निवारण) अधिनियम, 2013’ की आवश्यकता पड़ी, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति के लिए दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन:
- सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति को भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के तहत अवैध माना जाता है। इसके तहत वेश्यावृत्ति करने या इसे बढ़ावा देने के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।
- इसके तहत वेश्यावृत्ति करने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें गिरफ्तारियां, जुर्माना और सजा की व्यवस्था है।
वेश्यागृह में निरुद्ध करने सम्बन्धी दण्ड:
- वेश्यागृह में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए “अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956” के तहत कड़े दंड का प्रावधान है। इसमें वेश्यावृत्ति के संचालन या वेश्यागृह में बंधक बनाए गए व्यक्तियों के लिए दंड, जुर्माना और जेल की सजा निर्धारित की गई है।
- संक्षिप्त टिप्पणी:
(1) व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपयुक्त करना और उत्प्रेरित करना:
- यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए उकसाता है या उसे इसके लिए प्रेरित करता है। इसे “वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना” कहा जाता है और इसे दंडनीय अपराध माना जाता है।
(2) वेश वेश्यावृत्ति के लिए याचना करने पर दंड:
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से वेश्यावृत्ति के लिए याचना करता है, तो यह अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान होता है।
- विभिन्न शब्दों की परिभाषा:
(क) वेश्यागृह:
- वेश्यागृह वह स्थान है जहां वेश्यावृत्ति होती है, यानी एक ऐसा घर या परिसर जहां वेश्याओं द्वारा शारीरिक सेवाएँ दी जाती हैं।
(ख) सुधार संस्था:
- सुधार संस्था वह स्थान है जहां वेश्याओं और उनके शिकार व्यक्तियों को पुनर्वास और सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए सहायता दी जाती है।
(ग) वेश्यावृत्ति:
- वेश्यावृत्ति उस व्यवसाय को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं, शारीरिक संबंधों के बदले आर्थिक लाभ प्राप्त करती हैं।
(घ) वेश्या:
- वेश्या वह महिला होती है जो वेश्यावृत्ति करती है और शारीरिक सेवाएं प्रदान करने के बदले धन प्राप्त करती है।
(ङ) बालक:
- बालक वह व्यक्ति है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है और कानून के अनुसार इसे एक अवयस्क माना जाता है। बालक को विशेष कानूनी संरक्षण और अधिकार प्राप्त होते हैं।
अध्याय 8: विवाह एवं विवाह-विच्छेद (Marriage and Divorce)
- हिन्दू विधि में विवाह के स्वरूप का वर्णन:
- हिन्दू विवाह एक धार्मिक और संस्कारिक प्रक्रिया है, जो धर्म, सामाजिक परंपराओं और रीति-रिवाजों पर आधारित है। हिन्दू विवाह को एक अनश्वर बंधन माना जाता है, जो जीवनभर के लिए होता है और इसका उद्देश्य पति-पत्नी के बीच दैवीय और मानसिक सम्बन्धों का निर्माण करना है।
- यह एक संस्कार है, न कि केवल एक कानूनी अनुबंध, और इसमें आठ प्रमुख संस्कार होते हैं जैसे सात फेरे, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा आदि।
- वैध हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें और हिन्दू लड़की का मुस्लिम लड़के से विवाह:
- वैध हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें:
- दोनों पक्षों की उम्र कम से कम 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए।
- दोनों पक्षों को मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से विवाह करने का अधिकार होना चाहिए।
- दोनों पक्षों का हिन्दू धर्म से संबंधित होना चाहिए (मुस्लिम, ईसाई, या अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह नहीं किया जा सकता)।
- क्या एक हिन्दू लड़की मुसलमान लड़के से विवाह कर सकती है?:
- हिन्दू लड़की का मुस्लिम लड़के से विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं होता, क्योंकि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह केवल हिन्दू धर्म के व्यक्तियों के बीच हो सकता है। यदि लड़की और लड़का विभिन्न धर्मों के हैं तो उन्हें विशेष विवाह अधिनियम का पालन करना होगा।
- “हिन्दू विवाह एक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा” विवेचना:
- हिन्दू विवाह एक संस्कार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह धर्म और आस्था का एक अनश्वर बंधन है, न कि सिर्फ एक कानूनी अनुबंध।
- मुस्लिम विवाह एक संविदा है, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से शर्तों के तहत विवाह करते हैं, और इसे कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, हिन्दू विवाह को दैवीय माना जाता है जबकि मुस्लिम विवाह को कानूनी समझौता।
निर्णीत वादों का हवाला:
- “मूलविक और दूसरों” केस में भारतीय न्यायालय ने हिन्दू विवाह को संस्कार के रूप में स्थापित किया और मुस्लिम विवाह को संविदा के रूप में माना।
- संक्षिप्त टिप्पणी:
(1) दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights):
- यह एक कानूनी अधिकार है जिसमें यदि कोई पति या पत्नी विवाहिक संबंधों से अलग हो जाए, तो वह अदालत से यह मांग कर सकता है कि दूसरे पक्ष को फिर से विवाहिक संबंधों में प्रवेश करने का आदेश दिया जाए।
(2) न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation):
- यह एक कानूनी स्थिति है जिसमें पति और पत्नी एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका विवाह वैध रहता है। यह तलाक से पहले एक कदम हो सकता है।
- हिन्दू विधि के अन्तर्गत न्यायालय किन आधारों पर विवाह-विच्छेद की डिक्री दे सकता है?
- हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत, न्यायालय विवाह-विच्छेद की डिक्री दे सकता है यदि विवाह में किसी भी पक्ष से तलाक के लिए आधार साबित हो, जैसे:
- विवाह के पश्चात किसी एक पक्ष का परित्याग या क्रूरता।
- विवाह के बाद कोई अपराध करना, जैसे दुष्कर्म।
- मानसिक विकृति।
- विवाह का कोई अन्य बाधक कारण।
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में तलाक के अतिरिक्त आधार:
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के कुछ अतिरिक्त आधार होते हैं, जिनमें:
- मानसिक विकृति: यदि किसी पार्टी के पास मानसिक विकृति है, जो विवाह जीवन को प्रभावित करती है, तो तलाक का आधार बन सकती है।
- दुष्कर्म, क्रूरता या परित्याग: पति या पत्नी द्वारा दुष्कर्म या क्रूरता करना, या पति या पत्नी का परित्याग करना।
- साधारण रूप से असंतुष्ट और भरण-पोषण में असमर्थता: जब कोई पत्नी अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ होती है या पति द्वारा विवाह जीवन को त्याग दिया जाता है।
- नियमित रूप से घर छोड़ने की स्थिति: यदि कोई पार्टी बिना किसी कारण के घर छोड़ देती है और वापसी नहीं करती है।
- मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वैध विवाह के तत्व:
- वैध मुस्लिम विवाह के मुख्य तत्व:
- आग्रह और स्वीकृति: विवाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। इसे “इज्ज़ात” कहा जाता है, जो विवाह के प्रत्येक पक्ष द्वारा दी जाती है।
- गवाह: मुस्लिम विवाह में दो वयस्क गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है।
- महर (Dower): विवाह में एक मिन्नत या महर (दहेज) की पेशकश होती है जिसे पुरुष अपनी पत्नी को देना होता है।
- विवाह का प्रस्ताव और स्वीकारोक्ति: विवाह के लिए एक प्रस्ताव (इजाब) और स्वीकारोक्ति (कबूल) होना जरूरी है।
- मोहम्मदन कानून के तहत विवाह के लिए प्रतिबंध:
- विवाह में धोखाधड़ी: किसी को धोखाधड़ी से विवाह में सम्मिलित करना अवैध है।
- अनुशासनहीनता: विवाह में इस्लामिक शरियत के अनुसार अनुशासन का पालन करना आवश्यक है।
- विवाह में अविवाहित या तलाकशुदा से संबंध: तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिए विवाह की शर्तें अलग होती हैं, और विवाह के लिए विवाह की समयसीमा के नियम होते हैं।
- मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी द्वारा पति से तलाक के आधार: मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत, मुस्लिम पत्नी निम्नलिखित आधारों पर अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती है:
- पति द्वारा शारीरिक क्रूरता।
- पति का परित्याग: यदि पति अपनी पत्नी को निरंतर छोड़ देता है।
- पति का दुष्कर्म: यदि पति अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म करता है।
- मां-बाप या अन्य रिश्तेदारों के द्वारा उपेक्षा: अगर पति अपनी पत्नी और उसके परिवार का भरण-पोषण नहीं करता।
- मुस्लिम विधि में असंमती महर के लिए विधवा के अधिकार:
- असंमती महर (Unpaid Dower): मुस्लिम विधि में महर का भुगतान विवाह के बाद किया जाता है, यदि इसे भुगतान नहीं किया जाता है तो महिला को असंमती महर का अधिकार होता है। यह विधवा महिला के लिए एक कानूनिक अधिकार है, जो अपनी संपत्ति से उसका भुगतान कर सकती है।
महिलाओं और बालकों का भरण-पोषण
- दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार भरण-पोषण का आदेश:
- दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह अपनी पत्नी, बच्चों, या माता-पिता का भरण-पोषण करेगा, तो यह तब होता है जब:
- व्यक्ति द्वारा भरण-पोषण की आवश्यकता साबित होती है।
- विवाह के दौरान पति या पत्नी के द्वारा बुरा व्यवहार या परित्याग।
- माता-पिता या बच्चे बेसहारा हो और भरण-पोषण का अधिकार हो।
- प्रक्रिया में याचिका दायर करना, सुनवाई, और न्यायालय द्वारा आदेश शामिल हैं।
- भरण-पोषण स्वीकृत करने हेतु आवश्यक शर्तें:
- भरण-पोषण स्वीकृति के लिए आवश्यक शर्तें हैं:
- पति, पत्नी, बच्चों, या माता-पिता को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए।
- भरण-पोषण देने वाली पार्टी की ओर से कोई अनुशासनहीनता या परित्याग न हो।
- भरण-पोषण की शर्तों का प्रमाण होना चाहिए (जैसे आय की स्थिति और विवाह का अस्तित्व)।
- दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण के आदेश को परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है:
- भरण-पोषण आदेश को निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है:
- यदि किसी पक्ष के पास वित्तीय स्थिति बदल जाती है (जैसे नौकरी में बदलाव या चिकित्सा कारण)।
- यदि किसी पक्ष ने भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की है।
- यदि भरण-पोषण प्राप्त करने वाली पार्टी ने सुधारात्मक कार्य किए हों (जैसे आर्थिक स्थिति में सुधार)।
- एक हिन्दू स्त्री जो निर्वसीयत मरती है उसकी सम्पत्ति के वितरण से संबंधित विभिन्न नियम:
- जब एक हिन्दू स्त्री निर्वसीयत मरती है, तो उसकी सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पति, बच्चों, माता-पिता, और अन्य कानूनी वारिसों में विभाजित होती है। इसमें मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:
- पति और बच्चों का अधिकार: यदि स्त्री के पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी है, तो पति और बच्चों को सम्पत्ति में हिस्सा मिलता है।
- माता-पिता का अधिकार: अगर महिला की कोई संतान नहीं है, तो माता-पिता को सम्पत्ति का अधिकार मिलता है।
- वारिसों का हिस्सेदारी का निर्धारण: यदि कोई लिखित वसीयत नहीं है, तो सम्पत्ति को कानूनी तरीके से वारिसों में वितरित किया जाता है।
- स्वोधन (Stridhan) की प्रमुख विशेषताएँ एवं स्रोत:
स्वोधन एक हिन्दू महिला की सम्पत्ति है, जो शादी के बाद भी उसे अपने व्यक्तिगत अधिकारों के तहत स्वामित्व में रहती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- स्वतंत्र स्वामित्व: यह सम्पत्ति महिला की होती है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग या नष्ट कर सकती है।
- विवाह के समय प्राप्त सम्पत्ति: इसे शादी के अवसर पर महिला को दी गई सम्पत्ति माना जाता है, जैसे दहेज, उपहार आदि।
- स्वधीनता: स्त्रीधन का उपयोग महिला के विवाहित जीवन या उसकी मृत्यु के बाद भी महिलाओं के पास रहने वाले अधिकारों के तहत किया जाता है।
स्रोत:
- विवाह के समय दहेज: दहेज के रूप में महिला को प्राप्त संपत्ति।
- उपहार और उपस्थिति: परिवार से या ससुराल से मिलने वाले उपहार।
- व्यक्तिगत संपत्ति: जो महिला ने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से अर्जित की हो।
- नारी सम्पदा (Nari Sampada) क्या है और इसके परिणाम:
नारी सम्पदा वह सम्पत्ति है जो महिला के पास व्यक्तिगत रूप से होती है और जिसका वह स्वतंत्र स्वामित्व रखती है। इसे स्त्रीधन (Stridhan) भी कहा जाता है। यह सम्पत्ति महिला के विवाह, जन्म, या जीवन के अन्य अवसरों पर प्राप्त होती है, जैसे दहेज, उपहार आदि।
नारी सम्पदा के परिणाम:
- आर्थिक स्वतंत्रता: नारी सम्पदा महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है।
- कानूनी अधिकार: महिला को अपनी सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है, उसे बेचने, दान करने या लेन-देन करने का अधिकार होता है।
- विरासत में हिस्सा: महिला अपनी सम्पत्ति को अपने बच्चों या अन्य परिवार के सदस्यों को विरासत में दे सकती है।
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध में संशोधित अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत परिवर्तन:
- संशोधन 2005 के अनुसार, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में यह परिवर्तन किया गया कि अब पुत्री और पुत्र के बीच सम्पत्ति के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है। पहले, महिला को केवल अपने पति या पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था, लेकिन अब उसे भी सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त हैं।
- पुत्री का अधिकार: अब एक महिला को अपने पिता की सम्पत्ति में वही अधिकार है जो एक पुत्र को होता है।
- महिलाओं द्वारा दत्तक ग्रहण की सामर्थ्य:
- हिन्दू विधि के तहत, महिला को दत्तक ग्रहण करने का अधिकार है। महिला न केवल पुत्र बल्कि पुत्री को भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। यह अधिकार उसे हिन्दू दत्तक ग्रहण और दत्तक विधि अधिनियम, 1956 के तहत प्राप्त है।
- महिला को अपने पति की सहमति से या फिर विधवा होने पर अकेले दत्तक ग्रहण का अधिकार होता है।
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्त्रीधन एवं उत्तराधिकार:
- स्त्रीधन: स्त्रीधन वह सम्पत्ति है जो एक महिला को विवाह के समय या जीवन के अन्य अवसरों पर प्राप्त होती है। यह सम्पत्ति महिला की होती है और उसे अपनी इच्छा से उसका उपयोग करने का अधिकार होता है।
- उत्तराधिकार: हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, स्त्री को अपनी सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। इसके तहत, यदि महिला अपनी सम्पत्ति का मरणोपरांत उत्तराधिकार छोड़ देती है, तो उसके वारिसों को उसका हिस्सा मिलता है।
गर्भपात एवं नवजात शिशु विषयक अपराध
- गर्भपात (Miscarriage) से क्या अभिप्राय है और गर्भपात से संबंधित दंडप्रवधान:
- गर्भपात वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती महिला का गर्भ किसी बाहरी कारण से स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। यह प्रायः 20 सप्ताह के भीतर होता है।
- दंडप्रवधान: भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत गर्भपात के लिए दंड दिया जाता है। अगर गर्भपात महिला की सहमति से किया जाता है, तो यह मेडिकल गर्भपात अधिनियम, 1971 के तहत वैध होता है। लेकिन यदि किसी महिला का गर्भपात बिना सहमति के किया जाए, तो यह अपराध माना जाता है और दंडनीय होता है।
- नवजात शिशु विषयक अपराध:
- नवजात शिशु के खिलाफ अपराधों में हत्या, क्रूरता, या नवजात शिशु को छोड़ देना शामिल हैं। ये सभी अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय हैं।
लिंग चयन का प्रतिबंध:
- लिंग चयन के लिए गर्भवती महिला का लिंग निर्धारण करना और इस पर आधारित गर्भपात करना भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। यह अपराध प्रजनन, लिंग चयन और बालिका भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित है।
औद्योगिक विधियों के अंतर्गत सुरक्षा
- कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अल्पवयस्कों को सुरक्षाएँ:
- कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत, अल्पवयस्कों (14 वर्ष से कम आयु के बच्चों) को कारखानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- अल्पवयस्कों को काम करने के लिए अनुमत घंटे: बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होती और सप्ताह में 24 घंटे से ज्यादा नहीं काम किया जा सकता।
- बालकों के लिए काम का समय:
- बालकों के लिए काम का समय 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखाना अधिनियम के तहत सीमित किया गया है। उन्हें दिन में 4 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होती।
महिलाओं की रात्रि पाली में काम की मंजूरी:
- महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम करने के लिए विशेष अनुमतियाँ और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
चिकित्सीय परीक्षा संबंधी उपबन्ध:
- महिलाएँ और बच्चे जिन्हें खतरनाक कामों में कार्यरत किया जाता है, उन्हें नियमित चिकित्सीय जांच के लिए अधिनियम के तहत विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं।
48. भारत में “दहेज प्रथा के विकास एवं मूलभूत लक्षणों की व्याख्या:
दहेज प्रथा भारत में एक पुरानी सामाजिक परंपरा है, जिसमें विवाह के दौरान दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे और उसके परिवार को संपत्ति, धन, या अन्य मूल्यवान चीजें दी जाती हैं।
विकास:
- प्रारंभिक काल: दहेज का प्रारंभ विवाह के समय महिला को संपत्ति देने के रूप में हुआ था, जिसे “स्वधन” या “स्त्रीधन” कहा जाता था।
- मध्यकाल: दहेज की प्रथा ने विकृत रूप धारण किया, और यह दुल्हन के परिवार से अत्यधिक संपत्ति लेने का एक सामाजिक दबाव बन गया।
- आधुनिक समय: आजकल दहेज को एक अपराध माना जाता है, लेकिन यह अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, और यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दबाव के कारण लगातार बढ़ रहा है।
मूलभूत लक्षण:
- विवाह में अनिवार्य वस्तु: दहेज विवाह का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जिसे बिना दिए विवाह संपन्न नहीं हो सकता।
- सामाजिक दबाव: परिवारों पर दहेज देने और लेने के लिए सामाजिक दबाव होता है।
- अर्थशास्त्र: दहेज की मांग अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों द्वारा की जाती है और यह एक वित्तीय समझौते की तरह कार्य करता है।
49. दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रयोज्य “दहेज” की परिभाषा दीजिए:
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज की परिभाषा “किसी भी प्रकार की संपत्ति या धन जो एक पक्ष (दुल्हन के परिवार) द्वारा दूसरे पक्ष (दूल्हे के परिवार) को विवाह के समय या विवाह के बाद दी जाती है” के रूप में की गई है।
क्या यह विधि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही है?:
- हालांकि दहेज प्रथा पर नियंत्रण लगाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था, लेकिन यह अभी भी कई क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है।
- कारण:
- सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव, जहां दहेज को एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
- दहेज संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने में परिवारों द्वारा हिचकिचाहट और डर।
- पुलिस और न्यायिक प्रणाली में दोषपूर्ण कार्यान्वयन और असामान्य दंड।
50. दहेज देने या लेने के लिए शास्ति सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन:
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज देने या लेने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं:
- दहेज लेने पर दंड: यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- दहेज देने पर दंड: अगर किसी व्यक्ति को दहेज देने का दोषी पाया जाता है, तो उसे भी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- सजा: दहेज लेने और देने दोनों मामलों में सजा दी जाती है, और यह सजा पुरुषों, महिलाओं और उनके परिवारों के लिए समान रूप से लागू होती है।
51. विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता, दहेज मृत्यु और दहेज मृत्यु की उपधारणा:
- (क) विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता:
- क्रूरता से तात्पर्य शारीरिक या मानसिक यातना से है, जो एक महिला को उसके पति या ससुराल वालों द्वारा दी जाती है।
- इसमें शारीरिक हिंसा, अपमानजनक व्यवहार, या मानसिक उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत यह अपराध है।
- (ख) दहेज मृत्यु:
- दहेज मृत्यु वह स्थिति है जब एक महिला को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, और अंततः उसकी मौत हो जाती है।
- यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
- (ग) दहेज मृत्यु की उपधारणा:
- उपधारणा के अनुसार, यदि कोई महिला दहेज के लिए उत्पीड़ित हुई हो और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह माना जाता है कि उसकी मृत्यु दहेज उत्पीड़न के कारण हुई है।
- कानून में यह विरुद्ध माना जाता है और इसे अपराध माना जाता है, जब कोई महिला दहेज की वजह से मृत पाई जाती है। यह दहेज के संबंध में एक विशेष कानूनी धारणा है, जिससे आरोपी को अपराधी माना जा सकता है।
52. द्विविवाह (Bigamy) क्या है? इसके अपवाद क्या हैं?
- द्विविवाह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है। यह भारतीय कानून के तहत अपराध है, यदि व्यक्ति हिन्दू है तो यह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबंधित है।
- अपवाद:
- यदि एक व्यक्ति का पहला विवाह रद्द हो चुका है या उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो दूसरा विवाह वैध हो सकता है।
- इस प्रथा को एक वैध विवाह माना जाता है जब पहले विवाह में कोई कानूनी समस्या होती है।
53. ‘जारकर्म’ (Adultery) क्या है? जारकर्म के आवश्यक तत्व:
- जारकर्म वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति विवाहित व्यक्ति के साथ बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अपराध माना जाता था, हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।
- आवश्यक तत्व:
- एक व्यक्ति का विवाहित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना।
- यह सहमति से किया गया होना चाहिए और कोई कानूनी अवरोध नहीं होना चाहिए।
54. विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना:
- आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना तब होता है जब कोई व्यक्ति विवाहित महिला को धोखाधड़ी या छल से उसके घर से बाहर ले जाता है, या उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाता है। यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाता है।
- आवश्यक तत्व:
- महिला का धोखाधड़ी से फुसलाकर स्थानांतरित किया जाना।
- उद्देश्य महिला को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका उत्पीड़न या उसका अधिकार छीनना होता है।
55. व्यपहरण (Kidnapping) और अपहरण (Abduction) से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- व्यपहरण (Kidnapping):
- परिभाषा: व्यपहरण वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, अक्सर बलपूर्वक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 के तहत अपराध माना जाता है।
- प्रकार:
- व्यस्क व्यक्ति का व्यपहरण: जब किसी वयस्क व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध लिया जाता है।
- बालक का व्यपहरण: किसी बालक या लड़की को उसकी इच्छा के बिना उठाना, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 363A के तहत विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।
- अपहरण (Abduction):
- परिभाषा: अपहरण में किसी व्यक्ति को किसी स्थान से या स्थानों के बीच, धोखाधड़ी या बल का प्रयोग करके ले जाना शामिल होता है, लेकिन इसमें उस व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से नियंत्रित करने का उद्देश्य होता है। इसे IPC की धारा 364A के तहत परिभाषित किया गया है।
- प्रकार:
- बलपूर्वक अपहरण: किसी व्यक्ति को बल या धमकी के द्वारा अपहरण करना।
- धोखाधड़ी से अपहरण: किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या छल से अपहरण करना।
अंतर:
- व्यपहरण में व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया होती है, जबकि अपहरण में व्यक्ति का स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन उद्देश्य उसे नियंत्रण में रखना और उसका शोषण करना होता है।
- व्यपहरण का अधिकतर उद्देश्य आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ होता है, जबकि अपहरण का उद्देश्य आमतौर पर दंड, सजा या भय उत्पन्न करना होता है।
56. व्यपहरण एवं अपहरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
- व्यपहरण (Kidnapping) के प्रकार:
- बालकों का व्यपहरण: यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को 18 वर्ष से कम उम्र में उसकी सहमति के बिना उठाया जाता है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत परिभाषित है।
- व्यस्क व्यक्ति का व्यपहरण: किसी वयस्क व्यक्ति को उसके अपने घर से या किसी अन्य स्थान से उसकी सहमति के बिना उठा लेना। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 363A में आता है।
- अपहरण (Abduction) के प्रकार:
- बलपूर्वक अपहरण: इसमें किसी व्यक्ति को बल या हिंसा का प्रयोग करके उठा लिया जाता है। इसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
- धोखाधड़ी से अपहरण: इसमें किसी व्यक्ति को झांसा देकर या धोखाधड़ी से फुसलाकर उठाया जाता है।
- नारी या बालिका का अपहरण: इसमें महिलाओं और बालिकाओं का अपहरण किया जाता है, जो शारीरिक और मानसिक शोषण का कारण बनता है।
57. प्रसूति-प्रसुविधा और अनुतोष से सम्बन्धित विधि पर विचार-विमर्श कीजिए।
- प्रसूति लाभ (Maternity Benefit): यह एक कानूनी अधिकार है जो महिलाओं को प्रसव के दौरान या उसके बाद मिलने वाले लाभों से संबंधित है। इसके तहत महिला को उसकी कार्यस्थल पर अपनी प्रसूति और पुनः कार्य में शामिल होने तक छुट्टी मिलती है, साथ ही वेतन या अन्य सुविधाओं का अधिकार भी होता है।
- अनुतोष (Relief): यह महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य, आराम, और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। इसमें प्रसूति के बाद महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है।
58. (i) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नियोजित महिलाओं को कौन-कौन से प्रमुख लाभ एवं अधिकार प्राप्त हैं?
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत नियोजित महिलाओं को निम्नलिखित प्रमुख लाभ मिलते हैं:
- प्रसूति के लिए अवकाश: महिला को प्रसव के समय 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। यह छुट्टी निःशुल्क होती है, और महिला को बिना किसी नुकसान के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।
- भरण-पोषण: महिला को प्रसूति के दौरान वेतन का भुगतान किया जाता है।
- अन्य विशेष छुट्टियाँ: गर्भपात या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अतिरिक्त छुट्टियाँ दी जाती हैं।
58. (ii) मातृत्व हित लाभ अधिनियम में स्त्री की मृत्यु की दशा में मातृत्व हित लाभ के भुगतान के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं?
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत, यदि कोई महिला प्रसूति के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उसके परिजनों को एक महीने तक मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान महिला की मृत्यु के समय तक काम करती थी, और इसे उसके परिवार के सदस्य को जारी किया जाता है।
59. (i) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के तहत निरीक्षक (Inspectors) की नियुक्ति की जाती है, जो विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में महिलाओं के मातृत्व लाभ के अधिकारों की निगरानी करते हैं। निरीक्षकों के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित हैं:
- नियुक्ति: राज्य सरकार द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।
- अधिकार: निरीक्षकों को कंपनी या संस्था के स्थानों पर जाकर यह सुनिश्चित करने का अधिकार होता है कि मातृत्व लाभ का पालन हो रहा है।
- कर्तव्य: निरीक्षकों को उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का कर्तव्य होता है।
59. (ii) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
- (क) मातृत्व लाभ का अपवर्जन: जब कोई महिला नियमों का उल्लंघन करती है, जैसे कि अवकाश की अवधि का पालन नहीं करना या जानबूझकर मातृत्व लाभ का अपवर्जन करना, तो उसका मातृत्व लाभ रद्द किया जा सकता है।
- (ख) नियोजक द्वारा अधिनियम के उल्लंघन पर दण्ड: यदि कोई नियोजक मातृत्व लाभ अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना या सजा हो सकती है। जुर्माना के रूप में अधिकतम राशि दी जा सकती है।
- (ग) भ्रूणपात के लिए छुट्टी: यदि किसी महिला को भ्रूणपात (मिसकैरेज) होता है, तो मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत उसे छुट्टी मिलती है। यह छुट्टी आमतौर पर 6 सप्ताह की होती है, ताकि महिला मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो सके।
60. बाल मजदूर (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उन विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या कीजिए जो बच्चों के कार्य की दशाओं को विनियमित करते हैं।
बाल मजदूरी (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत निम्नलिखित उपबन्ध हैं:
- बालकों का कार्य निषेध: इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रमिक कार्य में नियोजित करने की अनुमति नहीं है।
- कार्य स्थल पर बच्चों के लिए सुरक्षित शर्तें: यदि बच्चों को किसी कार्य में लगाया जाता है, तो उन कार्यस्थलों को बालक के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाना अनिवार्य है।
- शिक्षा का अधिकार: यदि बालक काम करता है, तो उसे शिक्षा के अवसर मिलते रहना चाहिए।
- दंड का प्रावधान: यदि इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है, तो नियोजक को दंडित किया जाता है।
61. महिला श्रम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपबन्धों की व्याख्या कीजिए।
महिला श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण उपबन्धों के तहत महिलाओं को उनके कामकाजी अधिकारों की सुरक्षा दी जाती है। मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं:
- समान वेतन का अधिकार: महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिले।
- रात्रि पाली में काम करने पर प्रतिबंध: महिला श्रमिकों को रात्रि शिफ्टों में काम करने से पहले विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को रात के समय काम करने से रोका जाता है।
- प्रसूति अवकाश: मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है, जिसमें महिला को प्रसव के दौरान छुट्टी मिलती है और उसके वेतन का भुगतान किया जाता है।
- सुरक्षा और आरामदायक कार्य शर्तें: महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर आरामदायक और सुरक्षित कार्य शर्तें सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसमें शारीरिक सुरक्षा, मानसिक कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
62. बाल श्रम पर उच्चतम न्यायालय की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम के खिलाफ विभिन्न निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत:
- समीक्षा और सुधार: उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक फैसले दिए और सरकार से बालकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में काम करने की अपील की।
- बाल श्रम के खिलाफ दिशा-निर्देश: न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि बच्चों से शारीरिक, मानसिक शोषण और अपमानजनक कार्यों से बचने के लिए सख्त उपाय किए जाएं।
- बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए निर्देश: उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रमिकों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षित जीवन की ओर पुनः दिशा देने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए।
- विधायन में सुधार: अदालत ने बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 के तहत विधायन में सुधार की आवश्यकता की बात की और कार्यस्थल पर बच्चों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
63. किशोर न्याय से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की व्याख्या कीजिए।
किशोर न्याय (Juvenile Justice) का उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल करना है जो किसी कारणवश आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, और साथ ही उनके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना है।
किशोर न्याय अधिनियम, 2000:
- यह अधिनियम बच्चों की रक्षा और देखभाल के लिए लागू होता है।
- अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के अपराधों के लिए सजा देने के बजाय उनकी सुधार प्रक्रिया पर जोर देना है।
- अधिनियम के तहत बच्चों को वैकल्पिक दंड, जैसे कि सुधारक केंद्रों में भेजना, और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाती है।
64. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के संदर्भ में “देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक” और “विधि विवादित किशोर” अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है?
- देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक: ये वे बच्चे होते हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक या सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि वे परिवार से अलग हो गए हैं, या उनके माता-पिता नहीं हैं, या उनका शोषण हो रहा है।
- विधि विवादित किशोर: ये वे बच्चे होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं और किसी अपराध में लिप्त होते हैं। ये किशोर किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपनी दंड प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिनमें सुधारक कदम उठाए जाते हैं।
65. किशोर न्याय बोर्ड से आप क्या समझते हैं? इस बोर्ड से सम्बन्धित जाँच प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए।
किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) वह बोर्ड है जो किशोरों द्वारा किए गए अपराधों का न्यायिक निर्धारण करता है। यह बोर्ड निम्नलिखित कार्य करता है:
- जांच प्रक्रिया: बोर्ड किशोर अपराधियों के मामलों की जांच करता है, जिसमें बालक के अपराध, मानसिक स्थिति, और पारिवारिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जाता है।
- शक्तियाँ: बोर्ड के पास किशोरों को सुधार गृह भेजने, नशीली दवाओं के उपयोग के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करने, और उन्हें शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण देने के आदेश देने की शक्ति होती है।
66. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
- बालक गृह: बालक गृह वह संस्था है जहां बच्चों को सुरक्षा, देखभाल और शिक्षा दी जाती है। यह संस्थाएँ न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती हैं और इनका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास करना होता है।
- आश्रय गृह: आश्रय गृह वह संस्था है जो असहाय, परित्यक्त, या शोषित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह संस्थाएँ सामाजिक न्याय और बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती हैं।
67. किशोर अपराधियों की आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में सुधारक संस्थाओं का क्या योगदान है? स्पष्ट करें।
सुधारक संस्थाएँ किशोर अपराधियों की आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये संस्थाएँ:
- शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करती हैं।
- किशोरों के मनोवैज्ञानिक उपचार और सामाजिक समायोजन पर ध्यान देती हैं।
- स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल की व्यवस्था करती हैं।
- बच्चों को उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच सिखाने के लिए काम करती हैं।
68. किसी बालक के पुनर्वास तथा सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में क्या व्यवस्था है? क्या ये व्यवस्थाएँ अपने आप में पूर्ण हैं?
किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं:
- पुनर्वास कार्यक्रम: किशोर अपराधियों के लिए पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य से सुधार गृह, आश्रय गृह, और शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
- समाज में फिर से समावेशन: कार्यक्रम किशोरों को उनके परिवारों में वापस समायोजित करने, उन्हें रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
हालांकि, इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू करने में अभी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि पर्याप्त संसाधनों की कमी और किशोरों के लिए अधिक स्थिर पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता।
69. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए:
- संप्रेक्षण गृह: संप्रेक्षण गृह एक ऐसी संस्था है जहाँ किशोरों, जो अपराधों में लिप्त होते हैं या जिनके लिए न्यायिक आदेश है, उन्हें रखा जाता है। यहां उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुधार किया जाता है। इन घरों में किशोरों को अपराधियों की तरह नहीं बल्कि सुधार योग्य बच्चों के रूप में देखा जाता है, और उनका उद्देश्य पुनर्वास, शिक्षा, और सुधार प्रदान करना होता है।
- विशेष गृह: विशेष गृह उन बच्चों के लिए हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध हुए हैं या जो अन्यथा सुधार गृह में रखने योग्य नहीं होते। यह संस्थाएँ न्यायालय के आदेश पर स्थापित की जाती हैं और इनका उद्देश्य किशोरों को एक संरक्षित वातावरण में सुधार के अवसर प्रदान करना होता है। विशेष गृह में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक पुनः समायोजन के लिए उपयुक्त सुविधाएँ दी जाती हैं।
70. घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान का उल्लेख करें।
घरेलू हिंसा: घरेलू हिंसा का अर्थ किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, यौन, या भावनात्मक हिंसा से है जो किसी व्यक्ति (विशेष रूप से महिलाओं) के परिवार या घरेलू रिश्तों के भीतर होती है। इसमें शारीरिक शोषण, अपमानजनक व्यवहार, उत्पीड़न, यौन शोषण, या आर्थिक दमन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।
घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान:
- महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: इस कानून के तहत महिलाओं को उनके घरों में हिंसा से बचाने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं।
- महिला के लिए राहत: महिला को सुरक्षा आदेश, आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहायता, आश्रय आदि मिल सकते हैं।
- हिंसा के खिलाफ उपाय: महिला पुलिस अधिकारी और संरक्षण अधिकारी महिला को मदद प्रदान करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
- अधिकारों का उल्लंघन: अगर पति या परिवार का कोई अन्य सदस्य महिला के खिलाफ हिंसा करता है, तो महिला को न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार होता है।
71. दत्तक ग्रहण के अर्थ की व्याख्या कीजिए। इसके उद्देश्यों एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए।
दत्तक ग्रहण: दत्तक ग्रहण का अर्थ है, किसी बालक को कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति या परिवार के सदस्य द्वारा अपने बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार करना। इसमें बालक का पालन-पोषण और कानूनी अधिकार व्यक्ति या परिवार के तहत आते हैं।
उद्देश्य:
- बच्चों के लिए परिवार प्रदान करना: जिन बच्चों के पास परिवार नहीं होते, उन्हें दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थिर और प्यार भरा घर मिल सकता है।
- शोषण से सुरक्षा: बालक को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण देना, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाया जा सके।
- सामाजिक समावेशन: बच्चों का समाज में समावेश कर उनके अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करना।
परिणाम:
- कानूनी अधिकार: दत्तक ग्रहण के बाद, बालक को दत्तक माता-पिता की सारी संपत्ति पर अधिकार मिलता है।
- पालक माता-पिता का अधिकार: दत्तक माता-पिता को बालक की देखभाल और उसका पालन-पोषण करने का कानूनी अधिकार मिलता है।
- नाम और पहचान: बालक का नाम और पहचान उस परिवार से जुड़ जाती है।
72. दत्तक ग्रहीता के माता-पिता के निर्धारण सम्बन्धी क्या प्रावधान किये गये हैं? उल्लेख करें।
दत्तक ग्रहण के तहत दत्तक ग्रहीता (अडॉप्टिव पेरेंट्स) के माता-पिता का निर्धारण संबंधित कानूनों के अनुसार किया जाता है, जैसे कि हिन्दू दत्तक ग्रहण और देखभाल अधिनियम, 1956 के तहत। प्रावधानों के अनुसार:
- हिन्दू धर्म के अनुसार: दत्तक ग्रहण केवल उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो हिन्दू धर्म से संबंधित हों।
- माता-पिता की अनुमति: बच्चे को दत्तक ग्रहण करने से पहले माता-पिता या उनके कानूनी संरक्षकों की अनुमति प्राप्त करनी होती है।
- मूलक पहचान: बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से माता-पिता की पहचान की पुष्टि की जाती है।
- माता-पिता की उम्र: दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की आयु बच्चे से एक निश्चित सीमा तक अधिक होनी चाहिए।
73. दत्तक ग्रहण के अन्तर्गत पुत्र/पुत्री को प्राप्त अधिकारों का उल्लेख करें।
दत्तक ग्रहण के तहत पुत्र/पुत्री को प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- संपत्ति का अधिकार: दत्तक ग्रहण के बाद, दत्तक पुत्र/पुत्री को दत्तक माता-पिता की सम्पत्ति पर कानूनी अधिकार मिलता है।
- संपत्ति की उत्तराधिकारिता: दत्तक पुत्र/पुत्री दत्तक माता-पिता के उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे कि किसी पारिवारिक संपत्ति पर उनका अधिकार हो सकता है।
- नागरिक अधिकार: बच्चे को समाज में कानूनी पहचान और नागरिक अधिकार मिलते हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार।
- पारिवारिक और भावनात्मक सुरक्षा: दत्तक पुत्र/पुत्री को परिवार के सदस्य के रूप में भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है।
74. शिशु लैंगिक यौन सम्बन्धी कुकर्म से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें।
शिशु लैंगिक यौन सम्बन्धी कुकर्म (Child Sexual Abuse) वह अपराध है जिसमें किसी बालक/बालिका के साथ यौन शोषण किया जाता है। इसमें शारीरिक संपर्क, बलात्कार, यौन उत्पीड़न या अन्य यौन कृत्य शामिल हो सकते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक नुकसान का कारण बनता है और यह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
शिशु लैंगिक यौन सम्बन्धी कुकर्म को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों और प्रावधानों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offenses Act), जो बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
(क) मानवाधिकार और महिलाएँ
परिचय
मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। महिलाओं के मानवाधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्हें समाज में असमानता और अन्याय का सामना करना पड़ा है।
महिलाओं के मानवाधिकारों का महत्व
महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1979 में ‘महिला भेदभाव उन्मूलन संधि (CEDAW)’ को अपनाया गया। भारत में भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान, विशेष कानूनों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कई उपाय किए गए हैं।
महिलाओं के प्रमुख मानवाधिकार
- शिक्षा का अधिकार – हर महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसी योजनाएँ इसी उद्देश्य से लागू की गई हैं।
- स्वतंत्रता का अधिकार – महिलाओं को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने, कार्य करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- समान वेतन का अधिकार – समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, जिसे ‘समान वेतन अधिनियम’ द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
- हिंसा से सुरक्षा का अधिकार – घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं।
- राजनीतिक अधिकार – महिलाओं को मतदान, चुनाव लड़ने और सरकार में भागीदारी का अधिकार मिला हुआ है।
- उत्तराधिकार का अधिकार – हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिला है।
महिलाओं के मानवाधिकारों की चुनौतियाँ
- दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ आज भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
- कार्यस्थल पर लिंगभेद और यौन उत्पीड़न की घटनाएँ महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बाधित करती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
उपसंहार
महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव की भी आवश्यकता है। सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं को समानता और सम्मान देने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि वे भी स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।
(ख) मानवाधिकार और बालक
परिचय
बाल अधिकार (Children’s Rights) मानवाधिकारों का ही एक हिस्सा हैं, जो बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC – 1989) के तहत बच्चों के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है।
बच्चों के प्रमुख मानवाधिकार
- जीवन और अस्तित्व का अधिकार – प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।
- शिक्षा का अधिकार – भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- बाल श्रम से मुक्ति का अधिकार – ‘बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986’ के तहत बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार – सरकार द्वारा ‘मिड-डे मील’ और ‘आंगनवाड़ी’ जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।
- यौन शोषण और शारीरिक हिंसा से सुरक्षा का अधिकार – ‘पॉक्सो अधिनियम, 2012’ बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- परिवार और संरक्षण का अधिकार – अनाथ या बेसहारा बच्चों के लिए ‘किशोर न्याय अधिनियम’ के तहत देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
बच्चों के मानवाधिकारों की चुनौतियाँ
- बाल मजदूरी: कई गरीब परिवारों में बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा और बचपन प्रभावित होता है।
- बाल विवाह: भारत के ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई स्थानों पर बाल विवाह की परंपरा जारी है, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है।
- शोषण और हिंसा: बहुत से बच्चे घरेलू हिंसा, यौन शोषण, और बाल तस्करी जैसी समस्याओं के शिकार होते हैं।
- शिक्षा में असमानता: आर्थिक असमानता के कारण कई बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, जिससे वे विकास की मुख्यधारा से दूर रह जाते हैं।
उपसंहार
बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकार को कठोर कानूनों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। इसके अलावा, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय को भी जागरूक बनना होगा ताकि हर बच्चा अपने अधिकारों के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके।