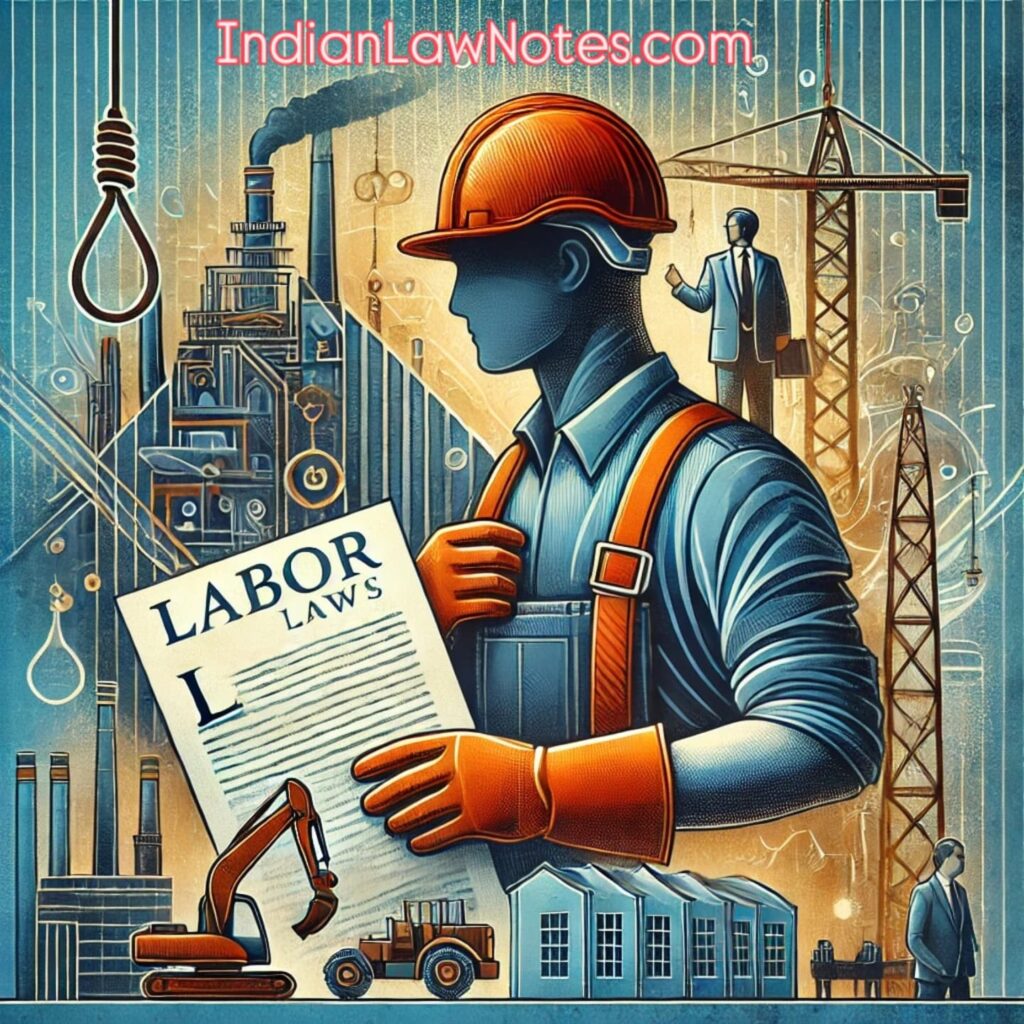लेख शीर्षक:
“मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों का शोषण: सामाजिक अन्याय और कानूनी संरक्षण की आवश्यकता”
🔸 भूमिका:
भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा श्रमिक वर्ग की मेहनत पर टिका है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और प्रवासी श्रमिक देश के निर्माण और विकास में अहम योगदान देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं श्रमिकों का सबसे अधिक शोषण होता है — कम वेतन, लंबी कार्य अवधि, असुरक्षित कामकाजी स्थितियां, और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना इनकी सामान्य स्थिति बन गई है।
🔸 प्रवासी श्रमिक कौन हैं?
प्रवासी श्रमिक वे मजदूर होते हैं जो रोजगार की तलाश में अपने मूल स्थान (गांव, कस्बे) से दूर दूसरे राज्य या शहरों में जाकर अस्थायी रूप से काम करते हैं। ये श्रमिक अकसर निर्माण, फैक्ट्री, होटल, कृषि, घरेलू काम और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं।
🔸 शोषण के प्रमुख रूप:
- कम मजदूरी: न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन नहीं किया जाता और श्रमिकों को बाजार दर से भी कम भुगतान मिलता है।
- लंबे काम के घंटे: श्रमिकों से 10–12 घंटे तक काम करवाया जाता है, जबकि कानूनन 8 घंटे का प्रावधान है।
- अनुबंधहीन और असुरक्षित रोजगार: अधिकांश श्रमिकों के पास लिखित अनुबंध नहीं होता, जिससे वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा का अभाव: न तो उन्हें उचित सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं और न ही बीमार होने पर वेतन या चिकित्सा सुविधा मिलती है।
- महिला श्रमिकों का दोहरा शोषण: उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है और यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी आम हैं।
- प्रवास के दौरान जोखिम: आवास, भोजन, स्वच्छता, परिवहन और भाषा संबंधी दिक्कतें उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में जीने को विवश करती हैं।
🔸 कानूनी प्रावधान और उनकी सीमाएं:
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- श्रम संहिताएं (Labour Codes): मजदूरों के लिए श्रम सुधारों की दृष्टि से ये कानून लाए गए हैं, लेकिन इनका पूर्ण क्रियान्वयन अब भी चुनौती बना हुआ है।
इन कानूनों के बावजूद, जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं होता। प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण नहीं होना, असंगठित क्षेत्र की निगरानी की कमी और भ्रष्टाचार इनके प्रमुख कारण हैं।
🔸 कोरोना महामारी और प्रवासी संकट:
2020 की कोविड-19 महामारी ने प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को सामने लाया। लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूरों को काम, भोजन और आवास के बिना सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव लौटना पड़ा। यह दृश्य भारत के श्रमिकों के प्रति संवेदनहीन नीति और तैयारी की विफलता का प्रतीक बन गया।
🔸 न्यायिक पहल और जनहित याचिकाएं:
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कई मामलों में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों को निर्देश दिए हैं। लेकिन निष्पादन की कमजोर कड़ी के कारण यह प्रभावी नहीं हो पा रहा है।
🔸 समाधान और सुझाव:
- प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण और पहचान पत्र
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पोर्टेबिलिटी (portability) ताकि वे किसी भी राज्य में लाभ ले सकें
- श्रमिकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास
- श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन और निगरानी
- नियोक्ताओं की जवाबदेही तय करना और श्रमिक संघों को सशक्त बनाना
- अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र स्थापित करना
🔸 निष्कर्ष:
मजदूर और प्रवासी श्रमिक समाज के सबसे कमजोर लेकिन सबसे ज़रूरी स्तंभ हैं। उनके श्रम का समुचित मूल्य देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी भी है। जब तक श्रमिकों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा ही रहेगा।