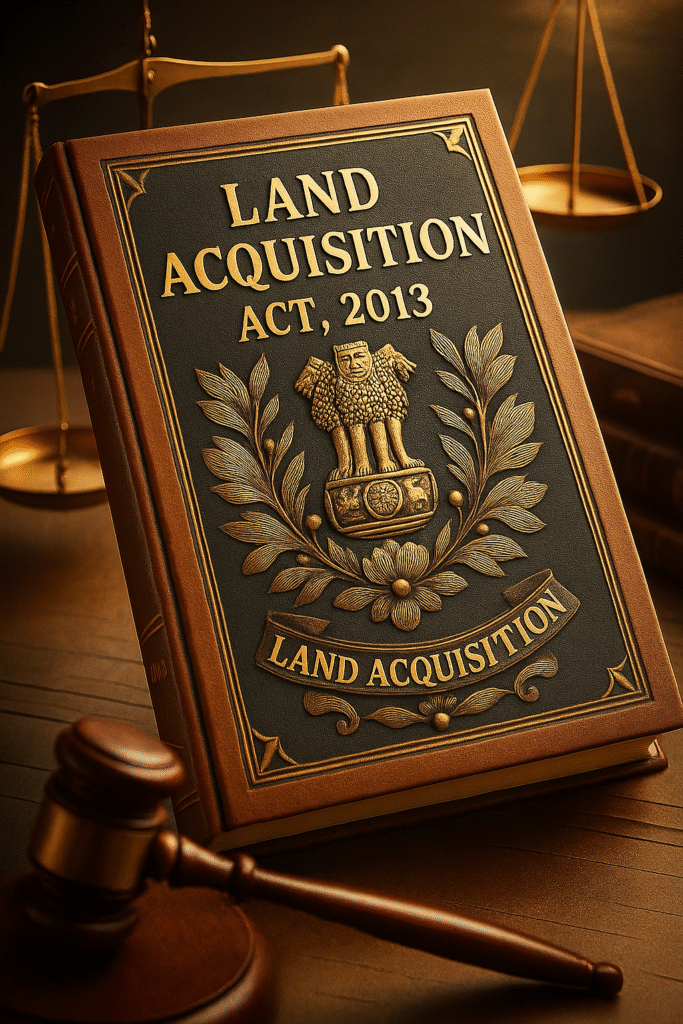भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013: विकास और न्याय का समन्वय
भूमिका
भारत जैसे विकासशील देश में आधारभूत संरचना, उद्योगों, शहरीकरण और सार्वजनिक परियोजनाओं के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। किंतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबे समय से विवादों और असमानता का विषय रही है। किसानों, आदिवासियों और भूमिहीनों के शोषण, अपर्याप्त मुआवज़े, और पुनर्वास की उपेक्षा जैसे अनेक मुद्दे सामने आते रहे। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए “अधिकार, मुआवजा और पारदर्शिता में सुधार तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013” लागू किया गया, जिसे संक्षेप में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 कहा जाता है।
पृष्ठभूमि और अधिनियम की आवश्यकता
पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ब्रिटिश शासनकाल का था, जो औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। उसमें भूमि अधिग्रहण में न तो जन-सहमति की आवश्यकता थी, न ही न्यायोचित मुआवज़ा या पुनर्वास का प्रावधान। यह कानून भूमि मालिकों के अधिकारों की अवहेलना करता था और उसे “सार्वजनिक प्रयोजन” के नाम पर भूमि से बेदखल किया जाता था।
भारत में कई आंदोलनों और विरोधों (जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, पोस्को प्रोजेक्ट विरोध, सिंगूर मामला आदि) के बाद सरकार पर दबाव बना कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो विकास के साथ-साथ प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इसी सोच के तहत संसद ने 2013 में यह अधिनियम पारित किया।
अधिनियम का उद्देश्य
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत और उत्तरदायी बनाना।
- अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करना।
- जन-सहमति और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य बनाना।
- भूमि अधिग्रहण को जनविरोधी नहीं, बल्कि जनकल्याणकारी बनाना।
प्रमुख प्रावधान
1. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment – SIA)
सभी बड़े परियोजनाओं में अधिग्रहण से पहले SIA अनिवार्य किया गया है, जिसमें यह अध्ययन होता है कि अधिग्रहण से स्थानीय लोगों, पर्यावरण, संस्कृति, रोजगार और आजीविका पर क्या असर पड़ेगा। यह रिपोर्ट जनसुनवाई के बाद सार्वजनिक की जाती है।
2. जन-सहमति की आवश्यकता
- यदि कोई निजी परियोजना के लिए भूमि ली जा रही है, तो कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की लिखित सहमति आवश्यक है।
- यदि परियोजना सरकारी और निजी साझेदारी (PPP) में है, तो 70% सहमति जरूरी है।
- यह प्रावधान भूमि मालिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाता है।
3. उचित मुआवजा और बाजार दर
- अधिग्रहण के लिए दी जाने वाली कीमत बाजार दर से दोगुनी (ग्रामीण क्षेत्रों में) और शहरी क्षेत्रों में कम से कम बराबर होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त 20% अतिरिक्त सोलातियम, रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टांप ड्यूटी आदि की भरपाई की जाती है।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) नीति
- जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित होती है उन्हें वैकल्पिक आवास, मासिक भत्ता, रोजगार, आजीविका सहायता, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, और समाज में पुनः समावेश का प्रावधान है।
- अधिग्रहण की प्रक्रिया R&R पूरा किए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती।
5. बहिष्कृत भूमि
कुछ क्षेत्रों जैसे जैव विविधता क्षेत्र, पवित्र धार्मिक स्थल, वन क्षेत्र आदि में अधिग्रहण प्रतिबंधित है।
6. लंबित परियोजनाओं पर लागू
जो अधिग्रहण 2014 से पहले शुरू हुए लेकिन अधूरे हैं, उन पर भी यह अधिनियम लागू होता है, जिससे पुराने मामलों में भी न्याय सुनिश्चित हो सके।
अधिनियम की विशेषताएं और सकारात्मक प्रभाव
- यह अधिनियम किसानों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने का एक सशक्त उपकरण बनता है।
- अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जन-सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।
- यह विकास और मानव अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन को विधिक अधिकार का दर्जा देता है, जो पहले नहीं था।
अधिनियम की आलोचनाएं और चुनौतियाँ
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में समय की अधिकता और प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण परियोजनाएँ विलंबित हो रही हैं।
- निजी कंपनियों को अधिग्रहण में अधिक समय और लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे निवेश प्रभावित होता है।
- कई राज्य सरकारों ने अपने संशोधित राज्य कानून बनाकर केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर कर दिया है।
- ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका व्यवहार में सीमित रह जाती है।
- मुआवज़े की राशि में भ्रष्टाचार और राजनीति का हस्तक्षेप भी सामने आया है।
उदाहरण और व्यवहारिक प्रभाव
सिंगूर मामला (पश्चिम बंगाल): टाटा मोटर्स को जमीन देने में किसानों की सहमति नहीं ली गई, जिससे टाटा को परियोजना रोकनी पड़ी। यदि यह अधिनियम पहले लागू होता, तो सहमति के बिना अधिग्रहण नहीं हो सकता था।
नर्मदा घाटी परियोजना: जहाँ हजारों लोगों का विस्थापन हुआ, लेकिन उचित पुनर्वास नहीं हुआ। अधिनियम के अनुसार अब बिना पुनर्वास के अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 भारत के कानूनी ढांचे में एक ऐतिहासिक सुधार है। यह अधिनियम विकास की अनिवार्यता और मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संवेदनशील संतुलन स्थापित करता है। यद्यपि इसके क्रियान्वयन में अनेक प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियाँ हैं, लेकिन यह अधिनियम भविष्य के भारत की समावेशी और न्यायपूर्ण विकास प्रक्रिया की नींव रखता है।
इस अधिनियम का सार यही है कि – “भूमि किसी की आजीविका है, वह केवल मापने और बेचने की वस्तु नहीं।” विकास आवश्यक है, लेकिन विकास का चेहरा मानवीय और न्यायपूर्ण होना चाहिए।