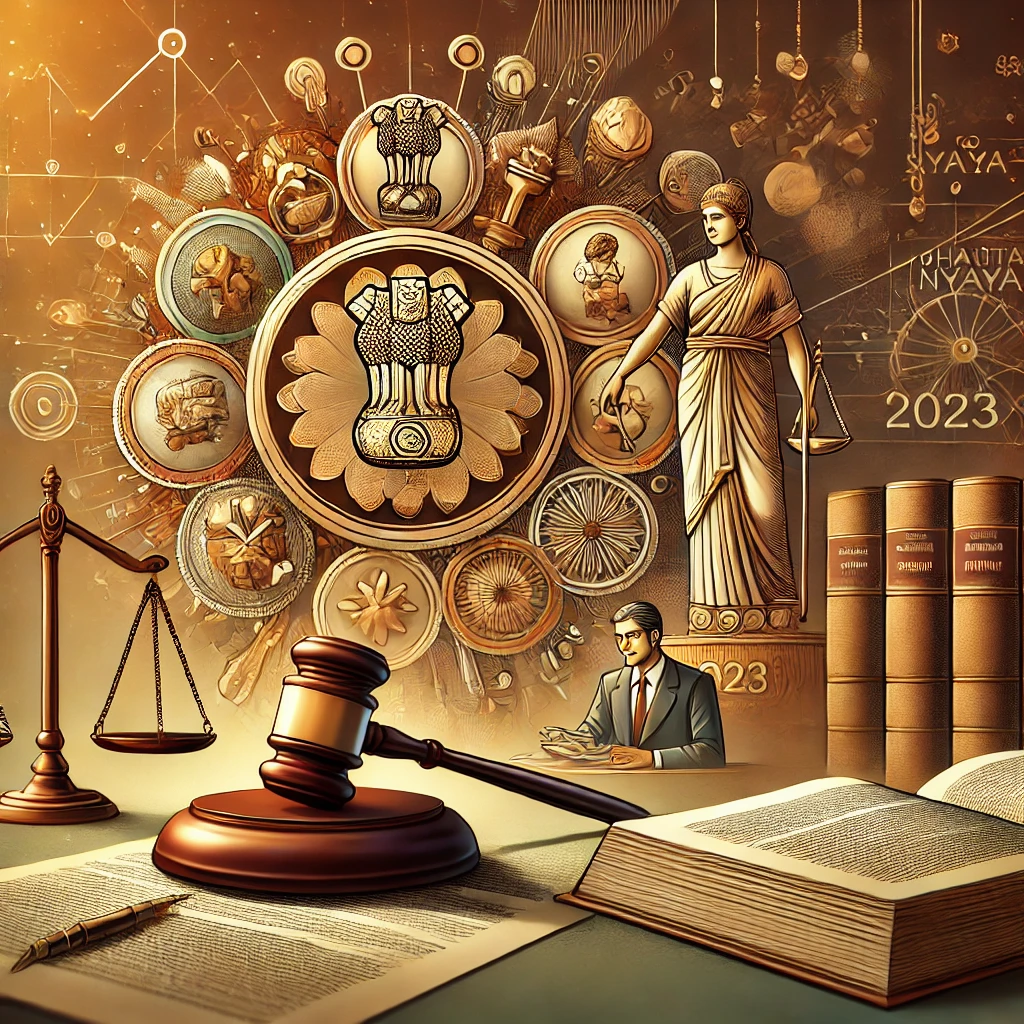शीर्षक: भारत में कानूनी कानून क्या है? – भारतीय विधि प्रणाली की समग्र संरचना
भारत का विधिक ढांचा एक जटिल लेकिन अत्यंत संगठित प्रणाली है, जो विविध ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और औपनिवेशिक प्रभावों से विकसित हुआ है। आज जो कानून भारत में लागू हैं, वे न केवल स्वतंत्रता के बाद बनाए गए हैं, बल्कि इनकी जड़ें ब्रिटिश शासन, धार्मिक परंपराओं, और स्थानीय प्रथाओं में भी हैं। भारत में कानूनी कानूनों की संरचना विविध विधियों के समावेश से बनी है, जिनमें नागरिक, दंड, व्यावसायिक, धार्मिक और प्रथागत कानून प्रमुख हैं।
✅ 1. नागरिक कानून (Civil Law)
नागरिक कानून वे नियम होते हैं जो व्यक्तियों के आपसी अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करते हैं। जैसे – संपत्ति कानून, अनुबंध कानून, परिवार कानून, उत्तराधिकार कानून आदि। इसमें विवादों के समाधान हेतु दीवानी मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। उदाहरणस्वरूप – भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 आदि।
✅ 2. दंड या आपराधिक कानून (Criminal Law)
आपराधिक कानून उन कृत्यों से संबंधित है जिन्हें समाज के लिए हानिकारक माना जाता है और जिन पर दंड निर्धारित है। भारत में दंड कानून का प्रमुख स्रोत भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) है, जिसमें अपराधों की परिभाषा, सजा और प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) भी दंड प्रक्रिया को संचालित करता है।
✅ 3. प्रथागत कानून (Customary Law)
भारत जैसे विविध सांस्कृतिक समाज में स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों को भी मान्यता प्राप्त है। कई समुदायों और जनजातियों के पास अपने स्थानीय customary कानून होते हैं, जो विवाह, उत्तराधिकार, भूमि उपयोग आदि विषयों को नियंत्रित करते हैं। कोर्ट कई मामलों में इन मान्य परंपराओं को मान्यता देता है जब तक वे संविधान या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हों।
✅ 4. धार्मिक कानून (Religious Law)
धार्मिक कानून, विशेष रूप से व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) के रूप में मौजूद हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग-अलग धार्मिक कानून लागू होते हैं, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में मार्गदर्शन करते हैं।
उदाहरण:
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937
✅ 5. कॉर्पोरेट कानून (Corporate Law)
व्यापारिक और औद्योगिक विकास के साथ कॉर्पोरेट कानूनों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कंपनियों की स्थापना, प्रबंधन, विलय, दिवालियापन आदि से जुड़े नियम होते हैं। प्रमुख कानूनों में शामिल हैं:
- कंपनी अधिनियम, 2013
- इनसॉल्वेंसी और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC)
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- SEBI कानून
✅ 6. संविधान और विधायिका आधारित कानून
भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है, जिसके अंतर्गत सभी अन्य कानूनों का निर्माण और व्याख्या होती है। संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून संविधान के अधीन होते हैं। जैसे –
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
✅ 7. औपनिवेशिक विरासत से प्राप्त कानून
ब्रिटिश शासन काल में बनाए गए कई कानून आज भी प्रभावी हैं, यद्यपि उन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है।
उदाहरण:
- भारतीय दंड संहिता, 1860
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
निष्कर्ष:
भारत की कानूनी प्रणाली बहुस्तरीय और बहुआयामी है, जो संविधान, विधायी कानून, धार्मिक परंपराओं, प्रथागत नियमों और ब्रिटिश कालीन कानूनों के समन्वय से बनी है। यह प्रणाली देश की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करते हुए नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करती है। इस प्रकार भारत में नागरिक, आपराधिक, धार्मिक, प्रथागत और कॉर्पोरेट कानूनों का संयोजन ही भारतीय “कानूनी कानून” की संपूर्ण संरचना बनाता है।