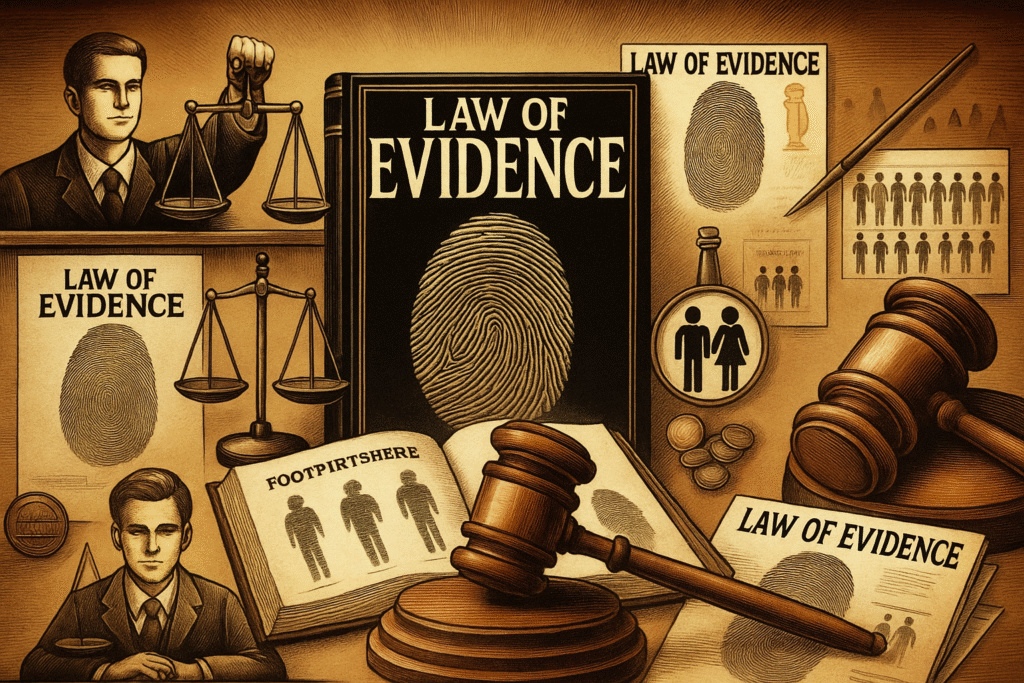भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 : स्वीकृति (Confession) और स्वीकारोक्ति (Admission) में अंतर तथा आपराधिक मामलों में स्वीकृति के साक्ष्य का मूल्य
⭐ प्रस्तावना (Introduction)
भारतीय न्याय प्रणाली में साक्ष्य (Evidence) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि न्यायालय का निर्णय मुख्यतः साक्ष्यों पर ही आधारित होता है। किसी व्यक्ति का कथन, वक्तव्य या कथ्य, यदि किसी विधिक विवाद में प्रासंगिक हो, तो वह साक्ष्य की श्रेणी में आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) ने साक्ष्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक व्यवस्थित रूप दिया है।
साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति (Confession) और स्वीकारोक्ति (Admission) दोनों ही प्रकार के कथन प्रासंगिक साक्ष्य माने जाते हैं, किंतु दोनों में पर्याप्त भिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। विशेषकर, आपराधिक मामलों में स्वीकृति (Confession) की भूमिका निर्णायक होती है। न्यायालय इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि आरोपी द्वारा दिया गया कथन स्वेच्छा से किया गया है या दबाव/प्रलोभन/धमकी के अंतर्गत।
⭐ स्वीकृति (Confession) की परिभाषा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में “स्वीकृति” की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। परंतु न्यायालयों ने अपने निर्णयों के माध्यम से इसे परिभाषित किया है।
- केलन बनाम किंग (Kelan v. King) में परिभाषित किया गया कि –
“Confession is an admission made by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed the crime.” - अर्थात, जब कोई अभियुक्त स्वयं यह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है अथवा उसके कथन से यह संकेत मिले कि वही अपराधी है, तो इसे स्वीकृति (Confession) कहा जाएगा।
👉 सरल शब्दों में, स्वीकृति का आशय है – अभियुक्त का वह वक्तव्य जिसमें वह अपराध की जिम्मेदारी स्वीकार करता है।
⭐ स्वीकारोक्ति (Admission) की परिभाषा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार –
“Admission is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, and under the circumstances, hereinafter mentioned.”
👉 इसका अर्थ है कि जब कोई पक्षकार किसी तथ्य के संबंध में ऐसा कथन करता है जिससे उस तथ्य की सत्यता का अनुमान लगाया जा सके, तो वह स्वीकारोक्ति (Admission) कहलाता है।
⭐ स्वीकृति (Confession) और स्वीकारोक्ति (Admission) में अंतर
| आधार (Basis) | स्वीकारोक्ति (Admission) | स्वीकृति (Confession) |
|---|---|---|
| परिभाषा | किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के संबंध में कथन, जिससे उस तथ्य का सत्यापन हो सके। | अभियुक्त द्वारा अपराध करने की स्वीकृति या ऐसा कथन जिससे उसकी अपराध में संलिप्तता सिद्ध हो। |
| प्रयोजन | सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में प्रयोज्य। | केवल आपराधिक मामलों में प्रयोज्य। |
| स्वरूप | सामान्य कथन, जो आंशिक हो सकता है। | अपराध स्वीकार करने का स्पष्ट कथन। |
| उदाहरण | “मैं उस स्थान पर मौजूद था।” (फैक्ट से जुड़ा कथन) | “मैंने हत्या की है।” (अपराध की सीधी स्वीकृति) |
| प्रासंगिकता | धारा 17 से 23 के अंतर्गत विनियमित। | धारा 24 से 30 के अंतर्गत विनियमित। |
| साक्ष्य मूल्य | पूर्ण साक्ष्य नहीं, किंतु अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्टिकरण हेतु प्रयोज्य। | यदि स्वेच्छा से किया गया हो तो अत्यंत मजबूत साक्ष्य। |
⭐ आपराधिक मामलों में स्वीकृति (Confession) का महत्व
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 में स्वीकृति की प्रासंगिकता और उपयोग की शर्तें दी गई हैं।
- स्वेच्छा का सिद्धांत (Section 24)
- यदि स्वीकृति भय, दबाव, प्रलोभन या वादे के कारण की गई हो, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि अभियुक्त ने स्वतंत्र इच्छा से अपराध स्वीकार किया है।
- पुलिस के समक्ष स्वीकृति (Sections 25 & 26)
- धारा 25: पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
- धारा 26: पुलिस हिरासत में की गई स्वीकृति भी तब तक मान्य नहीं होगी जब तक वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न की गई हो।
👉 इसका उद्देश्य है कि पुलिस द्वारा दबाव डालकर कराई गई झूठी स्वीकृति को रोका जा सके।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकृति (Section 164 CrPC और Section 27 Evidence Act)
- मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकृति यदि विधि अनुसार दर्ज की गई है, तो वह वैध और निर्णायक साक्ष्य मानी जाती है।
- धारा 27 के अंतर्गत discovery statement (अभियुक्त द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर बरामदगी) को आंशिक रूप से साक्ष्य माना जाता है।
- सह-अभियुक्त की स्वीकृति (Section 30)
- यदि दो या अधिक अभियुक्त एक साथ विचाराधीन हों, और उनमें से कोई स्वीकृति करता है, तो वह अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी प्रासंगिक हो सकती है।
- परंतु यह साक्ष्य मात्र सहायक (Corroborative) माना जाता है, स्वतंत्र आधार नहीं।
⭐ न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial Pronouncements)
- प्यारे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (AIR 1962 SC 690)
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वीकृति तभी मान्य है जब वह स्वेच्छा से की गई हो और किसी प्रकार के भय या प्रलोभन के कारण न हो।
- कंवर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (AIR 1954 SC 207)
- पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति को अमान्य करार दिया गया।
- काश्मीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1977 SC 2147)
- स्वीकृति तभी विश्वसनीय है जब वह पूर्ण रूप से अपराध स्वीकार करे और अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो।
- नारायण स्वामी बनाम सम्राट (Privy Council, 1939)
- निर्णय दिया गया कि स्वीकृति का आधार केवल अभियुक्त के शब्द नहीं बल्कि परिस्थितियों का विश्लेषण भी होना चाहिए।
⭐ स्वीकृति के साक्ष्य मूल्य की विवेचना
- सबसे मजबूत साक्ष्य
- यदि स्वीकृति स्वेच्छा से और मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो, तो यह अपराध सिद्ध करने के लिए अत्यंत मजबूत साक्ष्य होती है।
- स्वतंत्र साक्ष्य की आवश्यकता
- न्यायालय सामान्यतः केवल स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं करता, बल्कि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से उसकी पुष्टि चाहता है।
- आंशिक सत्यता की समस्या
- कभी-कभी अभियुक्त केवल कुछ तथ्य स्वीकार करता है और बाकी नकार देता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को पूरे बयान का विश्लेषण कर यह देखना होता है कि कौन-सा भाग विश्वसनीय है।
- सह-अभियुक्त की स्वीकृति का मूल्य
- यह केवल सहायक साक्ष्य के रूप में मान्य है। बिना अन्य साक्ष्य के केवल इसी आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
- आधुनिक दृष्टिकोण
- आजकल न्यायालय स्वीकृति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि कई बार पुलिस या अन्य पक्ष दबाव डालकर अभियुक्त से स्वीकृति करा लेते हैं।
⭐ निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत स्वीकारोक्ति (Admission) और स्वीकृति (Confession) दोनों ही साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनके प्रयोजन और प्रभाव अलग-अलग हैं।
- स्वीकारोक्ति सामान्यतः किसी तथ्य की पुष्टि हेतु प्रयोज्य है और सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में उपयोगी है।
- स्वीकृति केवल आपराधिक मामलों में प्रयोज्य है और यदि यह स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई हो, तो इसे सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता है।
परंतु न्यायालयों ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि केवल स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि वह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट न हो।
अतः कहा जा सकता है कि –
“स्वीकृति आपराधिक मामलों में एक शक्तिशाली किन्तु सावधानी से प्रयोग किए जाने वाला साक्ष्य है, जबकि स्वीकारोक्ति एक सामान्य साक्ष्य है जो तथ्यों की पुष्टि करने में सहायक होता है।”
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 :
स्वीकृति (Confession) और स्वीकारोक्ति (Admission) में अंतर तथा आपराधिक मामलों में स्वीकृति का साक्ष्य मूल्य
Q.1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में स्वीकृति (Confession) और स्वीकारोक्ति (Admission) का क्या अर्थ है?
उत्तर:
- स्वीकृति (Confession): ऐसा कथन जो अभियुक्त स्वयं अपराध स्वीकार करते हुए करता है या जिससे यह संकेत मिले कि वही अपराधी है।
- स्वीकारोक्ति (Admission): ऐसा कथन जो किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के संबंध में किया गया हो और जिससे उस तथ्य का अनुमान लगाया जा सके।
Q.2 स्वीकृति (Confession) और स्वीकारोक्ति (Admission) में मुख्य अंतर क्या है?
उत्तर:
| आधार | स्वीकारोक्ति (Admission) | स्वीकृति (Confession) |
|---|---|---|
| परिभाषा | तथ्य की पुष्टि करने वाला कथन | अपराध स्वीकार करने वाला कथन |
| प्रयोग | सिविल व आपराधिक दोनों मामलों में | केवल आपराधिक मामलों में |
| स्वरूप | आंशिक हो सकता है | अपराध की स्पष्ट स्वीकारोक्ति |
| धाराएँ | धारा 17 से 23 | धारा 24 से 30 |
| उदाहरण | “मैं घटना स्थल पर था।” | “मैंने हत्या की है।” |
Q.3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धाराएँ स्वीकृति (Confession) से संबंधित हैं?
उत्तर:
- धारा 24 – भय, प्रलोभन या वादे से की गई स्वीकृति अमान्य है।
- धारा 25 – पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति अमान्य है।
- धारा 26 – पुलिस हिरासत में की गई स्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष न हो तो अमान्य है।
- धारा 27 – अभियुक्त के कथन से प्राप्त तथ्य (Discovery) आंशिक रूप से मान्य।
- धारा 30 – सह-अभियुक्त की स्वीकृति अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी प्रासंगिक।
Q.4 पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति क्यों अमान्य मानी गई है?
उत्तर:
क्योंकि पुलिस द्वारा दबाव, मारपीट, प्रलोभन या धमकी देकर स्वीकृति कराई जा सकती है। न्याय की दृष्टि से यह असुरक्षित माना गया है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 व 26 इसे अमान्य करार देती हैं।
Q.5 मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वीकृति का क्या महत्व है?
उत्तर:
- यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत दर्ज की गई है तो यह सशक्त एवं निर्णायक साक्ष्य होती है।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि अभियुक्त ने बिना दबाव व स्वतंत्र इच्छा से अपराध स्वीकार किया है।
- इसका आधार CrPC की धारा 164 है।
Q.6 आपराधिक मामलों में सह-अभियुक्त की स्वीकृति का क्या साक्ष्य मूल्य है?
उत्तर:
- धारा 30 के अनुसार, सह-अभियुक्त की स्वीकृति अन्य अभियुक्तों के खिलाफ प्रासंगिक हो सकती है।
- किंतु यह केवल सहायक (Corroborative) साक्ष्य है, स्वतंत्र आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती।
Q.7 न्यायालयों ने स्वीकृति के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया है?
उत्तर:
- प्यारे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (AIR 1962 SC 690) – स्वीकृति तभी मान्य है जब वह स्वेच्छा से की गई हो।
- कंवर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (AIR 1954 SC 207) – पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति अमान्य।
- काश्मीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1977 SC 2147) – स्वीकृति तभी विश्वसनीय है जब अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो।
- नारायण स्वामी बनाम सम्राट (1939, Privy Council) – स्वीकृति का मूल्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।
Q.8 आपराधिक मामलों में स्वीकृति (Confession) का साक्ष्य मूल्य क्या है?
उत्तर:
- यदि स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई हो तो यह सबसे मजबूत साक्ष्य है।
- सामान्यतः केवल स्वीकृति पर दोषसिद्धि नहीं होती, बल्कि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पुष्टि भी आवश्यक होती है।
- सह-अभियुक्त की स्वीकृति केवल सहायक साक्ष्य है।
- न्यायालय स्वीकृति को संदेह की दृष्टि से देखता है ताकि झूठी या दबाव में की गई स्वीकृति से न्यायिक त्रुटि न हो।
Q.9 निष्कर्ष रूप में स्वीकृति और स्वीकारोक्ति का अंतर तथा महत्व कैसे स्पष्ट किया जा सकता है?
उत्तर:
- स्वीकारोक्ति (Admission): सामान्य तथ्य की पुष्टि हेतु प्रयोज्य, सिविल व क्रिमिनल दोनों मामलों में उपयोगी।
- स्वीकृति (Confession): केवल आपराधिक मामलों में प्रयोज्य और यदि स्वेच्छा से की गई हो तो अत्यंत शक्तिशाली साक्ष्य।
- परंतु न्यायालय केवल स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता; उसे अन्य साक्ष्यों से पुष्ट किया जाना आवश्यक है।