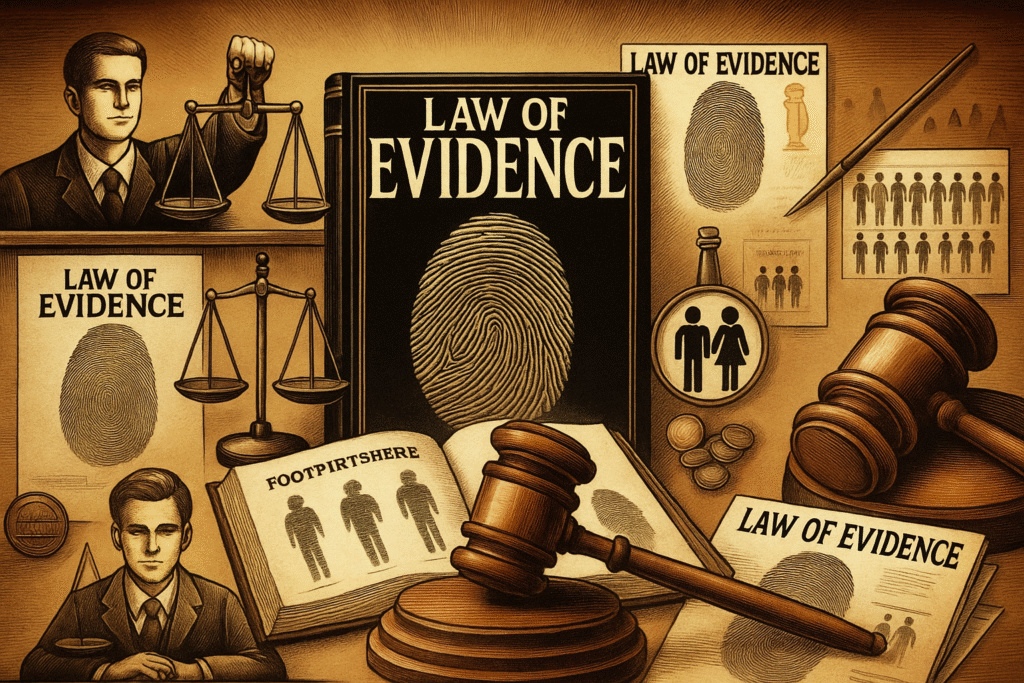भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की परिभाषा और उद्देश्य
भूमिका (Introduction)
भारतीय विधिक प्रणाली में साक्ष्य (Evidence) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि न्यायालय का कार्य केवल प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। किसी मुकदमे में जो तथ्य विवादास्पद होते हैं, उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि न्यायालय को यह बताया जाए कि किन तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है और किन्हें नहीं। इसी उद्देश्य से साक्ष्य संबंधी विधि बनाई गई है। भारत में साक्ष्य से संबंधित मुख्य कानून है – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872)। यह अधिनियम भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि इसके बिना न्यायालय निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक व्यापक और संगठित संहिता है, जिसने अंग्रेजी कानून से प्रेरणा लेकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की परिभाषा, उसकी ग्राह्यता (admissibility), प्रासंगिकता (relevancy), तथा प्रमाणन (proof) के नियम निर्धारित किए। इसके लागू होने से पहले भारत में विभिन्न प्रांतों में साक्ष्य संबंधी कोई एकरूप नियम नहीं था, बल्कि अलग-अलग प्रथाएँ और धार्मिक मान्यताएँ लागू होती थीं। इस अधिनियम के आने के बाद पूरे भारत में एक समान साक्ष्य संबंधी कानून लागू हुआ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा (Definition of Indian Evidence Act)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की परिभाषा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –
- सामान्य परिभाषा:
यह अधिनियम उन नियमों और सिद्धांतों का संकलन है, जो न्यायालय में तथ्यों के प्रमाणन, प्रासंगिकता और ग्राह्यता को नियंत्रित करता है। - अधिनियम की धारा 1 के अनुसार:
“यह अधिनियम भारत के सभी न्यायालयों में सिवाय उन न्यायालयों के जो मार्शल लॉ के अंतर्गत आते हैं और उन मामलों के जिनका निपटारा शपथ अधिनियम, 1873 अथवा किसी अन्य विशेष विधि द्वारा किया जाता है, पर लागू होगा।” - शास्त्रीय परिभाषा (Doctrinal Definition):
भारतीय साक्ष्य अधिनियम वह विधिक संहिता है, जो यह निर्धारित करती है कि –- न्यायालय किन तथ्यों को प्रासंगिक मानेगा,
- कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं,
- और साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी।
इस प्रकार यह अधिनियम न्यायालय में तथ्यों की स्थापना और सत्य की खोज का विधिक साधन है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इतिहास (Historical Background)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन (Sir James Fitzjames Stephen) द्वारा तैयार किया गया था। इससे पूर्व भारत में साक्ष्य का निर्धारण धार्मिक ग्रंथों, स्थानीय रीति-रिवाजों और अंग्रेजी कॉमन लॉ के आधार पर किया जाता था। इससे न्यायिक प्रणाली में एकरूपता का अभाव था। 1872 में इस अधिनियम को पारित कर 1 सितम्बर 1872 से लागू किया गया।
इस अधिनियम ने भारत में साक्ष्य कानून को एक नया रूप दिया और धार्मिक व प्रांतीय विविधताओं को समाप्त कर पूरे भारत में एक समान नियम लागू किया।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रकृति (Nature of the Act)
- प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law):
यह अधिनियम मूल रूप से प्रक्रिया संबंधी कानून है, substantive law नहीं। यह निर्धारित करता है कि न्यायालय में साक्ष्य कैसे प्रस्तुत होंगे और किन परिस्थितियों में स्वीकार किए जाएंगे। - सार्वभौमिक लागू (Uniformly Applicable):
पूरे भारत में यह अधिनियम एक समान रूप से लागू होता है। - व्यापक और वैज्ञानिक (Comprehensive and Scientific):
अधिनियम ने साक्ष्य के क्षेत्र को स्पष्ट, निश्चित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य (Objects of the Indian Evidence Act)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य न्यायालय को सत्य तक पहुँचाने और निष्पक्ष निर्णय देने में सहायता करना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है –
- सत्य की खोज (Discovery of Truth):
अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सत्य तथ्य ही न्यायालय में प्रस्तुत हों और असत्य तथ्यों को बाहर रखा जाए। - प्रासंगिक तथ्यों का निर्धारण (Determination of Relevant Facts):
अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि किन तथ्यों को प्रासंगिक (Relevant) माना जाएगा। न्यायालय उन्हीं तथ्यों पर विचार करेगा जो विवाद से जुड़े हैं। - समानता और एकरूपता (Uniformity and Consistency):
अधिनियम से पहले भारत में विभिन्न धर्मों और प्रांतों में अलग-अलग साक्ष्य नियम लागू थे। यह अधिनियम पूरे भारत में समान और एकरूप नियम लागू करता है। - न्यायालय की सहायता (Assistance to Courts):
यह अधिनियम न्यायालय को दिशा देता है कि किन प्रमाणों को स्वीकार करना है और किन्हें अस्वीकार करना है। इससे न्यायाधीश का विवेक मनमानी से मुक्त रहता है। - साक्ष्य की विधिक परिभाषा (Legal Definition of Evidence):
अधिनियम स्पष्ट करता है कि साक्ष्य में केवल गवाह का कथन और दस्तावेजी प्रमाण शामिल होंगे। इससे प्रमाणन की विधि को सीमित और निश्चित किया गया। - अनुचित और अविश्वसनीय साक्ष्य का बहिष्कार (Exclusion of Unreliable Evidence):
अधिनियम का उद्देश्य यह भी है कि अफवाह, अनुमान या अप्रमाणित तथ्यों को न्यायालय में स्थान न मिले। - निष्पक्षता और न्याय (Fairness and Justice):
अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त या वादी दोनों को समान अवसर मिले और कोई पक्ष साक्ष्य छिपा न सके। - न्यायिक निर्णयों की विश्वसनीयता (Reliability of Judicial Decisions):
साक्ष्य अधिनियम न्यायिक निर्णयों की नींव को मजबूत करता है ताकि न्यायालय के निर्णय निष्पक्ष और तर्कसंगत हों।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्व (Significance of the Act)
- न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता: यह अधिनियम न्यायिक कार्यवाही को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाता है।
- समान न्याय: सभी नागरिकों के लिए न्याय समान नियमों पर आधारित होता है।
- निष्पक्ष निर्णय: अधिनियम न्यायालय को निष्पक्ष निर्णय देने में सहायता करता है।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा: साक्ष्य की उचित व्यवस्था से कानून के शासन (Rule of Law) की रक्षा होती है।
न्यायिक दृष्टांत (Judicial Pronouncements)
- R v. Bertrand (1867): न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य का उद्देश्य न्यायालय को सत्य तक पहुँचाना है।
- State of UP v. Raj Narain (1975): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम सत्य और न्याय की खोज का साधन है।
- Hanumant Govind Nargundkar v. State of M.P. (1952): इसमें कहा गया कि साक्ष्य का आधार ठोस होना चाहिए और संदेह से परे होना चाहिए।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 भारतीय विधिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह केवल एक प्रक्रियात्मक कानून न होकर न्याय और सत्य की खोज का मार्गदर्शक है। इसका उद्देश्य न्यायालय को यह मार्ग दिखाना है कि किन तथ्यों पर विचार करना है और किन्हें बाहर रखना है। यह अधिनियम न्यायिक प्रक्रिया को एकरूप, निष्पक्ष और तर्कसंगत बनाता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि –
भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय की आँखों का प्रकाश है, जिसके बिना न्यायिक प्रक्रिया अधूरी और अंधकारमय हो जाएगी। यह अधिनियम न केवल न्यायालय को सत्य की राह दिखाता है, बल्कि नागरिकों को भी यह विश्वास दिलाता है कि न्यायालय का निर्णय ठोस साक्ष्यों और निष्पक्ष प्रक्रिया पर आधारित होगा।