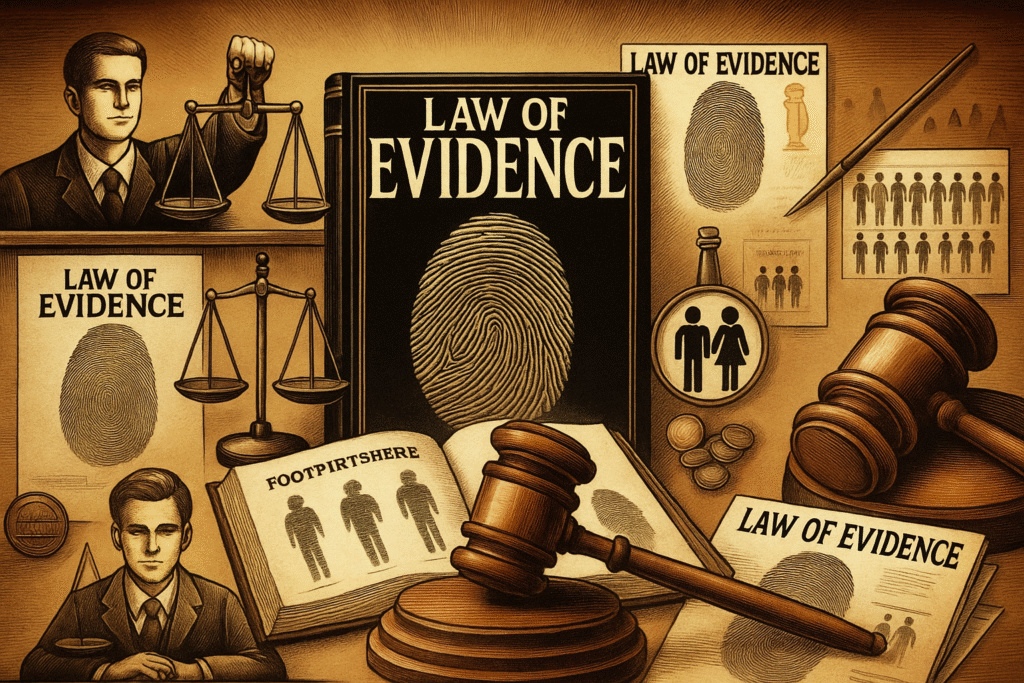भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषज्ञ साक्ष्य की भूमिका
भूमिका
न्यायिक कार्यवाही का मूल उद्देश्य है — सत्य की खोज और न्याय का निष्पक्ष निर्धारण। किन्तु अनेक बार न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रश्न आते हैं जो सामान्य व्यक्ति या यहाँ तक कि न्यायाधीश की साधारण समझ से परे होते हैं। उदाहरणस्वरूप – डीएनए परीक्षण, उँगलियों के निशान, हस्तलेखन का मिलान, मेडिकल रिपोर्ट, आग्नेयास्त्र का उपयोग, विस्फोटक पदार्थ, मादक पदार्थों की संरचना आदि। इन जटिल और तकनीकी विषयों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है। इस प्रकार विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Evidence) न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य न्यायालय को तथ्यात्मक जटिलताओं के समाधान में तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
1. विशेषज्ञ साक्ष्य की परिभाषा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में कहा गया है—
“जब न्यायालय को किसी ऐसे विषय पर राय बनाने की आवश्यकता होती है, जो विज्ञान, कला, विदेशी कानून, हस्तलेखन या उँगलियों के निशान पर आधारित हो, तो उस विषय के विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक होती है।”
अतः विशेषज्ञ साक्ष्य का आशय है— ऐसे व्यक्ति की राय जो किसी विशेष विद्या, कला, विज्ञान अथवा तकनीकी विषय में विशेष दक्षता और अनुभव रखता हो और जिसका ज्ञान सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक हो।
2. विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित प्रावधान
(A) धारा 45 – राय विशेषज्ञों की
न्यायालय विज्ञान, कला, हस्तलेखन, विदेशी कानून और उँगलियों के निशान पर विशेषज्ञ की राय को प्रासंगिक मानता है।
(B) धारा 45-A – इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर राय
धारा 45-A (आईटी अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ी गई) के अनुसार, जब न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में राय की आवश्यकता हो, तो साइबर विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक होगी।
(C) धारा 46
यदि तथ्यों से विशेषज्ञ की राय की पुष्टि होती है, तो वे तथ्य प्रासंगिक होंगे।
(D) धारा 47
हस्तलेखन की पहचान संबंधी राय।
(E) धारा 51
यदि किसी व्यक्ति की राय को प्रासंगिक ठहराया गया है, तो राय के आधार (grounds) भी प्रासंगिक होंगे।
3. विशेषज्ञ साक्ष्य का महत्व
(i) तकनीकी विषयों में न्यायालय की सहायता
न्यायालय कानून और तथ्यों की विवेचना में निपुण होता है, परंतु विज्ञान, चिकित्सा, फॉरेंसिक, डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान न्यायाधीश के पास नहीं होता। यहाँ विशेषज्ञ साक्ष्य आवश्यक हो जाता है।
(ii) वैज्ञानिक साक्ष्य की विश्वसनीयता
विशेषज्ञ राय वैज्ञानिक प्रयोगों, परीक्षणों और विश्लेषण पर आधारित होती है, जिससे निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं।
(iii) अपराध की पहचान
हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों में डीएनए, रक्त परीक्षण, फिंगरप्रिंट, साइबर ट्रैकिंग जैसे साक्ष्य अभियुक्त की पहचान में सहायक होते हैं।
(iv) न्याय की निष्पक्षता
विशेषज्ञ साक्ष्य का प्रयोग न्यायालय को निष्पक्ष और सटीक निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे गलत दोषसिद्धि या बरी होने की संभावना कम हो जाती है।
4. विशेषज्ञ साक्ष्य की प्रकृति
- विशेषज्ञ साक्ष्य मत (Opinion Evidence) है, न कि प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence)।
- यह सलाहकारी (Advisory) स्वरूप का होता है।
- न्यायालय विशेषज्ञ की राय पर पूर्णत: निर्भर नहीं होता, बल्कि उसे अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर परखता है।
- विशेषज्ञ साक्ष्य तभी महत्व रखता है जब वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और निष्पक्ष हो।
5. न्यायिक दृष्टिकोण
(i) State of Himachal Pradesh v. Jai Lal (1999)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—
“विशेषज्ञ साक्ष्य केवल राय है, और राय तभी मूल्यवान है जब उसके आधार स्पष्ट, तार्किक और वैज्ञानिक हों। न्यायालय को उसकी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।”
(ii) Murari Lal v. State of M.P. (1980)
न्यायालय ने कहा कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय महत्वपूर्ण है, परंतु इसे अन्य साक्ष्यों के साथ परखना चाहिए।
(iii) Ramesh Chandra Agrawal v. Regency Hospital (2009)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ साक्ष्य तभी स्वीकार्य है जब विशेषज्ञ की योग्यता और निष्पक्षता संदेह से परे हो।
(iv) Kishan Chand v. State of Haryana (2013)
न्यायालय ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट अत्यंत विश्वसनीय साक्ष्य है और अभियुक्त की दोषसिद्धि में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
6. विशेषज्ञ साक्ष्य के प्रकार
- मेडिकल साक्ष्य – पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चोटों का विश्लेषण, मृत्यु का कारण।
- फॉरेंसिक साक्ष्य – डीएनए, रक्त, उँगलियों के निशान, आग्नेयास्त्र परीक्षण।
- हस्तलेखन और दस्तावेज़ी साक्ष्य – लिखावट, हस्ताक्षर, कागजात की जाँच।
- डिजिटल और साइबर साक्ष्य – ई-मेल, कंप्यूटर डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग।
- तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य – विस्फोटक, रसायन, मशीनरी संबंधी जाँच।
7. विशेषज्ञ साक्ष्य की सीमाएँ
(i) मत आधारित साक्ष्य
विशेषज्ञ साक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। यह केवल राय है, जिसे गलत भी सिद्ध किया जा सकता है।
(ii) न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं
न्यायालय विशेषज्ञ की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है।
(iii) भ्रष्टाचार और पक्षपात
कई बार विशेषज्ञ को प्रभावित किया जा सकता है, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
(iv) विरोधाभासी राय
अक्सर दो विशेषज्ञ एक ही तथ्य पर भिन्न-भिन्न राय देते हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है।
(v) वैज्ञानिक त्रुटियाँ
प्रयोगशालाओं की त्रुटियाँ, तकनीकी खामियाँ या मानवीय भूल के कारण विशेषज्ञ राय गलत हो सकती है।
8. भारतीय न्यायपालिका में विशेषज्ञ साक्ष्य का व्यावहारिक प्रयोग
- हत्या और बलात्कार के मामले – डीएनए और मेडिकल साक्ष्य।
- आर्थिक अपराध – हस्तलेखन और दस्तावेज़ विशेषज्ञ।
- साइबर अपराध – डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ।
- आतंकवाद और बम विस्फोट – विस्फोटक और रासायनिक परीक्षण विशेषज्ञ।
9. सुधार की आवश्यकता
- स्वतंत्र फॉरेंसिक संस्थान : विशेषज्ञ रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- अद्यतन तकनीक : विशेषज्ञों को नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करना।
- पारदर्शिता : विशेषज्ञ रिपोर्टों की पारदर्शिता और स्वतंत्र समीक्षा।
- कानूनी प्रशिक्षण : विशेषज्ञों को न्यायिक प्रक्रिया की समझ देना ताकि वे अदालत में सटीक गवाही दे सकें।
निष्कर्ष
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषज्ञ साक्ष्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न्यायालय को उन जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी तथ्यों को समझने में मदद करता है जो सामान्य ज्ञान से परे होते हैं। यद्यपि यह केवल राय है और न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है, फिर भी सही परिस्थितियों में यह निर्णायक साबित हो सकता है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि—
“विशेषज्ञ साक्ष्य न्याय का सहयोगी है, प्रतिस्थापक नहीं।”
अर्थात् न्यायालय को अंतिम निर्णय करते समय विशेषज्ञ राय को अन्य साक्ष्यों के साथ संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए।