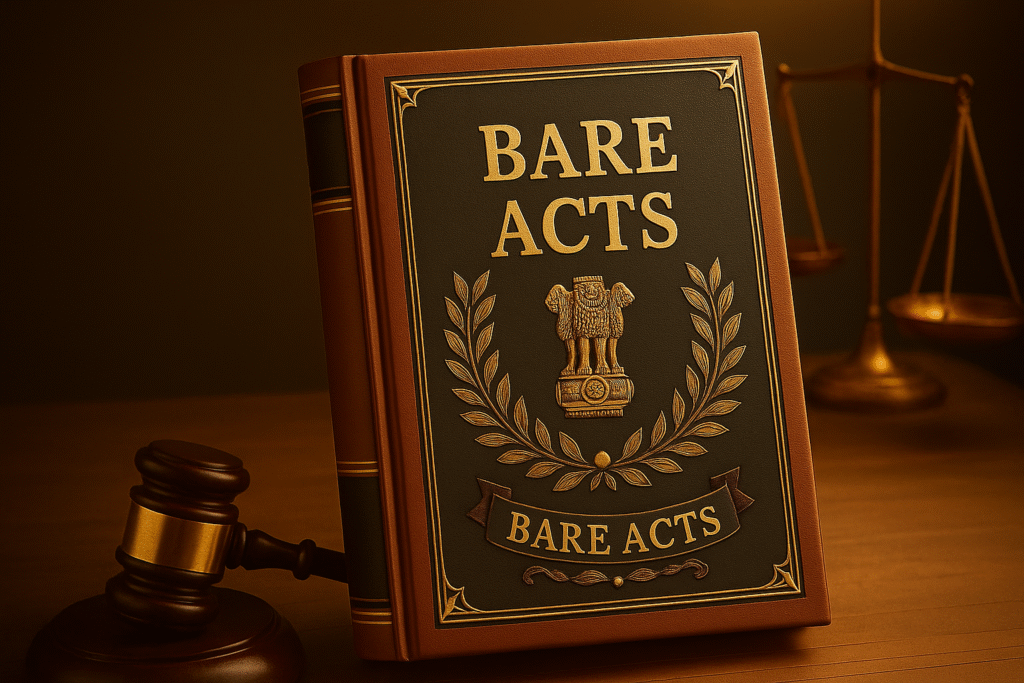भारतीय संविधान, 1950 : एक अध्ययन The Constitution of India, 1950: A Study
प्रस्तावना
भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और जीवंत संविधान है। यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और इसी दिन भारत को एक गणतंत्र (Republic) का दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की नींव है। यह न केवल शासन प्रणाली को परिभाषित करता है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और स्वतंत्रताओं की भी रक्षा करता है।
संविधान वह दस्तावेज़ है जो राज्य की संरचना, शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर, जिन्हें संविधान सभा का मुख्य शिल्पकार (Chief Architect of the Constitution) कहा जाता है, ने संविधान को सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित किया।
संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि
भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू हो गई थी। कई ऐतिहासिक अधिनियमों ने संविधान की नींव रखी, जैसे–
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिन्टो सुधार)
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 – यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है।
कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।
संविधान निर्माण की प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली और 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया।
संविधान लागू होने की तिथि
- संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया।
- 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ।
- 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था।
संविधान की प्रस्तावना (Preamble)
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। इसमें भारत को परिभाषित किया गया है–
“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए…”
प्रस्तावना में चार मूल उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:
- न्याय (Justice) – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
- स्वतंत्रता (Liberty) – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की।
- समानता (Equality) – अवसर और स्थिति की समानता।
- बंधुता (Fraternity) – व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना।
भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान – लगभग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों (मूल रूप में), वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ।
- संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव – भारत एक संघ है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
- संसदीय शासन प्रणाली – ब्रिटेन से प्रेरित, जहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वतंत्र हैं।
- मौलिक अधिकार – नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा हेतु।
- राज्य के नीति निदेशक तत्व – कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शन हेतु।
- धर्मनिरपेक्षता – राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा।
- संशोधन की प्रक्रिया – संविधान न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला।
- एकल नागरिकता – भारत में केवल एक नागरिकता है।
- आपातकालीन प्रावधान – राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल।
संविधान की संरचना
भाग (Parts): भारतीय संविधान मूल रूप से 22 भागों में विभाजित था। वर्तमान में यह 25 भागों में विभाजित है।
अनुसूचियाँ (Schedules): प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं, अब 12 हैं।
संविधान के प्रमुख भाग
- भाग I – संघ और उसका राज्य क्षेत्र
- भाग II – नागरिकता
- भाग III – मौलिक अधिकार
- भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व
- भाग IVA – मौलिक कर्तव्य
- भाग V – संघ की कार्यपालिका
- भाग VI – राज्य सरकारें
- भाग IX और IXA – पंचायत और नगरपालिकाएँ
- भाग X – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
- भाग XVIII – आपातकालीन प्रावधान
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
संविधान नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है–
- समानता का अधिकार (Equality)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Against Exploitation)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of Religion)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural & Educational Rights)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies – अनुच्छेद 32)
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP)
अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ये न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन शासन के लिए मार्गदर्शक हैं।
मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए।
86वें संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा से संबंधित एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई।
संविधान संशोधन (Amendments)
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। प्रमुख संशोधन हैं–
- 42वाँ संशोधन (1976) – इसे “लघु संविधान” कहा जाता है।
- 44वाँ संशोधन (1978) – आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन।
- 73वाँ संशोधन (1992) – पंचायती राज व्यवस्था।
- 74वाँ संशोधन (1992) – नगरपालिकाओं का गठन।
- 86वाँ संशोधन (2002) – शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना।
- 101वाँ संशोधन (2016) – GST व्यवस्था।
भारतीय संविधान के स्रोत
भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों से प्रेरित है, जैसे–
- ब्रिटेन – संसदीय प्रणाली, कानून का शासन।
- अमेरिका – मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग।
- कनाडा – संघीय प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्ति।
- आयरलैंड – राज्य के नीति निदेशक तत्व।
- जर्मनी – आपातकालीन प्रावधान।
- रूस (USSR) – मौलिक कर्तव्य।
- दक्षिण अफ्रीका – संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
भारतीय संविधान का महत्व
- यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गारंटी देता है।
- यह नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है।
- यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है।
- यह भारत की एकता और अखंडता बनाए रखता है।
- यह समय-समय पर संशोधन के माध्यम से बदलते युग के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के लोगों की आकांक्षाओं, सपनों और मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों पर आधारित है।
संविधान की जीवंतता इसी में है कि यह समाज और समय की बदलती जरूरतों के अनुसार स्वयं को ढाल सकता है। यही कारण है कि इसे विश्व का सबसे सफल और प्रभावशाली संविधान माना जाता है।
भारतीय संविधान, 1950 : प्रश्न-उत्तर (Q&A)
प्रश्न 1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) क्या है और इसका महत्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। यह भारत को “सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” घोषित करती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया गया है। प्रस्तावना संविधान की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करती है और मूल संरचना का हिस्सा है।
प्रश्न 2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं—
- लिखित और विस्तृत स्वरूप
- संघीय व्यवस्था (Federal System)
- एकात्मक प्रवृत्ति
- संसदीय शासन प्रणाली
- धर्मनिरपेक्ष राज्य
- मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- संविधान की सर्वोच्चता
- संशोधन की मिश्रित प्रकृति
इन विशेषताओं के कारण यह एक अद्वितीय संविधान है।
प्रश्न 3. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) क्या हैं?
उत्तर:
भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रमुख मौलिक अधिकार हैं—
- समानता का अधिकार (Art. 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Art. 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art. 23–24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Art. 25–28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Art. 29–30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (Art. 32)
प्रश्न 4. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का क्या महत्व है?
उत्तर:
भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में नीति निदेशक तत्व शामिल हैं। ये सरकार को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये अधिकार-न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, परंतु शासन की नीतियों की आधारशिला हैं।
प्रश्न 5. मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे—
- संविधान का पालन करना,
- राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना,
- देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना,
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना,
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना आदि।
प्रश्न 6. संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ संविधान में कैसे झलकती हैं?
उत्तर:
भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है परंतु एकात्मक प्रवृत्ति लिए हुए है। संघीय विशेषताएँ हैं—
- द्विस्तरीय शासन (केंद्र व राज्य)
- लिखित संविधान
- शक्तियों का विभाजन (Union, State, Concurrent List)
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- संविधान की सर्वोच्चता
परंतु आपातकालीन प्रावधानों और केंद्र को दी गई शक्तियों के कारण इसे “अर्ध-संघीय” कहा जाता है।
प्रश्न 7. संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
भारतीय संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इसकी विशेषताएँ हैं—
- वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है
- राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है
- प्रधानमंत्री “कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख” है
- द्विसदनीय विधायिका (लोकसभा और राज्यसभा)
यह प्रणाली लोकतंत्र को कार्यशील और उत्तरदायी बनाती है।
प्रश्न 8. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की प्रकृति समझाइए।
उत्तर:
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। यह तीन प्रकार की है—
- साधारण बहुमत से संशोधन (जैसे नागरिकता)
- विशेष बहुमत से संशोधन (जैसे मौलिक अधिकार)
- विशेष बहुमत + राज्यों की आधी संख्या की स्वीकृति (जैसे संघ-राज्य संबंध)
इससे संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों का संतुलन है।
प्रश्न 9. स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका भारतीय संविधान में क्या है?
उत्तर:
संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक, व्याख्याकार और प्रहरी है।
प्रश्न 10. भारतीय संविधान का महत्व और योगदान स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित है। संविधान ने भारत की एकता, अखंडता और विविधता में एकता को मजबूती दी है। इसके कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।