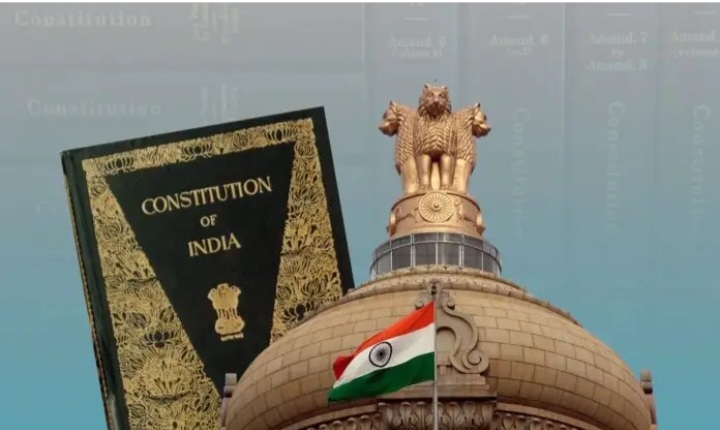शीर्षक: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और उससे जुड़े विवाद
(A Long Analytical Essay on Constitutional Amendment Process and Its Controversies in India)
परिचय
भारतीय संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, जिसे समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए संविधान में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसे संविधान संशोधन प्रक्रिया (Constitutional Amendment Process) कहा जाता है। यह प्रक्रिया संविधान की लचीलापन और कठोरता के बीच संतुलन स्थापित करती है। यद्यपि यह प्रक्रिया लोकतंत्र और विकास की दृष्टि से आवश्यक है, किंतु अतीत में कई बार इस पर विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, विशेषकर जब संशोधन की आड़ में राजनीतिक स्वार्थ या मूल अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ हो।
संविधान संशोधन की आवश्यकता
संविधान को स्थिर होते हुए भी समय के साथ बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। ऐसे कारण जिनसे संशोधन आवश्यक हो सकते हैं:
- नए सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
- विकसित होती लोकतांत्रिक समझ और मूल्य
- न्यायपालिका की व्याख्या को स्पष्ट करना
- राज्य एवं केंद्र के संबंधों को सुदृढ़ बनाना
- वैश्विक प्रावधानों और समझौतों को समायोजित करना
संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है:
1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (By Simple Majority):
- कुछ प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे – संसद की कार्यपद्धति, नागरिकता अधिनियम में बदलाव, निर्वाचन आयोग का कार्यविभाजन आदि।
2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (By Special Majority):
- संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
3. विशेष बहुमत + राज्य की सहमति (Special Majority + Consent of Half of States):
- कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे – संघीय ढांचा, राज्य की सीमाएँ, उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ आदि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और विवाद
1. पहला संविधान संशोधन (1951):
- विवाद: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई गईं।
- महत्व: यह दिखाता है कि कैसे मौलिक अधिकारों को सामाजिक न्याय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है।
2. 24वां संशोधन (1971):
- प्रावधान: संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की स्पष्ट शक्ति दी गई।
- विवाद: न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों पर खतरे की आशंका।
3. 42वां संशोधन (1976) – “मिनी संविधान”:
- प्रावधान: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए।
- विवाद: न्यायपालिका की शक्तियाँ सीमित करने का प्रयास, कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाना।
4. 44वां संशोधन (1978):
- प्रावधान: आपातकाल में मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई।
- महत्व: यह संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है।
5. 73वां एवं 74वां संशोधन (1992):
- प्रावधान: पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा।
- महत्व: स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम।
संविधान संशोधन से जुड़े प्रमुख विवाद
1. संसद की असीमित शक्ति का प्रश्न:
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
2. राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित संशोधन:
- आपातकाल (1975–77) के दौरान हुए संशोधनों को कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण माना जाता है।
3. न्यायपालिका की शक्तियों पर हमला:
- 42वें संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया था।
4. संघीय ढांचे पर प्रभाव:
- कुछ संशोधन राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं, जिससे संघवाद की भावना को नुकसान पहुँच सकता है।
संविधान संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएँ
- लचीली और कठोर दोनों: कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से तो कुछ विशेष प्रक्रिया से संशोधित होते हैं।
- संघीय विशेषता: कुछ संशोधनों में राज्यों की सहमति आवश्यक है।
- लोकतांत्रिक नियंत्रण: संसद में दोनों सदनों की विशेष बहुमत की आवश्यकता संशोधन को गंभीरता प्रदान करती है।
न्यायपालिका की भूमिका
भारतीय न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे की रक्षक है। वह यह सुनिश्चित करती है कि कोई संशोधन:
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।
- संविधान की आत्मा को नष्ट न करे।
- लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता, कानून का शासन जैसे मूल तत्वों को न छेड़े।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया एक सशक्त लोकतंत्र का प्रमाण है, जो समाज की बदलती जरूरतों को आत्मसात करने की क्षमता रखती है। हालांकि यह प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग संविधान की आत्मा को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संविधान संशोधन केवल राष्ट्रहित और जनकल्याण की भावना से ही किया जाए, न कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए। साथ ही न्यायपालिका का दायित्व है कि वह संशोधन की वैधता की समीक्षा कर लोकतंत्र और संविधान की मूल संरचना की रक्षा करे।