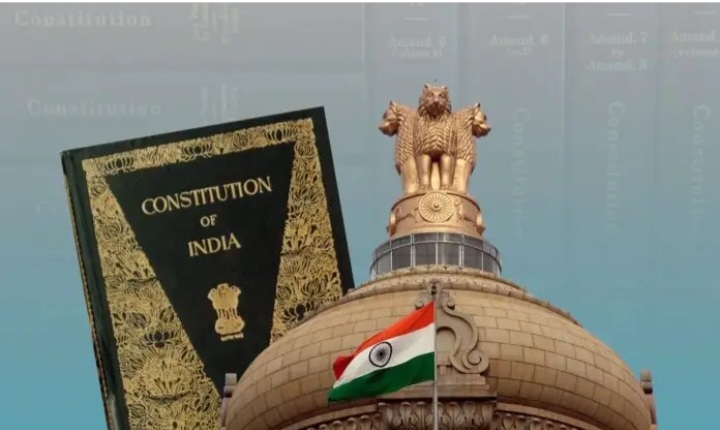शीर्षक: भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व
(Judicial Review in Indian Constitution: एक विस्तृत लेख)
परिचय
भारतीय लोकतंत्र का मूल स्तंभ संविधान है, और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर है। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह राज्य के कार्यों की वैधानिकता की समीक्षा करे, जिससे संविधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) कहा जाता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और विधि के शासन की रक्षा करता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक अभिन्न और अपरिवर्तनीय हिस्सा है।
न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा
न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है – न्यायपालिका द्वारा संसद, राज्य विधानसभाओं तथा कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना। यदि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध या अमान्य घोषित कर सकती है।
संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अलग शीर्षक नहीं है, लेकिन यह अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में निहित है:
- अनुच्छेद 13: संविधान विरोधी कानून स्वतः शून्य होंगे।
- अनुच्छेद 32: सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार।
- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय को अधिकार कि वह विधायी और कार्यकारी कार्यों की वैधता की समीक्षा कर सके।
इन अनुच्छेदों के माध्यम से न्यायपालिका को संविधान का रक्षक और संरक्षक माना गया है।
न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व
1. संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा
संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्य संविधान से ऊपर न हो।
2. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
अगर कोई विधायी या कार्यकारी निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इससे नागरिकों को अत्याचार और असंवैधानिक कार्यों से सुरक्षा मिलती है।
3. शक्ति का संतुलन
न्यायिक पुनरावलोकन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संविधान सम्मत संतुलन बनाए रखता है। इससे कोई भी संस्था निरंकुश नहीं बन पाती।
4. लोकतंत्र की स्थिरता
यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें भी संविधान के अधीन रहें।
5. अनुचित कानूनों को रोकना
अगर कोई कानून अल्पसंख्यकों, महिलाओं, वंचितों या किसी अन्य वर्ग के साथ अन्याय करता है, तो न्यायालय उसे अमान्य कर सकता है। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल मिलता है।
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नहीं बदल सकती। यही निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारतीय संविधान का अपरिहार्य अंग बनाता है।
2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
कोर्ट ने कहा कि संविधान में शक्ति और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और न्यायालय इस संतुलन का रक्षक है।
3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि बाद में इस पर केशवानंद मामले में पुनर्विचार हुआ, लेकिन इसने न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका को और सुदृढ़ किया।
न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएँ
- न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है।
- न्यायपालिका नीति निर्धारण (Policy Making) में हस्तक्षेप नहीं करती जब तक वह संविधान के विरुद्ध न हो।
- संसद की वैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाता है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायिक पुनरावलोकन
आज के डिजिटल और वैश्विक युग में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट शटडाउन, डेटा निगरानी, पर्यावरणीय विनियमन, जन विरोध प्रदर्शन, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मामलों में न्यायालय ने पुनरावलोकन के अधिकार का उपयोग करके नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है।
उदाहरण:
- पेगासस जासूसी मामला (2021): न्यायपालिका ने नागरिकों की निजता की रक्षा हेतु विशेष समिति गठित की।
- तीन तलाक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इस सामाजिक कुप्रथा को असंवैधानिक घोषित किया।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन न केवल एक संवैधानिक सिद्धांत है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा और नागरिक स्वतंत्रता की ढाल भी है। यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर एक आवश्यक नियंत्रण स्थापित करता है ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। न्यायिक पुनरावलोकन यह सुनिश्चित करता है कि “कानून के शासन” का सिद्धांत केवल सिद्धांत भर न रह जाए, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी लागू हो।
इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की आत्मा की सुरक्षा और जनता के अधिकारों की गरिमा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन अनिवार्य और अमूल्य है।