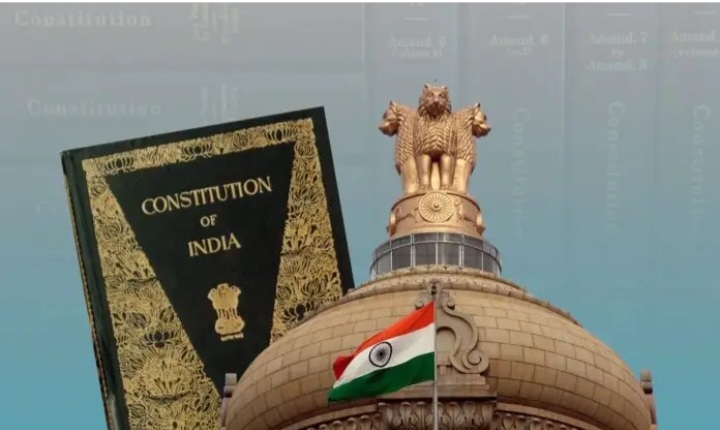भारतीय संविधान की प्रस्तावना: उद्देश्य और महत्व
परिचय
भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान का आदर्शात्मक परिचय है, जो इसके मूलभूत सिद्धांतों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। इसे संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। यह स्पष्ट करती है कि संविधान किन मूल्यों पर आधारित है, और इसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना न केवल संवैधानिक दिशा का मार्गदर्शन करती है, बल्कि यह राष्ट्र की आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करती है।
प्रस्तावना का पाठ
“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की;
समानता, अवसर की समता तथा स्थिति की समता प्राप्त कराने के लिए;
और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
प्रस्तावना के प्रमुख तत्व
भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित मूल तत्त्वों को दर्शाती है:
- हम भारत के लोग (We, the People of India):
यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि संविधान की सर्वोच्चता जनता में निहित है। भारत में सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता ही है। - सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign):
इसका अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है, और वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। - समाजवादी (Socialist):
यह सिद्धांत समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है। समाजवाद का तात्पर्य है कि संसाधनों का समान वितरण हो और हर नागरिक को जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएँ। - पंथनिरपेक्ष (Secular):
भारत कोई राजकीय धर्म नहीं मानता। हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। - लोकतंत्रात्मक (Democratic):
यह व्यवस्था लोगों द्वारा, लोगों के लिए, और लोगों की शासन प्रणाली को दर्शाती है। नागरिकों को मत देने, सरकार चुनने और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है। - गणराज्य (Republic):
इसका अर्थ है कि राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत रूप से नियुक्त।
प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य
- न्याय (Justice):
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई है। इसका तात्पर्य है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। - स्वतंत्रता (Liberty):
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। - समानता (Equality):
यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान अवसर प्राप्त करने का आश्वासन देता है। - बंधुता (Fraternity):
यह तत्व नागरिकों के बीच भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करता है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित बनी रहे।
प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व
- संविधान की आत्मा:
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और इसके मूल ढांचे (basic structure) का हिस्सा है। - दिशा-निर्देशक तत्व:
प्रस्तावना संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या में मार्गदर्शन प्रदान करती है। जब संविधान की किसी धारणा में अस्पष्टता होती है, तो प्रस्तावना के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। - संवैधानिक न्याय का आधार:
प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे आदर्शों के आधार पर न्यायालय अपने निर्णयों में सामाजिक और संवैधानिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
संशोधन और प्रस्तावना
- मूल संविधान में “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द नहीं थे।
- 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था।
- इस संशोधन ने प्रस्तावना को और अधिक समावेशी और सामाजिक न्यायोन्मुखी बनाया।
प्रस्तावना और राष्ट्र निर्माण
प्रस्तावना केवल संविधान का प्रारंभिक परिचय नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भी है, जिसमें भारत के नागरिकों और शासन व्यवस्था को उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा है। यह देश की विविधता में एकता को सुदृढ़ करती है और हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रेरक और मार्गदर्शक प्रकाश-स्तंभ है, जो भारत को एक समावेशी, समानतामूलक और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। यह भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा है, जो न केवल संवैधानिक दिशा प्रदान करती है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे का आधार भी बनती है। अतः यह आवश्यक है कि हम प्रस्तावना में निहित मूल्यों को न केवल समझें, बल्कि अपने आचरण और सामाजिक जीवन में भी उतारें।