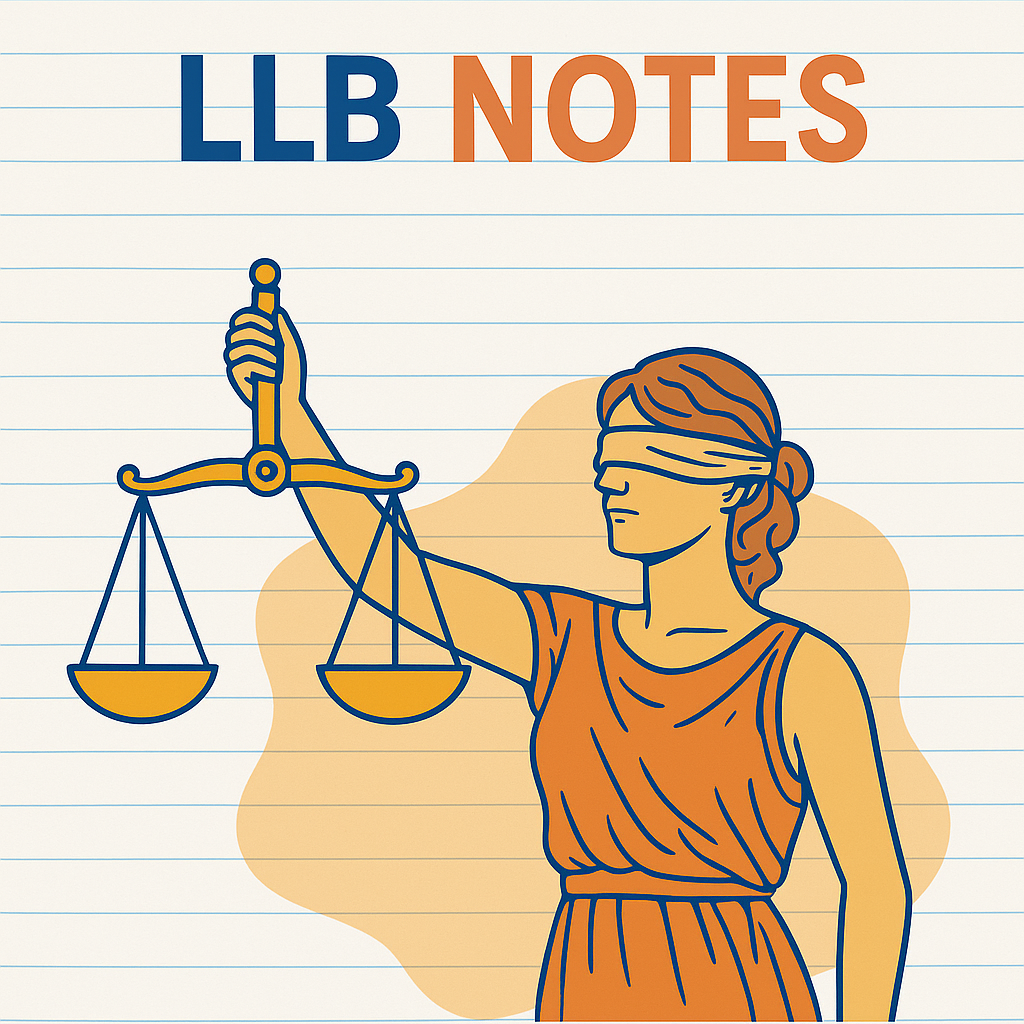भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत ‘प्रतिपूर्ति अनुबंध’ (Contract of Indemnity)
1. प्रस्तावना
व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत लेन-देन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे को संभावित हानि से बचाने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार के समझौते को “प्रतिपूर्ति अनुबंध” कहा जाता है। प्रतिपूर्ति का उद्देश्य उस व्यक्ति को वित्तीय या अन्य हानि से मुक्त रखना है जिसे वह किसी अनुबंध या अन्य कारण से भुगतने के लिए बाध्य हो सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में प्रतिपूर्ति का स्पष्ट प्रावधान धारा 124 और 125 में किया गया है।
2. परिभाषा (Section 124)
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 के अनुसार –
“प्रतिपूर्ति अनुबंध वह अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्ष वादा करता है कि वह दूसरे पक्ष को किसी कार्य के कारण, या उस कार्य के संपादन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के कारण, होने वाली हानि से क्षतिपूर्ति करेगा।”
सरल शब्दों में, जब एक व्यक्ति (प्रतिपूर्ति देने वाला) यह वचन देता है कि वह दूसरे व्यक्ति (प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाला) को किसी निर्दिष्ट कारण से होने वाली हानि की भरपाई करेगा, तो यह प्रतिपूर्ति अनुबंध कहलाता है।
उदाहरण –
यदि ‘A’ यह वादा करता है कि वह ‘B’ को उस क्षति से बचाएगा जो ‘C’ द्वारा दायर मुकदमे में हो सकती है, तो यह प्रतिपूर्ति अनुबंध होगा।
3. प्रतिपूर्ति अनुबंध की प्रकृति
- द्विपक्षीय अनुबंध – इसमें दो पक्ष होते हैं: प्रतिपूर्ति देने वाला (Indemnifier) और प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाला (Indemnified)।
- विशेष अनुबंध का प्रकार – यह विशेष अनुबंध (Special Contract) की श्रेणी में आता है, सामान्य अनुबंध के अतिरिक्त प्रावधानों के साथ।
- सशर्त अनुबंध – प्रतिपूर्ति तभी लागू होती है जब प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले को वास्तविक हानि होती है।
- वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन – इसका उद्देश्य हानि से आर्थिक रूप से बचाव प्रदान करना है।
- अच्छी नीयत (Good Faith) – इस प्रकार के अनुबंध में ईमानदारी और स्पष्टता आवश्यक है।
4. प्रतिपूर्ति अनुबंध के आवश्यक तत्व
- दो पक्षों का होना – एक प्रतिपूर्ति देने वाला और दूसरा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाला।
- वादा या आश्वासन – प्रतिपूर्ति देने वाला, प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले को हानि से बचाने का स्पष्ट वचन देता है।
- हानि का कारण – हानि का कारण कार्य या किसी अन्य व्यक्ति का कार्य होना चाहिए।
- विधिक उद्देश्य – अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए।
- प्रतिफल (Consideration) – अन्य अनुबंधों की तरह इसमें भी प्रतिफल होना आवश्यक है।
- स्वीकृति और प्रस्ताव – अनुबंध के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति के सामान्य नियम लागू होते हैं।
5. प्रतिपूर्ति देने वाले (Indemnifier) के अधिकार और कर्तव्य
(A) अधिकार –
- शर्तों का पालन कराने का अधिकार – प्रतिपूर्ति देने वाला अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य की मांग कर सकता है।
- प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले से सहयोग का अधिकार – कार्यवाही में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले से उचित सहयोग की अपेक्षा कर सकता है।
- प्रतिपूर्ति की सीमा तय करने का अधिकार – यदि अनुबंध में प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित है, तो प्रतिपूर्ति देने वाला उससे अधिक देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
(B) कर्तव्य –
- हानि की भरपाई करना – प्रतिपूर्ति देने वाले का मुख्य कर्तव्य है कि वह वचन के अनुसार हानि की भरपाई करे।
- समय पर भुगतान – क्षति होने पर प्रतिपूर्ति तुरंत करनी चाहिए, ताकि प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले को आर्थिक कठिनाई न हो।
- पूर्ण हानि की भरपाई – इसमें वास्तविक हानि के साथ-साथ कानूनी खर्च और मुकदमेबाजी के उचित व्यय भी शामिल होते हैं।
- ईमानदारी से कार्य करना – प्रतिपूर्ति देने वाला अनुबंध की शर्तों का पालन ईमानदारी से करे।
6. प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले (Indemnified) के अधिकार और कर्तव्य
(A) अधिकार (Section 125 के अनुसार) –
प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले को निम्न अधिकार प्राप्त हैं –
- मुकदमेबाजी में व्यय की प्रतिपूर्ति – यदि उसने प्रतिपूर्ति देने वाले के अनुरोध पर, या उचित कार्यवाही में मुकदमा लड़ा हो।
- समझौते में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति – प्रतिपूर्ति देने वाले की अनुमति से किए गए समझौते में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति।
- हानि की प्रतिपूर्ति – अनुबंध के अनुसार होने वाली किसी भी वास्तविक हानि की भरपाई प्राप्त करना।
(B) कर्तव्य –
- हानि की सूचना देना – जैसे ही संभावित हानि का अंदेशा हो, प्रतिपूर्ति देने वाले को सूचित करना।
- सहयोग करना – मुकदमेबाजी या अन्य कार्यवाही में प्रतिपूर्ति देने वाले को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- अनुबंध की शर्तों का पालन – प्रतिपूर्ति अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार आचरण करना।
7. न्यायिक दृष्टांत (Case Laws)
- Gajanan Moreshwar v. Moreshwar Madan (1942) – न्यायालय ने कहा कि प्रतिपूर्ति का उद्देश्य हानि होने के बाद क्षतिपूर्ति करना है, और इसे अनुबंध की भावना के अनुसार व्याख्यायित किया जाना चाहिए।
- Adamson v. Jarvis (1827) – इसमें प्रतिपूर्ति देने वाले को उस हानि की भरपाई करनी पड़ी जो प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले ने उसके निर्देश पर कार्य करते हुए उठाई थी।
- Osman Jamal & Sons Ltd. v. Gopal Purshottam (1928) – न्यायालय ने माना कि प्रतिपूर्ति अनुबंध केवल वास्तविक हानि तक सीमित है और अनुमानित लाभ की भरपाई नहीं की जा सकती।
8. निष्कर्ष
प्रतिपूर्ति अनुबंध व्यापार, बीमा और अन्य कानूनी लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनुबंध न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि विश्वास और व्यावसायिक स्थिरता को भी बढ़ाता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 और 125 के प्रावधान प्रतिपूर्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। एक सफल प्रतिपूर्ति अनुबंध के लिए आवश्यक है कि इसमें स्पष्ट शर्तें, सीमाएं, और ईमानदार आचरण शामिल हो, ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सकें।