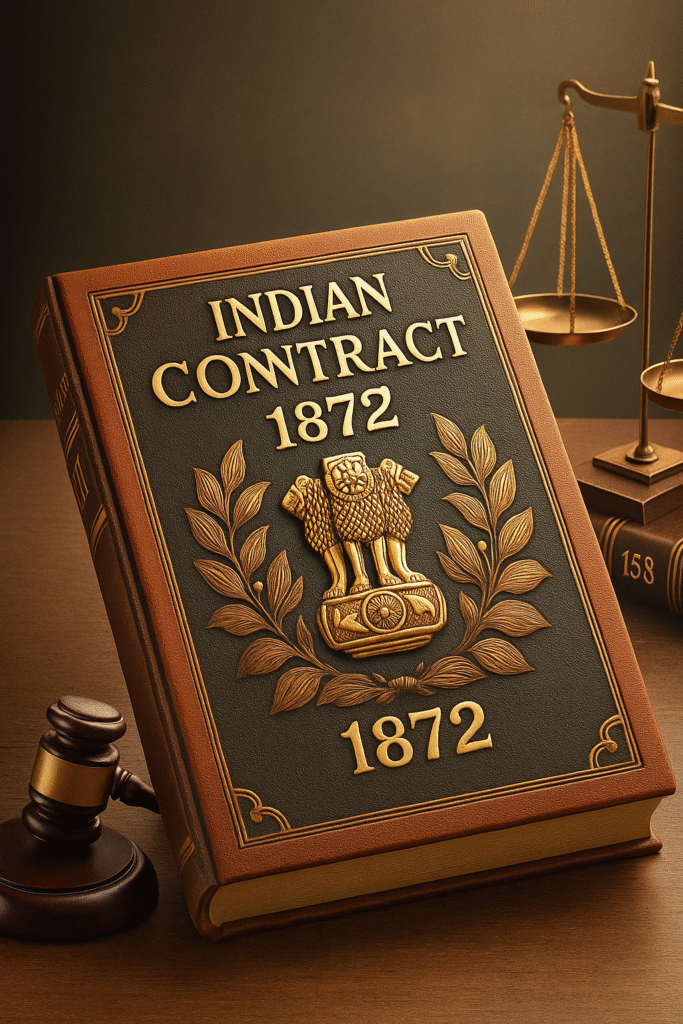भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की विशेषताओं, उद्देश्य एवं कानूनी प्रभाव का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
🔷 परिचय:
संविदा (Contract) मानव समाज के दैनिक जीवन और व्यापारिक गतिविधियों का आधार है। जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य, वस्तु, सेवा या मूल्य के आदान-प्रदान के लिए सहमत होते हैं, और वह सहमति कानून द्वारा बाध्यकारी हो जाती है, तब वह “संविदा” कहलाती है।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 ऐसा ही एक प्रमुख विधिक दस्तावेज है, जो इन अनुबंधों को विधिक स्वरूप प्रदान करता है।
🔷 अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
भारतीय विधि आयोग ने 19वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारिक और सामाजिक संरचना के लिए एक統िक संविदा कानून की आवश्यकता महसूस की। इसी के फलस्वरूप Indian Contract Act, 1872 अस्तित्व में आया।
यह अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को पारित हुआ और 1 सितंबर 1872 से पूरे भारत में (अब जम्मू-कश्मीर सहित) लागू हुआ।
🔷 अधिनियम की मूल संरचना:
प्रारंभ में यह अधिनियम छह भागों में विभाजित था:
- सामान्य सिद्धांत (General Principles)
- अनुबंध द्वारा क्षतिपूर्ति (Indemnity)
- अनुबंध द्वारा गारंटी (Guarantee)
- बैलमेंट और लियन (Bailment & Lien)
- एजेंसी (Agency)
- साझेदारी (Partnership) – अब Partnership Act, 1932 द्वारा नियंत्रित
वर्तमान में केवल पहले पाँच भाग ही प्रभावशील हैं।
🔷 अधिनियम के उद्देश्य:
- भारत में व्यापारिक अनुबंधों को विधिक मान्यता देना।
- न्यायिक व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करना।
- पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट करना।
- अनुबंध के उल्लंघन पर दंड और क्षतिपूर्ति के उपाय उपलब्ध कराना।
- विधिक प्रवर्तन योग्य अनुबंधों की पहचान सुनिश्चित करना।
🔷 संविदा की विधिक परिभाषा (Section 2(h)):
“कोई भी ऐसा समझौता जिसे विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जा सके, वह अनुबंध कहलाता है।”
यह परिभाषा दो तत्वों पर आधारित है:
- Agreement (समझौता) = प्रस्ताव + स्वीकृति
- Enforceability (प्रवर्तनशीलता) = कानून द्वारा बाध्यता
🔷 वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व:
- प्रस्ताव और स्वीकृति (Offer and Acceptance)
- प्रतिफल (Consideration)
- स्वतंत्र सहमति (Free Consent)
- योग्यता (Competency of Parties)
- वैध उद्देश्य (Lawful Object)
- विधिक बाध्यता का आशय (Intention to Create Legal Relations)
- अनुबंध विधि द्वारा निषिद्ध न हो
🔷 स्वतंत्र सहमति और उसके दोष (Sections 13–22):
- बल (Coercion)
- अवांछनीय प्रभाव (Undue Influence)
- धोखाधड़ी (Fraud)
- ग़लत विवरण (Misrepresentation)
- भ्रम (Mistake)
इनमें से किसी का प्रभाव हो तो अनुबंध शून्यनीय या शून्य हो सकता है।
🔷 संविदा के प्रकार (Classification):
| श्रेणी | उदाहरण |
|---|---|
| वैध अनुबंध (Valid) | सभी कानूनी तत्व उपस्थित |
| शून्य अनुबंध (Void) | विधिक प्रवर्तन अयोग्य |
| शून्यनीय अनुबंध (Voidable) | पक्षों की सहमति दोषयुक्त |
| अवैध अनुबंध (Illegal) | अपराध या नैतिकता के विरुद्ध |
| एकतरफा/द्विपक्षीय अनुबंध (Unilateral/Bilateral) | एक या दोनों पक्षों का वचन |
🔷 संविदा का समापन (Discharge of Contract):
संविदा समाप्त हो सकती है:
- प्राकृतिक निष्पादन द्वारा (By performance)
- समझौते द्वारा (By agreement)
- असंभवता द्वारा (By impossibility)
- उल्लंघन द्वारा (By breach)
- कानून द्वारा (By operation of law)
🔷 संविदा का उल्लंघन और उपचार (Breach & Remedies):
धारा 73 में उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
प्रमुख उपचार:
- हर्जाना (Compensation)
- विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance)
- निषेधाज्ञा (Injunction)
- Quantum Meruit
- संविदा निरसन (Rescission)
🔷 प्रमुख विशेष अनुबंध:
- Indemnity (धारा 124) – हानि से रक्षा
- Guarantee (धारा 126) – ऋण के लिए उत्तरदायित्व
- Bailment (धारा 148) – वस्तु को अस्थायी रूप से रखने का अनुबंध
- Agency (धारा 182) – एक व्यक्ति को दूसरे की ओर से कार्य करने का अधिकार
🔷 प्रमुख न्यायिक निर्णय:
- Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose (1903) –
नाबालिग का अनुबंध शून्य होता है। - Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1893) –
एकतरफा अनुबंध की वैधता। - Lalman Shukla v. Gauri Dutt (1913) –
प्रस्ताव की जानकारी आवश्यक है।
🔷 कानूनी महत्त्व (Legal Importance):
- अनुबंध अधिनियम व्यापार और सेवा क्षेत्र का आधार है।
- यह समाज में भरोसे और ज़िम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है।
- विवाद की स्थिति में न्यायालय इसे समाधान का माध्यम बनाता है।
- यह नागरिकों को उनके वैध अधिकारों की रक्षा करने का अवसर देता है।
🔷 निष्कर्ष:
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 भारतीय विधिक व्यवस्था का एक ऐसा स्तंभ है, जिस पर आधुनिक व्यापारिक, सामाजिक और कानूनी ढांचा टिका हुआ है। यह अधिनियम नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, और पारदर्शिता प्रदान करता है। इसमें निहित प्रावधानों ने भारत को एक सुरक्षित संविदात्मक राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है।