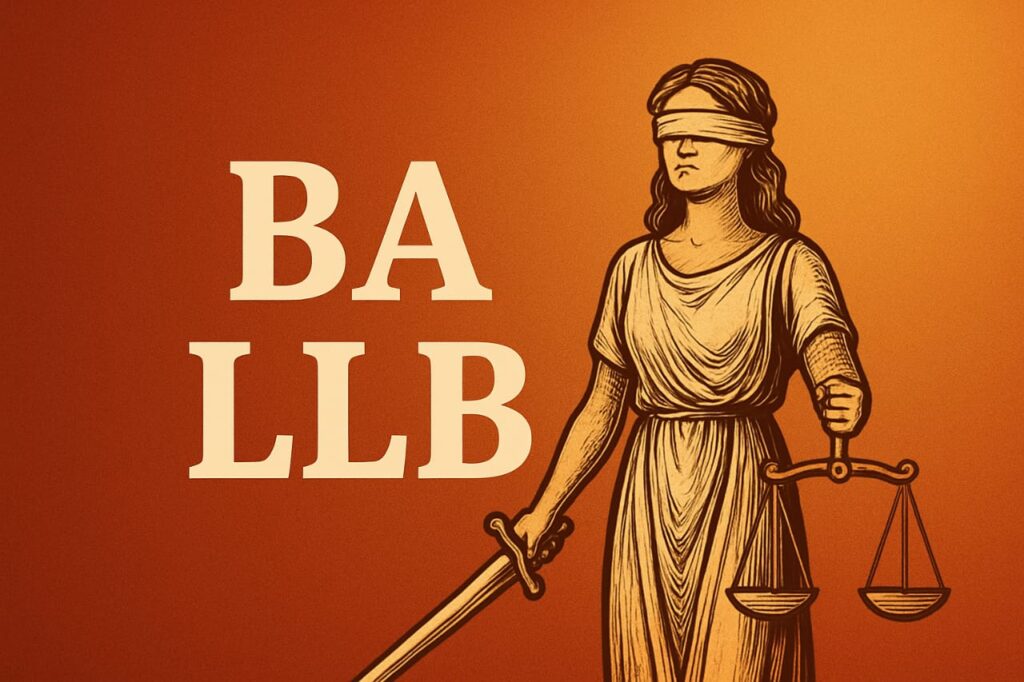भारतीय संघीय शासन व्यवस्था : स्वरूप, विशेषताएँ एवं चुनौतियाँ (Indian Federal System of Governance: Nature, Features and Challenges)
प्रस्तावना
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और भौगोलिक विविधता अत्यधिक व्यापक है। इतनी विविधताओं के बीच राष्ट्रीय एकता बनाए रखना किसी भी शासन प्रणाली के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। संविधान निर्माताओं ने इस विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसा राजनीतिक ढाँचा तैयार किया, जिसमें न केवल राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता मिले बल्कि केंद्र की मज़बूती भी बनी रहे। इसी कारण भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था (Federal System of Government) को अपनाया गया।
हालाँकि, भारत का संघवाद अमेरिकी मॉडल की तरह कठोर नहीं है और न ही ब्रिटिश मॉडल की तरह पूर्णतः एकात्मक (Unitary) है। यह एक मिश्रित ढाँचा (Mixed Structure) है, जहाँ संघीयता और एकात्मकता दोनों का संगम देखने को मिलता है। विद्वानों ने इसे “Quasi-Federal State” अथवा “अर्ध-संघीय राज्य” कहा है।
संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा
संघवाद (Federalism) ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में विभाजित होती हैं।
- के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare) : “संघवाद का सार यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा सुनिश्चित हो।”
- ए.वी. डाइसि (A.V. Dicey) : “संघीय शासन वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक स्तर को संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें अन्य स्तर छीन नहीं सकता।”
अर्थात संघीयता का मूल आधार संविधान द्वारा संरक्षित शक्तियों का विभाजन है।
भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को “राज्यों का संघ (Union of States)” कहता है। इसका तात्पर्य है कि भारत में राज्य अपने-आप में स्वतंत्र इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि उनका अस्तित्व संसद द्वारा बनाए गए प्रावधानों से है।
भारत का संघवाद पारंपरिक संघवाद से अलग है। अमेरिकी संघवाद “राज्यों का समझौता” है, जबकि भारतीय संघवाद “राज्यों का संघ” है। यही कारण है कि भारतीय संघवाद को अद्वितीय कहा जाता है, जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्व मौजूद हैं।
भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ
1. लिखित एवं विस्तृत संविधान
भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और अनेक संशोधन शामिल हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
2. शक्तियों का विभाजन
संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियाँ तीन सूचियों में बाँटी गई हैं :
- संघ सूची (Union List) – 100 विषय (जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा)
- राज्य सूची (State List) – 61 विषय (जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य)
- समवर्ती सूची (Concurrent List) – 52 विषय (जैसे शिक्षा, विवाह, अनुबंध)
3. संविधान की सर्वोच्चता
भारत में संविधान सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों ही इसकी अधीनता में कार्य करते हैं।
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
संविधान की रक्षा और व्याख्या का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। यह संघवाद का संरक्षक है।
5. द्विसदनीय संसद
भारत की संसद द्विसदनीय है – लोकसभा (जन प्रतिनिधि) और राज्यसभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व)। राज्यसभा संघीय ढाँचे को मजबूती प्रदान करती है।
6. संविधान की कठोरता
संविधान संशोधन की प्रक्रिया आंशिक रूप से कठोर है। विशेष रूप से संघ-राज्य संबंधी प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के साथ-साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक है।
एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features)
भारतीय संघवाद में कई प्रावधान ऐसे हैं जो इसे एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं :
- मजबूत केंद्र – विदेश नीति, रक्षा, मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण विषय केंद्र के अधीन हैं।
- राज्यों का अस्तित्व केंद्र से – अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है।
- आपातकालीन प्रावधान – अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है।
- गवर्नर की भूमिका – राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।
- एकल संविधान – भारत में केवल एक संविधान है, जबकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अलग संविधान है।
भारतीय संघवाद की प्रकृति पर विचार
- के.सी. व्हेयर : भारत “Quasi-Federal” है।
- डॉ. अंबेडकर : “भारत में संघीय प्रणाली है, किंतु संकट के समय यह एकात्मक रूप धारण कर लेती है।”
- सर्वोच्च न्यायालय (S.R. Bommai v. Union of India, 1994) : संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
संघ-राज्य संबंध
1. विधायी संबंध
- तीन सूचियों में शक्तियों का विभाजन।
- टकराव की स्थिति में अनुच्छेद 254 के अनुसार संघीय कानून को प्रधानता।
2. प्रशासनिक संबंध
- गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं।
- केंद्र राज्यों को नीतिगत निर्देश दे सकता है।
- राज्यों के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी में केंद्र की भूमिका।
3. वित्तीय संबंध
- कराधान में अधिकतर शक्तियाँ केंद्र के पास।
- वित्त आयोग (अनु. 280) राज्यों के लिए अनुदान और हिस्सेदारी की अनुशंसा करता है।
- GST परिषद (Goods and Services Tax Council) संघीय सहयोग का आधुनिक उदाहरण है।
भारतीय संघवाद की चुनौतियाँ
- राज्यों की वित्तीय निर्भरता – राज्यों के पास सीमित कराधान अधिकार हैं, जिससे वे केंद्र पर निर्भर रहते हैं।
- राजनीतिक दलों का संघर्ष – अलग-अलग दलों की सरकार होने पर नीति टकराव और मतभेद बढ़ जाते हैं।
- अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग – राष्ट्रपति शासन का बार-बार इस्तेमाल संघीय ढाँचे को कमजोर करता है।
- भाषाई एवं क्षेत्रीय विवाद – भाषा आंदोलन, राज्य पुनर्गठन और अलग राज्य की मांग संघवाद की चुनौतियाँ हैं।
- क्षेत्रीय दलों का उदय – यह राष्ट्रीय नीति निर्माण में अस्थिरता पैदा करता है।
- संसाधनों का असमान वितरण – प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक अवसरों की असमानता राज्यों के बीच असंतोष पैदा करती है।
संघवाद को मजबूत करने हेतु उपाय
- वित्तीय विकेंद्रीकरण – राज्यों को अधिक कराधान अधिकार प्रदान किए जाएँ।
- अनुच्छेद 356 का सीमित उपयोग – केवल वास्तविक संवैधानिक संकट में ही प्रयोग हो।
- अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) – राज्यों और केंद्र के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- राज्यसभा को सशक्त बनाना – राज्यों के हितों की रक्षा के लिए इसे अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है।
- स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन – 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों और नगरपालिकाओं को और सशक्त किया जाए।
- सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद – “Team India” की भावना के साथ नीतिगत सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए।
निष्कर्ष
भारतीय संघीय शासन व्यवस्था विश्व में अद्वितीय है। यह न तो पूर्णतः अमेरिकी संघीय मॉडल है और न ही ब्रिटिश एकात्मक मॉडल। इसे सही रूप में “संघीय ढाँचा युक्त अर्ध-संघीय व्यवस्था” कहा जा सकता है।
भारत का संघवाद प्रारंभिक काल में “केंद्र-सशक्त संघवाद” था, जो धीरे-धीरे “सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism)” और आज “प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive Federalism)” की दिशा में बढ़ रहा है।
संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, न्यायपालिका के सक्रिय दृष्टिकोण तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति ने इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा है। भविष्य में यदि वित्तीय विकेंद्रीकरण, राजनीतिक समन्वय और स्थानीय स्वशासन को और प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय संघवाद और अधिक मज़बूत होकर देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता रहेगा।