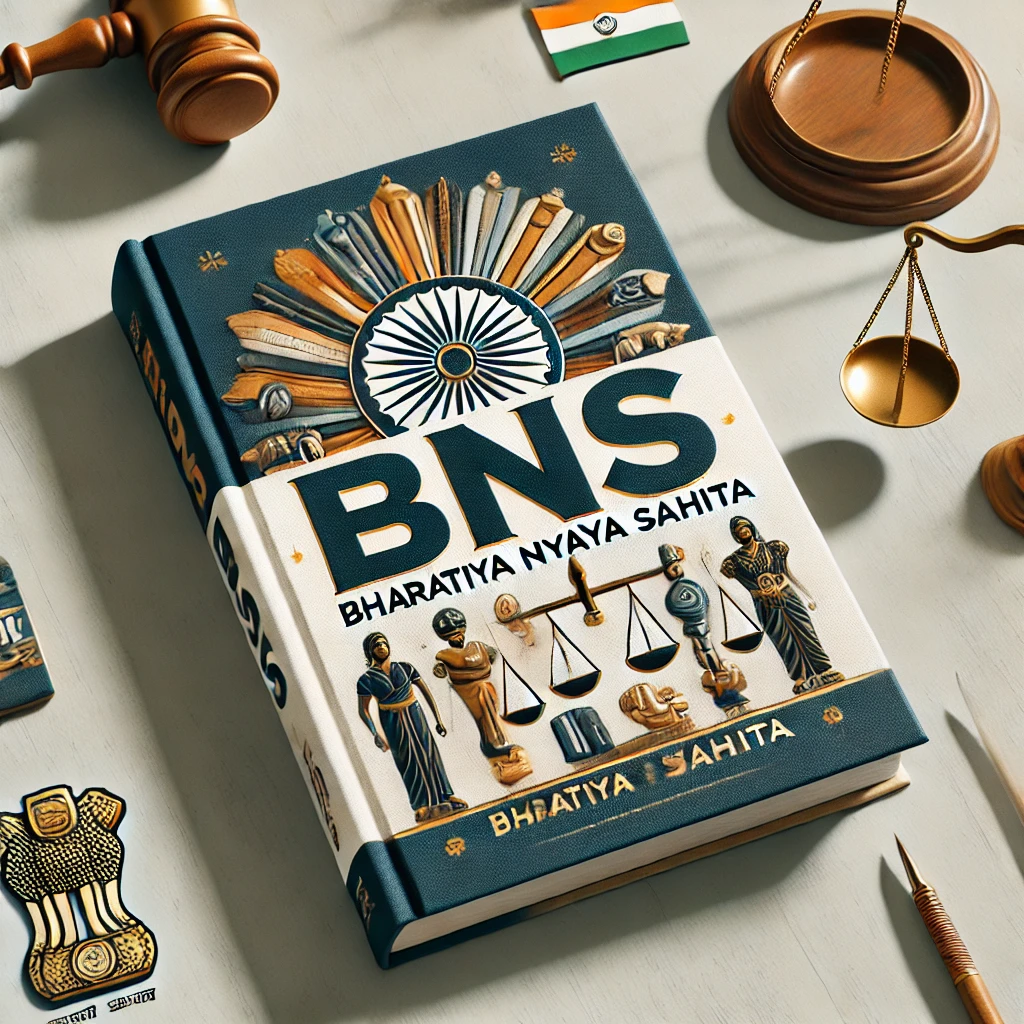भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1
धारा 1: संहिता का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
- संक्षिप्त नाम – इस अधिनियम को “भारतीय न्याय संहिता, 2023” कहा जाएगा।
- विस्तार – यह संहिता पूरे भारत पर लागू होगी।
- प्रारंभ – यह संहिता केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगी।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा इस संहिता की आधिकारिक पहचान प्रदान करती है।
- यह स्पष्ट करती है कि यह संहिता भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।
- इसका प्रभावी होने का समय केंद्र सरकार द्वारा तय अधिसूचना पर निर्भर करेगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2
धारा 2: क्षेत्रीय विस्तार
यह संहिता:
- भारत के भीतर घटित प्रत्येक अपराध पर लागू होगी।
- भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू होगी, जब तक कि अन्यथा कोई विशेष कानून न हो।
- भारतीय जलयान (जहाज) या वायुयान पर किए गए अपराधों पर भी लागू होगी, भले ही वे भारत की सीमा के बाहर हों।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा संहिता की क्षेत्रीय सीमा को स्पष्ट करती है।
- भारत के किसी भी भाग में घटित अपराध इस संहिता के अंतर्गत आएंगे।
- यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है, तो भी उसे इस संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है।
- भारतीय जहाजों या विमानों पर होने वाले अपराध भारत की कानूनी सीमा में माने जाएंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3
धारा 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर संहिता का प्रभाव
यदि कोई व्यक्ति, जो भारत के किसी भी कानून के अनुसार दंडनीय अपराध करता है और वह अपराध भारत की सीमा के बाहर किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को, इस संहिता के अनुसार, वैसे ही दंडित किया जा सकता है जैसे कि वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है, जो भारतीय कानून के अनुसार दंडनीय है, तो उसे भारत में उसी प्रकार दंडित किया जा सकता है जैसे कि वह अपराध भारत में किया गया हो।
- इस प्रावधान का उद्देश्य भारत के नागरिकों को विदेशों में किए गए अपराधों से बचने की स्वतंत्रता न देना और वैश्विक स्तर पर भारतीय कानून का प्रभाव बनाए रखना है।
- इस धारा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, विदेशी धरती पर किए गए गंभीर अपराधों, और भारतीय नागरिकों की संलिप्तता वाले मामलों में किया जा सकता है।
उदाहरण:
- यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में धोखाधड़ी या साइबर अपराध करता है, तो भारत लौटने पर उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी भूमि में आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है, तो भी भारतीय न्यायालय उसे भारतीय कानूनों के तहत दंडित कर सकते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 4
धारा 4: इस संहिता के प्रावधानों का लागू होना
- कोई भी अपराध जो इस संहिता में वर्णित है, वह किसी अन्य विशेष कानून के तहत दंडनीय नहीं होगा, सिवाय इसके कि यदि विशेष कानून में कुछ अलग से प्रावधान हो।
- इस संहिता में वर्णित अपराधों के संबंध में यदि किसी अन्य कानून में कोई अलग दंड निर्धारित किया गया हो, तो उस विशेष कानून के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह स्पष्ट करती है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत वर्णित अपराधों के संबंध में अगर कोई विशेष कानून पहले से लागू हो, तो उस विशेष कानून के दंड प्रावधानों का पालन किया जाएगा, न कि इस संहिता के तहत दंड।
- उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराध को विशेष कानून (जैसे आतंकवाद के खिलाफ कानून) में अधिक कड़ा दंड निर्धारित है, तो उसे वही दंड मिलेगा, न कि सामान्य संहिता के तहत।
- हालांकि, अगर विशेष कानून में कुछ विशिष्ट निर्देश नहीं हैं, तो फिर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू होंगे।
उदाहरण:
- आतंकवाद विरोधी कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए अधिक कड़े दंड का प्रावधान हो सकता है, तो उस विशेष कानून के तहत दोषी को सजा मिलेगी, न कि इस संहिता के तहत।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 5
धारा 5: संहिता का दायरा और अपवाद
- इस संहिता के तहत सभी अपराधों का विवेचन किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं।
- यदि किसी अन्य विशेष कानून के तहत किसी अपराध का विशेष प्रकार से विवेचन, प्रक्रिया या दंड निर्धारित किया गया हो, तो उस कानून के अनुसार उस अपराध की सुनवाई और दंड प्रक्रिया की जाएगी।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह निर्धारित करती है कि संहिता का प्रभाव सभी प्रकार के अपराधों पर होगा, लेकिन यदि कोई विशेष कानून किसी अपराध के लिए अलग से प्रावधान या दंड निर्धारित करता है, तो उस विशेष कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- उदाहरण के लिए, यदि आतंकवाद विरोधी कानून या दहेज प्रताड़ना कानून में किसी अपराध के लिए विशिष्ट प्रक्रिया या सजा तय की गई हो, तो उस मामले में इस संहिता के सामान्य प्रावधानों की जगह वही विशेष कानून लागू होगा।
उदाहरण:
- अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद संबंधी अपराध करता है, तो उसे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सजा मिलेगी, न कि सामान्य संहिता के प्रावधानों के अनुसार।
- इसी तरह, दहेज उत्पीड़न के मामले में विशेष कानून के अनुसार सुनवाई और दंड प्रक्रिया होगी।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि विशेष कानून की प्राथमिकता होती है, और यदि किसी अपराध के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई हो, तो वही लागू होगी।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 6
धारा 6: दंड की प्रकृति
इस संहिता के तहत यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, तो वह दंड किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे:
- मौत की सजा
- कारावास (जो कठोर या साधारण हो सकता है)
- जुर्माना
- सजा और जुर्माना दोनों
यह धारा यह स्पष्ट करती है कि संहिता के तहत निर्धारित अपराधों के लिए, न्यायालय को विभिन्न प्रकार के दंड देने की स्वतंत्रता है, और यह दंड उस अपराध की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा दंड की विविधता को सुनिश्चित करती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर, सजा मौत से लेकर जुर्माने तक हो सकती है।
- मौत की सजा अधिक गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित हो सकती है, जैसे कि हत्या, आतंकवाद आदि।
- कारावास का दंड ऐसे अपराधों के लिए हो सकता है, जो गंभीर तो हैं, लेकिन उनकी प्रकृति मौत की सजा की नहीं होती।
- जुर्माना सामान्य रूप से उन अपराधों के लिए हो सकता है जिनमें वित्तीय हानि हुई हो या जो कम गंभीर प्रकृति के हों।
- सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान भी कुछ मामलों में हो सकता है।
उदाहरण:
- हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए मौत की सजा हो सकती है।
- चोरी या जमानत का उल्लंघन जैसे अपराधों में कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध के आधार पर उचित और न्यायपूर्ण दंड दिया जाए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 7
धारा 7: असाधारण परिस्थितियों में दंड में छूट
- अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए मजबूर था या उसे किसी ऐसी असाधारण स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे उस व्यक्ति के लिए अपराध करना अनिवार्य हो गया, तो उस व्यक्ति को दंड में छूट दी जा सकती है।
- यह छूट केवल विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है, जैसे कि आत्मरक्षा, मनोविज्ञानिक दबाव या ऐसी अन्य परिस्थितियाँ जिनमें अपराध करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति से परे था।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा विवेचना करती है कि यदि किसी व्यक्ति ने विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आत्मरक्षा के तहत, या बेवजह दबाव में आकर अपराध किया हो, तो उसे दंड से मुक्त किया जा सकता है या दंड में कमी की जा सकती है।
- इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कभी-कभी अपराध करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के कारण अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
उदाहरण:
- यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में किसी हमलावर को मार देता है, तो उसे हत्या के आरोप से मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कार्रवाई संवेदनशील परिस्थितियों में की गई थी।
- यदि कोई व्यक्ति मनोविज्ञानिक दबाव के कारण कोई अपराध करता है, तो भी उसे सामान्य दंड से छूट मिल सकती है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया में केवल सामान्य परिस्थितियों में ही दंड तय किया जाए, और विशेष परिस्थितियों में एक नरम दृष्टिकोण अपनाया जाए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8
धारा 8: छूट या दंड में बदलाव के लिए अपील की प्रक्रिया
- अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और वह दंड में छूट या दंड के स्तर में बदलाव की मांग करता है, तो उसे अपील करने का अधिकार होगा।
- अपील को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, जहां से दंड में संशोधन या कमी की जा सकती है, यदि इसके लिए उचित कारण हो।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा अपील की प्रक्रिया को परिभाषित करती है, जिसके माध्यम से कोई दोषी व्यक्ति अपील कर सकता है और दंड में छूट या दंड की कठोरता में बदलाव की मांग कर सकता है।
- अपील उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, और यदि अदालत को यह लगता है कि दंड अधिक है या अन्य कारणों से बदलाव की आवश्यकता है, तो दंड को संशोधित किया जा सकता है।
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्याय की प्रक्रिया में एक लचीलापन है, जिससे किसी दोषी व्यक्ति को गलत सजा न मिले और उसे उचित न्याय मिल सके।
उदाहरण:
- यदि किसी व्यक्ति को दी गई सजा अत्यधिक कड़ी महसूस होती है, तो वह अपील दायर कर सकता है और न्यायालय से सजा में कमौती की मांग कर सकता है।
- यदि किसी दोषी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया गया है और वह यह साबित करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वह अपील करके जुर्माने में छूट प्राप्त कर सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपील का अधिकार प्रत्येक दोषी व्यक्ति को मिले, ताकि किसी भी अन्याय को सुधारने का मौका मिल सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 9
धारा 9: अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सुनवाई
इस धारा के तहत, भारत के न्यायालय उन अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सुनवाई करेंगे जो भारत की न्यायिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसके अंतर्गत, ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय होते हैं और जिनकी सुनवाई भारत के न्यायालयों में की जाती है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा भारत की न्यायिक अधिकारिता को स्थापित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत के न्यायालय उन अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं जो भारत के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
- इसका उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में ही न सुना जाए, बल्कि भारत में भी उन अपराधों की सुनवाई की जा सकती है जो भारत के कानूनी ढांचे के तहत दंडनीय हों।
- इस धारा के माध्यम से, भारत अंतर्राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि भारत में किए गए अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकदमा भारत के न्यायालयों में चल सके।
उदाहरण:
- मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सुनवाई भारत के न्यायालयों में की जा सकती है, यदि ये अपराध भारत के क्षेत्र में किए गए हैं।
- यदि कोई भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में संलिप्त होता है, तो उसे भारतीय न्यायालय में न्याय दिलाने का अधिकार होगा।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मामले में भारत भी अपने न्यायालयों का उपयोग करके वैश्विक न्याय की प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 10
धारा 10: न्यायालयों की क्षेत्राधिकार सीमा
- इस धारा के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए न्यायालयों की क्षेत्राधिकार सीमा उन अपराधों पर लागू होती है जो भारत के क्षेत्र में किए गए हों या जिनका प्रभाव भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर हो।
- यदि अपराध भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन इसका प्रभाव भारत के क्षेत्र में पड़ा हो, तो भारत का न्यायालय उस अपराध की सुनवाई करने के लिए सक्षम होगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा क्षेत्राधिकार की सीमा तय करती है, यानी कि भारत के न्यायालयों को किस तरह के अपराधों की सुनवाई का अधिकार होगा।
- अगर कोई अपराध भारत के बाहर हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव भारत में पड़ा है, तो भारत का न्यायालय उस मामले को सुन सकता है।
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को भी यदि भारत में प्रभाव पड़ा हो, तो भारतीय न्यायालय उन्हें सुनने के लिए सक्षम होंगे।
उदाहरण:
- यदि कोई अपराधी भारत से बाहर किसी देश में अपराध करता है, लेकिन वह अपराध भारत के नागरिकों को प्रभावित करता है, तो भारत का न्यायालय उस अपराध की सुनवाई कर सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है, तो भारत का न्यायालय उस अपराध की सुनवाई करने का अधिकार रखेगा।
यह धारा भारत के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यदि अपराध का प्रभाव भारत में है, तो भारत के न्यायालयों को उस पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 11
धारा 11: विदेशी अपराधों की सुनवाई
- विदेशी अपराध को भारत के न्यायालयों में सुनने की प्रक्रिया इस धारा के तहत तय की गई है। यदि कोई अपराध भारत के बाहर हुआ है, तो उसे भारत के न्यायालय में तब तक सुना जा सकता है जब तक कि वह अपराध भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र में न आता हो।
- यदि विदेशी अपराध का प्रभाव भारत में पड़ा हो या वह भारत के नागरिकों या संपत्ति को प्रभावित करता हो, तो ऐसे अपराधों की सुनवाई भारतीय न्यायालयों में की जा सकती है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह निर्धारित करती है कि विदेशी अपराधों की सुनवाई भारत के न्यायालयों में की जा सकती है यदि अपराध का प्रभाव भारत में पड़ा हो।
- इसका उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होने वाले अपराधों को भी यदि उनका असर भारत पर हो, तो भारतीय न्यायालय उन्हें सुनने के अधिकार से बाहर नहीं रखेंगे।
- उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति विदेशी देश में किसी अपराध को अंजाम देता है, लेकिन उसका प्रभाव भारत के नागरिकों या भारत में स्थित संपत्ति पर पड़ता है, तो उसे भारत के न्यायालय में सुना जा सकता है।
उदाहरण:
- यदि कोई व्यक्ति विदेशी वेबसाइट के माध्यम से भारत के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करता है, तो भारत के न्यायालय में उस मामले की सुनवाई की जा सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति विदेशी भूमि पर किसी भारत सरकार के अधिकारी को नुकसान पहुँचाता है, तो भारत का न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई अपराध भारत के बाहर हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर पड़ा है, तो भारत के न्यायालयों को सुनवाई का अधिकार मिलेगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 12
धारा 12: सुनवाई के दौरान गवाहों का संरक्षण
- इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति गवाह के रूप में किसी मामले में बयान देता है, तो गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि गवाहों को किसी प्रकार के दबाव, धमकी या प्रताड़ना से बचाया जाए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के अपने बयान दे सकें।
- यदि गवाह को अपने बयान देने के कारण सुरक्षा खतरे का सामना होता है, तो न्यायालय गवाहों के संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठा सकता है, जैसे उन्हें गुमनाम रखना या सुरक्षित स्थान पर रखना।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और उनके साक्ष्य देने के अधिकार की रक्षा करती है।
- इसका उद्देश्य गवाहों को डर या दबाव से मुक्त करना है, ताकि वे सही और निष्पक्ष तरीके से अपने बयान दे सकें।
- गवाहों की सुरक्षा गवाहों के अधिकारों का उल्लंघन न होने दे, और सुनिश्चित करें कि उनका बयान बिना किसी भय के लिया जाए।
उदाहरण:
- यदि कोई गवाह आतंकवाद या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मामले में बयान देता है और उसे धमकियाँ मिलती हैं, तो न्यायालय उसे सुरक्षित स्थान पर रख सकता है और गुमनाम रख सकता है।
- यदि कोई गवाह नशीली दवाओं से जुड़े मामले में बयान देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो न्यायालय गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि वे बिना किसी डर या भय के न्यायालय में सही और निष्पक्ष साक्ष्य प्रदान कर सकें।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 13
धारा 13: जमानत और हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार
- इस धारा के तहत, जमानत पर किसी व्यक्ति को रिहा करने की प्रक्रिया और हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार को स्पष्ट किया गया है।
- यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे सकता है, जब तक कि यह न्यायिक दृष्टिकोण से उचित हो।
- हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को उचित उपचार, स्वास्थ्य देखभाल और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
स्पष्टीकरण:
- इस धारा का उद्देश्य यह है कि गिरफ्तारी के बावजूद व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए और अगर संभव हो तो जमानत पर रिहाई दी जाए।
- जमानत देने से पहले, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपित व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में कोई अन्याय न हो और वह न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए उपलब्ध रहे।
- साथ ही, यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचाया जाए और उसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलें।
उदाहरण:
- यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो वह न्यायालय से जमानत पर रिहाई की मांग कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती है, तो उसे उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी।
- किसी व्यक्ति को अगर झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो उसे जमानत पर रिहाई मिल सकती है, जब तक कि मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही हो।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के मानवाधिकार सुरक्षित रहें और यदि कानूनी स्थिति अनुमति देती है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 14
धारा 14: दोष सिद्धि के सिद्धांत
- धारा 14 के अनुसार, किसी आरोपी के दोष सिद्धि से पहले, उसे निर्दोष माना जाएगा। इसका मतलब है कि अपराधी होने का आरोप केवल साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर तय किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त साक्ष्य के दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
- इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के सिद्ध दोष से पहले उसे निर्दोष माना जाए, जब तक कि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य उस व्यक्ति के दोष को साबित न कर दें।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा दोष सिद्धि के सिद्धांत को लागू करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
- यदि साक्ष्य अपर्याप्त हैं या दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं, तो व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा।
- यह सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष और सही तरीके से काम करे।
उदाहरण:
- यदि किसी आरोपी पर किसी अपराध का आरोप है, तो उसे दोषी ठहराने से पहले न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खिलाफ काफी और उचित साक्ष्य उपलब्ध हैं।
- यदि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं और साक्ष्य अपर्याप्त हैं, तो उसे निर्दोष माना जाएगा और उस पर दोष नहीं लगाया जा सकेगा।
यह धारा दोष सिद्धि के सिद्धांत को लागू करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी व्यक्ति को निर्दोष माना जाए, जब तक कि उसके खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश न किए जाएं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 15
धारा 15: आरोपपत्र की प्रस्तुति और आरोपों की स्पष्टता
- इस धारा के अनुसार, जब किसी आरोपी पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो आरोपपत्र (charge sheet) को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस आरोपपत्र में उस अपराध से संबंधित सभी साक्ष्य, गवाहों के बयान, और साक्ष्यों का वर्णन होगा, ताकि न्यायालय उस मामले को ठीक से समझ सके और आरोपी पर आरोपों की गंभीरता को निर्धारित कर सके।
- आरोपपत्र में उन सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा जिनका आरोपी पर आरोप है, ताकि आरोपी को समझ में आ सके कि उस पर क्या आरोप है। इस प्रक्रिया में आरोपों की स्पष्टता और सटीकता सुनिश्चित की जाती है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपपत्र में सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से और सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ताकि आरोपी और न्यायालय दोनों को सही से जानकारी मिल सके।
- आरोपपत्र को न्यायालय में पेश करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें सभी साक्ष्य और तथ्य सही तरीके से शामिल हों।
- आरोपी को यह अधिकार होता है कि वह आरोपपत्र को ध्यान से पढ़े और समझे, ताकि वह अपने बचाव के लिए उचित कदम उठा सके।
उदाहरण:
- अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है, तो आरोपपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि आरोपी ने कहाँ और कब चोरी की और क्या साक्ष्य हैं जो इस आरोप का समर्थन करते हैं।
- अगर किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है, तो आरोपपत्र में हत्या से जुड़ी सभी साक्ष्य, जैसे गवाहों के बयान, मौजूद प्रमाण, और दृश्य साक्ष्य बताए जाएंगे।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपपत्र में स्पष्टता और सटीकता हो, ताकि न्यायालय और आरोपी दोनों को सही जानकारी मिल सके और मामले की सुनवाई निष्पक्ष रूप से हो।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 16
धारा 16: आरोपी के पास अपना बचाव करने का अधिकार
- इस धारा के तहत, प्रत्येक आरोपी को अपने खिलाफ लगे आरोपों से बचाव करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि आरोपी को अपनी निर्दोषता साबित करने का अवसर दिया जाएगा। उसे न्यायालय में अपना बचाव प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
- आरोपी को यह अधिकार भी होगा कि वह गवाहों को आग्रह कर सके, साक्ष्य पेश कर सके, और अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सके। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपी को न्यायपूर्ण सुनवाई का पूरा अवसर मिले, ताकि वह अपने बचाव के लिए सभी प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत कर सके।
- इसके अलावा, आरोपी को वकील (अगर वह चाहे) नियुक्त करने का अधिकार भी होगा, ताकि उसका कानूनी बचाव सही ढंग से किया जा सके। यदि आरोपी के पास वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो न्यायालय नि:शुल्क वकील की व्यवस्था कर सकता है।
स्पष्टीकरण:
- इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले और उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो।
- इसे न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक तरीका माना जाता है, ताकि आरोपी को आरोपों के संबंध में अपनी सत्यता या निर्दोषता साबित करने का समान अवसर मिल सके।
- इस धारा के तहत, यदि आरोपी को अपने अधिकारों के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय उसे इस कानूनी समर्थन की व्यवस्था कर सकता है।
उदाहरण:
- अगर किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है, तो वह अपने गवाहों को पेश कर सकता है, जो यह साबित कर सकते हैं कि वह समय और स्थान पर वहां नहीं था।
- यदि किसी आरोपी को सार्वजनिक बचाव वकील की आवश्यकता है, तो न्यायालय उसे यह वकील नियुक्त कर सकता है, ताकि वह अपना उचित बचाव कर सके।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को हर संभव तरीका दिया जाए ताकि वह अपने बचाव में उचित साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत कर सके और उसके मानवाधिकार की रक्षा की जा सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 17
धारा 17: आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार
- इस धारा के तहत, आरोपी को यह अधिकार होता है कि वह अपने बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सके और गवाहों को बुला सके। यदि आरोपी चाहता है कि उसके बचाव के लिए कुछ साक्ष्य पेश किए जाएं या गवाह बुलाए जाएं, तो उसे न्यायालय से अनुमति मिलनी चाहिए।
- इसके अलावा, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी को अपने बचाव में सभी उचित साक्ष्य पेश करने का अवसर मिले और वह अपने बचाव में सभी तथ्यों और गवाहों को अदालत में पेश कर सके।
- यह धारा आरोपी के अधिकार को सुनिश्चित करती है कि वह केवल आरोपों का सामना नहीं करेगा, बल्कि उसके पास अपना बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय और साधन होगा। इससे आरोपी को यह मौका मिलता है कि वह साक्ष्यों के आधार पर अपनी निर्दोषता साबित कर सके।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा न्यायिक निष्पक्षता और न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आरोपी को सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो।
- आरोपी को विधिक प्रक्रिया के दौरान यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए कोई भी प्रमाण, दस्तावेज, या गवाह पेश कर सके।
उदाहरण:
- यदि किसी व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप है, तो वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी या गवाहों के माध्यम से यह साबित कर सकता है कि वह इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं था।
- अगर किसी आरोपी को लगता है कि उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य झूठे हैं, तो वह इन साक्ष्यों का विरोध कर सकता है और अपनी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने बचाव का पूरा मौका मिले, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपूर्ण परिणाम हासिल हो सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 18
धारा 18: साक्ष्य की स्वीकृति और अस्वीकृति
- धारा 18 के तहत, न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार कर सके, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया जाता है। यदि साक्ष्य उचित और प्रमाणिक होते हैं, तो उन्हें स्वीकार किया जाता है, लेकिन यदि वे अवैध, झूठे, या अप्रासंगिक होते हैं, तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।
- न्यायालय साक्ष्य की वैधता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करता है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया में सही रूप से और कानूनी तरीके से प्रस्तुत किए जाएं। यदि कोई साक्ष्य कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होता, तो न्यायालय उसे अस्वीकार कर सकता है।
- इस धारा का उद्देश्य यह है कि साक्ष्य केवल कानूनी और वैध तरीके से पेश किए जाएं, ताकि किसी भी आरोपी या पक्ष के सत्यापन में कोई बाधा न आए और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हो।
स्पष्टीकरण:
- न्यायालय साक्ष्य की स्वीकृति या अस्वीकृति में यह ध्यान रखता है कि वे कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं या नहीं।
- यदि कोई साक्ष्य दस्तावेज़ या गवाहों से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह सत्य और कानूनी तरीके से प्रस्तुत हो, और न्यायालय की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
उदाहरण:
- यदि एक आरोपी के खिलाफ दस्तावेज़ साक्ष्य पेश किया गया है, लेकिन वह दस्तावेज़ कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं है, तो न्यायालय उसे अस्वीकार कर सकता है।
- यदि किसी गवाह का बयान अस्पष्ट या प्रासंगिक नहीं है, तो न्यायालय उसे स्वीकृत नहीं करेगा।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य केवल कानूनी और प्रमाणिक रूप से ही अदालत में प्रस्तुत किए जाएं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चले।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 19
धारा 19: साक्ष्य प्रस्तुत करने के समय सीमा
- धारा 19 के अनुसार, साक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह समय सीमा न्यायालय द्वारा तय की जाती है, और इसमें किसी भी प्रकार की देरी को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जा सकता है।
- इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साक्ष्य समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि सुनवाई की निष्पक्षता बनी रहे और किसी पक्ष को समय का लाभ न मिले।
- न्यायालय किसी भी कारण से समय सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन इसे बहुत ही जरूरी और व्यावहारिक कारणों से किया जाता है।
- साक्ष्य प्रस्तुत करने की समय सीमा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी कारणवश समय पर साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो वह साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है, या अस्वीकृत हो सकता है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य उचित समय में प्रस्तुत किए जाएं और किसी भी प्रकार की देरी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो।
- यदि कोई पक्ष समय सीमा में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, तो न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उसे स्वीकार न करे।
उदाहरण:
- यदि किसी आरोपी के खिलाफ गवाहों का बयान पेश किया जाता है, तो गवाहों को तय समय सीमा में न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए।
- अगर किसी पक्ष को नया साक्ष्य प्रस्तुत करना हो, तो न्यायालय तय करेगा कि वह साक्ष्य कितने समय के भीतर पेश किया जा सकता है।
यह धारा न्यायिक प्रक्रिया की समयबद्धता और न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 20
धारा 20: गवाहों का बयान लेने का तरीका
- धारा 20 के तहत, गवाहों से बयान लेने का तरीका निर्धारित किया गया है। गवाहों के बयान को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और उनके बयान को न्यायालय में पेश किया जाता है, ताकि पक्षों के दावे और प्रतिवादों को सही तरीके से सुना जा सके।
- इस धारा के अनुसार, गवाह से बयान मौखिक रूप में लिया जाता है, और यह बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लिया जाना चाहिए। गवाह को स्वतंत्र रूप से अपने विचार और अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार या अनुचित प्रभाव न पड़े।
- बयान लेने की प्रक्रिया में गवाहों के प्रति सम्मान बनाए रखा जाता है, और उन्हें यह सूचित किया जाता है कि उनका बयान कानूनी दायित्व के तहत लिया जा रहा है। इसके अलावा, गवाहों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी सूचित किया जाता है, ताकि वे पूरी तरह से समझ सकें कि वे क्या कह रहे हैं और उनका बयान किस उद्देश्य से लिया जा रहा है।
- यदि गवाह लिखित बयान देना चाहता है, तो वह अपने बयान को लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है, बशर्ते कि यह बयान पूरी तरह से सत्य और संबंधित हो।
स्पष्टीकरण:
- इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गवाहों से बयान सही, निष्पक्ष, और स्वच्छंद तरीके से लिया जाए, ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई गलतफहमी या न्याय का हनन न हो।
- गवाह से गलत बयान देने या झूठ बोलने के लिए सजा का प्रावधान भी होता है, जिससे गवाहों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होता है।
उदाहरण:
- अगर एक गवाह एक साक्ष्य के रूप में बयान दे रहा है कि वह घटना के समय वहां था, तो उसका बयान स्वतंत्र रूप से लिया जाएगा और उसे सत्य और निर्दोष रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- अगर गवाह को लिखित रूप में बयान देना है, तो वह अपना बयान लिखकर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यह बयान केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह पूरी तरह से सत्य हो।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों का बयान पूरी न्यायिक निष्पक्षता के साथ लिया जाए, ताकि न्याय की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 21
धारा 21: गवाहों की पूछताछ और क्रॉस-एग्जामिनेशन
- धारा 21 के अनुसार, गवाहों की पूछताछ और उनके क्रॉस-एग्जामिनेशन का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गवाह द्वारा दिया गया बयान सही और सत्य है। क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान, आरोपी या उसका वकील गवाह से प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि गवाह के बयान की प्रामाणिकता और सत्यता की जांच की जा सके।
- क्रॉस-एग्जामिनेशन में गवाह से पूछे गए प्रश्न उसके पहले के बयान और उसकी साक्ष्य से संबंधित होते हैं। इसके तहत, गवाह को यह बताया जाता है कि वह जो कुछ भी कह रहा है, वह सत्य होना चाहिए, और यदि गवाह ने झूठ बोला या गलत बयान दिया, तो उसका प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
- इस धारा के तहत, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि गवाहों से केवल वैध, सत्य, और प्रासंगिक प्रश्न पूछे जाएं। यदि कोई प्रश्न अनुचित या अवमाननात्मक होता है, तो उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।
- क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि गवाह पर अत्याचार या दबाव नहीं डाला जाए। यह साक्ष्य के सत्यापन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाह ने सही और निष्पक्ष बयान दिया है।
स्पष्टीकरण:
- क्रॉस-एग्जामिनेशन एक अधिकार है, जो पक्ष को अपने तर्क को साबित करने के लिए मिलता है। इसके माध्यम से गवाह के बयान की सत्यता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
- हालांकि, यह कानूनी प्रक्रिया के तहत नियंत्रित होता है, ताकि गवाह के साथ अनुचित या अवमाननात्मक व्यवहार न हो।
उदाहरण:
- अगर एक गवाह कहता है कि उसने दृश्य में किसी अपराध को होते हुए देखा, तो क्रॉस-एग्जामिनेशन में उसके बयान पर सवाल उठाया जा सकता है, जैसे “क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने सही व्यक्ति को देखा?”
- यदि गवाह ने कहा कि उसने साक्ष्य नहीं देखा, तो क्रॉस-एग्जामिनेशन में यह पूछा जा सकता है कि उसने क्यों या कैसे साक्ष्य नहीं देखा।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों से लिए गए बयान पूरी तरह से सत्य और साक्ष्य के आधार पर हों, जिससे न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित बने।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 22
धारा 22: गवाहों की अनदेखी या अस्वीकृति
- धारा 22 के अनुसार, यदि कोई गवाह किसी भी कारण से न्यायालय में पेश होने से इनकार करता है या गवाह की पेशी से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता है, तो न्यायालय उसे दंडित करने का अधिकार रखता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई भी देर या रुकावट न आए।
- इस धारा के तहत, यदि गवाह सत्य बोलने से इंकार करता है या अपनी गवाही देने में अवरोध डालता है, तो न्यायालय उसे सजा दे सकता है। गवाहों को यह याद दिलाया जाता है कि उनके द्वारा दिया गया बयान कानूनी दायित्व के तहत है, और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें न्यायालय की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त, यदि गवाह द्वारा अस्वीकृति की जाती है या वह कानूनी रूप से बाधित होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है, जैसे अदालत में पेशी के लिए कॉन्टेम्प्ट (अवमानना) का मामला दायर करना।
- न्यायालय के पास गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का अधिकार भी होता है, यदि यह पाया जाता है कि गवाह झूठ बोल रहा है या अपनी गवाही में धोखा दे रहा है। गवाह की इस विरोधात्मक स्थिति के आधार पर न्यायालय की निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा गवाहों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की चेतावनी देती है और न्यायालय को यह अधिकार देती है कि यदि गवाह सत्य बोलने से इंकार करता है, तो उसे दंडित किया जाए।
- गवाह को न्यायालय के सामने साक्ष्य देने की कानूनी जिम्मेदारी को याद दिलाया जाता है और यदि वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है।
उदाहरण:
- यदि कोई गवाह न्यायालय में गवाही देने से इंकार करता है, तो न्यायालय उसे सजा दे सकता है या अवमानना के लिए कार्यवाही कर सकता है।
- अगर किसी गवाह को पहले ही अदालत में पेश होने के लिए समन किया गया हो, लेकिन वह अनुपस्थित रहता है, तो न्यायालय उसकी गलती को दंडनीय मान सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों का सहयोग न्यायिक प्रक्रिया के सही संचालन में हो, ताकि न्याय का संपूर्ण निष्पक्ष रूप से निष्पादन हो सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 23
धारा 23: गवाहों का संरक्षण और सुरक्षा
- धारा 23 के अनुसार, गवाहों को उनके साक्ष्य देने के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार की धमकी, भय या दबाव से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गवाह स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने बयान दे सकें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे।
- यदि गवाह को खतरे या हानि का सामना हो, तो न्यायालय को गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। यह सुरक्षा गवाह को शारीरिक, मानसिक, या सामाजिक खतरे से बचाने के लिए हो सकती है।
- गवाहों की सुरक्षा के लिए, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि गवाहों को कोई नुकसान न पहुंचे और उनका गोपनीयता बनाए रखा जाए। न्यायालय गवाहों के नाम, पते, और साक्ष्य की गोपनीयता भी सुनिश्चित कर सकता है, ताकि गवाह को किसी भी प्रकार का प्रतिशोध या आत्म-रक्षा का डर न हो।
- इसके अलावा, इस धारा के तहत, यदि कोई गवाह न्यायालय में अपने बयान से इंकार करता है या खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो वह न्यायालय से सुरक्षा की मांग कर सकता है, और न्यायालय इस पर निर्णय ले सकता है कि गवाह को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए।
स्पष्टीकरण:
- गवाह की सुरक्षा न्याय प्रक्रिया के सही तरीके से संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। बिना किसी डर के गवाह अपने बयान देने में सक्षम होते हैं, और इससे सत्य का उद्घाटन होता है।
- गवाहों की सुरक्षा संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक अधिकारों के अनुरूप है, और यह समान न्याय सुनिश्चित करने का एक साधन है।
उदाहरण:
- अगर कोई गवाह किसी आपराधिक मामले में गवाही दे रहा है और उसे लगता है कि अपराधियों से उसे खतरा हो सकता है, तो वह न्यायालय से अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।
- अगर गवाह की पहचान सार्वजनिक होने के बाद उसके जीवन को खतरा हो, तो न्यायालय उसकी पहचान को गोपनीय रखने का आदेश दे सकता है और उसे संरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों को स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ अपने बयान देने का अवसर मिले, ताकि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और सही तरीके से पूरी हो सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 24
धारा 24: गवाहों को आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना
- धारा 24 के तहत, न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गवाहों के द्वारा दिए गए बयान को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गवाहों के बयान की सत्यता और विश्वसनीयता पर उचित विचार किया जाए।
- यदि कोई गवाह अपना बयान देने में स्पष्ट रूप से गलत जानकारी देता है या उसके बयान में विरोधाभास होते हैं, तो न्यायालय उसे आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह गवाह के बयान के उन हिस्सों को अस्वीकार कर सके जो संदिग्ध या अविश्वसनीय हैं, और केवल उन हिस्सों को स्वीकार कर सकता है जो सच्चे और विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।
- इसके अलावा, यदि गवाह द्वारा दिया गया बयान किसी कानूनी या नैतिक दबाव के तहत होता है या उसे झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो, तो उस बयान को अस्वीकृत किया जा सकता है। न्यायालय इस स्थिति में गवाह के बयान की सत्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा और अगर गवाह पर कोई अन्यायपूर्ण दबाव डाला गया हो तो वह बयान अवैध या अमान्य घोषित कर सकता है।
- यदि गवाह किसी निश्चित मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाता, तो न्यायालय उसके बयान के उस हिस्से को स्वीकार नहीं कर सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। न्यायालय का यह अधिकार है कि वह गवाह के बयान की पूरी या आंशिक विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के बाद ही उस पर निर्णय ले।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा गवाहों के बयान के सत्यापन में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करती है। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह गवाह के बयान के उन हिस्सों को स्वीकार करे जो उचित और विश्वसनीय हों और बाकी हिस्सों को अस्वीकृत कर दे।
- यह धारा गवाहों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता को भी उजागर करती है, ताकि न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचा जा सके।
उदाहरण:
- यदि एक गवाह कुछ घटनाओं के बारे में सही जानकारी देता है लेकिन कुछ तथ्यों में विरोधाभास करता है, तो न्यायालय उस गवाह के बयान के सिर्फ सत्य हिस्से को स्वीकार कर सकता है।
- अगर गवाह ने दबाव में आकर झूठ बोला है, तो उसके बयान के उन हिस्सों को अस्वीकृत किया जा सकता है, जिनमें उसने गलत जानकारी दी है।
यह धारा न्यायालय को स्वतंत्रता और विवेक प्रदान करती है ताकि वह साक्ष्य की सत्यता को पूरी तरह से जांच सके और उचित फैसले तक पहुंच सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 25
धारा 25: गवाहों का बयान रिकॉर्ड करना
- धारा 25 के अनुसार, न्यायालय में किसी भी गवाह का बयान कानूनी रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। यह बयान मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है, और इसे न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बयान के सही होने की पुष्टि करने के लिए न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि गवाह का बयान सही तरीके से और स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।
- गवाह के बयान को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते वह सत्य हो और कानूनी तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। न्यायालय गवाह का बयान प्रारंभिक रूप से लेकर समाप्ति तक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड करता है, जिससे किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव या झूठी जानकारी को दूर किया जा सके।
- गवाह के बयान को रिकॉर्ड करते समय, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि बयान ध्यानपूर्वक और संपूर्णता के साथ दर्ज हो। यदि गवाह का बयान किसी कारणवश कंट्रोल किया गया है या उसे किसी दबाव में दिया गया है, तो उस बयान को अदालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यदि गवाह का बयान साक्षात्कार के दौरान बदल जाता है या वह अपने पहले दिए बयान से पलट जाता है, तो अदालत उसे गवाह की गवाही में बदलाव के रूप में देखेगी और इस बदलाव को साक्ष्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसे साक्ष्य में विरोधाभास के रूप में लिया जाएगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा न्यायालय को गवाहों के बयान की विश्वसनीयता और सत्यता को सुनिश्चित करने का अधिकार देती है।
- गवाह का बयान कानूनी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और वह भविष्य में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हो सकता है।
उदाहरण:
- यदि किसी गवाह ने न्यायालय में बयान दिया और वह स्वतंत्र रूप से और सत्य के आधार पर दिया गया था, तो उसे साक्ष्य के रूप में मान्य किया जाएगा।
- यदि गवाह का बयान लिखित रूप में है और उसमें गलत जानकारी है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है और न्यायालय इसे मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम मान सकता है।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाह का बयान न्यायालय में सही और निष्पक्ष तरीके से दर्ज हो, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई गलतफहमी या दबाव न हो और सच्चाई का साक्षात्कार किया जा सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 26
धारा 26: गवाहों के बयान पर प्रश्न पूछने का अधिकार
- धारा 26 के अनुसार, न्यायालय में गवाहों के बयान पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायालय की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान होती है, ताकि गवाहों के बयानों की सत्यता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सके।
- गवाहों से प्रश्न पूछने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि गवाह को सही तरीके से और कानूनी तौर पर सवाल पूछे जाएं। प्रश्नों का उद्देश्य गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता को जांचना और सुनिश्चित करना होता है कि गवाह ने स्वतंत्र रूप से और सच्चाई के आधार पर बयान दिया है।
- इस धारा के तहत, न्यायालय को यह अधिकार है कि वह गवाह से किए गए प्रश्नों के संबंध में उचित निर्णय दे सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाहों के बयान में कोई विरोधाभास या भ्रम नहीं हो।
- यदि गवाह के बयान में संदेह उत्पन्न होता है या वह बयान देने में असमर्थ होता है, तो न्यायालय गवाह से अतिरिक्त प्रश्न पूछने का आदेश दे सकता है, ताकि उसकी गवाही को पूरी तरह से समझा जा सके।
- गवाह के बयान पर पूछे गए प्रश्नों में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ये प्रश्न गवाह से उसकी साक्ष्य को स्पष्ट करने, गवाह की सत्यनिष्ठा की जांच करने और बयानों के विरोधाभास को दूर करने के उद्देश्य से हो सकते हैं।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा न्यायालय को साक्ष्य के सत्यापन के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार देती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि गवाह द्वारा दिया गया बयान सत्य हो और विश्वसनीय हो।
- गवाह से किए गए प्रश्न कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और उनका उद्देश्य न्यायालय के सामने सत्य को प्रस्तुत करना होता है।
उदाहरण:
- यदि एक गवाह किसी अपराध के बारे में गवाही दे रहा है, और उसके बयान में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, तो न्यायालय गवाह से अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गवाह का बयान सत्य है।
- यदि गवाह अपनी गवाही में किसी विशेष तथ्य पर अस्पष्टता दिखाता है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है।
यह धारा न्यायिक प्रक्रिया को सत्य और निष्पक्ष बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से गवाहों के बयानों की सत्यता और विश्वसनीयता की पूरी जांच की जाती है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 27
धारा 27: गवाहों के बयान में विरोधाभास
- धारा 27 के अनुसार, यदि किसी गवाह के द्वारा दिए गए बयान में विरोधाभास या विपरीत जानकारी मिलती है, तो न्यायालय को इसे पूरी तरह से सत्यापित करना होगा। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गवाहों के बयान में दिए गए किसी भी प्रकार के विरोधाभास को सही तरीके से संबोधित किया जाए और मामले की सत्यता की जांच की जा सके।
- यदि गवाह का बयान पहले दिए गए बयानों के विपरीत या विरोधाभास के रूप में आता है, तो न्यायालय को गवाह से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है। गवाह से पूछा जा सकता है कि क्यों उसने पहले दिए गए बयान से अलग बात कही है, और उसे साक्ष्य के रूप में स्पष्ट करना पड़ सकता है।
- गवाह के बयान में विरोधाभास होने पर न्यायालय गवाह को दोबारा बयान देने का निर्देश दे सकता है ताकि विरोधाभास दूर किया जा सके। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि गवाह सच्चाई से न भटके और स्पष्टता से अपनी गवाही दे।
- विरोधाभास के कारण, अगर किसी गवाह का बयान पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाता है, तो न्यायालय उसे अस्वीकार भी कर सकता है और उस पर निर्णय में विचार नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सत्य और विश्वसनीय गवाहों की गवाही को साक्ष्य के रूप में लिया जाए।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि गवाह के बयान में विरोधाभास है, तो न्यायालय उसे सही रूप में पेश करने के लिए उसे सही तरीके से प्रश्न पूछे और गवाही की सत्यता की जांच करे।
- गवाह का बयान तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उस पर कोई स्पष्टता न हो और विरोधाभास दूर न किया जाए।
उदाहरण:
- यदि एक गवाह पहले कहता है कि उसने अपराध स्थल पर कुछ देखा था, लेकिन बाद में कहता है कि वह उस दिन वहां नहीं था, तो यह विरोधाभास होगा और न्यायालय गवाह से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
- यदि गवाह का बयान स्पष्ट नहीं होता है और उसमें विरोधाभास मिलता है, तो न्यायालय उसे अस्वीकार कर सकता है और गवाही पर विचार नहीं करेगा।
यह धारा गवाहों के बयान की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि केवल सच्चाई पर आधारित निर्णय लिए जा सकें।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 28
धारा 28: गवाहों के बयान में खंडन और पुष्टि
- धारा 28 के तहत, यदि कोई गवाह किसी पूर्व बयान से विरोध करता है या वह अपने बयान में विपरीत जानकारी देता है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह गवाह से खंडन और पुष्टि की प्रक्रिया के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट करें। इसका उद्देश्य गवाह के बयान की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करना है।
- जब गवाह का बयान किसी पिछले बयान के विपरीत होता है, तो न्यायालय गवाह से स्पष्ट रूप से पूछ सकता है कि वह अपना बयान क्यों बदल रहा है या क्यों वह पहले दिए गए बयान से असहमत हो रहा है। गवाह को इस विरोधाभास की पुष्टि करनी होती है और यह बताना होता है कि उसने अपना बयान क्यों बदला।
- खंडन और पुष्टि की प्रक्रिया के दौरान, यदि गवाह अपने बयान को सही ठहराने में असफल होता है या यदि उसके बयान में कोई विरोधाभास है, तो न्यायालय इस गवाह की गवाही को अस्वीकार कर सकता है और उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा।
- खंडन और पुष्टि के लिए न्यायालय गवाह को एक निश्चित समय सीमा दे सकता है, ताकि गवाह अपने बयान में किए गए किसी भी विपरीत कथन को स्पष्ट कर सके और उसे सिद्ध कर सके कि उसका बयान सत्य था या है।
स्पष्टीकरण:
- गवाह के बयानों में बदलाव या विपरीत बयान देने पर न्यायालय को खंडन और पुष्टि का अवसर देना आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाह ने सही बयान दिया है और कोई झूठ या गलतफहमी नहीं है।
- यदि गवाह के बयान में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान न्यायालय को उसे स्पष्ट करना होता है।
उदाहरण:
- यदि गवाह पहले कहता है कि उसने अपराध स्थल पर एक व्यक्ति को देखा, लेकिन बाद में वह कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा, तो न्यायालय उसे स्पष्ट करने का अवसर दे सकता है।
- यदि गवाह अपने बयान में बदलाव करता है और यह प्रतिवादी के पक्ष में विपरीत होता है, तो अदालत उसे स्पष्ट करने के लिए पूछेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसका बयान सही है या नहीं।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाह का बयान स्पष्ट और सत्य हो, ताकि न्यायालय साक्ष्य के आधार पर उचित निर्णय ले सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 29
धारा 29: गवाहों के बयान पर क्रॉस-प्रश्न का अधिकार
- धारा 29 के अनुसार, गवाहों के बयान पर क्रॉस-प्रश्न (cross-examination) पूछने का अधिकार प्रतिवादी या आरोपी पक्ष को दिया गया है। इसका उद्देश्य गवाह के बयान की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करना है।
- जब गवाह ने न्यायालय में अपना बयान दिया है, तो आरोपी पक्ष (या प्रतिवादी पक्ष) को उस गवाह से उसके बयान पर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। यह प्रक्रिया गवाह की साक्षात्कार के दौरान, उसकी साक्ष्य को परखने और उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए होती है।
- क्रॉस-प्रश्न के दौरान, गवाह से न्यायालय के सामने दिए गए बयान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है और यह पता किया जाता है कि गवाह का बयान सत्य और विश्वसनीय है या नहीं। गवाह से पूछे जाने वाले सवाल गवाह के बयान के विरोधाभास, स्पष्टता, और सत्यता को चुनौती देने के उद्देश्य से होते हैं।
- क्रॉस-प्रश्न के दौरान, प्रतिवादी पक्ष को सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन प्रश्नों का तरीका न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। प्रश्नों का उद्देश्य गवाह की सत्यनिष्ठा की जांच करना और गवाही में किसी प्रकार के विरोधाभास या गलतफहमी को उजागर करना होता है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाह के बयान पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रतिवादी पक्ष को दिया गया है, ताकि साक्ष्य को सही तरीके से परखा जा सके।
- क्रॉस-प्रश्न के दौरान, गवाह की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को जांचने की प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय को सच्चाई तक पहुंचने में सहायता मिलती है।
उदाहरण:
- यदि गवाह ने कहा कि उसने अपराध स्थल पर अपराधी को देखा था, तो प्रतिवादी पक्ष उसे क्रॉस-प्रश्न कर सकता है, जैसे, “क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप उसे ठीक से पहचान पा रहे थे?”
- यदि गवाह ने पहले अपने बयान में कोई विरोधाभास किया हो, तो प्रतिवादी पक्ष यह जानने के लिए गवाह से सवाल पूछ सकता है कि उसने क्यों अपना बयान बदला।
यह धारा गवाहों के बयानों की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को स्थापित करती है, ताकि न्यायालय साक्ष्य के आधार पर सही और निष्पक्ष निर्णय ले सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 30
धारा 30: गवाह के बयान पर पुनः-प्रश्न का अधिकार
- धारा 30 के अनुसार, गवाह के बयान के बाद, वकील को गवाह से पुनः-प्रश्न (Re-examination) पूछने का अधिकार होता है। पुनः-प्रश्न, गवाह से पहले के दिए गए बयान में किए गए स्पष्ट या निराकरण को सुधारने या स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
- पुनः-प्रश्न का उद्देश्य गवाह से किसी प्रकार की अस्पष्टता या विरोधाभास को दूर करना है, जो पहले की क्रॉस-प्रश्न के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। यह वकील द्वारा गवाह से फिर से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है, जिसमें गवाह से पहले दिए गए बयान को साफ किया जाता है और उसकी सत्यता और साक्ष्य को मजबूत किया जाता है।
- पुनः-प्रश्न में, गवाह से केवल उन प्रश्नों का जवाब लिया जा सकता है जो गवाह के क्रॉस-प्रश्न के दौरान उत्पन्न समस्याओं का समाधान करते हैं या जो बयान की सत्यता को स्पष्ट करते हैं। यह पुनः-प्रश्न क्रॉस-प्रश्न के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें वकील को गवाह की विश्वसनीयता को फिर से साबित करने का अवसर मिलता है।
- यह पुनः-प्रश्न केवल क्रॉस-प्रश्न के बाद किया जाता है, और इसका उद्देश्य गवाह से पूछे गए सवालों के संदर्भ में किसी भी स्पष्टता या अस्पष्टता को हल करना होता है।
स्पष्टीकरण:
- गवाह की सत्यता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पुनः-प्रश्न आवश्यक होता है, खासकर जब गवाह के बयान में अस्पष्टता हो या विरोधाभास हो।
- गवाह का पुनः-प्रश्न न्यायालय के सामने प्रस्तुत साक्ष्य को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने का एक तरीका होता है, जिससे न्यायालय को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है।
उदाहरण:
- यदि गवाह ने पहले कहा था कि उसने अपराधी को देखा था, लेकिन क्रॉस-प्रश्न में उस पर सवाल उठाए गए थे कि वह दृश्य अस्पष्ट था, तो पुनः-प्रश्न में वकील गवाह से स्पष्ट करवा सकता है कि उसने दृश्य को किस तरह से देखा था और क्या वह सही पहचान कर रहा था।
- यदि गवाह के बयान में कोई विरोधाभास उत्पन्न हुआ हो, तो पुनः-प्रश्न द्वारा गवाह से उस विरोधाभास को साफ करने का प्रयास किया जाता है।
यह धारा गवाह के बयान की सत्यता और स्पष्टता को बनाए रखने में मदद करती है, ताकि न्यायालय को सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में कोई बाधा न हो।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 31
धारा 31: गवाह की संदेहास्पद या झूठी गवाही पर दंड
- धारा 31 के अनुसार, यदि कोई गवाह जानबूझकर झूठी गवाही देता है या साक्ष्य में छेड़छाड़ करता है, तो उसे कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। गवाहों का कर्तव्य होता है कि वे न्यायालय के सामने सत्य बोलें, और यदि वे झूठी गवाही देते हैं, तो यह अपराध माना जाएगा।
- यह धारा इस बात की पुष्टि करती है कि यदि गवाह का बयान जानबूझकर गलत या झूठा पाया जाता है, तो वह गवाह दंडनीय होगा। इस धारा का उद्देश्य गवाहों को सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना और न्यायालय में झूठी गवाही देने के खतरों से अवगत कराना है।
- यदि गवाह ने झूठी गवाही दी है और यह साबित हो जाता है कि गवाह का बयान जानबूझकर झूठा था, तो गवाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है और उसे दंड या सजा दी जा सकती है।
- यह धारा गवाहों के सत्य बोलने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि अदालत में गलतफहमी या अन्याय न हो और सच्चाई सामने आ सके। झूठी गवाही देने वाले गवाह को सजा देने का उद्देश्य न्यायालय के साक्ष्य के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करना है।
स्पष्टीकरण:
- गवाह का कर्तव्य है कि वह अदालत में अपने बयान में सत्य का पालन करे और कोई भी झूठी जानकारी न दे।
- यदि गवाह जानबूझकर झूठी गवाही देता है या साक्ष्य में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है, तो उसे दंडनीय ठहराया जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप उसे सजा मिल सकती है।
उदाहरण:
- यदि गवाह जानबूझकर झूठा बयान देता है कि उसने किसी अपराध को होते हुए देखा था, जबकि उसने सच में ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो उस गवाह पर धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- अगर गवाह ने साक्ष्य को तोड़-मरोड़कर पेश किया, तो इसे भी झूठी गवाही माना जा सकता है, और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यह धारा न्यायालय के सामने सत्यता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, ताकि गवाहों द्वारा दिया गया बयान सच्चा और विश्वसनीय हो।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 32
धारा 32: मृतक के बयानों को स्वीकार करना (Dying Declarations)
- धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मृतक के बयानों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से संबंधित है। इस धारा के तहत, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व उसने कोई बयान दिया हो, जो उसके मृत्यु के कारण या मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण हो, तो वह बयान साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि यह बयान सच्चा हो।
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट है और उसने अपने आखिरी क्षणों में किसी घटनाक्रम या अपराध के बारे में बयान दिया है, तो वह बयान स्वीकृत हो सकता है और न्यायालय में गवाही के रूप में पेश किया जा सकता है।
- मृतक का बयान तब ही साक्ष्य माना जाता है जब वह मृत्यु के निकट या मृत्यु के बाद की स्थितियों में दिया गया हो, और उसका उद्देश्य मृत्यु के कारणों या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करना हो। यह मृतक के बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि मृतक के पास झूठ बोलने का कोई उद्देश्य नहीं था और वह अंतिम समय में सच बोलने की प्रवृत्ति रखता था।
- मृतक का बयान तब तक स्वीकृत किया जा सकता है जब तक कि वह आत्महत्या या मृत्यु के कारणों से संबंधित न हो, अर्थात यदि बयान किसी अपराध के बारे में हो, तो इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण:
- मृतक के बयान को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह बयान मृत्यु के निकट दिया गया हो और वह मृत्यु के कारणों या उस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो।
- यह प्रावधान साक्ष्य की वैधता को सुनिश्चित करता है और यह न्यायालय को मदद करता है, खासकर जब अन्य गवाह नहीं होते या मृतक ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी हो।
उदाहरण:
- यदि किसी व्यक्ति ने अपने मरने से पहले बयान दिया कि उसे किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी और वह अब मरने जा रहा है, तो यह बयान मृतक का बयान माना जाएगा और इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यदि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो और मरने से पहले किसी अपराध के बारे में बयान दे, तो वह बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि वह बयान मृत्यु के कारण या आत्महत्या से जुड़ा हो।
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बयान देता है, तो उसे अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह न्याय में सहायक होता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 33
धारा 33: प्रत्यक्ष गवाह के बयान को स्वीकार करने का अधिकार (Admissibility of Statements of Persons Who Cannot Be Cross-examined)
- धारा 33 के तहत, अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं है (यानी वह जीवित नहीं है, या वह किसी कारणवश न्यायालय में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता), तो उस व्यक्ति का पहले दिया गया बयान गवाही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई गवाह न्यायालय में नहीं आ सकता, तो उसके पहले दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए।
- इस धारा के तहत, गवाह की गवाही को पहले ही किसी अन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि जब गवाह मृत हो गया हो या वह किसी कारणवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। हालांकि, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि गवाह का बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए जब वह पहले किसी अन्य जगह या समय में दिया गया हो।
- यह धारा उन गवाहों के बयानों को स्वीकार करती है, जो क्रॉस-प्रश्न से बचने के कारण गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। यह तब होता है जब गवाह या तो मृत हो, बीमार हो, या अन्य कारणों से अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में, गवाह के पहले के बयान को अदालत द्वारा साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि गवाह की गवाही किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होने पर भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सके।
- गवाह का बयान पहले किसी अन्य समय या स्थान पर लिया गया हो, और अब वह गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
उदाहरण:
- यदि एक गवाह किसी घटना के बारे में पहले पुलिस स्टेशन में बयान देता है, लेकिन बाद में वह बीमार हो जाता है और न्यायालय में गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता, तो उसके पहले के बयान को धारा 33 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- अगर किसी गवाह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था, लेकिन बाद में वह मृत हो गया, तो उसके बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि उस बयान का न्यायालय में प्रयोग किया जा सके।
यह धारा गवाहों की अनुपस्थिति के बावजूद साक्ष्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है, जिससे न्यायालय में सच्चाई और न्याय के साथ निर्णय लिया जा सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 34
धारा 34: एकाधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध का साझा इरादा (Common Intention of Several Persons)
- धारा 34 का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि जब एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को साझा इरादे से करते हैं, तो उन व्यक्तियों को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके तहत यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ मिलकर एक अपराध करता है, और सभी का इरादा उस अपराध को करने का था, तो उन सभी को समान रूप से दंडित किया जा सकता है।
- साझा इरादा का तात्पर्य है कि सभी अपराधी किसी अपराध को पूर्व नियोजित तरीके से करते हैं, और उनका उद्देश्य वही होता है। जैसे कि हत्या, लूट, या अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में अगर अपराधियों का इरादा एक साथ मिलकर अपराध करने का था, तो वे सभी उस अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे।
- धारा 34 के तहत, यदि किसी अपराध को करने का इरादा साझा था, तो उस अपराध के लिए सभी अपराधियों को एक समान जिम्मेदार माना जाएगा, चाहे किसी एक व्यक्ति ने उस अपराध को अंजाम दिया हो। इसका मतलब यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया, तो बाकी सभी को साझा इरादा होने के कारण उसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।
- इस धारा का मुख्य उद्देश्य सामूहिक अपराधों को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी अपराधियों को उनके द्वारा किए गए साझा अपराध के लिए समान दंड मिले।
स्पष्टीकरण:
- जब एक से अधिक व्यक्तियों का साझा इरादा होता है और वे किसी अपराध को मिलकर करते हैं, तो उन सभी को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।
- यह धारा विशेष रूप से गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, अपहरण आदि के मामलों में लागू होती है, जहां अपराधियों का उद्देश्य एक जैसा होता है।
उदाहरण:
- यदि तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करने का इरादा रखते हैं और उस इरादे के तहत हत्या कर देते हैं, तो धारा 34 के तहत सभी तीनों व्यक्तियों को समान रूप से दंडित किया जा सकता है, भले ही किसी एक व्यक्ति ने हत्या को अंजाम दिया हो।
- यदि दो व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं, और दोनों का इरादा लूट करने का था, तो दोनों को लूट के लिए समान जिम्मेदारी के तहत दंडित किया जा सकता है।
यह धारा इस बात की पुष्टि करती है कि साझा इरादा से किया गया अपराध, जहां सभी अपराधियों का उद्देश्य एक जैसा था, उन सभी को समान रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए एक कानूनी आधार देती है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 35
धारा 35: अपराध के किए जाने के लिए मानसिक स्थिति का अनुमान (Presumption of Mental State for Committing Offense)
- धारा 35 के तहत, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी होता है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध के दौरान उस व्यक्ति का मानसिक स्थिति अपराध करने के लिए संचालित था। इसका मतलब यह है कि न्यायालय उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकता है, खासकर जब कोई व्यक्ति अपने कृत्य के परिणामस्वरूप अपराध करता है।
- इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी व्यक्ति के अपराध करने के इरादे और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो यह माना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपराध सचेत रूप से और आत्मनिर्भर रूप से किया था।
- उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जाता है और यह साबित किया जाता है कि उसने अपराध के दौरान मानसिक रूप से सुसंगत और निर्धारित स्थिति में अपराध किया था, तो धारा 35 के तहत उसकी मानसिक स्थिति को एक निर्णायक पहलू माना जा सकता है।
- धारा 35 इस बात का अनुमान करने की अनुमति देती है कि एक व्यक्ति ने जब अपराध किया था, तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति आधिकारिक रूप से मान्य और अपराध करने की क्षमता रखने योग्य थी।
स्पष्टीकरण:
- मानसिक स्थिति के आधार पर अपराधी की कुशलता और नियंत्रण क्षमता को न्यायालय संदेह से बाहर साबित कर सकता है।
- यह धारा अपराध करने के मानसिक पहलू को समझने और उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।
उदाहरण:
- यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है और यह साबित हो जाता है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह से सजग था और उसे अपने कृत्य के परिणामों का ज्ञान था, तो न्यायालय उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अनुमान कर सकता है और उसे दंडित कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति ने अपराध करते वक्त मानसिक स्थिति में अस्थिरता का प्रदर्शन किया, तो न्यायालय उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे मुक्ति दे सकता है या कम सजा दे सकता है।
यह धारा अपराधों के दौरान मानसिक स्थिति और इरादे को सही ढंग से समझने में सहायक होती है, जिससे न्यायालय को अपराधी के व्यक्तिगत या मानसिक पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिलता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 36
धारा 36: अपराध के दौरान व्यक्ति की नीयत और व्यवहार का अनुमान (Presumption of Intent and Conduct During the Commission of an Offense)
- धारा 36 के तहत, यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि उस व्यक्ति का इरादा और व्यवहार उस अपराध को अंजाम देने के समय अपराध के लिए पूर्वनिर्धारित था। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध को किया है, तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि अपराध करने का उसका इरादा और व्यवहार उसी अपराध को करने के लिए पहले से तय था।
- इस धारा का उद्देश्य यह है कि जब कोई अपराधी किसी अपराध को पूर्वविवेक और पूर्वनिर्धारित तरीके से करता है, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसका व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। न्यायालय यह भी अनुमान कर सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसी प्रकार था जैसे उस अपराध को करने का इरादा पहले से बना हो।
- उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हत्या करने के इरादे से किसी व्यक्ति को गोली मारता है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि उसकी नीयत और व्यवहार पहले से हत्या करने के उद्देश्य से थे।
स्पष्टीकरण:
- धारा 36 में यह बताया जाता है कि अपराध करने के समय आरोपी का इरादा और व्यवहार क्या था, इसे अनुमान के रूप में देखा जा सकता है।
- यह धारा उस समय के मानसिक स्थिति और क्रियाओं के आधार पर न्यायालय को निर्णय लेने का अधिकार देती है, विशेषकर जब गवाहों के बयान या परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होतीं।
उदाहरण:
- अगर किसी व्यक्ति ने लूट करने के लिए पहले से योजना बनाई थी, तो न्यायालय यह मान सकता है कि उस व्यक्ति का इरादा और व्यवहार लूट के अपराध को अंजाम देने के लिए पूर्वनिर्धारित था, भले ही उसने लूट के समय किसी विशेष व्यक्ति से कोई संवाद नहीं किया हो।
- अगर किसी व्यक्ति ने हत्या के लिए हथियार एकत्र किया और एक निर्दिष्ट स्थान पर जाकर हत्या की, तो न्यायालय यह मान सकता है कि उस व्यक्ति की नीयत और व्यवहार पहले से हत्या को अंजाम देने के लिए निर्धारित थे।
इस प्रकार, धारा 36 अपराधी के इरादे और व्यवहार का अनुमान करने का अवसर प्रदान करती है, ताकि अपराध के दौरान उसके उद्देश्य और मानसिक स्थिति को समान रूप से समझा जा सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 37
धारा 37: जब एक से अधिक व्यक्ति समान अपराध करते हैं, लेकिन विभिन्न उद्देश्यों से (Acts Done by Several Persons in Furtherance of Common Objective)
- धारा 37 यह प्रावधान करती है कि यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध को अंजाम देते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य भिन्न होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने उद्देश्य के अनुसार अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहां एक अपराध में कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से हर व्यक्ति का उद्देश्य या भूमिका अलग होती है।
स्पष्टीकरण:
- यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी मंशा या उद्देश्य अलग-अलग होते हैं, तो हर व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार दंड दिया जाएगा।
- इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अपराधी समान रूप से दोषी होंगे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी और मंशा को देखकर सजा दी जाएगी।
उदाहरण:
- यदि तीन लोग मिलकर डकैती करते हैं, लेकिन उनमें से एक का उद्देश्य केवल चोरी करना था, जबकि दूसरे ने हिंसा का सहारा लिया और तीसरे ने केवल मार्गदर्शन किया—तो तीनों की सजा अलग-अलग हो सकती है।
- यदि दो लोग मिलकर हत्या करते हैं, लेकिन एक का इरादा केवल घायल करने का था और दूसरे का इरादा जान लेने का था, तो दोनों को अलग-अलग दंड दिया जा सकता है।
महत्व:
- यह धारा सुनिश्चित करती है कि हर अपराधी को उसके वास्तविक कृत्य और उद्देश्य के आधार पर दंड मिले, न कि केवल इस आधार पर कि वह अपराध में शामिल था।
- यह उन मामलों में मददगार होती है, जहां अपराध सामूहिक रूप से किया गया, लेकिन सभी की भूमिका भिन्न थी।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 38
धारा 38: जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध करते हैं, लेकिन उनकी दोषिता की डिग्री भिन्न होती है (Persons Concerned in Criminal Act May be Guilty of Different Offences)
- धारा 38 यह प्रावधान करती है कि जब एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि सभी को एक ही अपराध के लिए समान रूप से दोषी ठहराया जाए।
- यदि किसी अपराध में अलग-अलग व्यक्तियों की भूमिका और इरादा अलग-अलग था, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी दोषिता की डिग्री के अनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहां एक ही घटना में कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से हर व्यक्ति ने अलग-अलग प्रकार की आपराधिक भूमिका निभाई होती है।
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से दंडित करने के बजाय, उनके कृत्यों के अनुसार दंड दिया जाए।
उदाहरण:
- तीन लोग मिलकर एक घर में चोरी करने जाते हैं।
- पहला व्यक्ति घर में प्रवेश करता है और चोरी करता है।
- दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा होकर निगरानी करता है।
- तीसरा व्यक्ति भागने के लिए वाहन लेकर तैयार रहता है।
→ तीनों अपराध में शामिल हैं, लेकिन उनकी दोषिता की डिग्री अलग है, इसलिए उनकी सजा भी अलग-अलग हो सकती है।
- किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए दो लोग हमला करते हैं।
- पहला व्यक्ति केवल घायल करना चाहता था, लेकिन दूसरे ने जान लेने के लिए वार किया।
→ पहला व्यक्ति गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हत्या का दोषी हो सकता है।
- पहला व्यक्ति केवल घायल करना चाहता था, लेकिन दूसरे ने जान लेने के लिए वार किया।
महत्व:
- यह धारा न्याय प्रणाली में उचितता और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर व्यक्ति को उसके वास्तविक अपराध के अनुसार सजा मिले, न कि केवल इस आधार पर कि वह अपराध में शामिल था।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 39
धारा 39: स्वेच्छा से किया गया कार्य (Voluntary Act)
- इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से (voluntarily) कोई कार्य करता है, जो कानून द्वारा अपराध माना गया है, तो वह उत्तरदायी होगा।
- यहाँ “स्वेच्छा से” का अर्थ यह है कि कार्य जानबूझकर, बिना किसी जबरदस्ती या बाहरी दबाव के किया गया हो।
- यदि कोई कार्य गलती से, भूलवश, या किसी मजबूरी में किया गया हो, तो वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा।
स्पष्टीकरण:
- इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को तभी अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए, जब उसने वह कार्य जानबूझकर और स्वतंत्र इच्छा से किया हो।
- यदि किसी व्यक्ति से कोई आपराधिक कृत्य अजाने में, दुर्घटनावश, या किसी के दबाव में हुआ है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा।
उदाहरण:
- स्वेच्छा से किया गया अपराध
- यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर मारता है, तो वह हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा।
- यदि कोई व्यक्ति किसी का पर्स छीनकर भागता है, तो वह चोरी का दोषी होगा।
- ग़लती से किया गया कार्य (जो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा)
- यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी को धक्का दे देता है और वह गिरकर घायल हो जाता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में किसी को चोट पहुँचा देता है, तो यह स्वेच्छा से किया गया कार्य नहीं माना जाएगा।
महत्व:
- यह धारा सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जाए, जब उसने अपराध को जानबूझकर किया हो।
- इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अपराध और दुर्घटना में अंतर होता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 40
धारा 40: अपराध की परिभाषा (Definition of Offence)
- इस धारा के तहत, “अपराध” (Offence) उस किसी भी कार्य या चूक (किसी आवश्यक कार्य को न करना) को कहा जाता है,
- जिसे भारतीय न्याय संहिता या किसी अन्य प्रचलित कानून द्वारा दंडनीय घोषित किया गया हो।
- अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं:
- सक्रिय अपराध (Commission of Offence) – जब कोई व्यक्ति अवैध कार्य करता है।
- निष्क्रिय अपराध (Omission of Duty) – जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से आवश्यक कार्य करने में असफल रहता है।
स्पष्टीकरण:
- इस धारा में यह परिभाषित किया गया है कि अपराध केवल वह कार्य नहीं है, जो कानून के विरुद्ध किया जाता है, बल्कि वह चूक भी अपराध हो सकती है, जहां कोई व्यक्ति अपने कानूनी दायित्व को पूरा नहीं करता।
- यह धारा अपराध की व्यापक परिभाषा को स्पष्ट करती है, ताकि कोई भी अवैध कार्य या कानूनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास अपराधी न कर सके।
उदाहरण:
- सक्रिय अपराध (Active Crime)
- हत्या करना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, बलात्कार करना आदि।
- कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से घायल करता है – यह एक अपराध है।
- निष्क्रिय अपराध (Omission as Crime)
- किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना।
- माता-पिता का अपने छोटे बच्चे को भोजन या आवश्यक देखभाल न देना।
- कोई व्यक्ति, जो कानूनन बचाव के लिए बाध्य है, किन्तु वह बचाने में असफल रहता है।
महत्व:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध केवल करने से ही नहीं बनता, बल्कि कानूनी दायित्व न निभाने से भी कोई व्यक्ति दोषी हो सकता है।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून की नजर में कार्य और चूक दोनों ही अपराध हो सकते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 41
धारा 41: विशेष विधियों के अंतर्गत अपराध (Offence under Special Laws)
- इस धारा के अनुसार, यदि कोई कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अलावा किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसे भी “अपराध” (Offence) माना जाएगा।
- यह धारा यह स्पष्ट करती है कि अपराध केवल भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही नहीं होते, बल्कि अन्य विशेष कानूनों के तहत भी कोई कार्य अपराध हो सकता है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा विभिन्न विशेष कानूनों को मान्यता देती है, जो भारतीय न्याय संहिता से अलग होते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में अपराधों को नियंत्रित करते हैं।
- यदि कोई कार्य विशेष विधियों (Special Laws) या स्थानीय कानूनों (Local Laws) के तहत अपराध घोषित किया गया है, तो वह व्यक्ति उन कानूनों के तहत दंडनीय होगा।
उदाहरण:
- विशेष कानूनों के तहत अपराध
- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act, 1985) के तहत मादक पदार्थों की तस्करी।
- प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत रिश्वत लेना।
- आईटी एक्ट, 2000 के तहत साइबर अपराध।
- पॉक्सो एक्ट, 2012 के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध।
- स्थानीय कानूनों के तहत अपराध
- किसी राज्य के अवैध खनन कानून का उल्लंघन।
- नगर निगम द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन, जो दंडनीय हो सकता है।
महत्व:
- यह धारा सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति यह तर्क देकर नहीं बच सकता कि उसका कृत्य भारतीय न्याय संहिता में उल्लिखित नहीं है, यदि वह किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह विभिन्न विषय-विशेष कानूनों को न्यायिक प्रक्रिया में एकीकृत करता है और अपराधों की परिभाषा को व्यापक बनाता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 42
धारा 42: किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा (Punishment of Offence under Multiple Laws)
- यदि किसी कार्य (अपराध) के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 और किसी अन्य विशेष या स्थानीय कानून दोनों में सजा का प्रावधान है, तो अपराधी को केवल एक ही सजा मिलेगी।
- अपराधी को वह सजा दी जाएगी, जो अधिकतम या अधिक उपयुक्त हो, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जाएगी।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित न किया जाए।
- यदि कोई अपराध भारतीय न्याय संहिता और किसी अन्य कानून, जैसे कि विशेष या स्थानीय विधियों के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, तो अभियुक्त को दोनों कानूनों के तहत अलग-अलग दंड नहीं दिया जाएगा।
उदाहरण:
- रिश्वतखोरी का मामला
- यदि कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत लेता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 दोनों के तहत अपराध होगा।
- लेकिन उसे एक ही कानून के तहत सजा मिलेगी, जो अधिक उपयुक्त होगी।
- साइबर अपराध और धोखाधड़ी
- यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) दोनों के तहत अपराध हो सकता है।
- लेकिन उसे एक ही कानून के तहत सजा दी जाएगी, ताकि उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित न किया जाए।
महत्व:
- यह धारा न्याय की निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है ताकि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार-बार दंडित न किया जाए।
- इससे यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को यह तय करना होगा कि अधिकतम या उचित दंड कौन सा होगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 43
धारा 43: विधि द्वारा प्राधिकृत कार्य (Acts Authorized by Law)
- यदि कोई कार्य कानून द्वारा अधिकृत (authorized by law) है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।
- यह धारा उन व्यक्तियों की रक्षा करती है जो कानून के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, भले ही उनके कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को हानि हो।
- यदि कोई व्यक्ति कानून के प्रावधानों के भीतर रहकर कोई कार्य करता है, तो वह आपराधिक दायित्व से मुक्त रहेगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपराधी नहीं ठहराया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सरकारी आदेशों, कानूनी प्रक्रियाओं, या अन्य वैध अधिकारों के तहत कार्य करता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
उदाहरण:
- पुलिस द्वारा की गई गिरफ़्तारी
- यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध अपराधी को कानून के तहत गिरफ़्तार करता है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा।
- लेकिन यदि पुलिस अधिकारी बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करता है, तो यह अवैध होगा।
- न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय
- यदि कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित करता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।
- डॉक्टर द्वारा सर्जरी
- यदि कोई डॉक्टर कानून के अनुसार मरीज की सर्जरी करता है और उसमें जटिलताओं के कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो यह अपराध नहीं होगा।
- लेकिन यदि डॉक्टर लापरवाही से इलाज करता है, तो यह अपराध हो सकता है।
महत्व:
- यह धारा उन व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति वैध कर्तव्यों का पालन करते हुए झूठे मुकदमों में न फंसे।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 44
धारा 44: आकस्मिक कारणों से होने वाली हानि (Accident in Doing a Lawful Act)
- यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से स्वीकृत कार्य (lawful act) करता है और आकस्मिक रूप से (accidentally) कोई क्षति (harm) हो जाती है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।
- इस धारा के अंतर्गत यह आवश्यक है कि व्यक्ति की मंशा (intention) या लापरवाही (negligence) से हानि न हुई हो।
स्पष्टीकरण:
- यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा था और किसी अन्य को बिना किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य या लापरवाही के नुकसान होता है, तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा।
- यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहाँ कोई दुर्घटना सावधानीपूर्वक किए गए कार्य के दौरान घटित होती है।
उदाहरण:
- यातायात दुर्घटना
- यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चला रहा है, लेकिन अचानक किसी पैदल यात्री को टक्कर लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा यदि चालक की कोई लापरवाही साबित नहीं होती।
- खेल के दौरान चोट लगना
- क्रिकेट के खेल में यदि एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है और गलती से दूसरे खिलाड़ी को गंभीर चोट लग जाती है, तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह एक वैध खेल गतिविधि के दौरान हुआ।
- निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना
- यदि एक निर्माण कार्य के दौरान कोई मज़दूर सावधानी बरतते हुए कार्य कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा।
महत्व:
- यह धारा उन व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जो बिना किसी दुर्भावना के कानूनी कार्य कर रहे थे और किसी अनहोनी के कारण हानि हो गई।
- इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि गलती से हुई दुर्घटनाओं को जानबूझकर किए गए अपराधों से अलग किया जाए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 45
धारा 45: अपरिहार्य परिस्थितियों में किया गया कार्य (Act Done Under Compulsion or Necessity)
- यदि कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने या किसी अन्य की जान बचाने के लिए बिना किसी आपराधिक इरादे (criminal intent) के कोई कार्य करता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।
- यह धारा आवश्यकता (necessity) के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति को परिस्थितियों की मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है।
स्पष्टीकरण:
- यदि कोई कार्य अपने या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए किया जाता है, और उसमें अपराध करने की मंशा नहीं होती, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
- लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब कोई अन्य विकल्प मौजूद न हो और कार्य को करने की मजबूरी हो।
उदाहरण:
- भूख से बचने के लिए चोरी
- यदि कोई व्यक्ति तीव्र भूख के कारण भोजन चुराता है, तो न्यायालय यह देख सकता है कि यह कार्य अत्यधिक आवश्यकता के कारण हुआ था या आपराधिक मंशा से।
- आत्मरक्षा में हमला
- यदि कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी हमलावर पर हमला करता है और उसे गंभीर चोट लग जाती है, तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह आत्मरक्षा के तहत किया गया था।
- बाढ़ में बचाव कार्य
- यदि कोई व्यक्ति किसी को बचाने के लिए जबरन किसी की नाव लेता है और उसे उस परिस्थिति में ऐसा करना अनिवार्य था, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा।
महत्व:
- यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहाँ व्यक्ति ने बिना किसी आपराधिक मंशा के परिस्थिति की मजबूरी में कार्य किया हो।
- यह न्याय की निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है ताकि कोई व्यक्ति अत्यधिक आपातकालीन स्थिति में भी कानूनी संरक्षण पा सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 46
धारा 46: शिशु की आपराधिक दायित्व से मुक्ति (Act of a Child is Not an Offence)
- यदि कोई सात वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई ऐसा कार्य करता है, जो सामान्य परिस्थितियों में अपराध होता, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।
- इस धारा के तहत, ऐसा माना जाता है कि सात वर्ष से कम उम्र का बच्चा सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझ सकता, इसलिए वह आपराधिक उत्तरदायित्व (criminal liability) से मुक्त रहेगा।
स्पष्टीकरण:
- इस धारा का आधार यह है कि बच्चों में अपराध करने की मंशा (mens rea) नहीं होती।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 82 के समान, यह भी बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
- सात वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए अगली धाराओं में प्रावधान दिया गया है।
उदाहरण:
- खिलौने की दुकान से चोरी
- यदि कोई छह साल का बच्चा किसी दुकान से खिलौना चुरा लेता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसकी मंशा अपराध करने की नहीं थी।
- बच्चे द्वारा गलती से नुकसान पहुँचाना
- यदि एक पाँच वर्षीय बच्चा खेल-खेल में किसी की खिड़की का कांच तोड़ देता है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा।
महत्व:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि छोटे बच्चों को अपराधी घोषित न किया जाए।
- यह न्याय प्रणाली को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, ताकि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47
धारा 47: मानसिक विकार वाले व्यक्ति की आपराधिक दायित्व से मुक्ति (Mental Disorder and Criminal Liability)
- यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकार (mental disorder) का शिकार है और उस कारण वह अपने कार्यों के परिणामों को समझने में असमर्थ है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
- मानसिक विकार के कारण यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवहार नियंत्रित नहीं कर पाता, तो उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा उन व्यक्तियों के लिए है जिनमें मानसिक विकार के कारण वे अपने कार्यों के परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं।
- मानसिक विकार को चिकित्सा दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है, और केवल चिकित्सकीय प्रमाण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों को समझ सकता था या नहीं।
उदाहरण:
- मानसिक रोगी द्वारा हमला
- यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकार का शिकार होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, लेकिन उस समय वह सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझ पा रहा था, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
- मानसिक रोगी द्वारा संपत्ति का नुकसान
- यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकार के कारण अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
महत्व:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मानसिक विकार वाले व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी स्थिति यह न बताती हो कि वे अपने कार्यों के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं थे।
- यह मानवीय दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है, ताकि मानसिक विकार वाले व्यक्तियों को दंडित करने के बजाय उन्हें इलाज और सहायता प्रदान की जाए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 48
धारा 48: अपराधी द्वारा झूठे बयान का संज्ञान (False Statements by the Accused)
- यदि आरोपी (accused) अपने बयान में झूठ बोलता है और ऐसा करना उसे अपराध का दोषी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो अदालत उस बयान को संज्ञान में नहीं लेगी।
- इस धारा के तहत, यदि आरोपी ने जानबूझकर गलत बयान दिया, तो वह अदालत की प्रक्रिया को धोखा देने के लिए जिम्मेदार होगा।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा उन मामलों में लागू होती है जब आरोपी किसी अपराध से बचने के लिए झूठ बोलता है और अदालत को धोखा देने की कोशिश करता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी आरोपी के झूठे बयान को सिद्ध प्रमाण (evidence) के रूप में स्वीकार न किया जाए।
उदाहरण:
- चोरी के आरोपी का झूठा बयान
- यदि एक व्यक्ति चोरी के मामले में आरोपित है और वह झूठा बयान देता है कि वह घटना के समय घर पर नहीं था, जबकि जांच से यह पता चलता है कि वह वहाँ था, तो उसके बयान को अदालत में मान्यता नहीं दी जाएगी।
- मर्डर के आरोपी का झूठा बयान
- यदि आरोपी हत्या के मामले में अपने बयान में झूठा दावा करता है कि उसने हत्या नहीं की, जबकि सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
महत्व:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अदालत में किसी भी झूठे बयान को स्वीकार न किया जाए और सत्य को प्राथमिकता दी जाए।
- यह आरोपी को यह चेतावनी भी देती है कि झूठ बोलने से अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे उसके खिलाफ और अधिक गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 49
धारा 49: अपराधी द्वारा दी गई सजा का उल्लंघन (Violation of Punishment by the Accused)
- यदि कोई अपराधी (accused) अदालत द्वारा निर्धारित सजा (punishment) का पालन करने से इंकार करता है, या अदालत के आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा दंडित किया जाएगा।
- इस धारा के अंतर्गत, अपराधी द्वारा सजा का उल्लंघन करने पर उसे अपराधी मानते हुए सजा में वृद्धि की जा सकती है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा अदालत के आदेशों का पालन न करने पर लागू होती है। यदि अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है और वह व्यक्ति उस सजा का पालन नहीं करता, तो अदालत उसे कानूनी दंड दे सकती है।
- यह किसी प्रकार के संविधानिक उल्लंघन या अदालत के आदेश की अवमानना के रूप में देखा जा सकता है।
उदाहरण:
- सजा की अवज्ञा
- यदि अदालत ने एक आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है और वह जानबूझकर उस आदेश का पालन नहीं करता, तो अदालत उसे अधिक कठोर सजा दे सकती है।
- सजा को बदलने से मना करना
- यदि कोई व्यक्ति अदालत द्वारा निर्धारित समाज सेवा की सजा को नहीं करता और इसका उल्लंघन करता है, तो वह अधिक सजा का पात्र हो सकता है।
महत्व:
- यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अदालत के आदेशों की अवमानना करने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाए।
- यह न्यायिक प्रक्रिया की साक्षमता और अधिकारिता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि अदालत के आदेशों का उल्लंघन न हो और न्याय की प्रक्रिया सुचारु रूप से चले।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 50
धारा 50: अपराधी की गिरफ्तार और जमानत के अधिकार (Arrest and Bail Rights of the Accused)
- अरेस्ट के समय जानकारी देना
यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे तुरंत यह जानकारी दी जाएगी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या आरोप उस पर लगाए गए हैं। - जमानत का अधिकार
गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसे अपने जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, अगर उसे कानूनी तौर पर जमानत मिलने का हक हो। - समान अवसर
आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के समय यह स्पष्ट जानकारी दी जाएगी कि उसे कब और कैसे जमानत मिल सकती है।
स्पष्टीकरण:
- यह धारा व्यक्ति के संविधानिक अधिकारों की रक्षा करती है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना उचित प्रक्रिया के अवैध तरीके से गिरफ्तार न किया जाए।
- गिरफ्तारी और जमानत के नियम सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- गिरफ्तारी के दौरान आरोपों की स्पष्टता और जमानत का अवसर व्यक्ति के समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
उदाहरण:
- गिरफ्तारी के समय जानकारी देना
यदि पुलिस किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करती है, तो उन्हें तुरंत यह जानकारी देनी होगी कि यह आरोप उस पर लगाए गए हैं। साथ ही उसे यह बताया जाएगा कि गिरफ्तार होने के बावजूद, वह जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन कर सकता है, यदि उसके पास उचित कारण हैं। - जमानत का आवेदन
एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद यह अधिकार मिलेगा कि वह जमानत का आवेदन कर सके, बशर्ते वह इस अपराध के लिए जमानत योग्य हो।
महत्व:
- यह धारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
- यह गिरफ्तारी के दौरान पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, ताकि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों से वंचित न हो।