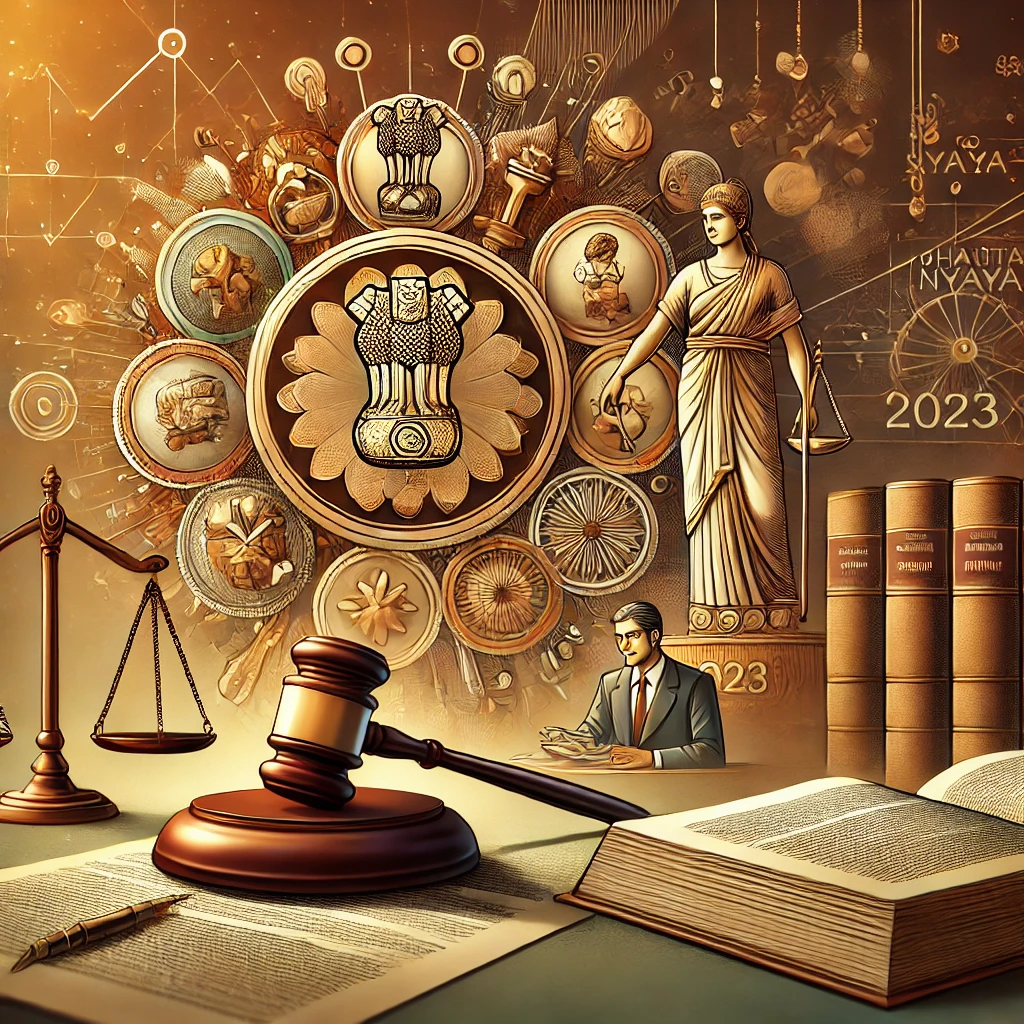“भारतीय न्याय संहिता की धारा 60: अपराध की योजना छिपाना और दायित्व की कानूनी सीमा”
🔷 प्रस्तावना (Introduction):
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में अनेक ऐसी धाराएँ हैं जो न केवल अपराध करने वाले व्यक्ति को, बल्कि अपराध को जानबूझकर छिपाने वाले को भी उत्तरदायी ठहराती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण धारा है — धारा 60, जो स्पष्ट रूप से यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध की जानकारी रखता है, जिसकी सज़ा केवल कारावास है, और फिर भी वह जानबूझकर उसे छिपाता है या पुलिस को गलत सूचना देता है, तो वह भी अपराध में भागीदार माना जाएगा और सज़ा का भागी बन सकता है।
🔷 धारा 60 का आशय (Meaning of Section 60):
धारा 60 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति:
- किसी अपराध की योजना के बारे में पहले से जानता है;
- लेकिन जानबूझकर उस जानकारी को छुपाता है;
- या पुलिस या प्रशासन को भ्रमित करने के लिए झूठी जानकारी देता है,
तो ऐसे व्यक्ति को भी सज़ा का भागीदार माना जाता है — भले ही उसने स्वयं अपराध नहीं किया हो।
🔷 सज़ा का निर्धारण (Punishment Criteria):
यह सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध हो पाया या नहीं:
- अगर अपराध पूरा हो गया —
छिपाने वाले को मुख्य अपराध की अधिकतम सज़ा का 1/4 (एक-चौथाई) तक की जेल हो सकती है। - अगर अपराध नहीं हो पाया (रोक दिया गया या विफल रहा) —
तो छिपाने वाले को मुख्य अपराध की अधिकतम सज़ा का 1/8 (एक-आठवां हिस्सा) तक की जेल हो सकती है।
🔷 उदाहरण द्वारा स्पष्टता (Illustration for Clarity):
उदाहरण 1:
‘राम’ को पता है कि ‘श्याम’ चोरी की योजना बना रहा है।
राम पुलिस को झूठ बोलता है कि श्याम तो शहर में नहीं है।
श्याम चोरी कर लेता है।
अब राम को भी चोरी की अधिकतम सज़ा (मान लीजिए 7 साल) का 1/4 यानी 1.75 साल तक की जेल हो सकती है।
उदाहरण 2:
अगर श्याम चोरी नहीं कर पाता, तो राम को अधिकतम 7 साल का 1/8 यानी लगभग 10.5 महीने तक की सज़ा हो सकती है।
🔷 कानूनी उद्देश्य (Legislative Intent):
इस धारा का उद्देश्य है:
- अपराध में प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग दोनों को रोकना।
- नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व को मजबूत करना।
- कानून के प्रति नागरिकों में ईमानदारी और जवाबदेही उत्पन्न करना।
🔷 पूर्ववर्ती समतुल्य प्रावधान (Corresponding Provision in IPC):
भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) में इस प्रकार का प्रावधान धारा 118 और 119 में आता था, लेकिन BNS में इसे अधिक स्पष्ट, संगठित और व्यावहारिक रूप दिया गया है।
🔷 व्यवहारिक महत्त्व (Practical Importance):
- यह धारा पुलिस को सटीक जानकारी मिलने में सहायक बनती है।
- अपराधियों को सहायता देने वाले “छिपे साथियों” पर भी लगाम लगती है।
- यह एक निवारक प्रभाव (deterrent effect) पैदा करती है कि कोई अपराध का गुप्त समर्थन न करे।
🔷 सीमाएँ और शर्तें (Limitations and Conditions):
- यह धारा केवल उन्हीं अपराधों पर लागू होती है जिनमें केवल कारावास की सज़ा है — न कि जुर्माने या मृत्युदंड सहित अन्य दंडों वाले गंभीर अपराधों पर।
- अज्ञानता या अनजाने में चूक को अपराध नहीं माना जाएगा। सज़ा तब ही होगी जब यह स्पष्ट हो कि व्यक्ति ने जानबूझकर और उद्देश्यपूर्वक सूचना छिपाई।
🔷 निष्कर्ष (Conclusion):
भारतीय न्याय संहिता की धारा 60, आधुनिक न्याय व्यवस्था की उस सोच का परिचायक है जिसमें न केवल अपराध करने वाले को, बल्कि उसके साथ देने वाले गुप्त या परोक्ष सहयोगियों को भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह धारा कानूनी उत्तरदायित्व की परिधि को विस्तारित करती है और समाज में सहयोग और न्याय की भावना को बल देती है।
यदि हर नागरिक यह समझे कि अपराध की जानकारी छिपाना भी स्वयं में अपराध है, तो यह भारतीय समाज को अधिक न्यायप्रिय और उत्तरदायी दिशा में ले जाने का माध्यम बनेगा।